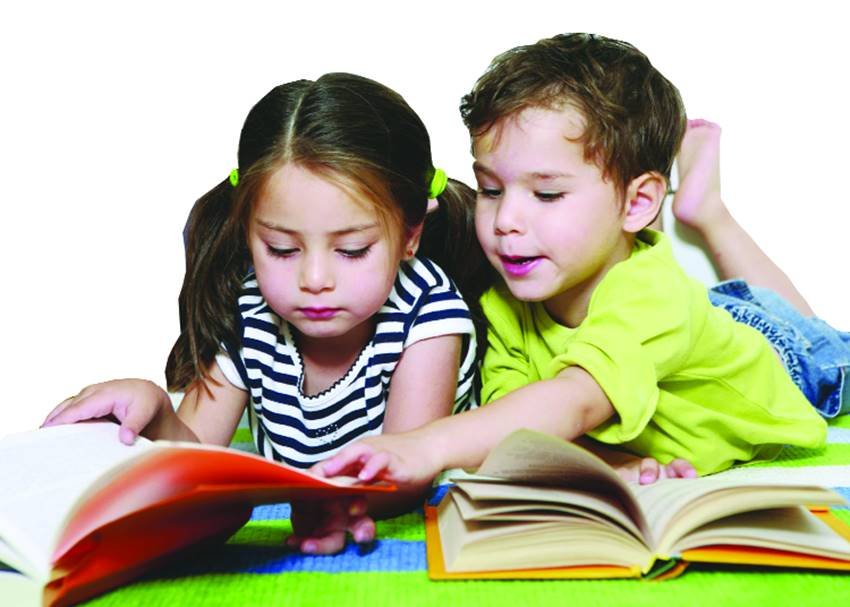दिविक रमेश
स्तक का कोई विकल्प नहीं है। पुस्तक के अभाव को इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, सीडी, मोबाइल की उपस्थिति से दूर करने के मामले में कोई हल नहीं निकलने वाला। ये सब एक-दूसरे के साथ-साथ हैं। चुनौती यह है कि सब के साथ रहते-रहते भी कैसे इनमें से हर एक के महत्त्व को बनाए रखा जाए और इनके सही और संतुलित उपयोग करने की स्थितियां बनाई जाएं। बात साफ है कि एक के अस्तित्व को मिटा कर दूसरे के अस्तित्व को बरकरार रखने वाली प्रवृत्ति से पिंड छुड़ा कर ही हम सही रास्ते की तलाश कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी भी अनेक प्रकार से मददगार है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। बहुत-सी पठन-सामग्री इसके प्रदत्त साधनों द्वारा अधिक आसानी से प्राप्त हो सकती है। ई-बुक्स भी आज की एक सच्चाई है।
पठन की चिंता का प्रश्न ‘पाठ्य-पुस्तकों’ के पठन से अलग, साहित्य आदि की पुस्तकों से जुड़ा है। पाठ्य-पुस्तकों को तो रो-पीट कर या खुशी-खुशी पढ़ना ही पड़ता है।
हम अपनी परम्परा में झाकें तो ‘प्रेम के ढाई आखर’ के पक्ष में यह भी मिलता है कि ‘पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय’। गहराई से सोचने पर इस कथन का आशय यह है कि साहित्य-सृजन जीवन के अनुभव के बिना संभव नहीं होता। वह कलात्मक अनुभव होता है। ऐसा साहित्य ही कृत्रिम न होकर सहज संवेदनाओं से संपन्न होने के कारण पाठकों को भी ग्राह्य होता है। यह बात बालसाहित्य के क्षेत्र में भी लागू होती है। बहुत से रचनाकार, रचनात्मकता को ताक पर रख कर, तथाकथित अच्छी बातों को लय-छंदों में बांधने को ही बालसाहित्य का लेखन मानते हैं। वे ‘बालक का साहित्य’ न लिख कर ‘बालक के लिए’ लिखते रह जाते हैं। यानी वे बाल-हृदय को न जानने की कोशिश करते हैं और न ही खुद अपने भीतर के बालक के प्रति सजग हो पाते हैं। ‘यह करो, वह मत करो’ की शैली में आज भी बच्चों को उपदेश देने को ही बालसाहित्य की इति समझते हैं। ऐसे साहित्य से बालक भागेगा नहीं तो क्या करेगा। आत्मालोचन किए बिना दोष बालक पर लगा दिया जाएगा कि उसमें पढ़ने की रुचि को लकवा मार गया है। समझना होगा कि बालक को न उपदेश चाहिए और न अंधविश्वासों के अंधेरों का घटाटोप। उसे कल्पना चाहिए, लेकिन ऐसी जो जमीन पर खड़ी प्रतीत हो। उसे वैज्ञानिक सोच से संपन्न (जो वैज्ञानिक उपकरणों या सिद्धांतों के कविता या कहानी आदि के चौखटों में फिट उपयोगी साहित्य से भिन्न होता है) रचनात्मक साहित्य चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा सद्साहित्य रचा नहीं जा रहा है। खूब रचा जा रहा है, लेकिन दूसरे ढंग का भी कम अंबार नहीं लगाया जा रहा और उसके पैरवीकार भी कम नहीं हैं।
हमें बच्चों से बतियाती हुई, उनका मनोरंजन करती हुई, उन्हें दोस्त मानती और बनाती हुई वैविध्यपूर्ण रचनाएं अधिक से अधिक और निरंतर देनी होंगी, अगर उनमें पठन की रुचि में सच में वृद्धि करना चाहते हैं। अगर हम सच में पठन की इस समस्या से जूझ कर सफल होना चाहते हैं तो हमें बहुत बचपन से ही बच्चे की ओर ध्यान देना होगा। आज अनेक पुस्तकें और सर्वे उपलब्ध हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि अलग-अलग आयु के बच्चों में पुस्तक-संस्कृति का प्रकाश कैसे उदित और विकसित किया जाए। मगर एक तथ्य सामान्य रूप में जान लेना चाहिए कि बड़ों (माता-पिता, शिक्षकों, अभिभावकों आदि) को बच्चों का, इस पठन के क्षेत्र में भी, रोल मॉडल बनना होगा। जब बड़े ही छुटपन से न बच्चे को समय और साथ देंगे, बल्कि अपनी जान छुड़ाने को उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे या उसकी आंखों को टीवी/ कंप्यूटर का परदा सौंप कर निश्चिंत हो लेंगे, तो पुस्तक-संस्कृति का क्या होगा, समझा जा सकता है। बच्चा हम बड़ों के हाथ में कितनी बार कितनी पुस्तकें देख पाता है, यह भी सोचा जाना चाहिए।
एक बड़ा सवाल बालक की पुस्तक तक पहुंच का भी है। एक समय था जब अच्छी पत्रिकाओं और पुस्तकों के लिए छोटा-बड़ा स्थान घरों में होता ही नहीं, बल्कि सजा होता था। आज पुस्तकें प्राथमिकता की दृष्टि से किस पायदान पर हैं, कम से कम हिंदी क्षेत्रों में, तो असलियत जान कर सिर पीट कर रह जाएंगे। पुस्तकालयों के अभाव के बारे में भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। पूरे देश में चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। पुस्तकें उपहार में देना जब बड़ों को ही नाक-भौं सिकोड़ने का सुअवसर प्रदान कर दिया करता है, तो ऐसे महाजनों के अनुकरण करने पर बच्चों को लताड़ क्यों!
अच्छी बात है कि आज निजी और सामूहिक स्तर पर पढ़ने की आदत में वृद्धि के कुछ प्रयास हो रहे हैं। यहीं पुस्तकों की अनाप-शनाप कीमतों पर भी सोचा जाना चाहिए। कितने ही माता-पिता या अभिभावक कीमतें देख कर ही हतोत्साहित हो जाते हैं। माना कि सुंदर और आकर्षक पुस्तकें प्रकाशित करना आज की लगभग अनिवार्यता है, क्योंकि इसके अभाव में वह पुस्तक की ओर आएगा ही नहीं। यह भी सच है कि ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च बहुत आता है, इसलिए कीमतें उसी के अनुसार ऊंची रखनी पड़ती हैं। इसका समाधान सरकार और प्रकाशक दोनों स्तर पर खोजे जाने की आवश्यकता है।
कई बड़े यह भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ बहुत धैर्य से काम लेना होता है। तानाशाही से मनवाया गया काम आत्मसंतुष्टि या सही मायनों में अहंकार-तुष्टि दे सकता है, लेकिन बच्चे के किसी काम का नहीं होता है। बच्चे में पठन की रुचि की वृद्धि के लिए हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि ‘पढ़ना’ उसे ‘सजा’ देना न लगे। बच्चे के प्रति, उसकी आयु के तकाजे और उसकी उम्र की तैयारी को देखते हुए, सदा उसकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का आत्मीय भाव से समाधान करने वाला रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी उपेक्षा को शुरू से ही खूब समझता है। वह बिना बात अपना मखौल उड़ाया जाना भी पसंद नहीं करता। बच्चा भी चाहता है कि उससे उसके बड़े उसे सम्मान देते हुए बतियाएं।
इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चे को अनुशासन से अलग रखा जाना चाहिए। अनुशासन उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसे बच्चे तक पहुंचाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे कि वह सब उसका कोई अपना उस तक पहुंचा रहा है, कोई बाहरी या अपरिचित आदमी नहीं। अपने प्रति उसमें विश्वास की भावना जगाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। हां, बच्चे को पढ़ने, खेलने आदि का समय निर्धारित करने में बड़ों को पूरी मदद करनी चाहिए। उसके लिए धौंस या एहसान के भाव से काम नहीं लिया जाना चाहिए। पढ़ने को खेलने के विकल्प का रूप समझने की भूल से बचना होगा। कई बड़ों को अपने बच्चों से कहते सुना जाता है कि अगर नहीं पढ़ोगे, तो खेलने भी नहीं दिया जाएगा। यह बालक-विरोधी व्यवहार है। पढ़ना और खेलना दो अलग-अलग बातें हैं और दोनों जरूरी हैं। इसलिए दोनों को किया जाना चाहिए, यह समझ विकसित करनी होगी। इसलिए कहा यह जाना चाहिए कि तुम्हें खेलने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ना भी चाहिए। संक्षेप में इतना ही कि पुस्तक एक प्रेम है, खौफ नहीं, इस भावना को साहित्यकारों और बड़ों को खुद समझते हुए बच्चों में संस्कार के रूप में निरंतर भरते रहना होगा। ०