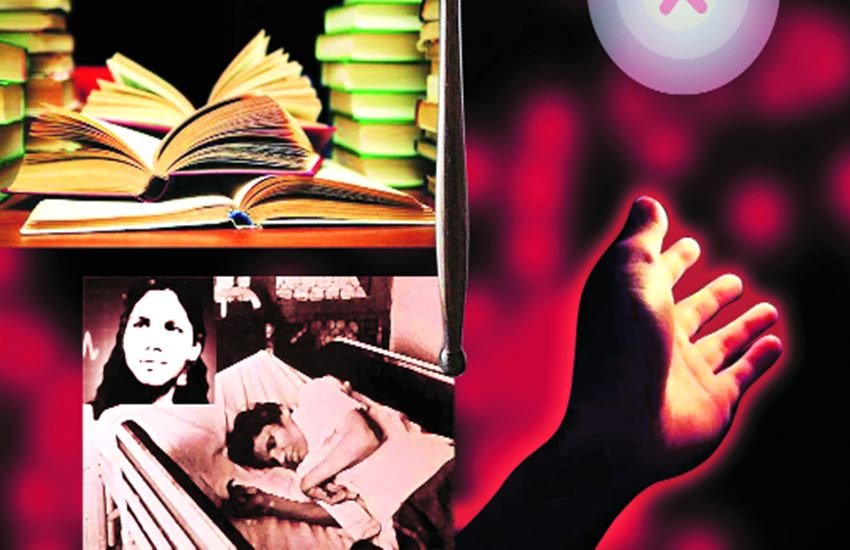बरमती आश्रम में लाइलाज बीमारी से जूझते बछड़े के जीवन-मृत्यु का सवाल उठा और यह साबित हो गया कि उसे जिलाए रखना संभव नहीं है तो गांधीजी ने कहा कि उस जीव की मृत्यु का प्रबंध करना असल में उसे तमाम कष्टों से निजात दिलाना होगा। हकीकत में ऐसा किया भी गया और जब इसके लिए गांधीजी की आलोचना हुई तो उन्होंने अक्टूबर, 1928 के नवजीवन (गुजराती) में लिखा। ‘मेरी मौजूदगी में डॉक्टरों ने बछड़े को जहरीला इंजेक्शन दिया और सारी प्रक्रिया दो मिनट से कम में समाप्त हो गई। प्रश्न है कि क्या मैं लाइलाज बीमारी से जूझते किसी इंसान के प्रसंग में ऐसी ही प्रक्रिया (इच्छा-मृत्यु) के पक्ष में होऊंगा। और क्या मैं खुद पर ऐसा ही नियम लागू करना पसंद करूंगा। मेरा जवाब है- हां। ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर आॅपरेशन करते वक्त जब किसी मरीज के शरीर पर तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करता है और वह हिंसा नहीं कहलाता, वैसे ही यदि किसी के लिए जीवन, मृत्यु से अधिक कष्टदायक हो तो उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाना हिंसा नहीं है।’
गांधीजी के इन विचारों के नवजीवन में प्रकाशन के करीब नब्बे साल बाद कष्टों से निजात दिलाने वाली मृत्यु की नैतिकता का प्रश्न एक बार फिर हमारे देश में चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने इच्छामृत्यु (पैसिव यानी निष्क्रिय) कानून का एक मसविदा तैयार कर उसे स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला है और इस बारे में आम जनता व विशेषज्ञों की राय जानने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पर लोग आज तक तक लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। इस प्रस्तावित कानून में लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को यह हक देने की बात है कि वे अपनी बीमारी की चिकित्सा बंद करने के लिए डॉक्टर से कह सकें और स्वाभाविक मृत्यु पा सकें। उल्लेखनीय है कि अभी तक खुद सरकार ऐसा अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है।
गौरतलब है कि दो साल पहले भी यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में उठ चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के संदर्भ में सवाल उठाया गया था कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसी वसीयत करने की इजाजत दी जा सकती है कि बीमारी के कारण मृतप्राय जैसी स्थिति में पहुंचने पर उसका इलाज बंद कर दिया जाए और जीवनरक्षक प्रणालियां और उपकरण हटाकर उसे मरने दिया जाए। अदालत के सामने अहम सवाल यह था कि क्या मृतप्राय स्थिति में पहुंच गए व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। इस सवाल को इसलिए जटिल माना गया क्योंकि हमारा संविधान जीवन का पक्षधर है और किसी भी रूप में मृत्यु की वकालत नहीं करता।
जीते जी मौत की वसीयत के मामले से जिंदा हुए इच्छामृत्यु और दयामृत्यु के प्रश्न पर सर्वोच्च अदालत ने सिर आई बला को टालने की नीयत से इस मामले में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर उनकी राय मांग ली। नोटिस में कहा गया कि इस मामले में समाज, नैतिकता, धर्म और चिकित्सा विज्ञान शामिल है और यह मानवता से जुड़ा मसला है, इसलिए सभी राज्यों की राय जानना भी जरूरी है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया था और सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने साफ किया था कि एक तो हमारे देश में इच्छा या दयामृत्यु को कोई कानूनी दर्जा हासिल नहीं है और इसे खुदकुशी माना जाता है। दूसरे, यदि इसका अधिकार दिया गया तो इसके दुरुपयोग की आशंका अधिक है।
निस्संदेह किसी कानून के दुरुपयोग की आशंका उससे संबंधित मामले की सुनवाई या कानून बदलने में बाधा नहीं हो सकता, लेकिन यह देखते हुए दुनिया में करीब एक दर्जन देशों में इसकी इजाजत देने संबंधी कानून बन चुके हैं। यह जरूरी हो गया है कि भारत में भी इस जरूरत की एक स्पष्ट कानूनी व्याख्या दी जाए और इसके पक्ष या विपक्ष में मामला अब चर्चा से आगे बढ़े। यही वजह है कि अब सरकार इसे लेकर किसी एक अंतिम राय तक पहुंचना चाहती है ताकि इससे संबंधित कानून को अमली जामा पहनाया जा सके। हालांकि इच्छामृत्यु की आवश्यकता से जुड़े दो ही पहलू ऐसे हैं, जिन्हें लेकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में दुविधा बनी हुई है। इस बारे में पहला सवाल यह है कि क्या दयामृत्यु या इच्छामृत्यु (निष्क्रिय-पैसिव) स्वैच्छिक रूप से की गई आत्महत्या है, और दूसरी दुविधा यह है कि कहीं यह अनैच्छिक रूप से दूसरों के हाथों की गई हत्या तो नहीं है।
फिलहाल हमारी सरकार की राय दूसरी दुविधा के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई है। कानून के नजरिए में अभी हमारे यहां जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक दया या इच्छामृत्यु के मामले में या तो मरीज खुद अपने जीवन के बारे में कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं होता है, लिहाजा स्वार्थवश उसके रिश्तेदार उसके लिए इच्छामृत्यु की मांग उठाते हैं। अगर इसमें कोई स्वार्थ न भी हो तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के पक्ष में है और उसमें मृत्यु के अधिकार जैसी कोई बात नहीं है, लिहाजा ऐसी मृत्यु गैरकानूनी है। दो राय नहीं कि मृत्यु की मांग खुद में एक जटिल प्रश्न है।
इसे यह कहकर खारिज किया जा सकता है जो चीज मनुष्य दे नहीं सकता, उसे छीनने का अधिकार सिवाय प्रकृति के किसी को नहीं है। भारत जैसे देश के संबंध में यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। इच्छामृत्यु (यूथनेसिया) की इजाजत मिलने पर उसके दुरुपयोग की आशंका के अलावा एक खतरा यह भी है कि तब आत्महत्या के इच्छुक लोग यूथनेसिया की आड़ में अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। यों तो चिकित्सा विज्ञन नीम बेहोशी में पड़े व्यक्तियों के जीवन में कभी भी लौट आने की संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन इन सभी तर्कों के बावजूद इसका एक पक्ष यह है कि वे लोग, जिनके लिए मृत्यु का अर्थ मरना नहीं कष्टकर और असाध्य स्थितियों से छुटकारा पाना है, मौत को एक समाधान की तरह देखते हैं। कुछ बरस पहले तक देश में गर्भपात को गलत माना जाता था। लेकिन जब गर्भ के कारण किसी मां का जीवन ही संकट में पड़ जाए तो इसे उचित ठहराया जाने लगा।
इच्छामृत्य के प्रसंग में अरुणा रामचंद्र शानबाग के बेहद चर्चित मामले का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिनकी ओर से छह साल पहले 2009 में सुप्रीम कोर्ट को यह दरख्वास्त दी गई थी कि वह (कोर्ट) उनके जीवन का अंत करने की इजाजत दे। करीब चार दशक पहले अरुणा के साथ मुंबई के उस अस्पताल में क्रूरतापूर्ण ढंग से बलात्कार किया गया था जहां वह नर्स थी।
इस हादसे के कारण अरुणा को लकवा मार गया और वह अपनी आवाज खो बैठी थी। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु होने तक चार दशकों के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने फोर्स फीडिंग के सहारे अरुणा को जिलाए रखा, जबकि उनकी हालत में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में आरंभ में शानबाग मामले की सुनवाई के वक्त तत्कालीन मुख्य न्यायाधीन केजी बालाकृष्णन और जस्टिस एके गांगुली की खंडपीठ ने सवाल उठाया था कि क्या यह याचिका इच्छामृत्यु की मांग जैसी नहीं है?
इस पर शानबाग के वकील ने दलील दी थी कि फोर्स फीडिंग के सहारे शानबाग को जिलाए रखने की कोशिश असल में सम्मान के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हासिल है। शानबाग के मामले से साफ हो गया था कि यह असल में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इच्छामृत्यु पाने के अधिकार का मसला है। किसी बीमारी के ठीक नहीं होने और उसके कारण भयानक पीड़ा होने की दशा में कुछ देशों में लोगों को इसका अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि स्विटजरलैंड में। वहां आत्महत्या तो जुर्म ही है, पर लाइलाज बीमारी वाली दशाओं में डॉक्टर की मदद से हासिल की गई मृत्यु की इजाजत 1942 से ही लोगों को दी गई है।
इस काम को वहां अपराध नहीं माना जाता और इसके लिए डॉक्टरों को सजा नहीं होती। शेष दुनिया में भी सहज मृत्यु की जरूरत के बारे में एक समझ इधर के वर्षों में कायम हुई है। कई देशों में कड़ी निगरानी के तहत इसकी छूट दी गई है। जैसे नीदरलैंड में डॉक्टरों की मदद से दी गई इस तरह की मृत्यु को वैध माना गया है। अमेरिका में इस मुद्दे पर हुए मतदान के आधार पर वहां के पंद्रह राज्यों में ‘असिस्टेड सुसाइड’ के रूप में वैधता देने की कोशिश की गई। हालांकि ओरेगांव के सिवा कहीं और फिलहाल यह वैध नहीं है। ओरेगांव में सम्मानजनक मृत्यु से संबंधित अधिनियम 1997 से ही लागू है। इसी तरह अल्बानिया और लग्जमबर्ग में भी यूथनेसिया को कानूनन सही माना गया है। आॅस्ट्रेलिया के एक प्रांत (नार्दर्न टेरीटरी) में 1995-1997 के बीच इसकी इजाजत थी।
हमारे समाज में परंपरा के रूप में स्वेच्छा मृत्यु का एक स्वरूप भी पहले से मौजूद है। जैसे हिंदू धर्म में समाधि लेने और जैन धर्म में संथारा लेने की परंपरा। इन परंपराओं के तहत स्वस्थ व्यक्ति तक स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकता है। ‘मनुस्मृति’ में ऐसी मृत्यु का विकल्प सुझाते हुए लिखा गया है कि जब एक गृहस्वामी अपने शरीर को झुर्रियों से भरा पाए, जब वह अपने बच्चों को देख ले, उसे उठकर उत्तर-पूर्व की दिशा की ओर सीधे चल पड़ना चाहिए और पानी और हवा के सेवन के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते हुए अपने शरीर को नष्ट होने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा बुढ़ापे में उठाए जाने वाले विकल्प का उदाहरण है पर असाध्य बीमारी में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका एक उदाहरण 1982 में आचार्य विनोबा भावे ने पेश किया था। वे जब काफी बीमार हो गए तो उन्होंने देहत्याग का फैसला कर लिया और अपने अंतिम दिनों में भोजन और दवा लेने से इनकार कर दिया। इस तरह भूखे रह कर 15 नवंबर, 1982 में उनकी मृत्यु हो गई। ये सभी स्वैच्छिक या पुराणों में लिखित उदाहरण हैं, पर जहां तक स्वेच्छा मृत्यु को कानूनी जामा पहनाने का सवाल है, तो बहुस्तरीय भारतीय समाज में ऐसा कर पाना आसान नहीं है।
इसका सबसे जटिलतम पहलू यही है कि कानूनन ऐसी छूट देने पर इसका गलत फायदा न उठाया जाने लगे। असल में, कई डॉक्टर भी मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वर्षों से बिना कोई हरकत किए बिस्तर पर पड़ा है तो उसे मौत की नींद सुलाने का इंतजाम ही किया जाए। कुछ वर्ष पहले जर्मनी में एक वाकया सामने आया था, जब 26 साल से निस्पंद बिस्तर पर पड़े एक मरीज ने एक कम्युनिकेटर के जरिए यह संदेश दिया था कि ढाई दशक के इस अरसे में उससे जो कुछ कहा गया, जो कुछ उसके आसपास घटित हुआ, उसे उन सबका अहसास है।
मशहूर फॉमूर्ला-वन रेसर शूमाकर भी जब स्पेन में स्कीइंग करते वक्त घायल होकर नीमबेहोशी में चले गए थे, तो उनकी जीवन में वापसी की नगण्य संभावना थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और दवाओं की बदौलत शूमाकर होश में आ गए।
केंद्र सरकार ने जिस तरह से इस मामले पर सभी पक्षों की राय जानने की प्रक्रिया शुरू की है, उसके आधार पर उसे इस मुद्दे से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं के प्रति सतर्क बताया जा सकता है। अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले (ज्ञान कौर) में व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 21 लोगों के जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी सुनिश्चित करता है और इस अनुच्छेद में जीवन को खत्म करने का अधिकार देने की बात नहीं कही गई है। अदालत के अनुसार जीने का अधिकार एक स्वाभाविक अधिकार है, जबकि स्वेच्छा मृत्यु या आत्महत्या करना अस्वाभाविक तौर पर जीवन का अंत करना है, जिसे इस अनुच्छेद की व्याख्या में नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति आर्थिक विवशता, शारीरिक अपंगता और इस कारण पैदा हुए मानसिक दबाव में अपनी जिंदगी खत्म करने को बाध्य होता है तो इसे सम्मानजनक मृत्यु नहीं कह सकते। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले तेजाबी हमले से बुरी तरह झुलसी झारखंड की एक महिला सोनाली ने इच्छामृत्यु की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया था।
मुमकिन है कि इस विषय पर समाज और कानून की राय अलग-अलग ही रहे, पर दोनों को ही इस पर अवश्य विचार करना होगा कि अगर किसी वजह से एक मनुष्य की जीने की ललक और ऊर्जा खत्म हो जाती है और मृत्यु उसे जीवन से बड़ी और मुक्त करने वाली प्रतीत होती हैए तो ऐसे व्यक्ति को दया मृत्यु की दी जाने वाली छूट न तो अनैतिक और न ही धर्म विरुद्ध कहलाएगी। ऐसे व्यक्ति को इच्छामृत्यु की छूट देना अनैतिक नहीं हो सकता जिसके जीने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हों और उसे सिर्फ इसलिए जिलाए रखा गया हो क्योंकि अभी हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब कोई व्यक्ति दिमागी रूप से सक्रिय है लेकिन उन लाइलाज बीमारियों के कारण भयंकर पीड़ा झेल रहा है जिनमें रिकवरी की कोई संभावना नहीं है तो अवश्य ऐसी मांग पर विचार किया जाना चाहिए। यहां डॉक्टर तय करें कि क्या उस व्यक्ति के बचने और जीवन में लौटने की कोई संभावना शेष है या नहीं। अगर ऐसी कोई संभावना नहीं है तो ऐसे में मृत्यु कई समस्याओं से छुटकारे के रूप में सामने आती है। जाहिर तौर पर इसके लिए भी कायदे-कानून और दिशानिर्देश तय किए जाने चाहिए। यह काम अदालत पर नहीं छोड़ा जाए। इसे तय करे हमारे देश की सरकार यानी संसद जो इसके लिए एक स्पष्ट कानून बनाए।