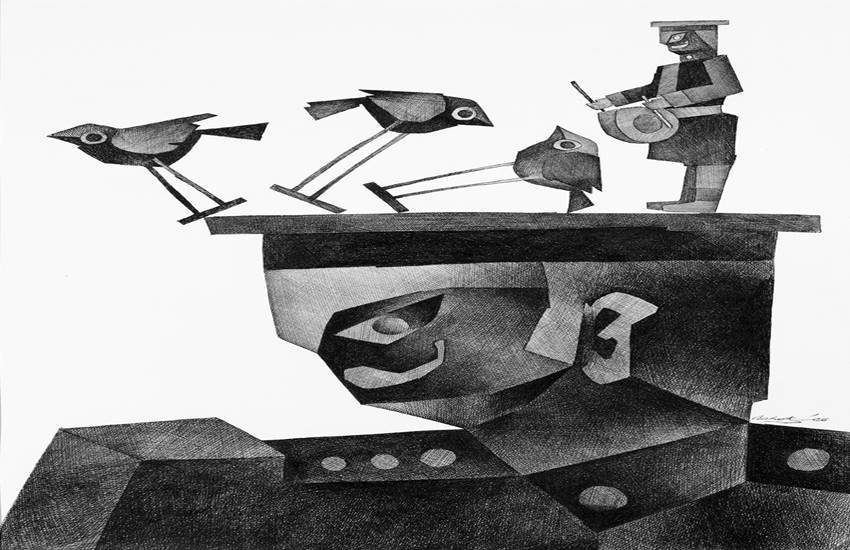सत्यदेव त्रिपाठी
यह रोजी-रोटी प्रधान युग है। इसी का प्रताप है कि थिएटर-कला के प्रेमी आज रोजगार की दृष्टि से बात कर ले रहे हैं, वरना कहा जाता रहा है कि थिएटर रोजगार की चीज नहीं, शौकिया करने की चीज है। उससे जीवन-यापन नहीं हो सकता, उसे पेशे के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। मगर मराठी में लोगों ने यह परंपरा बनाई है- बनाए रखी है। वे आज भी दर्शक के पास अपना नाटक लेकर जाते हैं, दर्शकों में लगाव और ललक जगाते हैं। थिएटर की भाषा में इसे भ्रमणशील नाटक (टूरिंग थिएटर) कहते हैं, जिसकी मराठी में सैकड़ों सालों से चली आती परम्परा है कि ये लोग गांवों-गिरावों तक जाकर नाटक करते हैं। आज भी कर रहे हैं। ऐसी ही परंपरा हिंदी में भी थी। पारसी थिएटर कंपनियों के साथ और आजादी के बाद भी कानपुर की नौटंकियों और ‘दरभंगा थिएटर’ आदि में। पर वह लुप्त हो गई। उसी तरह बंद हुए बाजार-दर-बाजार शामियाना लगा कर होते थिएटर, जिनके प्रचार दिन भर होते रिक्शे पर माइक लेकर और देखने उमड़ते चारों तरफ के गांव वाले। लेते चवन्नी-अठन्नी के टिकट। यही था थिएटर का रोजगार और सही था। तब जरूरतें कम थीं, इरादे नाट्यमय थे। तब लखपती बनने, एसी कार में चलने, विशाल बंगलों में रहने की चाहत भी न थी। आज ऐसा होता, तो न रोजगार की चर्चा होती, न चिंता। आज की पीढ़ी और भावी पीढ़ियां खोलें थिएटर का यह सदर दरवाजा, तो रोजगार की सही और अच्छी संभावना तो बनेगी ही, पुनर्जीवित होगी थिएटर की वह लुप्तप्राय परंपरा भी। सबसे बड़ी बात कि थिएटर आम दर्शक तक पहुंचेगा, जो कला का असली श्रेय-प्रेय होता है।
पहले की पीढ़ी में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर जैसे लोग रहे, जो प्रेरक बने थे। आज तो आ गई हैं वेब शृंखलाएं, जो और दुधारू साबित हो रही हैं। अच्छा कमा रहे हैं थिएटर के बच्चे और इसके लिए मुंबई जाने की जरूरत भी नहीं। ये सब थिएटर के ही गौण उत्पाद हैं। सो, थिएटर के ही रोजगार हुए। शायद तब 1970 के दशक में इतने मालूमात नहीं थे, इतना खुला आसमान नहीं था। वैसे तब भी प्रायोगिक सिनेमा के आंदोलन, उसके बाद टीवी पर तमाम चैनलों के खुलने और एटनबरो की फिल्म ‘गांधी’ के साथ थिएटर के लोगों की पर्दे के माध्यम पर जोरदार उपस्थिति ने सीढ़ी तो क्या, एक उपयोगी कार्यशाला का काम किया और तब से ही यह थिएटर जगत फिल्म उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में बड़ा रोजगार बन गया। अब यह बढ़ता जा रहा है। इसी सह-संबंध के चलते एक नया चलन शुरू होता दिख रहा है कि जब फिल्म में ही जाना है, तो थिएटर के साथ फिल्म से भी परिचित क्यों न किया-कराया जाए! लिहाजा, थिएटर वाले भी नाटक की कार्यशाला के साथ फिल्म-आस्वाद के कार्यक्रम भी कार्यशाला की ही तरह करने लगे हैं। नाट्य कार्यशाला थिएटर की भी हो, तो आते हैं फिल्म वाले ही, जो थिएटर को दगा देकर पर्दे पर चले गए हैं। इसी तरह रंगमंडल आज नाट्योत्सवों के बदले फिल्मोत्सव कर रहे हैं- बहुधंधी युग की बहुउद्देशीय वृत्ति को सार्थक कर रहे हैं। इन्हीं समारोही आयोजनों-कार्यक्रमों में छिपा है आज के थिएटर का असली रोजगार। नाट्य-पेशे की और पेशेवर (रोजगारी) होते नाट्य की मुख्यधारा आज यही है।
इसकी शुरूआत आजाद भारत के संविधान और व्यवस्था बनने के साथ हुई। लेकिन तब उसमें समारोही आयोजन इस तरह शामिल न थे। तब संस्कृति मंत्रालय के तहत नृत्य-संगीत-नाट्य और लोककलाएं आदि सभी को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनीं और यह सब सीखने-सिखाने, करने-कराने के लिए अनुदान निर्धारित हुए। सभी प्रदेशों की राजधानियों में इन सबकी अकादमियां बनीं, जिनमें निर्देशक, अध्यक्ष, सचिव, सलाहकार, समितियों के सदस्य आदि तमाम पद निकले। इन सबके लिए बड़े-बड़े कलाकारों को राजधानी बुलाया गया और आजीविका का मामला वहीं से तभी से चल निकला। इसमें नाटक करने वालों के लिए विविध किस्म के अनुदान तय हुए। नाट्यमंडल बनाने-चलाने के लिए अनुदान, उसमें कलाकारों के लिए वेतन-अनुदान, निर्मितियों के लिए निर्माण अनुदान आदि जैसे तमाम प्रावधान बने। इस तरह की सहायताओं से चल रहे या बिना सहायताओं के भी चलने वाले रंगमंडल अपने सालाना नाट्योत्सव मनाते थे। अपने ही चुने हुए नाटकों के एकाधिक प्रदर्शनों को समारोही माहौल में करते थे- उत्सव मनाते थे। मगर इसमें रोजगारपरकता या व्यावसायिकता कैसे आई!विभिन्न कलाओं के विकास की शृंखला में अकादमियों के समांतर ही नाटक के लिए खासतौर पर राष्ट्रीय नट्य विद्यालय का खुलना रंगक्षेत्र में युगांतकारी परिघटना सिद्ध हुआ है। इसमें नि:शुल्क ही नहीं, जेबखर्ची वेतन (स्टाइपेंड) के साथ तीन सालों का प्रशिक्षण शुरू हुआ और उसके बाद विद्यालय का रंगमंडल भी बना। विद्यालय से निकले स्नातकों में से ही कुछ चयनित लोग इस रंगमंडल में वेतनभोगी रंगकर्मी के रूप में लिए जाने लगे। इस तरह कलाकार की आजीविका के अवसर बढ़े और कलाकर्म के प्रति समर्पण भाव से काम करने के लिए जरूरी निश्चिंतता भी बढ़ी- उन्मुक्त होकर नाटक करने के दिन आए। इसके अलावा नाट्य-विद्यालय के ढेरों स्नातक धीरे-धीरे रानावि के ढेरों विस्तारित पाठ्यक्रमों के रूप में पूरे देश में थिएटर को बढ़ावा देने के लिए बनी योजनाओं से भी कलाकर्म के साथ अपना जीवन-यापन करने लगे। मगर अचानक रानावि में राष्ट्रीय स्तर का नाट्योत्सव शुरू हो गया- ‘भारंगम’। पूरे देश से प्रविष्टियां मंगा कर समिति द्वारा चयन होने लगा। ठाठ से रहने, आरामदेह आवागमन के साथ फीस भी काफी अच्छी। एकाध साल तो नाटक चले नाटक की तरह, फिर ‘नाटक’ होने शुरू हुए- घमासान मच उठी। भारंगम से नाटक नहीं, नाटक के चयनित होने और उसकी सुविधाओं-प्राप्तियों पर तानें टूटने लगीं। समीकरण बनने लगे। फिर सारे रंग मंडलों को नाट्योत्सव के लिए अनुदान मिलने लगे, जिसमें भारी बंदरबांट होने लगी। इस तरह नाट्योत्सव-फिल्मोत्सव, नाट्य-कार्यशालाएं और फिल्म-आस्वाद के कार्यक्रम आदि समान लोभ-मोहों के ही रूप हैं।
आजकल ऐसे सारे आयोजन मिल कर थिएटर(वालों) की आय के अच्छे-खासे बड़े स्रोत बन गए हैं। कई थिएटर समूह वाले आज इसी के भरोसे पल-बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों के अफसरान भी इस दीवानगी से परे नहीं हैं। उनके आने से समूह और कार्यक्रम का रुतबा भी बढ़ता है। वे मुख्य या विशिष्ट अतिथि आदि के रूप में पधारते हैं। सरकारी फंड से कुछ अनुदान-विज्ञापन आदि दे-दिला देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इस प्रभाव के चलते थिएटर के लिए बड़े क्षेत्रफल की जमीनें वगैरह भी मिल जाने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर थिएटर एक उद्योग-प्रतिष्ठान का जरिया बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलकाजी साहब और बव कारंत के जमाने में रानावि और भारत भवन ने जो काम किए, वे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। पर आज इन अनुदानों के खेल में काम की गुणवत्ता घटती जा रही है। अनुदान पाने वालों की फेहरिस्त, उन्हें अनुदान मिलने की बारंबारता, आने वाले अतिथियों की सूची आदि देखने से असलियत का पता लग जाएगा कि कुछ है, जो नाटकेतर है। प्रस्तुतियां देखने पर तो यकीन हो जाता है। इस प्रक्रिया से थिएटर जितना पेशा-पैसा कमा रहा है, उतना पेशेवर नहीं हो रहा है। पेशेवर होने का मूल मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं, अनुशासित और अच्छा काम होता है- यानी पेशेवर होने का सही मतलब काम से ही है, बेच कर पैसा कमाने से नहीं। और कहना होगा कि यह भी हर क्षेत्र में हो रहा है। शोधछात्र किताबों में उतना सर नहीं खपाता, जितना अपने शोध निर्देशक की भक्ति में। प्राध्यापक उतनी पढ़ाई नहीं करता, जितना प्रोजेक्ट और पदोन्नति पाने के जुगाड़।
याद आते हैं फिर हबीब साहब जैसे लोग, जिन्होंने अनुदान से काम किए जरूर, पर वे लोग रंगकर्म के शैदाई रहे। थिएटर की प्रकृति भी ऐशो-आराम की नहीं। यह उसका मकसद नहीं, फितरत नहीं। लेकिन जिन ईहाओं के लिए ये लोग थिएटर के गलियारे की सीढ़ियों पर चले और चल रहे हैं, वे सीढ़ियां अगर इन महलों के सिंह-द्वार खोल रही हैं, तो ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, थिएटर छोड देंगे। इस तरह थिएटर के लिए खोले जा रहे और अब खुल चुके रोजगार के ये रास्ते थिएटर को ही बेरोजगार कर देने के लक्षण दिखा रहे हैं। पेशेवर न होकर ये पेशा (धंधा) बनते जा रहे हैं। अनुदानों के ऐसे वरदानों के जलजलों के लिए ही पुराणों में भस्मासुरी वरदान की मिसालें गढ़ी गई हैं। ये वरदान भी उसी रास्ते की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।