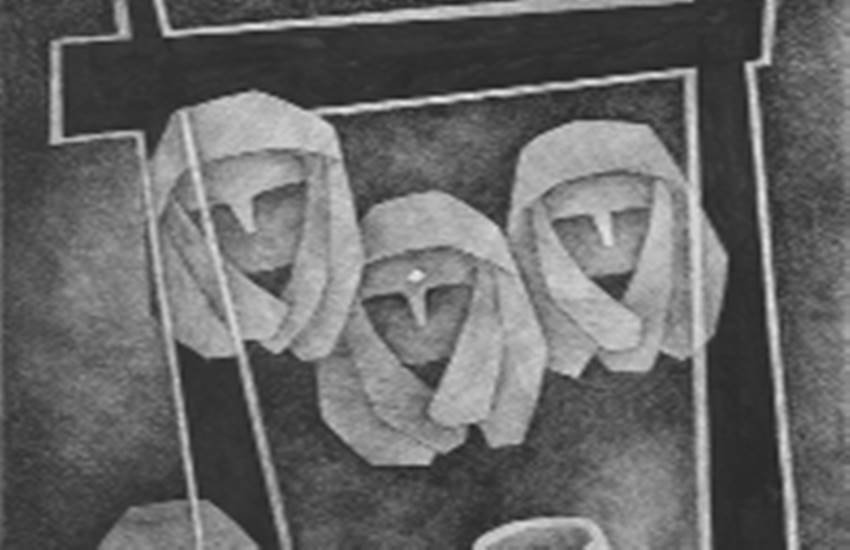हमारे देश में स्त्री को बौद्धिकता के साथ जोड़ कर देखने की कोई परंपरा नहीं रही। इसलिए जन-मानस का कोई अभ्यास भी बौद्धिक स्त्री की स्वीकार्यता को लेकर सहज भाव से तैयार नहीं हो सका। यहां नवजागरण के समय उठाए गए तमाम स्त्री नाम याद आ सकते हैं और यह तर्क भी किया जा सकता है कि ‘फलां फलां तो थीं ही।’ लेकिन क्या वस्तुस्थिति ऐसी थी? सुदूर अतीत में विदुषी घोषा को अश्विनी कुमारों को संबोधित करके पहला वाक्य यही कहना पड़ा था कि ‘हे अश्विनी कुमारो, मैं ज्ञान बुद्धिहीना नारी हूं।’ यानी अपनी बौद्धिक क्षमता को स्वत: कमतर मान लेने पर ही आपको बौद्धिकों के समाज में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। अगर स्त्रियां ऐसा नहीं करतीं, तो लगातार बौद्धिक कहा जाने वाला समाज उन्हें तरह-तरह से बताता है कि वे बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश न करें और अगर प्रवेश करती हैं तो वहां भी पितृसत्ता द्वारा निर्धारित दायरे के भीतर ही रहें।
दो बहुत प्रत्यक्ष स्थितियां समाज ने बौद्धिक स्त्री के लिए बनाई हैं। एक तो जब वह बौद्धिक क्षेत्र में समानता का दावा करती है और कई बार अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाती है, तब उसे छल-बल से रोकने की हजार कोशिशें होती हैं। उसकी राह में सामंती मानसिकता के कांटे बिछाए जाते हैं, उसे अपमानित और बहुधा दंडित किया जाता है। बुद्धि का प्रयोग करने और ज्ञानपिपासा की अभिव्यक्ति पर दंडित किए जाने की लंबी परंपरा मौजूद रही है। यह मानसिकता आज भी हमारे समाज में बहुत गहरे जड़ जमाए बैठी है और लगातार स्त्री को अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए अपमानित, उपेक्षित, प्रताड़ित और दंडित करती रहती है। यह अकादमिक जगत से लेकर लगभग सभी बौद्धिक क्षेत्रों में होता रहा है।
दूसरा तरीका बेहद परंपरागत है, जहां भारतीय मानस में स्त्री की दैवीय छवियां बहुत मान्य और पूजनीय रही हैं और तब एक बौद्धिक स्त्री, विद्वान की श्रेणी में न आकर पूजनीया की श्रेणी में डाल दी जाती है। वह हाड़-मांस की मानवी होने की सहजता और जन जीवन में घुल-मिल जाने की स्वाभाविकता से परे एक खास दुनिया की प्राणी मान ली जाती है, जो लगभग पराभौतिक छवि है। यह छवि कोई दिक्कत नहीं पैदा करती, कोई चुनौती नहीं रखती, उसका काम उसके दैवीय रूप से ढंक दिया जाता है, इसलिए उसका नाम लेना आसान हो जाता है।
अनुकूलन की ऐसी व्यवस्था एक तरफ स्त्री को उसके इतिहास से काट देती है, उसके रोल मॉडल से दूर कर देती है और दूसरी तरफ ज्ञान संधान के सब रास्ते बंद कर देती है। ज्ञान के लिए व्याकुलता और जिज्ञासा स्त्री के लिए कुछ ऐसी बना दी जाती है, जैसे वह उसकी विद्वता को कम कर देगी, रूप और लावण्य बिला जाएगा! सत्संग और बहसें उसके चरित्र को दूषित कर देंगी! तर्क करती, बहस करती स्त्री हमारे समाज को कभी स्वीकार नहीं रही। नवजागरण के समय भी, नई शिक्षा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों की आवश्यकता पुरुषों के लिए मानी गई थी, स्त्रियों के लिए बड़ी हिम्मत करके स्त्री-धर्म शिक्षा की ही बात की जा रही थी। लंबे समय तक गृहविज्ञान लड़कियों के लिए अनिवार्य विषय हुआ करता था। प्रगति और संघर्ष के इतने वर्षों बाद, आज भी कहीं-कहीं यह बना हुआ है।
इसी के बरक्स लेखन की बौद्धिक गतिविधियों के बीच स्त्री हस्तक्षेप को भी देख सकते हैं। यहां भी एक पूरा दौर स्त्री-विमर्श को स्त्री की यौन आजादी तक सीमित कर देने का रहा। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बुद्धि-विवेक इससे दूर कर दिए गए। समाज में हो रहे स्त्री आंदोलनों को नजरअंदाज किया गया। स्त्री के सामाजिक सरोकार परे ढकेल दिए गए। ऐसी यौन आजादी की बात की गई, जो कोई भविष्योन्मुखी रास्ता नहीं बनाती। यह पूरा पितृसत्तात्मक स्थितियों के अनुकूल और बाजार की आवश्यकतानुसार तैयार किया गया लगता है, जिसने नकली स्त्री-विमर्शकार और सतही स्त्री-विमर्श के लेखक तैयार किए।
इसका विरोध करती एक कोशिश उसी दौर में स्त्रियों की तरफ से हुई दिखती है, जो स्त्री के सही यथार्थ की बात कर रही थी। उसके संघर्षों और परिस्थितियों की आवाज बन रही थी। लेकिन ऐसी आवाजों को दबाया या उपेक्षित किया गया। प्रतिभाशाली की उपेक्षा करना लेखन-तंत्र का भी एक बड़ा औजार है। जेंडर विभेद की स्थिति इतनी गहरी है कि जहां-जहां स्त्रियों ने बड़ा काम किया या बड़ा दायरा बनाया, वहां-वहां उनका नाम लेने का साहस प्राय: नहीं किया गया। साहस इतना भी नहीं दिखता कि अगर स्त्रियों ने साहित्य भाषा को नया आयाम दिया और उल्लेखनीय बदलाव किया तो उसे स्वीकार किया जाए। दरअसल, इतने लंबे समय तक स्त्री लेखन की उपेक्षा और साहित्येतिहास से उनकी जानबूझ कर बनाई गई अनुपस्थिति भी इसका एक आधार तैयार करती है।
सभी कलाओं में स्त्री के प्रवेश के साथ उसकी सरपरस्ती की स्थितियां भी बनाई गई थीं। यह एक स्त्री आई है- गाने, अभिनय करने, लिखने, यह अकेले कैसे रह सकती है? इसका गॉडफादर कौन है? अकेले, अपने अस्तित्व के साथ खड़ी स्त्री हमारी समाज संरचना से गायब है। और यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है- अपनी जगह बनाना और वहां मजबूती से खड़े होना। उसके अपने समाज यानी समाज के भीतर उसकी अपनी सामाजिकता का प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन चूंकि वह संरचना के भीतर नहीं है, इसलिए समस्यामूलक है और सबसे पहले इससे टकराना जरूरी हो जाता है। इसलिए ‘कब्जे की भूमि’ के सिंद्धांत को कलाओं में भी लागू किया गया था।
सरपरस्ती की कोशिशें और फिर उसके सरपरस्त के अनुसार उसका कद निर्धारित किया जाना भी इसी सिद्धांत से निकल कर आया था। इससे इनकार कर देने वाली स्त्रियों को पता है कि उनकी राह आसान नहीं रह जाती। जबकि स्त्री कला-जगत में इसलिए आती है कि उसे यहां जेंडर-बोध से ऊपर उठ कर दुनिया को जानने-समझने का विकल्प दिखाई पड़ता है। वह यहां आती है कि ज्ञान का संधान कर सके, वह अपने सहकर्मियों या बौद्धिकों से बतियाती है कि ज्ञान के नए आयाम से परिचित हो सके, लेकिन कहीं भी उसे बौद्धिक या विद्वान के रूप में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। देह की सीमा से आगे स्त्री को बुद्धि के स्तर पर समानता का स्थान देने में अब भी हिचकिचाहट बनी हुई है।
हमारे साहित्य इतिहास में ऐसी स्त्रियां भी रही हैं, जिन्होंने ऐसी सरपरस्ती से इनकार किया और जाहिर है कि इसके कारण उनका संघर्ष कई गुना बढ़ा। मीरां को संप्रदाय-निरपेक्ष कवि माना गया। उन्हें प्राय: फुटकर खाते में डाल कर पढ़ा-पढ़ाया गया। अपने निर्णय और अपनी ‘अनूठी चाल’ चलने के एवज में उन्हें अपने समय में क्या-क्या न सहना-सुनना पड़ा? और बौद्धिक जगत ने भी लंबे समय तक उनका कोई स्वागत नहीं किया। बहुत बाद में मीरां पर नए सिरे से और नए संदर्भों में बात होनी शुरू हुई। आज के संदर्भ में अगर देखें तो स्त्रियों ने संघर्ष के बाद अपनी जो जगह बनाई थी, बौद्धिक भागीदारी की अपनी दावेदारी दिखाई थी, एक बार फिर उन्हें उसी संघर्ष को दुहराना पड़ रहा है।
आज बड़े सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदि के रूप में उनकी उपस्थिति कम होने लगी है। तमाम आयोजनों में उन्हें मुख्य भूमिकाओं से या तो हटा दिया जाता है या उनकी उपस्थिति को महत्त्व नहीं दिया जाता। कभी-कभी तो बड़े आयोजनों में एक भी स्त्री की भागीदारी नहीं दिखती। पत्र-पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी स्त्रियों की संख्या नगण्य ही है। इस तरह बौद्धिक क्षेत्रों में उसकी गहरी भागीदारी भी लगातार उपेक्षित की जाती रही है।