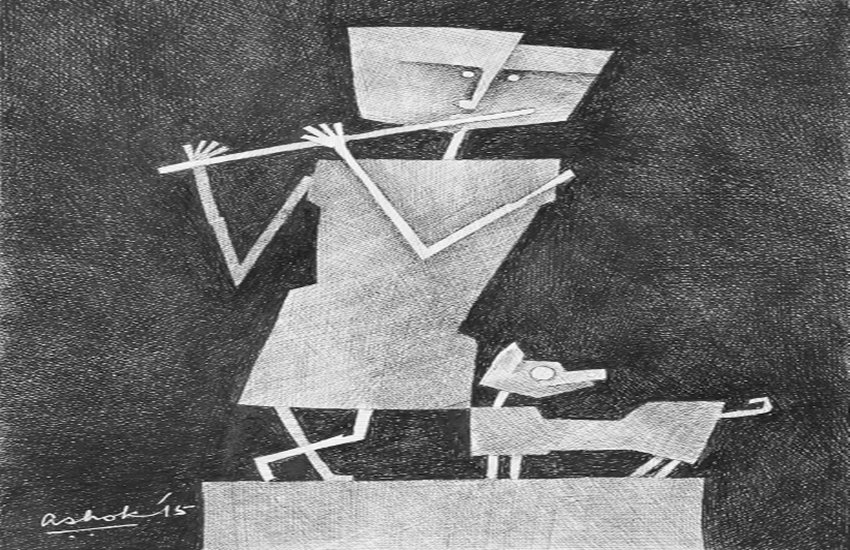साहित्य को गति और दिशा देने में साहित्यिक आंदोलनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आंदोलन न सिर्फ साहित्य में आए गतिरोध को दूर करता है, बल्कि वह उसे युग संदर्भों से जोड़ कर समय और समाज की केंद्रीय संवेदना का वाहक भी बनाता है। समाज की तरह ही साहित्य में भी आंदोलनों का न होना एक तरह से जड़ता का द्योतक है। जीवंत समाज और जीवंत साहित्य दोनों के लिए आंदोलनधर्मिता आवश्यक है। पर दुखद यह है कि हिंदी समाज और हिंदी साहित्य दोनों में ही आंदोलनधर्मिता लगभग समाप्त हो गई है। तो क्या साहित्यिक आंदोलनों के खत्म होने को समाज में आंदोलनों की अनुपस्थिति से जोड़ा जा सकता है? प्राय: ऐसा जोड़ कर देखा जाता है, पर यह साहित्य और समाज के संबंधों का अतिसरलीकरण है। साहित्यिक आंदोलनों का अपने समाज से प्रत्यक्ष रिश्ता होता भी है और नहीं भी। साहित्य समाज से बिंब-प्रतिबिंब जैसा रिश्ता नहीं होता है। साहित्य समाज से निरपेक्ष नहीं होता, तो वह उससे पूरी तरह नाभि-नाल-बद्ध भी नहीं होता। साहित्य और समाज के बीच सापेक्ष स्वायत्तता का संबंध होता है। यह हमेशा जरूरी नहीं कि साहित्य की विकास प्रक्रिया समाज की विकास प्रक्रिया के अनुरूप हो। साहित्य की विकास प्रक्रिया के अपने आंतरिक कारण भी होते हैं। इसलिए साहित्य में हुए परिवर्तनों को समाज में आए परिवर्तनों से हमेशा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचंड दौर में छायावाद का उदय साहित्य के आंतरिक कारणों से अधिक हुआ। प्रगतिवाद को समाज में आए परिवर्तनों से जोड़ा जा सकता है, तो प्रयोगवाद के रूप में हुए परिवर्तन के लिए साहित्य के आंतरिक कारण जिम्मेदार थे। साहित्य की विषय-वस्तु और रूप में परिवर्तन कभी समाज-सापेक्ष होता है तो कभी समाज निरपेक्ष भी। साहित्यिक आंदोलन से समाज की अनुकूलता हमेशा आवश्यक नहीं है। प्रगतिशील आंदोलन बीसवीं सदी का सबसे विराट साहित्यिक आंदोलन था। 1936 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के साथ मार्क्सवादी और गैर-मार्क्सवादी सभी तरह के लेखक जुड़े। इस संगठन का स्वरूप अखिल भारतीय था और दूसरी भाषाओं तक इसका विस्तार था। पर बहुत जल्दी ही यह संगठन संकीर्णतावाद का शिकार हो गया और लेखक संघ कम्युनिस्ट पार्टी के साहित्यिक मोर्चे के रूप में काम करने लगा। 1953 में प्रगतिशील लेखक संघ एक संगठन के रूप में लगभग विघटित हो गया। संगठन तो विघटित हो गया, पर प्रगतिशील आंदोलन में देश भर के साहित्यकारों में जो प्रगतिशील चेतना विकसित करने का व्यापक काम किया था, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। लोग छोटे-छोटे शहरों में अपने तरीके से काम करते रहे। बाद में इस संगठन को फिर से पुनर्जीवित किया गया। आगे चल कर जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच जैसे दो और लेखक संगठन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों क्रमश: माकपा और भाकपा (माले) से जुड़े हुए अस्तित्व में आए। इस तरह तीन कम्युनिस्ट पार्टिया बनीं तो तीन लेखक संगठन भी बन गए। इन तीनों संगठनों ने अपने-अपने तरीके से साहित्य को प्रगतिशील आंदोलन की चेतना से जोड़े रखने में भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य का मूल चरित्र अब भी जनपक्षधर, बाजार विरोधी और गैर-सांप्रदायिक बना हुआ है तो इसमें इन संगठनों की भी बड़ी भूमिका है। पर आज ये तीनों संगठन साहित्य के संदर्भ में लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं। कोई भी नया लेखक इन संगठनों से नहीं जुड़ रहा है। विराट प्रगतिशील आंदोलन धीरे-धीरे इतिहास की वस्तु बनने की ओर अग्रसर है। इसका असर हिंदी साहित्य पर भी दिखना शुरू हो गया है।
प्रगतिशील आंदोलन की सबसे बड़ी समस्या पार्टीबद्धता रही। अगर यह आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी से स्वतंत्र साहित्य का आंदोलन होता, तो यह आज भी संदर्भवान होता। भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टियों के हाशिए पर चले जाने के कारण लेखक संगठन भी हाशिए पर चले गए और साहित्य में प्रगतिशील चेतना की चमक भी फीकी पड़ने लगी। हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से एक ही विराट साहित्यिक आंदोलन था और वह था प्रगतिशील आंदोलन। दुर्भाग्य से इस आंदोलन की रस्सी राजनीति से बंधी हुई थी और जैसे ही वह राजनीति संकटग्रस्त हुई यह आंदोलन भी संकटग्रस्त हो गया। प्रगतिशील आंदोलन के सामानांतर हिंदी में कोई साहित्यिक आंदोलन खड़ा ही नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि प्रगतिशील आंदोलन से बाहर रहे लेखकों में साहित्यिक उत्कृष्टता की कमी थी, पर उनमें वह सामूहिक चेतना समाज संपृक्तता और सांगठनिक क्षमता नहीं थी, जो प्रगतिशील आंदोलन को चुनौती दे सके। इसलिए अपनी तमाम सीमाओं और संकीर्णताओं के बावजूद हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन ही एकमात्र आंदोलन बना रहा। आज इस आंदोलन के समाप्तप्राय होते ही ऐसा लगना स्वाभाविक है कि साहित्य से आंदोलनधर्मिता समाप्त हो गई है। आंदोलनधर्मिता का समाप्त हो जाना संकट तो है ही, पर यह एक अवसर भी है- दलगत राजनीति से अलग साहित्य के स्वधर्म को पहचानते हुए एक वैकल्पिक आंदोलनधर्मिता विकसित करने का। बाजार और सत्ता का जो सुनियोजित हमला आज साहित्य पर हो रहा है उसके लिए नए तरह की आंदोलनधर्मिता की जरूरत है।
सन् दो हजार के बाद साहित्य का परिदृश्य बहुत कुछ बदला है। लेखन में कोई भी ऐसी प्रधान प्रवृत्ति नहीं, जिसके आधार पर इस दौर का कोई नामकरण किया जाए। इस दौर में हर तरह की रचनात्मक प्रवृत्तियां मौजूद हैं। गांव पर लिखने वाले भी हैं और शहर पर भी। उच्चवर्गीय जीवन पर लिखने वाले भी हैं और निम्नवर्गीय जीवन पर भी। कस्बाई परिवेश पर लिखने वाले हैं तो पिछड़े अंचल की कहानियां कहने वाले भी हैं। शिल्प के स्तर पर भी पर्याप्त विविधता है। स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को भी इस दौर में विभाजन का आधार नहीं बनाया जा सकता। स्त्री रचनाकारों के लेखन में भी कोई सामान्य प्रवृत्ति या एकरूपता नहीं है। साहित्य के इतिहास में यह शायद पहली बार है कि इतनी अधिक संख्या में रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं और उन्हें किसी एक व्यापक पहचान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उन्हें न तो नई कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी आदि जैसी किसी नई साहित्यिक प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा जा सकता है और न ही उनका नामकरण किसी पीढ़ी के नाम पर हो सकता है। विचारधारा को लेकर तो उनमें कोई साम्य है ही नहीं। अब न कोई पीढ़ी जैसी बात है और न विचारधारा की। किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति का अनुसरण करने का तो सवाल ही नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में यह बहुलता का दौर है। यह शायद सबसे लोकतांत्रिक दौर है जब लेखन के क्षेत्र में किसी तरह का कोई बंधन या दबाव नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में यह अभूतपूर्व है।
अतिशय लोकतंत्र जहां सृजनात्मकता के लिए बहुत ऊर्वर होता है वही अगर लेखक के पास दृष्टि न हो तो यह बहुत संभव है कि उसका लेखन पतनशील प्रवृत्तियों का शिकार होकर अराजक हो जाए। कुछ रचनाकारों में ऐसी प्रवृत्तियां घर कर रही हैं। साहित्य के लोकतांत्रिक परिवेश का फायदा उठा कर कुछ अराजक किस्म का गैर-साहित्यिक लेखन, साहित्य में प्रवेश करने लगा है। इसके पहले कि साहित्य का वर्तमान अतिशय लोकतांत्रिक परिवेश अराजकता का शिकार हो, लेखक संगठनों से अलग एक नई आंदोलधर्मिता विकसित कर लेनी होगी। साहित्य की सामाजिक सार्थकता के साथ-साथ उसके स्वत्व को लेकर एक सचेत आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा सचेत आंदोलन, जो साहित्य के अस्तित्व और अस्मिता दोनों को महत्त्व देता हो और जिसकी प्रतिबद्धता सिर्फ साहित्य के प्रति हो तथा जो साहित्य को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रयत्नशील हो।