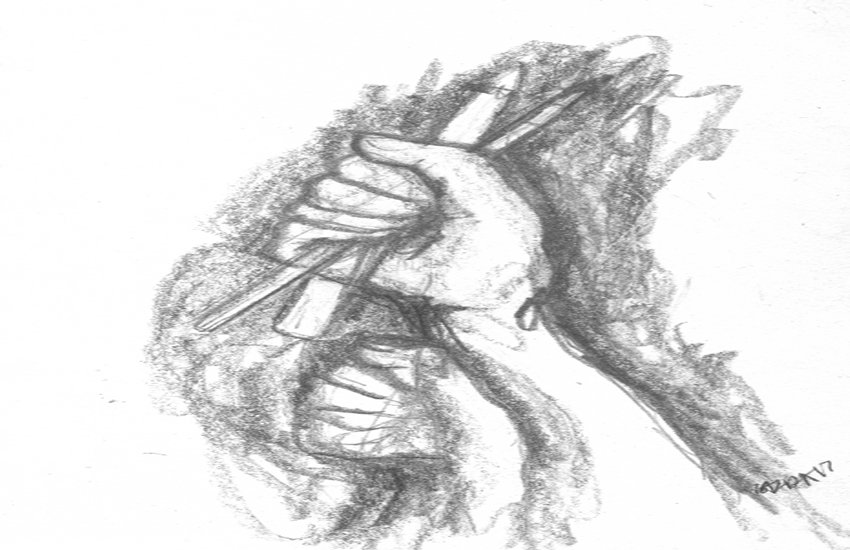इधर हिंदी में लंबी कहानियों का चलन बढ़ा है। आश्चर्य है कि इन कहानियों में भी कथा तत्त्व की घोर उपेक्षा हो रही है। कथा के सहारे कहानी को आगे न बढ़ा कर तरह-तरह के विवरणों, दृश्यों और ज्ञानवर्धक व्याख्यानों के सहारे उसे लंबा खींचने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कथा रस के बिना इन कहानियों को पढ़ना पाठकों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। कहानी का लंबा होना अपने आप में कोई दोष नहीं है। जब कोई कहानी अपने समय के वृहत्तर यथार्थ को बड़े फलक पर प्रस्तुत करेगी, तो उसका लंबा हो जाना स्वाभाविक है। पर आज की कहानी इस कारण से लंबी नहीं हो रही है। वह लंबी इसलिए हो रही है कि कहानीकार ने जो कुछ भी देखा-सुना या जाना होता है उसे कहानी में प्रस्तुत कर देता है। वह तय ही नहीं कर पाता कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। इसलिए कहानी विवरण मात्र बन कर रह जाती है। यथार्थ से कहानी के लिए उपयोगी सामग्री का चयन करने की जगह कथाकार समूचे यथार्थ को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है। समय के बड़े सत्य को अभिव्यक्त किए बिना कहानी का लंबा होना कहानीकार की क्षमता नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मक विफलता का द्योतक है।
इस समय लिखी जा रही लंबी कहानियों में मुख्यत: तीन प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। कुछ कहानियों में छोटी-सी घटना या बात को जबर्दस्ती खींच कर बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखती है। इसका सबसे आसान तरीका अतीत या वर्तमान की किसी घटना, दृश्य या परिस्थिति को लेकर पात्रों की लंबी-लंबी मानसिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन है। ऐसे वर्णन प्राय: ऊब पैदा करते हैं। कई बार तो कहानीकार पात्रों की ओट न लेकर सीधे खुद वर्णन करने लगता है। ऐसा प्राय: वातावरण निर्माण के नाम पर किया जाता है। किसी न किसी बहाने अनावश्यक वर्णन की प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इससे कहानी तो लंबी बन जाती है, पर वह घोर उबाऊ हो जाती है।
दूसरी तरह की वे कहानियां हैं, जिनमें कहानीकार किसी घटना, स्थिति, प्रथा, समाज या क्षेत्र विशेष के बारे में तमाम सूचनाएं इकट्ठा करता है और उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देता है। कहानीकार इस गर्व से भरा होता है कि उसने बहुत शोध-कार्य के बाद एक लंबी कहानी लिखी है। लेकिन वास्तव में हो यह रहा है कि वह अपना शोध-कार्य ही लिख देता है, उसमें कहानी कहीं रहती ही नहीं है। सूचना विस्फोट के इस दौर में कहानी के माध्यम से वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक या तथ्यात्मक ज्ञान देने से बड़ा अज्ञान कुछ नहीं हो सकता है। आज ज्ञान के अनेकानेक स्रोत उपलब्ध हैं। नेट पर तमाम तरह की सूचनाएं मौजूद हैं। ऐसे में कोई कहानी इसलिए महत्त्वपूर्ण हो ही नहीं सकती है कि उसमें किसी विषय पर बहुत जानकारियां दी गई हैं। आज का पाठक काफी पढ़ा-लिखा है। ज्ञान के मामले में वह कहानीकार से भी आगे है। विशुद्ध जानकारी की दृष्टि से भी देखें तो कहानीकार पाठक को ऐसा कुछ नया नहीं दे पाता है, जो वह पहले से न जानता हो। वैसे भी कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए कहानी नहीं पढ़ता। ज्ञान के लिए वह दूसरे स्रोतों को तलाशता है। कहानीकार को किसी भी विषय पर कहानी लिखने के लिए शोध-कार्य अपने ज्ञान के लिए करना चाहिए, पाठक को ज्ञान देने के लिए नहीं। ज्ञान का संवेदना में रूपांतरण कहानी ही नहीं, किसी भी रचना की पहली शर्त है। पर कहानीकार इस बात को न समझते हुए सीधे ज्ञान को ही पाठकों के सामने परोस दे रहा है। वह जिस भी विषय पर कहानी लिखता है, उसमें अपने आप को उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करने लगता है।
किसी विषय का कहानीकार होना और विशेषज्ञ होना, दो अलग बातें हैं। यहां हमें कथावस्तु और कथानक के अंतर को समझना चाहिए। कथावस्तु वह सामग्री है, जिसे कहानीकार अपनी रुचि के अनुरूप जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। जैसे किसान जीवन, मध्यवर्गीय जीवन, कामकाजी स्त्री का संघर्ष, दलित जीवन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन आदि। इस चुनी हुई सामग्री को जब विविध तरह के पात्रों, उनके क्रिया-व्यापारों और घटनाओं में व्यवस्थित और निरूपित किया जाता है, तो कथानक की सृष्टि होती है। कहानीकार समर्थ है या नहीं, इसका पता कथानक निर्माण से चलता है, कथावस्तु के चयन से नहीं। कहानी अपने कथानक के कारण महत्त्वपूर्ण या कमजोर होती है, कथावस्तु के कारण नहीं। किसी विषय (कथावस्तु) पर कहानी लिखने के लिए उस विषय से संबंधित तमाम जानकारियों का होना आवश्यक है, पर कहानीकार होना इस विशेषज्ञता से आगे की स्थिति है। कथावस्तु का वर्णन करना विशेषज्ञता है और कथानक निर्माण कहानी कला है। कहानीकार में विशेषज्ञता और कहानी-कला दोनों का मेल होता है। शोध और परिश्रम करके लंबी कहानियां लिखने वाले इस दौर के अधिकतर लेखक विशेषज्ञता की पहली सीढ़ी को पार नहीं कर पा रहे हैं। वे कहानी के नाम पर सिर्फ कथावस्तु की प्रस्तुति कर रहे हैं।
इधर यथार्थ के रोचक वर्णन के सहारे भी लंबी कहानियां लिखने की प्रवृत्ति उभर रही है। ऐसी कहानियों में किसी स्थान विशेष के जीवन को बगैर किसी लेखकीय हस्तक्षेप के प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। स्थानीय शब्दों और मुहावरों के प्रयोग के साथ ही वहां के लोगों की दिलचस्प गतिविधियों के वर्णन द्वारा कहानी में रोचकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसी कहानियां सिर्फ दृश्य कोलाज बन कर रह जाती हैं। कहानीकार एक स्थान विशेष के तरह-तरह के दृश्यों को एक साथ प्रस्तुत करने को अपनी उपलब्धि के रूप में देखता है। कथा और कथ्य दोनों की अनुपस्थिति के कारण इन दृश्य-वर्णनों को पढ़ने के बाद अंत में पाठक के हाथ में शून्य ही लगता है। उपर्युक्त तीन प्रधान प्रवृत्तियों से युक्त इस दौर की लंबी कहानियों के कारण पाठक कहानी विधा से दूर हो रहे हैं। प्रेमचंद ने तिलिस्म, रहस्य, रोमांच, और सतही भावों की दुनिया से हिंदी कहानी को निकाल कर अपनी अद्वितीय कहानी-कला द्वारा उसे यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया था। अगर हमारे कहानीकार बिना कथा-रस वाली उबाऊ कहानियां लिखते रहे, तो बाजार के दबाव में कहानी बहुत जल्दी अपनी यथार्थवादी जमीन छोड़ कर बाजारोन्मुख हो जाएगी। उबाऊ कहानियों का फायदा उठा कर ही ‘लप्रेक’ जैसी चीजें बाजार में आने भी लगी हैं। एफएम रेडियो पर भी कहानियां सुनाई जा रही हैं।
अगर कहानीकारों ने इधर-उधर से जोड़ कर बिना कथा-रस के, विवरणों की भरमार वाली कहानियां लिखना जारी रखा, तो बहुत जल्दी कहानी में भी कविता के तर्ज पर साहित्यिक कहानी और लोकप्रिय कहानी का विभाजन शुरू हो जाएगा। यह विभाजन हिंदी कहानी और संपूर्णता में हिंदी साहित्य के लिए आत्मघाती होता। अब समय आ गया है कि कहानी की आलोचना करते समय सफल कहानी के लिए उस प्राथमिक कसौटी का सख्ती से पालन किया जाए कि जिस गद्य रचना को कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई कहानी है कि नहीं। कहानी को बड़ा बनाने के लिए कहानीकार ने बेवजह घटनाओं और प्रसंगों को बढ़ाया तो नहीं है? वह किसी बहाने शोध से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या तो नहीं कर रहा है? और सबसे अहम बात कि उसने शुरू से आखिर तक पाठकों की जिज्ञासा और उत्सुकता बनाए रखने में सफलता पाई है कि नहीं? इन कसौटियों पर खरा न उतरने वाली कहानियों को खारिज करना ही होगा, चाहे उसका कहानीकार कितना भी ख्यात या अपना मित्र ही क्यों न हो? कहानी को बचाने के लिए कहानीकार की जगह हमें कहानीपन के पक्ष में खड़ा होना ही होगा।