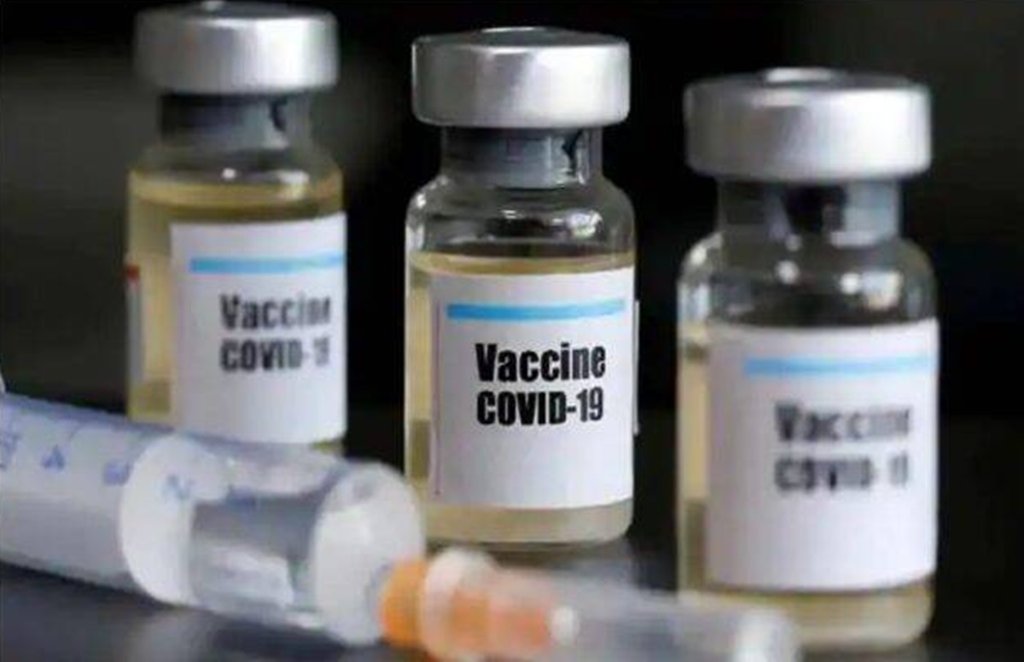भारत इस समय प्रकृति प्रदत्त आपातकाल झेल रहा है। इसका फैलाव वैश्विक है, लेकिन अदृश्य शत्रु की रणनीति को समझने में हुई गफलत के कारण सारा देश अत्यंत कष्टकर पीड़ा में है। ऐसे कठिन समय में जिस प्रकार की राष्ट्रव्यापी एकता और एकजुटता की आवश्यकता होती है, वह दुर्भाग्य से अपेक्षित परिमाण में इस समय भारत में नहीं उभरी है। मुख्य रूप से इसका सीधा संबंध देश की दलगत राजनीति में लगातार होते रहे सैद्धांतिक और मूल्यगत क्षरण से जुड़ता है।
स्वतंत्रता के पांचवें-छठे दशक में विश्वविद्यालयों में हर युवा गांधी- और उनके आदर्शों की- जीवंत उपस्थिति का अनुभव करता था, उनके अनेक सहयोगियों के दर्शन और उनके विचारों को सुनने का अवसर भी पाता था। गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा से सभी किसी न किसी ढंग से प्रभावित होते थे। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से निकल कर जीवन के कार्य-क्षेत्र में पांव रखने वाले हर युवा के साथ गांधी किसी न किस रूप में उपस्थित रहते थे। उनका एक-एक वाक्य युवाओं की वैचारिकता को झकझोर देता : ‘भारत अपने मूल स्वरूप में कर्मभूमि है, भोगभूमि नहीं।’ हर एक को मार्ग निर्देशन देता था उनका यह कथन : ‘भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया है, उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं।’ लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस मनोबल की आवश्यकता होती है वह भी गांधी के चिंतन में सर्वत्र दिखाई देता था : ‘हमारी सभ्यता का मूल तत्व ही यह है कि हम सब अपने सब कामों में, फिर वे निजी हों या सार्वजनिक, नीति के पालन को सर्वोच्च स्थान देते हैं।’
इन वाक्यों को समझने और उनमें निहित दर्शन को जीवन में उतरने में वर्षों लगाए जा सकते हैं, और लोगों ने लगाए हैं। इनकी सार्थकता तो नीति के व्यावहारिक पालन के इर्द-गिर्द ही ढूंढ़ी जा सकती है। व्यक्ति से लेकर सत्ता के सर्वोच्च स्तर तक के लिए नैतिकता की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट हैं। सामान्य व्यक्ति तो ‘महाजनो येन गत: स पंथा:’ में आज भी विश्वास रखता है। अगर देश की राजनीति; और उससे जुड़े राजनेता; अपने इस उत्तरदायित्व को भूल जाएं, तो निश्चित रूप से नीति-पथ से बिलगाव हर स्तर पर बढ़ता ही जाएगा।
कहने की आवश्यकता नहीं कि पिछले कई दशकों से मूल्यों के क्षरण ने देश को अपनी गहराती उपस्थिति से परिचित करा दिया है। अगर आज देश की राजनीति, सत्ता पक्ष तथा विपक्ष, में मूल्यों के प्रति वैसी ही प्रतिबद्धता होती जैसी पचास और साठ के दशक में थी, तो निश्चित ही कोरोना के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान में सभी एकजुट होते, राजनीति नहीं हो रही होती, आरोप-प्रत्यारोप में लगाया जा रहा समय लोगों के दारुण दुख और असहनीय कष्टों के निवारण में लगाया जा रहा होता! सरकारों की कमियां बताना विपक्ष का अधिकार है, साथ ही जनहित में राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों में पूर्ण सहयोग देना भी उसका कर्तव्य है। उसमें सुधार के लिए सुझाव देना बंद करना आवश्यक नहीं है, मगर राष्ट्रीय या राज्य स्तर के निर्णय के साथ खड़े न होना नैतिकता के आधार पर उचित नहीं माना जाएगा।
टीके लगाने को लेकर जो स्थिति बनी है, वह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, उसके बाबजूद लोगों का मनोबल बढ़ाने, टीके के लिए प्रोत्साहित करने, और व्यवस्था में सहयोग देने की आवश्यकता को कोई भी नकार नहीं सकता है। जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आए, केंद्र तथा राज्य सरकारों को पक्ष-विपक्ष भूल कर सभी सुझावों पर दिल खोल कर सार्थक विचार-विमर्श करना चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल और राजनेता को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विश्व पटल पर भारत की उभरती स्थिति को लेकर अनेक देश चिंतित हैं, वे भारत को कमजोर करना चाहेंगे, अनेक अंतरराष्ट्रीय लाबियां भारत को आत्मनिर्भर बनते नहीं देखना चाहती हैं, उनके चंगुल में फंसने से सभी को बचना होगा। देश के कोई भी तत्व, जो किसी भ्रमवश इनके चंगुल में फंस जाएंगे, उन्हें देश कभी क्षमा नहीं करेगा।
साठ के दशक में भी देश में पक्ष-विपक्ष था, मतभेद थे, मगर युद्ध के समय सभी एक पंक्ति में खड़े थे। राजनेताओं में दलगत मतभेदों के होते हुए भी पारस्परिक संबंधों में सम्मान तथा शालीनता की उपस्थिति से जनता भी परिचित थी। सारे देश को यह विश्वास था कि राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण या आपदा के समय सभी साथ आ जाएंगे। पक्ष और विपक्ष, दोनों की साख की स्वीकार्यता हर ओर थी। आज के युवा के समक्ष पक्ष-विपक्ष मिल कर जो चित्र उकेरते हैं, उसमें राष्ट्रीय एकजुटता, पारस्परिकता तथा विश्वास कहीं दिखाई नहीं देता है। संवाद की कमी हर ओर लगातार बढ़ती दिखती है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक चहल-पहल को लेकर विश्व का ध्यान भारत की तरफ खिंचा है।
भारत के विरोधी देश इसकी प्रगति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवधान डालने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे। यह दुर्भाग्य है कि इस समय भारत किसी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने घर को संभाल पाने में अक्षमता, दूरदृष्टि की कमी और उचित समय पर अपेक्षित संसाधन और समन्वय न कर पाने के लिए चर्चित है। इसमें राजनीति भी है, वैश्विक लाबियां हैं, अनेकानेक स्वार्थ हैं। हमारी प्रशासनिक कमियां और व्यवस्था की कमजोरियां हमें स्वयं भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में देश का सबसे बड़ा संबल उसकी राष्ट्रीय एकजुटता ही हो सकती है; भारत के हर निवासी और हर मतदाता की यही अपेक्षा है।
पिछले सात दशकों में भारत के मतदाता की राजनीतिक समझ और परिपक्वता निश्चित रूप से बढ़ी है, मगर अधिकांश राजनीतिक दल इसे समझ नहीं पाए हैं, और इसका मुख्य कारण उनका सैद्धांतिक मूल्यों से लगातार दूर जाना और राजनीति को एक पेंशन वाला ‘जॉब’ बना देना है। इसी के परिणामस्वरूप वे जनता से, उसकी आवश्यकताओं की समझ और अपने उचित कर्तव्यबोध से भी बहुत दूर जा चुके हैं। क्षेत्रीयता, जातिगत समीकरणों तथा पांथिक/ सांप्रदायिक आधार पर उभरे राजनीतिक दल वैश्वीकरण के इस युग में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, या यों कहें कि उन्होंने इसे समझने का प्रयास ही नहीं किया।
क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज भी देश में अनेक ऐसे समुदाय और समूह हैं, जो टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके किसी सम्मानित या पांथिक व्यक्ति ने उन्हें किसी न किसी कारण इससे दूर रहने को कहा है! हर सम्मानित राजनेता का, वह किसी भी दल का क्यों न हो, यह कर्तव्य है कि वह लोगों की आशंकाओं को दूर करे, उनके बीच जाकर समय बिताए! दलाई लामा के शांति, सद्भाव और सहयोग के प्रयासों की सराहना चीन को छोड़ कर सारे विश्व में होती है।
वे मानते हैं कि हर मानव समाज और समुदाय में विचारों तथा हितों में भिन्नता होगी ही। पर तथ्य यह है कि आज के समय में हम सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं, और इस पृथ्वी पर सबको साथ-साथ ही रहना है। इसलिए मतभेद चाहे व्यक्तियों के बीच हों या राष्ट्रों के, रास्ता केवल संवाद का ही है। भारत के राजनीतिक दलों को इसे समझना, स्वीकार करना होगा, तभी उनकी साख बचेगी। इस पारस्परिकता से भारत और हर भारतीय की प्रतिष्ठा तथा वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी।