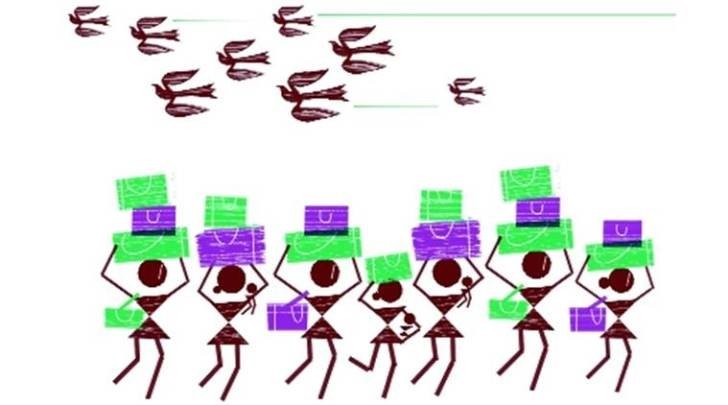नवनीत शर्मा
समानुभूति उसी समाज में रची-बसी है, जिसमें यह लोक-आस्था बची है कि ‘जाके पैर फटी न बिवाई सो क्या जाने पीर पराई’। परानुभूति यानी दूसरे की अनुभूति करने के लिए भी स्व को केंद्रित करते हुए हमने उस मूल्य को अपनाया, जिसके अंतर्गत हम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करें, जैसा कि हम स्वयं के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं।
किसी अन्य की पीड़ा के प्रति सहानुभूति हमें सहज और सरल भाव लगता है। इससे परोपकार और दया जैसे भाव पनपते हैं। ऐसे ही समाज में, जहां बहुत सारे स्कूल और कालेज ही परोपकार से प्रेरित होकर खोले गए हों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी परोपकारी शिक्षा और ‘कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलटी’ के सहारे भावी नागरिकों में उद्यमिता और क्षमताएं विकसित करना चाहती हो, वहां सहानुभूति के बरक्स समानुभूति के पाठ दुरुह ही लगेंगे।
समानुभूति ऐसी मानवीय संवेदना है, जिसमें दूसरे की भावना समझने से आगे बढ़ कर ऐसी कल्पनाशीलता है, जिसमें स्वयं को उसी परिस्थिति में रख कर उस क्षण और मनोभाव को अंगीकार करने का प्रयास होता है। गांधी जब शौचालय साफ करने को कहते हैं, तो वह दलित कर्म और जाति के प्रति सहानुभूति से विलग एक समानुभूति विकसित करने का प्रयास है, जिसमें स्वच्छ और निर्मल रहना अगर ईश्वरीय है, तो इसमें हमारी सहायता करने वाला ‘हरिजन’।
मुक्तिबोध इसे भिन्न प्रस्थान बिंदु से देखते हैं और लिखते हैं कि ‘जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए’। कांचा इलैया तो इससे भी भिन्न दावा करते हैं कि जिस दिन हम दलित झाडू रख देंगे उस दिन ब्राह्मणवादी स्वच्छता और निर्मलता के मानक ध्वस्त हो जाएंगे। दलित, हरिजन, दलित-बहुजन, आदिवासी और बहुजन की भाषायी और चुनावी राजनीति के बीच सहानुभूति और समानुभूति का अंतर ही व्याप्त है।
जिस समाज में अंगहीनता भी हास-परिहास का विषय हो और दृष्टि बाधित को ‘सूर’, मूक-बधिर को ‘बिना सिग्नल का रेडियो’, ‘लंगड़ा’, ‘लूला’, ‘काना’ जैसी शब्दावली चलन में हो, वहां दया और श्रद्धाजनित सहानुभूति तो हो सकती है, पर समानुभूति नहीं। इसके प्रयास में जो पाठ स्कूली किताब का हिस्सा बना, उसमें ‘श्यामा की गुड़िया’ के अगर आंख, कान, नाक, जीभ और हाथ नहीं हैं, तो उसे उल्लू की आंख, खरगोश के कान, हाथी की सूंड, बिल्ली की जीभ और बंदर के हाथ लगा कर सक्षम बनाने की सीख है।
ऐसे में उनके लिए भिन्न ‘विशेष’ स्कूल खोले जाएं या उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए ‘सामान्य’ स्कूल और कक्षा का हिस्सा बनाया जाए, शिक्षा विमर्श में समावेशी शिक्षा की चिंता का विषय बना रहता है। अपंग, विकलांग, अपाहिज, दिव्यांग, निशक्तजन और भिन्न रूप से सशक्त के प्रयोग के भाषायी विमर्श और नीति निर्माण में हस्तक्षेप सहानुभूति और समानुभूति के मध्य हिलोरें लेता रहता है।
स्त्री के पक्ष में समानुभूति प्राय: ‘स्त्रैण’ होने और पुरुष की यौनिकता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। जिस समाज दर्शन में यह मान्य हो कि अगर स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह कुलटा हो जाती है, उस समाज में स्त्री समानुभूति को पौरुष या मर्दानगी की कमी देखा जाता है। पर समानुभूति के उदाहरण साहित्य रचनाकर्म से लेकर लोकजीवन तक विरले ही हैं। किन्नर और अन्य किसी लैंगिकता के प्रति समानुभूति तो विलुप्त है ही, साथ ही सहानुभूति भी व्यंग्यात्मक श्रद्धा या भय का ही हिस्सा है।
अन्य धर्म, प्रांत, भाषा, रंग आदि के लिए समानुभूति भी उस सामाजिकता में पनपना जटिल है, जहां उन पर आधारित लोकोक्तियां और कहावतें रोजमर्रा का विमर्श बुनती हों। अल्पसंख्यकों को उनकी वेशभूषा, जीवनचर्या से चिह्नित करना, पूर्वोत्तर के लोगों को ‘चिंकी’, ‘चाउमीन’ कहना, अन्य रंग कद-काठी का परिहास करना ऐसे समाज की बानगी प्रस्तुत करता है, जो दिखता भले समरस हो, पर गहरे भीतर विखंडित है। रंग-भेद केवल लैंगिक न होकर जातीय भी है, काले ब्राह्मण और गोरे शूद्र को लेकर अनन्य उपमाएं हैं।
यही रंगभेद गोरा होने की क्रीम के लिए भारत को एक बड़ा बाजार बनाता है। अन्य धर्म के मतावलंबियों के लिए चुटकुले और उन्हें मंदबुद्धि समझना ‘सामान्य’ हो चला है। अन्य भाषाओं के प्रति दुराव भी रोज की बातचीत में व्याप्त है, उर्दू बोलने को जबान का ‘वेश्या’ सरीखा होना या दक्षिणी भाषाओं का लोटे में कंकड़ डाल कर हिलाने जैसा समझना, यही दुराव हिंदी के प्रति अहिंदी भाषी राज्यों में व्याप्त है। अन्य प्रांतीय व्यंजनों, नृत्यों और गीतों को लेकर उपहास बनाना न केवल लोक विमर्श है, पर उसे सिनेमाई चित्रण में उकेर कर भुनाने का प्रयास भी जारी है।
हिंदी सिनेमा में दक्षिणी, अल्पसंख्यकों, भिन्न यौनिकता के पात्रों का चित्रण पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, इसी तरह प्रांतीय सिनेमा में इसका उलट पूर्वाग्रह होना आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसे व्यतिक्रम में किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, छात्र, अध्यापक या किसी भी अन्य द्वारा आवाज उठाने, आंदोलन या संघर्ष करने को संशय की नजर से और सुचारु यातायात में व्यवधान मात्र देखना ‘स्वाभाविक’ है।
संघर्ष करने की जीवटता को ढीठ, आलसी, सुविधाभोगी का पर्याय मान लिया गया है। जिस समाज ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन के सहारे नब्बे वर्ष आजादी की लड़ाई लड़ी, वह मात्र सत्तर वर्ष में उसे बिसरा चुका है। नेहरू से यह पूछे जाने पर कि अंग्रेजों ने लगभग दस वर्षों तक उन्हें जेल में रखा, क्या उन्हें उनसे घृणा नहीं होती, उन्होंने गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, ‘पाप से घृणा करो पापी से नहीं। घृणा वैमनस्य पैदा करती है, वैश्विकता नहीं।’
इसी क्रम में ‘दुनिया के मजदूरो एक हो’ और ‘मजदूरो दुनिया को एक करो’ के बीच समानुभूति और सहानुभूति का अंतर व्याप्त है। चिकित्सा विज्ञान पढ़ने वालों में मरीज के साथ समानुभूति को पेशेवर नहीं माना जाता, पर समानुभूति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित किया जाना अपरिहार्य है, जो कि शिक्षा व्यवस्था का अब शायद ही सरोकार है। जिस शिक्षा व्यवस्था में मेरिटवाद और प्रथम आने की ललक और प्रतियोगिता अंतर्निहित हो, उसमें समानुभूति के पनपने की संभावना शून्य ही है।
शिक्षा को ‘उबंतु’ के दर्शन को आत्मसात करना होगा, जिसमें ‘मैं हूं, क्योंकि हम हैं’ का मूल केंद्रित हो। यह भाव पढ़ाना जटिल है, क्योंकि कक्षायी गतिविधियों और शिक्षा विमर्श में सफलता और मेरिट, संसाधनों के बंटवारे का आधार है और अधिक से अधिक संसाधनों पर काबिज होना नवउदारवाद का लक्ष्य है। ऐसे में गांधी, टैगोर, आंबेडकर और फ्रेरे शिक्षा और शिक्षा नीतियों के विमर्श में नेपथ्य में धकेल दिए जाते हैं और सहानुभूति की संस्कृति और परोपकार द्वारा शिक्षा-दान मंच पर मुख्य भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में पीएचडी प्रवेश और अध्यापक चयन में उच्च शिक्षा केंद्रों का ‘अग्रहार’ बना रहना कोई विस्मय नहीं उत्पन्न करता। यह शिक्षा व्यवस्था एकलव्य, कर्ण और अर्जुन को न केवल अलग-अलग खेमों में रखती है, बल्कि धनुर्धारी के सहोदरपन की समानुभूति को पनपने से भी रोकती है। यह कहना निरापद ही है कि शिक्षा का समवर्ती सूची में होना राज्य-राष्ट्र के बीच समानुभूति और सहानुभूति का अंतर ही है। ऐसे में शिक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापक, अध्यापक शिक्षा के दारोमदार और सरोकार पुनर्रचना की मांग करते हैं, अन्यथा समानुभूति के पाठ राजनीतिक रस्साकशी और सामाजिक वितान में उलझ कर दिवास्वप्न ही रह जाएंगे।