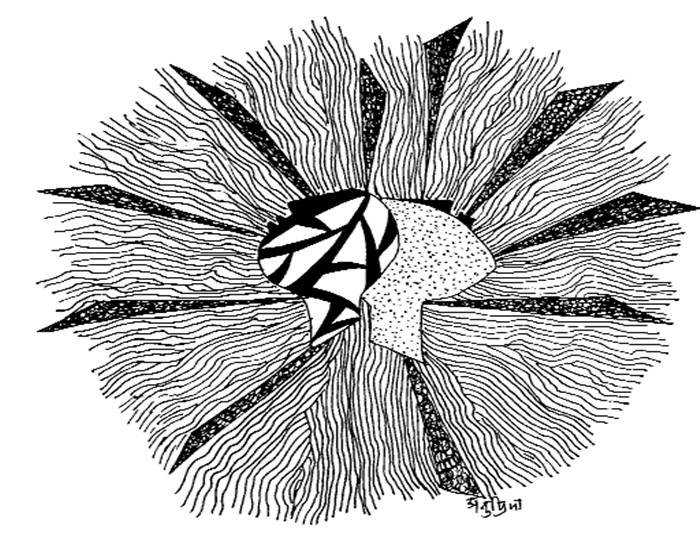मणींद्र नाथ ठाकुर
समय बदल रहा है। राजनीति बदल रही है। हम जनतंत्र के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अस्मिता ही विश्लेषण का दृष्टिबिंदु हो गई है। जो कुछ भी अब तक सर्वमान्य था, अब अस्मिता के चश्मे से एकपक्षीय लगने लगा है। जिन इतिहासकारों की बातों को ब्रह्मवाक्य माना जाता था, उन पर भी शक किया जाने लगा है कि शायद सत्य से ज्यादा उनके लिए विचारधारा महत्त्वपूर्ण थी। शायद यह एक नया वैचारिक युग है। मुझे इस बात को मानने में कोई मुश्किल नहीं है कि आधुनिकता का वैचारिक युग संकट में है, इस बात को मान लेना भी सहज नहीं लग रहा है कि हम उत्तर-आधुनिक युग में रह रहे हैं। उत्तर-आधुनिकता की इतिहास दृष्टि में कोई केंद्रीय कथ्य नहीं है, कोई मेटानेरेटिव नहीं है। क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता भी हो सकता है?
आज के समय में हर समाज अपना इतिहास खोजता है और अस्मिता संघर्ष के इस युग में उस इतिहास का राजनीतिक महत्त्व भी है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक ही है। अगर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए राष्ट्रीय इतिहास रचने की जरूरत पड़ी, तो अस्मिता संघर्ष के लिए इतिहास का पुनर्लेखन क्यों नहीं होगा। वैसे भी मुख्यधारा का इतिहास जन-इतिहास नहीं था, धटना प्रधान या व्यक्ति प्रधान था। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हर किसी को अपना इतिहास जानने का हक है। और अपनी जाति का स्वर्ण युग खोजने का भी हक है।
भारतीय इतिहास को ही लें तो बात समझ में आ जाती है। अंगरेजों ने हमारा औपनिवेशिक इतिहास लिखा; राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने स्वर्णयुग खोजा; मार्क्सवादियों ने वर्ग संघर्ष से इतिहास की व्यख्या की; सबाल्टर्न इतिहास दृष्टि ने जमीनी इतिहास लिखने की कोशिश की। लेकिन इन सबके बावजूद दलित समुदाय का इतिहास रह गया; आदिवासी समुदाय का इतिहास उजागर नहीं हो पाया। या फिर इतिहास में उन्हें केवल निमित्तमात्र समझ लिया गया। आज के युग में जब इतिहास का राजनीतिक महत्त्व इतना बढ़ गया है, इस तरह के इतिहास लेखन पर सवाल उठना लाजिमी है।
अस्मिता की राजनीति से इतिहास लेखन में एक और समस्या आ गई। एक तरफ तो जातियों के स्वर्ण युग की खोज होने लगी, दूसरी तरफ उनके वर्तमान दयनीय हालत के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाने लगी। जिम्मेदारी तय किया जाना राजनीतिक तौर पर महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि उससे फिर यह तय होना था कि उस समुदाय का खलनायक कौन होगा। अस्मिताएं छोटी-बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी इतिहास दृष्टि एक जैसी है। उसमें नायक, खलनायक और उत्थान-पतन की कहानी एक जैसी है। इस नई इतिहास दृष्टि ने इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री की स्वीकार्यता में भी बदलाव लाया है। इतिहास के लिए अगर केवल सरकारी दस्तावेजों पर निर्भर रहा जाए तो समस्या है।
आधुनिक इतिहासकरों के इस आधार पर वस्तुनिष्ठ होने के दावे में कुछ खास तथ्य नजर नहीं आता, क्योंकि इन दस्तावेजों का अपना एक दृष्टिकोण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दस्तावजों से कितना सच निकाला जा सकता है, इसमें शक है। इसलिए अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि आत्मकथाओं और लोककथाओं को क्यों नहीं इतिहास की सामग्री के रूप में उपयुक्त माना जाए। खासकर उन समुदायों के लिए यह तर्क सही लगता है, जिनका या तो सरकारी रिकॉर्ड में कुछ नहीं है और न ही मुख्यधारा के इतिहासकारों ने उनकी सुध ली है।
मुख्यधारा के इतिहासकारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण नायक वीर कुंवर सिंह को इतिहास के पन्नों में कोई खास जगह नहीं दी है। अब कुछ इतिहासकार और साहित्यकार मिल कर उस इलाके की लोककथाओं और किंवदंतियों से तथ्य एकत्रित कर इस इतिहास को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में उन्हें केवल एक विद्रोही जमींदार से ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है। लेकिन लोकस्मृति में उनकी छवि किसानों के साथ सहानुभूति रखने वाले और जनहित के लिए प्रतिबद्ध जमींदार के रूप में है। उनकी यह छवि लोकगीतों और जनमानस में जीवित है। क्या फिर इस आधार पर इतिहास में उनके लिए नई जगह खोजना संभव है, या फिर हमें इसके लिए औपनिवेशिक सरकार की उपलब्ध फाइलों पर निर्भर रहना चाहिए। इसी तरह विद्यापति के बारे में इतिहास के दस्तावेजों में शायद ज्यादा कुछ हो, लेकिन हर सामाजिक अवसर पर उनके गीतों को सुना जा सकता है, उनके गीत महिलाओं की सुरीली आवाज में जिंदा हैं। तो क्या विद्यापति का इतिहास लिखने के लिए इन स्रोतों को नहीं उचित मान लेना चाहिए। लेकिन अगर इतिहास लेखन को यह स्वतंत्रता दी जाए तो कई कठिनाइयां भी हो सकती हैं। फिर भारत का कोई हिंदू इतिहास होगा और कोई मुसलिम या दलित इतिहास होगा। फिर क्या इतिहास को किसी बौद्धिक विमर्श के रूप में माना जाना संभव हो पाएगा। समस्या यह है कि जहां एक तरफ इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक विधा के रूप में मानने के अपने खतरे हैं, तो दूसरी तरफ शुद्ध रूप से एक व्यक्तिपरक कथा के रूप में मानने के भी कई खतरे हैं। अब प्रश्न है कि इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है।
सोचने की बात यह है कि क्या यह संभव है कि इतिहास को अस्मिता की राजनीति से अलग कर सत्य की खोज तक सीमित रखा जाए। अगर अस्मिता की राजनीति से इसे अलग कर दिया जाए तो शायद यह मान लेना संभव हो पाएगा कि इतिहास का एक मेटानेरेटिव भी है और एक लोककथा भी। दोनों का अपना महत्त्व है। यह तभी हो पाएगा जब हम मेटानेरेटिव को भी लगातार सुधारते जाएं। जनश्रुतियों और लोकसाहित्य को इतिहास के स्रोतों में जगह दें। लेकिन इतिहास में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ऐसा मान लें। अगर अस्मिता की राजनीति से इसे अलग कर लें तो शायद इतिहास की गलतियों को स्वीकार कर आगे सुधार की बात हो सकती है। इतिहास की घटनाओं से वर्तमान की राजनीति को तय करना खतरनाक हो सकता है। शायद इसलिए गांधी ने कहा था कि वह देश भाग्यशाली है, जिसका कोई इतिहास नहीं है।
इस बात को समझने के लिए राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को देख सकते हैं। इस विवाद में इतिहासकारों ने हमारा ध्यान इस घटना की ऐतिहासिकता की ओर केंद्रित कर दिया था। जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी एक राजा के समय उसके धर्म से इतर के धर्म को मानने वालों के लिए कठिन समय रहा हो और उनके धार्मिक स्थलों को हानि पहुंचाई गई हो। फिर किसी एक खास मामले में अगर इतिहासकारों को इस प्रयास का फायदा मिल भी जाए तो दूसरे मामलों में इसका क्या फायदा हो सकता है। इसलिए इससे बेहतर शायद एक राजनीतिक तर्क होता, जिसमें सवाल इतिहास की सत्यता पर नहीं, बल्कि एक जनतांत्रिक तर्क के आधार पर किया जाता। इतिहास की घटनाओं को सही करने की राजनीतिक पहल जनतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है।
कुल मिलाकर इतना समझना कठिन नहीं है कि अगर हम इतिहास के उभरते दृष्टिकोणों को नकारना चाहें तो संभव नहीं है, लेकिन इस चक्कर में इतिहास के मेटानेरेटिव देने की क्षमता को नकारना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि एक के आभाव में इतिहास अधूरा है और दूसरे के आभाव में इतिहास बेकार है। इन दोनों के बीच सामंजस्य तभी संभव है जब इतिहास को अस्मिता की राजनीति और वैज्ञानिकता के आग्रह से भी मुक्त कर सकें।