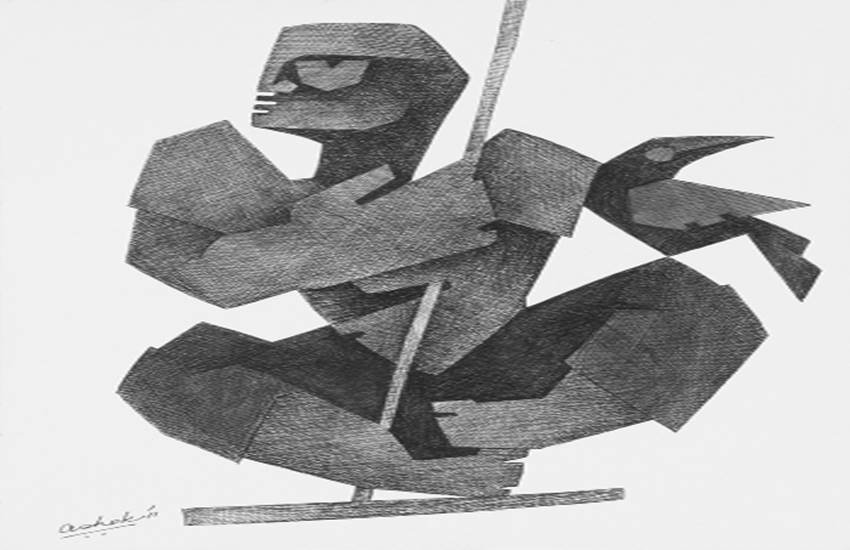आज सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का असर साहित्यिक वातावरण पर भी पड़ रहा है। वैसे हमेशा की तरह वर्तमान समय में भी साहित्यकारों से यही उम्मीद की जाती है कि समाज और राजनीति की विकृतियों से प्रभावित हुए बिना वे एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करेंगे। प्रेमचंद ने जो बात साहित्य के लिए कही थी कि वह राजनीति का अनुगामी न होकर उसका पथप्रदर्शक है, वह साहित्यकारों के लिए भी सच है। साहित्यकार को राजनीति और समाज की प्रचलित धारा में समायोजित होने की जगह उसकी बुराइयों के प्रति अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। साहित्यकार की प्रतिबद्धता किसी भी तरह की सामाजिक या राजनीतिक सत्ता के प्रति न होकर आम जन के प्रति होनी चाहिए। तभी वह हर तरह की सत्ता को आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की निगाह से देख सकता है।
पर लगता है कि आज के समय में ये सब बातें अप्रासंगिक हो चुकी हैं। साहित्य और साहित्यकार दोनों का स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा है। साहित्य में आ रही नई पीढ़ी को साहित्य की परंपरा और विरासत से बहुत मतलब नहीं है। उसके लिए साहित्य साध्य नहीं, साधन है। साहित्य उनके लिए अस्तित्व की अनिवार्यता न होकर एक शौक है। साहित्य-कर्म का साध्य की जगह साधन और अनिवार्यता की जगह शौक में बदल जाना बिल्कुल नई परिघटना है। हर नया लेखक इस परिघटना को चुनौती देने की जगह न सिर्फ इसे स्वीकार कर रहा, बल्कि अपने पूर्ववर्ती लेखकों की तुलना में बीस ही साबित हो रहा है।
इस प्रवृत्ति का सबसे खतरनाक परिणाम यह हो रहा है कि नए लेखकों में साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता क्रमश: क्षीण होती जा रही है। साहित्य मात्र के प्रति गरिमा का बोध समाप्त हो रहा है। साहित्य के प्रति गहरे सरोकार न होने के कारण साहित्य पर मंडरा रहे खतरों से भी उन्हें कोई बेचैनी महसूस नहीं होती। यह अकारण नहीं है कि पिछले कुछ सालों से हिंदी में साहित्य के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़े बुनियादी सवालों पर न तो कोई बहस हुई है और न ही कोई सार्थक आयोजन। यह बात तब और रेखांकित करने वाली हो जाती है, जब इधर के वर्षों में साहित्य का संकट बहुत बढ़ा है और युवा साहित्यकारों की संख्या पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। कितनी विडंबनात्मक स्थिति है कि साहित्य पर संकट बढ़ रहा है और साहित्य के पक्ष में लड़ने वाली आवाजें खत्म हो रही हैं।
हिंदी में ऐसे नए लेखकों की संख्या बढ़ रही है, जो साहित्य शौकिया रचते हैं। साहित्य का मतलब उनके लिए सिर्फ अपना लेखन होता है। उन्हें किसी पुराने या अपने समकालीन लेखक की रचनाओं में कोई दिलचस्पी नही होती। वे यह मान कर चलते हैं कि हिंदी समाज उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बाध्य है। वे चाहते हैं कि उनकी रचनाओं को सब पढ़ें, पर वे किसी की रचना को पढ़ना जरूरी नहीं समझते। युवा लेखक प्राय: यह शिकायत करते हैं कि पुरानी पीढ़ी के लेखक उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ते। पर बड़ा सवाल यह है कि नया लेखक किस नए लेखक की रचना को पढ़ता है?
साहित्य के क्षेत्र में लोकतंत्र परम आवश्यक है। साहित्यकार बाहरी दुनिया में तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष करता है, पर उसने साहित्य की दुनिया से लोकतंत्र को लगभग बेदखल कर दिया है। साहित्य की दुनिया शायद सबसे अलोकतांत्रिक है। सहिष्णुता के लिए संघर्ष करने वाले स्वयं कितने सहिष्णु हैं, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। साहित्यकार बाहर की दुनिया में जिन चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, अपनी दुनिया में उन्हीं के भीतर आकंठ डूबा रहता है। कभी विचारधारा, तो कभी क्षेत्र, कभी जाति तो कभी कुछ के नाम पर यहां बार-बार लोकतंत्र की हत्या होती है। यहां फैसले योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि निजी संबंधों के आधार पर किए जाते हैं। साहित्यकारों के अपने-अपने गिरोह और गुट हैं। ऐसे माहौल में जब कोई युवा लेखक आता है, तो उसका विचलन स्वाभाविक है। इसलिए सारा दोष नए लेखकों पर डाल देना उचित नहीं है। उनका दोष यह है कि वे इस माहौल को बदलने की जगह उसमें समायोजित हो जाना अधिक पसंद करते हैं।
तो, बुनियादी सवाल है कि आज का युवा लेखक साहित्य की भीतरी बुराइयों के प्रति विद्रोह करने की जगह उसमें शामिल क्यों हो जाता है? इसका मूल कारण यह है कि साहित्य के क्षेत्र में उसे कोई आदर्श दिखाई नहीं देता, जिसके आचरण से वह प्रेरणा ग्रहण कर सके। साहित्य की बड़ी शख्सियतें इन बुराइयों से ग्रस्त हैं। यहां जो लोग महत्त्वपूर्ण बन रहे हैं, वे भी जोड़-तोड़, जुगाड़ और तरह-तरह की दुरभिसंधियों की बदौलत ही बन रहे हैं। साहित्य में जिसकी भी थोड़ी-बहुत हैसियत है, उसमें साहित्येतर साधनों की बड़ी भूमिका है। जोड़-तोड़, जुगाड़, चमचागिरी, सेवाभाव, आज्ञाकारिता, अंधश्रद्धा आदि साहित्य में सफलता पाने के रास्ते हैं। लोग इसी रास्ते सफल होते हैं और दूसरों से यही चाहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नया-नया प्रवेश करने वाला युवा जब देखता है कि ईमानदार और नैतिक लेखकों की कोई कद्र नहीं है, जो कुछ भी बनाने या बिगाड़ने की हैसियत में नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है, तब वह युवा अपनी रही-सही नैतिकता और मूल्यबोध को भी तिलांजलि देकर पूरी तरह सफलता के खेल में शामिल हो जाता है। यानी आज जो युवा कर रहे हैं वह उन्होंने बुजुर्गों से ही सीखा है। यह बात अलग है कि युवाओं ने इस खेल में उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है।
आज का नया लेखक यह बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि साहित्य में सफल होने के सारे रास्ते साहित्येतर हैं। इसलिए उसकी सारी कोशिशें साहित्येतर रास्तों को साधने में होती हैं। उन रास्तों पर चलते हुए उसका अधीर और अवसरवादी हो जाना स्वाभाविक है। वह सब कुछ जल्दी पा लेना चाहता है। आज साहित्य की दुनिया में पहले से चले आ रहे अवसरवाद को युवाओं ने चरम पर पहुंच दिया है। आज न कोई किसी के विरोध में है, न पक्ष में। सभी अवसर की फिराक में रहते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सहमति और असहमति भी मुद्दा आधारित न होकर व्यक्तिगत लाभ-लोभ आधारित हो गया है।
पहले सहमति और असहमति का एक मुख्य आधार विचारधारा होती थी। इसके चलते लेखकों को एक ‘स्टैंड’ लेना पड़ता था। छोटे-मोटे अपवादों को छोड़ दें तो उनकी पहचान स्पष्ट थी। आज के अधिकतर नए लेखकों की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा न होने से किसी मुद्दे पर उनका कोई स्पष्ट ‘स्टैंड’ भी नहीं होता। यह मानते हुए भी कि विचारधारा आधारित गुटबाजी ने हिंदी साहित्य का बहुत नुकसान किया है, फिर भी ऐसा लगता है कि आज के माहौल से वह विचारधारा आधारित बंटवारा कहीं अधिक ठीक था। कम से कम ऐसी अराजकता और अवसरवाद तब नहीं था। दरअसल, किसी खास विचारधारा से मुक्त नई पीढ़ी से उम्मीद थी कि वह विचारधारा आधारित साहित्यिक विभाजन और मूल्यांकन की खतरनाक परिपाटी से हिंदी साहित्य को निकाल कर सृजन और आचरण का एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगी। पर, यह उम्मीद अब लगभग समाप्त हो चुकी है। साहित्य का रिश्ता विचारधारा से न होना सृजन के लिए अच्छा ही है, पर विचारों से तो उसका रिश्ता होना ही चाहिए। समस्या यह है कि साहित्य के क्षेत्र में आ रहे नए रचनाकार विचारधारा से मुक्त होते-होते विचारों से भी मुक्त होने लगे हैं। वे विचारधारा विहीन ही नहीं, विचारविहीन भी होते जा रहे हैं। यह विचारहीनता ही नई पीढ़ी की समस्त बुराइयों की जड़ में है।