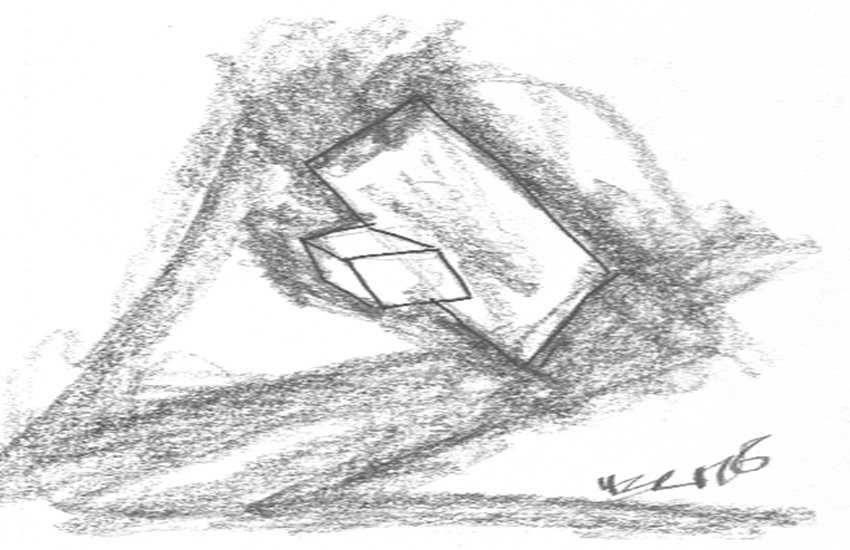हर रचनाकार अपनी रचनात्मकता के स्रोत तक जाने की कोशिश करता होगा? यह सवाल हर विधा में काम कर रहे रचनाकारों के लिए है। विन्सेंट वॉन गॉग मानते थे कि हर पेंटिंग में जीवन होता है और वह जीवन कलाकार की आत्मा ही उसे प्रदान करती है। महान संगीतकार बेटोफेन के बारे में एक मशहूर लेखक ने लिखा कि वे तो इतने बधिर हैं कि खुद को चित्रकार समझ बैठते हैं! रचनात्मकता के स्रोत में थोड़ी गहराई में उतरने पर दिखता है कि विधाएं भले अलग-अलग हों, कोई स्रोत है जो हर कलाकार के मन-मस्तिष्क से होकर प्रवाहित होता है, और वह अक्सर एक ही स्रोत होता है, अलग-अलग वाह्य अभिव्यक्तियों के बावजूद। किशोरी अमोनकर जब गाती थीं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता था कि कौन है जो उनके जरिए, उन्हें गा रहा है! अक्सर कोई रचनात्मक ऊर्जा कलाकार का एक माध्यम के रूप में मानो इस्तेमाल करती प्रतीत होती है। पर ऐसा कहने में रचनात्मकता को एक रहस्यमयी प्रक्रिया बनाने के खतरे हैं। उस पर अनावश्यक और बोझिल आध्यात्मिकता की खरोंचे भी पड़ सकती हैं।
विक्टर ह्यूगो कहते थे कि मैं तभी लिखता हूं जब प्रेरणा मिलती है, पर मैंने यह तय किया हुआ है कि किसी भी हाल में मैं रोज सुबह नौ बजे प्रेरित होता रहूं! टीएस एलियट ने रचनात्मकता के बारे में एक बड़ी विवादस्पद बात कह डाली कि अपरिपक्व कवि नकल करते हैं; महान कवि तो चोरी करते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा: ‘खराब कवि जो भी उठाते हैं, उसे भद्दा बना कर छोड़ देते हैं, जबकि उम्दा कवि उसे बेहतर बना डालता है या कम से कम कुछ अलग तो बना ही देता है।’ हर लेखक के अपने अनुभव होते हैं, जिन्हें वह अपने संस्कारों के आलोक में देखता-समझता है। उन अनुभवों के साथ उसका गहरा तादात्म्य भी स्थापित हो जाता है। उन्हीं अनुभवों को वह अपनी रचनाओं में व्यक्त किए चलता है। ऐसा अचेतन या अवचेतन स्तर पर भी होता है, क्योंकि लेखक के लिए खुद यह जान पाना मुश्किल हो सकता है कि कौन-सी रचना अतीत में हुए किस अनुभव से उपजी है। अक्सर लेखक इस बारे में कोई प्रश्न उठाने में खतरा भी महसूस कर सकता है कि वे अनुभव वास्तविक हैं या काल्पनिक, छिछले हैं या गहरे; या फिर मूलभूत रूप से किस मानसिक उद्वेलन से उपजे हैं। ये बातें उठाने से लेखन का प्रवाह रुक सकता है। अक्सर इस तरह के मूलभूत सवालों में लेखक खतरा महसूस करता है। लेखक या कवि किसी गहरी या अंतिम अंतर्दृष्टि की खोज में नहीं रहता, अपनी आंशिक अंतर्दृष्टि को साझा करने की एक व्याकुलता होती है, उसमें और अपनी ‘खोज’ पर प्रश्न उठाने से उसकी अभिव्यक्ति बाधित होगी, इस तथ्य से वह अच्छी तरह परिचित होता है। प्रश्न की आंच में बहुधा कई निष्कर्ष मुरझा सकते हैं, जबकि लेखक उन निष्कर्षों को पूरे विश्वास के साथ व्यक्त करना चाहता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो लेखक की संस्कारबद्धता उसके लिखने का स्रोत हो सकती है।
भावनाएं या विचार भी रचनाकार को लेखन की दिशा में ले जाते हैं। पर विचार का महिमामंडन न करके उनकी संरचना को खंगालने की कोशिश की जानी चाहिए। गौरतलब है कि विचार भी खास किस्म के संस्कार से ही उपजते हैं। अक्सर वे स्मृतियों के प्रत्युत्तर के रूप में व्यक्त होते हैं। लेखक स्मृतियों से अपनी ऊर्जा लेता है। सुखद स्मृतियों से भी और दुखद यादों से भी। इन्हें लेकर अलग-अलग रस निर्मित करता है। क्या मृत स्मृतियां उत्कृष्ट, जीवंत लेखन को जन्म दे सकती हैं? इस प्रश्न को लेखक दर्शन और मनोविज्ञान के पाले में धकेल देता है। हाइकू के जनक बाशो स्मृतियों पर निर्भर नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण को उकेरते हैं। हां, गहरी ऊब और द्वंद्व भी लेखन या किसी अन्य तरह की सृजनशीलता की ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं। अक्सर कलाकार के जीवन और लेखन में भयंकर द्वंद्व देखा जा सकता है। वार ऐंड पीस का संत लेखक टॉलस्टॉय अपनी पत्नी के साथ भयंकर कलह में जीता रहा। अपने मशहूर उपन्यास अन्ना कैरेनिना के प्रारंभ में ही उन्होंने दुखी परिवार की दशा के बारे में लिखा है। दरअसल, द्वंद्व एक तरह की ऊर्जा पैदा करता है और किसी सृजनशील व्यक्ति में यह ऊर्जा सौंदर्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से व्यक्त भी हो सकती है, पर उसके पीछे छिपा बैठा, बिलबिलाता, तड़पता रचनाकार दुनिया की नजर से बचा रह जाता है। निदा फाजली इसे बखूबी कहते हैं: ‘मेरी आवाज तो परदा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए।’ पर खामोशी के पीछे छिपे जख्मों को कौन देख पाता है! शब्दों के सौंदर्य में खोए पाठक और दर्शक बस वाहवाही में मगन हो जाते हैं।
प्रतिष्ठा की कामना, खुद को बाकियों से अलग दिखाने की इच्छा भी लेखन के लिए प्रेरित कर सकती है। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा लेखन या किसी और कला की ओर ले जा सकती है। और व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित लेखक किसी राजनेता की तरह भयंकर परिश्रमी और उर्वर भी हो सकता है। अनवरत चलने वाले विचार के बीच का पल भर का अंतराल सृजनशीलता का एक समृद्ध स्रोत होता है। यह अंतराल बहुत कीमती होता है और संभवत: यही सृजनात्मक संवेग को जन्म देता है; उसके बाद इसकी अभिव्यक्ति तो एक तरह से यंत्रवत होती है, बाहरी माध्यमों का सहारा लेती है। नंदलाल बोस ने इस यांत्रिकता से बचने के लिए रंग भी खुद बनाए। तो यह प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या अनवरत चलने वाले विचारों में कोई सृजनशीलता होती है, या फिर उनके खुद-ब-खुद थम जाने से उपजी खामोशी सृजनशील होती है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्किमिडीज की अंतर्दृष्टि, जो उनके दिमाग में नहाते वक्त कौंधी थी, एक अलग तरह की रचनात्मकता की तरफ इशारा करती है, जिसकी जमीन विचारों के निरंतर प्रवाह से हट कर है। जो वैज्ञानिक निर्वस्त्र होकर अपनी खोज की घोषणा करते हुए सड़कों पर दौड़ लगा सकता है, वह परंपरागत विचारों की गिरफ्त से तो जरूर ही बाहर रहा होगा। और भी बहुत कुछ हो सकता है। मन की हर बारीक से बारीक हरकत और उसकी अभिव्यक्ति पर आंखें टिकाए रखना आसान नहीं होता। सृजनात्मकता अपने आप में ही बड़ी कोमल वस्तु है, इसकी पीड़ा को समझना, इसके मार्ग पर चलना, इसे संजोए रखना, बुझने से रोकना, यह सब कुछ एक चुनौती जैसा है, खासकर आज के माहौल में जहां हर स्तर पर एक उठा-पटक मची हुई है। सही अर्थ में एक गहरे सृजनशील व्यक्ति के लिए आज का समय तरह-तरह की अनिश्चितताओं और संदेहों से भरा हुआ है। फिर भी बात यही सच है कि जो रचेगा, आखिर में वही बचेगा।