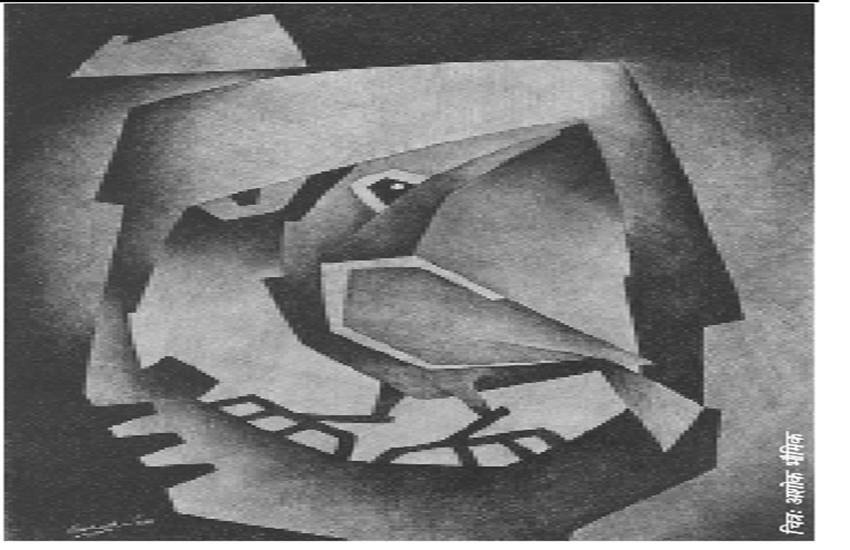वादों में वाद, परिवारवाद। कोई भी इससे परे नहीं है। कहा जाता है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, वकील का बेटा/ बेटी वकील हो सकता है, तो फिर राजनीति में परिवारवाद क्यों नहीं चल सकता? बात एक तरह से सही है, पर पहले हमें इस बात का फैसला करना होगा कि डॉक्टरी या वकालत की तरह राजनीति भी एक पेशा, प्रोफेशन है कि नहीं। हमारे शहर में एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे। दूर-दूर से लोग उनसे इलाज कराने आते थे। डॉक्टर साहब बहुत सरल व्यक्ति थे, उनके जेहन में लोकसेवा के अलावा कुछ नहीं था। खुले दिल से मरीजों की सेवा करते थे, पर फिर भी उनके पास अटूट धन जमा हो गया था। उनका बेटा अपने पिता की शोहरत और संपन्नता में पला-बढ़ा और अपने को उनकी ‘गद्दी’ का दावेदार समझने लगा। डॉक्टरी करके उसने दवाखाने पर बैठना शुरू कर दिया, पर पिता की मृत्यु के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं चली। मरीज उसको पेशेवर डॉक्टर कहने लगे, जिसकी नीयत सेवा से हट कर लाभांश पर टिक गई थी। उसके लिए मरीज सिर्फ बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदने और सामाजिक दबदबा बनाने का जरिया था।
वास्तव में हर पेशे में परिवारवाद हावी है। सब अपनी ‘गद्दी’ अपने ही घर के बच्चे के लिए छोड़ जाना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति की जड़ मनुवादी जातिवाद में निहित है। जातिप्रथा का मकसद पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही कार्य करवाने का था- ब्राह्मण पढ़ाई-लिखाई करेंगे, क्षत्रिय शस्त्र धारण करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे आदि। इसी आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था बनी और गद्दी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही। पर यह सब तब तक ठीक था, जब तक सामाजिक गतिशीलता (सोशल मोबिलिटी) नहीं थी। लगभग सौ साल के आधुनिकरण की वजह से हमारा समाज मूलभूत रूप से बदल चुका है। हर व्यक्ति, परिवार और समाज आज किसी भी पेशे में आसानी से आ-जा सकता है। इस परिस्थिति के बावजूद गद्दी की मानसिकता अब भी व्याप्त है। जो जिस जगह बैठ गया, वह अपनी औलाद को उसका पूरा कब्जा देकर ही उठना चाहता है। यह बात हर पेशे पर लागू है।
पर क्या राजनीति को भी हम पेशा मान लें? अमूमन हम राजनीति को पेशा नहीं मानते। उसको समाज सेवा से जोड़ कर देखते हैं और राजनेता को हम सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, जिसका जीवन मूल्यों, विचारधारा, संघर्ष और समाज की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। सत्ता, शोहरत और दौलत उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि सबसे बड़े लक्ष्य- जन उत्थान की प्राप्ति- का जरिया मात्र है। हम मानते हैं कि वह सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है, बल्कि हमारे-आपके सुख-दुख बांटने के लिए निस्वार्थ भाव से इसमें जुटा है। आजादी की लड़ाई से निकले तमाम महानायकों ने अपने चरित्र और कार्य से नेताओं के प्रति हमारी सोच को बल दिया और हम राजनीति को समाज सेवा ही मानने लगे। पर जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था परिपक्व होने लगी और नई चुनौतियां इस व्यस्था से सामने आने लगीं, सत्ता सेवा पर हावी होने लगी। आज स्थति यह है कि राजनेता बिना सत्ता के अपने को सेवा के लिए अक्षम मानते हैं।
इस भाव के चलते अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होती है। वाजिब है कि सत्ता पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जरूरी है। आडंबर भी जरूरी है और ताकत की नुमाइश भी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए धन अर्जित करना अनिवार्य है। धन के जरिए ही राजनीतिक समर्थकों की फौज खड़ी की जा सकती है और गुंडों को पाला जा सकता है। राजनेता इसीलिए भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते जा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और सत्ता पाने के बाद उसका पूरी तरह से दोहन करते हैं।
राजनीतिक मठाधीशी आज की राजनीति का सच है। अपनी ‘गद्दी’ बनाना और फिर उसे अगली पीढ़ी के लिए कायम रखना ही इसका अंतिम लक्ष्य है। सेवा भाव और विचारधारा से इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति एक फ्री मार्केट प्लेस बन चुकी है। जिसके पास गहरी जेब है और पर्याप्त बाहुबल है वह सत्ता के लिए समर में उतर सकता है। उसको अपने मार्केट को समझ कर बल और धन का प्रचुर निवेश करना है और फिर सत्ता से उत्पन्न लाभांश की फसल काटनी है। पेशेवर राजनीति की यह एक सरल-सी मार्केट इकोनॉमिक्स है। जैसा बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों में होता है, वैसा ही राजनीति में होता है। पिता स्टार्ट-अप लांच करता है और कंपनी को एक ऊंचाई तक ले जाता है। उसके रहते ही औलाद कंपनी से जुड़ जाती है और फिर टेक ओवर कर लेती है। पिता की बनाई गद्दी संतान को काबिलियत पर नहीं, बल्कि विरासत में मिल जाती है।
राजनीति में परिवारवाद असल में सार्वजनिक जीवन के निजीकरण का जबर्दस्त उदाहरण है। यह हमारे वर्तमान का सच है और हमें इस सच को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। पर जैसा हमारे शहर के डॉक्टर साहब की औलाद के साथ हुआ वैसा ही पेशेवर राजनीति में भी होता है। उनके बेटे के पास गद्दी और दौलत तो है, पर अपने पिता-सी शहाफत नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे कई खानदानी राजनीतिक पूत मिल जाएंगे, जो सपूत बनने में अक्षम हैं। परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड के बाजार की उठा-पटक में हम और आपकी वही भूमिका है, जो उपभोक्तावादी समाज में एक ग्राहक की होती है। उसे बाजार का राजा तो जरूर कहा जाता है, पर वास्तव में वह एक लाचार बंदी है। बाजार जो भी अपनी शर्तों पर उसके सामने परोस देगा, उसको वह ग्रहण करना ही पड़ेगा। उसको अपनी इच्छा बनानी ही पड़ेगी। ऐसा वाणिज्य ही राजनीति है और ऐसी राजनीति वाणिज्य है। परिवारवाद इस वाणिज्य के लिए जरूरी है।