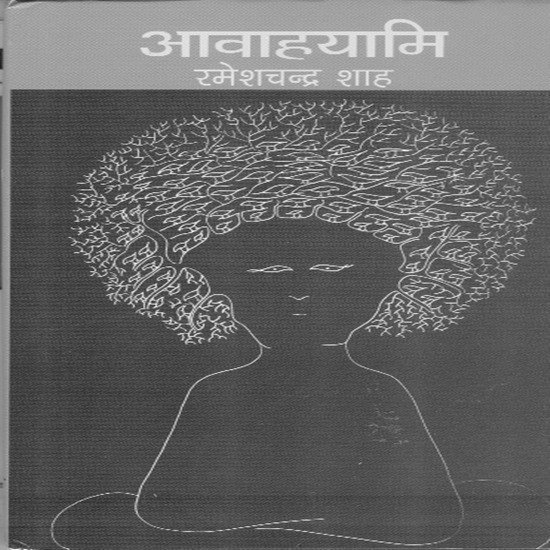वरिष्ठ रचनाकार रमेशचंद्र शाह की पुस्तक आवाहयामि के संस्मरणों में आजादी के बाद के हिंदी साहित्य का पूरा युग समाया हुआ है। अज्ञेय, जैनेंद्र कुमार, मुक्तिबोध, बालकृष्ण राव, विजयदेवनारायण साही, निर्मल वर्मा आदि के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलुओं को इन संस्मरणों के माध्यम से जानना खासा दिलचस्प अनुभव है। जिन लेखकों से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, उनके पत्रों को अपनी छोटी-बड़ी टिप्पणी के साथ उन्होंने इस पुस्तक में शामिल कर लिया है। इस लिहाज से यह पुस्तक संस्मरण और पत्रों का मिश्रण है।
अज्ञेय पर लिखे संस्मरण में वे बताते हैं कि सत्तर के दशक में अज्ञेय के संपादन में निकले ‘नया प्रतीक’ पर ‘पूर्वग्रह’ के पहले ही अंक में ‘फिर बैतलवा डाल पर’ शीर्षक से कड़ा प्रहार किया गया। अज्ञेय ने पत्रिका के सलाहकारों में शाह को भी शामिल किया था। ‘नया प्रातिक’ के सलाहकारों में शाह का नाम देख कर अशोक वाजपेयी अत्यधिक क्षुब्ध हुए थे। उन्होंने शाह से यहां तक कहा कि ‘इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।’ शाह लिखते हैं: ‘इतिहास की यह अवधारणा मेरे लिए नई थी। सहयोगी या सलाहकार तो मैं अशोकजी का भी था ही। ‘पहचान सीरीज’ में उन्होंने मेरी भी कविताओं की पुस्तिका प्रकाशित की थी।’ अज्ञेय और अशोक वाजपेयी के बीच विरोध एकतरफा नहीं था, बल्कि दोनों तरफ से था। शाह की रचनाएं तो ‘नया प्रतीक’ में छपती थीं, पर आलोचनात्मक लेख ‘पूर्वग्रह’ में। एक बार अज्ञेय ने उनसे उलाहना के स्वर में कहा कि आप सलाह तो मुझे देते हैं और लेख ऐसी पत्रिकाओं को, जिनके कारण साहित्यिक पत्रकारिता पर सबसे अधिक संकट आता है।
हिंदी में जिस एक साहित्यकार को सबसे अधिक हमले झेलने पड़े, वे अज्ञेय थे। उनके व्यक्तित्व और साहित्य-कर्म को लेकर तरह-तरह के अमर्यादित दुष्प्रचार किए गए। उन्हें पूंजीपतियों का दलाल, सीआइए का एजेंट, जनता का दुश्मन और न जाने क्या-क्या कहा गया। जीवनपर्यंत वे संगठित हमले झेलते रहे। बावजूद इसके, उन्होंने अपने लेखन और जीवन में उच्च मानदंड को कायम रखा। मर्यादा और संयम को कभी नहीं खोया। शाह ने सही लक्षित किया है कि वात्स्यायनजी जीवन और समाज से मिली सारी कड़वाहटों के बावजूद कटु नहीं हो सके, बल्कि उत्तरोत्तर सौम्य और प्रशांतात्मा होते गए। अज्ञेय की छवि प्राय: यही थी कि वे असंवादधर्मी और एकांतप्रिय व्यक्ति हैं। लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर इसका खंडन किया है। वे लिखते हैं, ‘जिस अज्ञेय को मैंने पंद्रह वर्षों के निकट सान्निध्य से जाना, जिन्हें वत्सल निधि द्वारा आयोजित लेखक-शिविरों में या सांस्कृतिक यात्राओं में सक्रिय देखा, उनका कहीं कोई मेल इस बहुप्रचारित छवि से बैठता नहीं दिखा।’
जैनेंद्र पर लिखे संस्मरण से पता चलता है कि अज्ञेय अपने पहले काव्यसंग्रह ‘भग्नदूत’ की भूमिका जयशंकर प्रसाद से लिखवाना चाहते थे। अपनी इसके लिए उन्होंने जैनेंद्रजी को इस उम्मीद से माध्यम बनाया कि निकट संबंध के कारण प्रसादजी उनकी बात नहीं टालेंगे। पर प्रसादजी यह कह कर टाल गए कि ‘मैंने कभी किसी की भूमिका नहीं लिखी।’ लेखक को लगता है कि प्रसाद द्वारा अपनी इस उपेक्षा से अज्ञेय बहुत मर्माहत हुए होंगे। उन्होंने आगे प्रसाद को ‘विश्वविद्यालय का कवि’ घोषित करके एक तरह से इसका बदला लिया।
जैनेंद्र के दो पक्ष हैं। एक उनका रचनाकार रूप और दूसरा चिंतक रूप। अज्ञेय जैनेंद्र के चिंतक रूप को महत्त्वपूर्ण नहीं मानते थे। उन्होंने उनके चिंतन पक्ष की निर्मम आलोचना की है। एक दिलचस्प बात यह है कि जैनेंद्र के चिंतक रूप के बारे में मुक्तिबोध की भी वही राय थी, जो अज्ञेय की थी। मुक्तिबोध ने एक बार जैनेंद्र की चर्चा छिड़ने पर लेखक से कहा था, ‘जहां तक सृजनात्मक प्रतिभा का प्रश्न है, जैनेंद्र को मैं वात्स्यायनजी से भी श्रेष्ठतर सर्जक मानता हूं। पर विचारक रूप उनका मुझे उतना आकर्षित नहीं करता। चिंतन उनका तर्काश्रित और तर्कसंगत होने के बजाय मनमाना इच्छित चिंतन लगता है। सोफिस्ट्री।’ उनकी तर्क प्रणाली पर सोफिस्ट्री का आरोप अज्ञेय ने भी लगाया है।
वीरेंद्रकुमार जैन पर लिखे संस्मरण में लेखक ने बताया है कि उनके ही घर पर उसने प्रेमचंद का अंगरेजी में लिखा वह प्रसिद्ध लेख पढ़ा था, जिसमें प्रेमचंद ने जैनेंद्र को ‘दि मोस्ट अंडरस्टैंडिंग फिक्शन राइटर इन हिंदी’ तथा अज्ञेय और वीरेंद्रकुमार जैन को ‘सर्वाधिक संभावनाशील कथाकारों’ के रूप में रेखांकित किया था। वीरेंद्रकुमार जैन और मुक्तिबोध की कविताओं में बहुत समानता थी। वीरेंद्रकुमार जैन को मार्क्सवाद से कोई समस्या नहीं थी, पर उन्हें अरविंद दर्शन अधिक रास आता था। शाह लिखते हैं, ‘अब समझ में आता है कि हिंदी की तत्कालीन साहित्यिक राजनीति को देखते हुए यह सर्वथा स्वाभाविक घटना थी।… जिस प्रतिष्ठानी मशीनरी ने ‘ग्राम्या’ और ‘युगवाणी’ के कवि की भरपूर आरती उतार चुकने के बाद, उस कवि में आरविंदी यूटोपिया के प्रति रुझान देखते ही उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका, वही प्रतिष्ठानी मशीनरी अब श्रीअरविंद के चिंतन को, मार्क्स की तुलना में विशुद्ध स्वदेशी यूटोपिया को इस कदर गंभीरता से अपना लेने वाले नए दौर के कवि वीरेंद्रकुमार जैन को कैसे इतनी आसानी से बख्श देती।’
विजयदेवनारायण साही को लेखक ने बार-बार गुरुदेव कह कर संबोधित किया है। उन्होंने एक बार जब साही से यह जिज्ञासा जाहिर की कि आखिर क्यों लोहिया की अंगरेजी नेहरू की अंगरेजी की तुलना में बड़ी फीकी और बेस्वाद लगती है, जबकि उनकी हिंदी इतनी जानदार होती है? साही ने बताया कि डॉ. साहब राजी ही नहीं होते थे हिंदी में लिखने को। हम लोगों ने पीछे पड़ कर उकसाया कि आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखिए। बस जादू हो गया। हिंदी भी अपना तेज तभी प्रकट करती है, जब कोई लोहिया उसे छेड़े। इस तरह की न जाने कितनी दिलचस्प बातें और जानकारियां इन संस्मरणों में भरी पड़ी हैं।
कई जगह ऐसा लगता है कि लेखक में आत्ममुग्धता हावी हो रही है। कई बार यह भी लगता है कि लेखक संस्मरण का उपयोग अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए कर रहा है। पर, इन मानवीय कमजोरियों के बावजूद इन संस्मरणों से गुजरना आजादी के बाद के हिंदी साहित्य के इतिहास से गुजरने जैसा है।
दिनेश कुमार
आवाहयामि: रमेशचंद्र शाह; किताबघर प्रकाशन, 4855-56/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 400 रुपए।