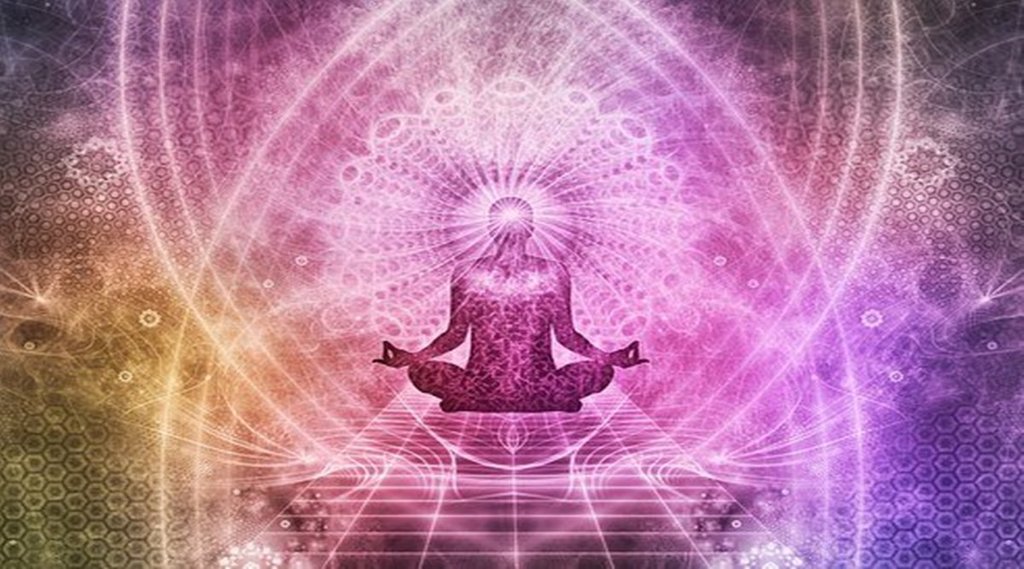स्वयं की खोज तो सभी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से। परमात्मा के असीम प्रेम की एक बूंद मानव में पाई जाती है, जिसके कारण हम उनसे जुड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसका लोप हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं। सांसारिक बंधनों में आनंद ढूंढ़ते ही रह जाते हैं, परंतु क्षणिक ही खुशी पाते हैं। जब हम क्षणिक संबंधों, क्षणिक वस्तुओं को अपना जान कर उससे आनंद मनाते हैं, जब की हर पल साथ रहने वाला शरीर भी हमें अपना ही गुलाम बना देता है। हमारी इंद्रियां अपने आप से अलग कर देती हैं। यह इतनी सूक्ष्मता से करती हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता की हमने यह काम किया है?
आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तो सर्विदित है। जब इस संबंध में शंका या संशय, अविश्वास की स्थिति अधिक होती है, तभी दूरी बढ़ती जाती है और हम विभिन्न रूपों से अपने को सफल बनाने का निरर्थक प्रयास करते रहते हैं, जिसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। यह तो असंभव सा जान पड़ता है कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग पहचान बनाने की कोशिश करें तो कोई क्या करे?
जब हमें सत्य पता चलता है तो जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है व पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लग पाता। ऐसी स्थिति का हमें पहले ही ज्ञान हो जाए तो शायद हम अपने जीवन में पूर्ण आनंद की अनुभूति के अधिकारी बन सकते हैं। हमारा इहलोक तथा परलोक भी सुधर सकता है। अब प्रश्न उठता है की यह ज्ञान क्या हम अभी प्राप्त कर सकते हैं? हम अभी जान सकते हैं कि अंत समय में किसकी स्मृति होगी, हमारा भाव क्या होगा? हम फिर अपने भाव में अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। गीता के आठवें अध्याय श्लोक संख्या आठ में भी बताया गया है कि-
यंयंवापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित:।
अर्थात्- हे कुंतीपुत्र अर्जुन! यह मनुष्य अन्तकाल में जिस-जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस-उस को ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अध्यात्म बड़ा सरल है। फिर भी लोग मन में कई भ्रांतियां पाल लेते हैं कि कहीं आध्यात्मिक होने पर घर छोड़कर संन्यास लेना पड़ जाए, कहीं बैरागी न हो जाऊं, कहीं गृहस्थ धर्म न छोड़ दूं।
अध्यात्म तो हमें जीवन जीना सिखाता है। जैसे कोई भी मशीन खरीदने पर उसके साथ एक ‘मैन्युअल बुक’ आती है, ऐसे ही तन-मन को चलाने के लिए गीता आदि आध्यात्मिक शास्त्र और गुरु होते हैं जो हमें शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि अहंकार का प्रयोग करना सिखाते हैं। घर-गृहस्थी में तालमेल बिठाना सिखाते हैं, समाज में आदर्श के रूप में रहना सिखाते हैं, मन को सुलझाना सिखाते हैं। अत: धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी को आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए।
अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? जैसे आप कभी पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। पहाड़ियों पर मंजिल भी वैसी ही होती है, जैसा रास्ता। अध्यात्म की यात्रा भी ऐसी ही होती है जिसमें रास्ते का ही आनंद है। अध्यात्म कहता है कि बीतते हुए हर पल का आनंद लो, उस पल में रहो, हर पल को खुशी के साथ जियो। द्वंद्वों में संभाव में रहो क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी की अवस्था है। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। इसमें जीवन भर चलते रहना है।
यदि ‘अभी में’ रहकर उस आनंद भाव में नहीं आए तो कभी नहीं आ पाएंगे और जब भी आएंगे, उस समय भी अभी ही होगा। वैसे हम पूरा जीवन अभी-अभी की शृंखला में जीते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अभी-अभी-अभी में ही जीते हैं। फिर भी मन भूतकाल या भविष्य में ही बना रहता है और भूतकाल का दुख या भविष्य का डर या लालच में ही मन घूमता रहता है लेकिन जब हम अभी में आते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रारम्भ होता है। फिर हम इस अभी-अभी की कड़ी को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए मुक्ति अभी में है, भविष्य में नहीं। अत: यदि हम जीवन भर अभी को पकड़ कर रखें फिर हम जहां हैं जैसे हैं, वहीं आध्यात्मिक हो सकते हैं।