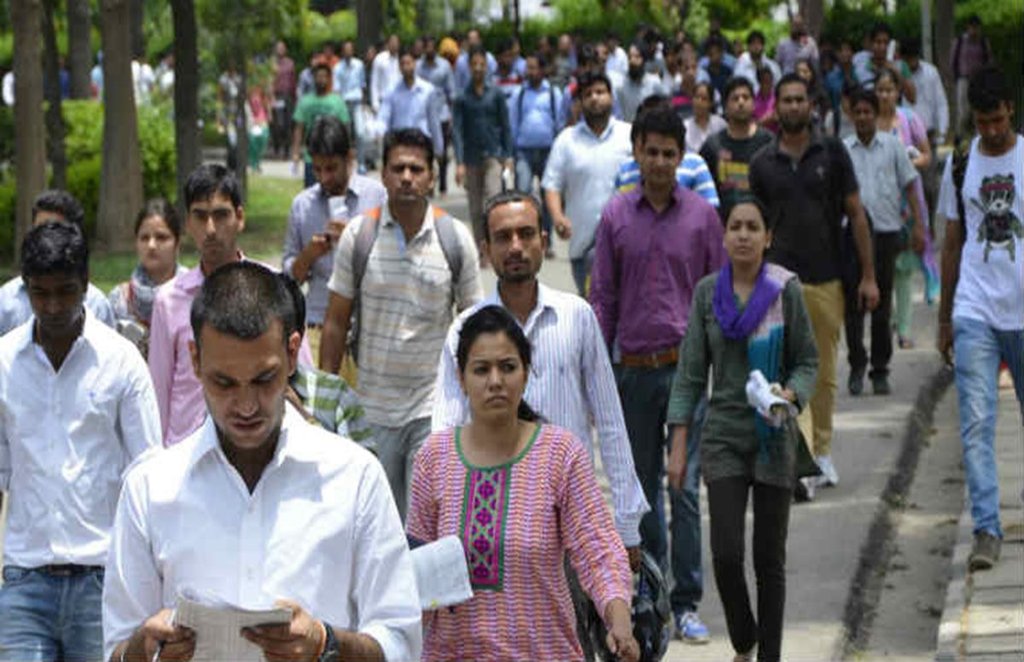अभिषेक कुमार सिंह
शहरीकरण को विकास का प्रतीक माना जाता है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों, महानगरों में निवास करता है। यह भी दावा किया जाता है कि आबादी के परिप्रेक्ष्य अब जितने भी परिवर्तन होने हैं, उनका सीधा असर हमारे शहरों की दशा-दिशा पर पड़ेगा। लेकिन ये शहर कैसे हैं और इनकी भावी रूपरेखा क्या है, इसे लेकर अभी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बन पाई है। हालांकि इस बीच देश में स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं का प्रचार जोरशोर से होता रहा है।
इस विरोधाभास पर हाल में एक नजर सुगमता के साथ रहन-सहन के उस सूचकांक (ईज आॅफ लिविंग इंडेक्स) के जरिए डाली गई है, जिसे हाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इस सूचकांक से पता चला है कि रहन-सहन के लिहाज से ज्यादातर उत्तर भारतीय शहरों में लापरवाही का आलम पसरा हुआ है, हालांकि दक्षिण भारतीय शहरों ने इस मामले में एक उम्मीद अवश्य जगाई है।
रहन-सहन से जुड़े इस सूचकांक में साफ-सफाई और अन्य सहूलिययों के आधार पर देश के शहरों की श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके दो अहम आधार रखे गए। एक वर्गीकरण में उन शहरों को शामिल किया गया, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है, जैसे दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, बंगलुरु, पुणे और अमदाबाद आदि। जबकि दूसरे में दस लाख से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया है।
स्वच्छता और सहूलियतों का पैमाना अपना कर यह तय करने की कोशिश की गई कि रहन-सहन के लिहाज से इन शहरों की गुणवत्ता किस कोटि की है। आकलन में पाया गया कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बंगलुरु, पुणे और अमदाबाद देश के सबसे अच्छे शहरों में हैं। जबकि दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इसमें एक रोचक आकलन भी सामने आया।
पता चला कि रहन-सहन के स्तर पर बड़े शहरों की सूची में बेंगलुरु शीर्ष पर भले ही हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में चेन्नई, कोयंबटूर और नवी मुंबई ज्यादा अच्छे शहर हैं। यहां अहम सवाल यह है कि आखिर शहरों की गुणवत्ता किन पैमानों से आंकी जा सकती है। तो इसका जवाब यह मिला कि सस्ते आवास, साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की उपलब्धता के अलावा सुरक्षा और मनोरंजन की सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच से पता चलता है कि कोई शहर रहने लायक है या नहीं।
इस तरह के पैमानों पर शहरों के आकलन से कुछ सवालों के जवाब अवश्य मिलते हैं, लेकिन कई अहम और खड़े हो जाते हैं, जिनकी अनदेखी करना मुश्किल है। जैसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर साफ-सफाई और सहूलियत के मामले में हमारे उत्तर भारतीय शहर किस दुविधा में फंसे हुए हैं। शिमला को छोड़ कर कोई अन्य शहर इस लायक क्यों नहीं माना जा रहा है कि वहां एक आम इंसान अच्छा जीवन जी सकता है।
यह एक बड़ी विडंबना है कि हमारी राजनीति में जिस उत्तर भारत का वर्चस्व दिखाई देता है, वह अपने शहरों को दुरुस्त करने के मामले में दक्षिण भारतीय शहरों से मात खा जाती है। दक्षिण से उत्तर भारत के शहरों के पिछड़ जाने की अहम वजह यह है कि हमारी सरकार भले ही देश के सौ शहरों को स्मार्ट शहरों में तब्दील करने की ख्वाहिशमंद हो, लेकिन उत्तर भारत में अनियोजित ढंग से बसते शहरों की बसावट के उनके अंदाज में घोर बेतरतीबी बिखरी हुई है। इस समस्या का नतीजा यह निकल रहा है कि सरकारी की योजनाओं के बावजूद खुद-ब-खुद बनने और बिगड़ने वाले ऐसे ज्यादातर शहरों ने शहरीकरण की शक्ल ही बिगाड़ कर रख दी है।
कहा जा रहा है कि 2028 तक हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी-घनत्व वाला मुल्क होगा। यानी अगले छह-सात वर्षों के भीतर इस मामले में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब वहां जनसंख्या में गिरावट का दौर शुरू हो चुका होगा और भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही होगी। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2013 की जनसंख्या रिपोर्ट का है। आबादी की जरूरतों के मद्देनजर और विकसित देशों की देखादेखी हमारे देश में शहरीकरण को तो बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस तब्दीली का हमारी सरकारों और योजनाकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि आज देश के ज्यादातर शहर बेकाबू और अनियोजित फैलाव के शिकार हो गए हैं।
इसकी तसदीक वर्ष 2018 में विश्व बैंक की एक अन्य रिपोर्ट ‘अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया’ में की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में ज्यादातर शहरीकरण बहुत ही गुपचुप ढंग से और बेतरतीबी के साथ हो रहा है। शहरी नियोजन की सारी नीतियों- कवायदों को ताक पर रख कर और आंख मूंद कर होने वाला यह शहरीकरण देश को ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसमें ऐसे शहरों की ऐसी तस्वीर उभरती है जो कूड़े के ढेर से अटे दिखाई देते हैं और जहां की असंख्य इमारतें भूकंप के हल्के से झटके में ढहने को तैयार लगती हैं।
शहरों की जिंदगी में सुधार की जरूरत का एक संकेत दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में भी मिला था।
इस सूचकांक में शहरों का आकलन पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और ढांचागत सुविधाओं आदि पांच प्रमुख मानकों पर किया जाता है। दुनिया के एक सौ चालीस देशों के प्रमुख शहरों में से लोगों के निवास के उपयुक्त शहरों का आकलन करने वाला यह सूचकांक यानी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) जारी करती है। उल्लेखनीय यह है कि 2019 में इस सूचकांक में भारत के चुनिंदा शहरों की स्थिति और बदतर ठहराया गया था। जैसे देश की राजधानी दिल्ली इस सूचकांक में 2018 के मुकाबले छह स्थान फिसल कर एक सौ अठाहरवें नंबर पर पहुंच गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा अपराधों में बढ़ोत्तरी को इसकी अहम वजह माना गया था। इसी तरह मुंबई दो पायदान नीचे गिर कर एक सौ उन्नीसवें स्थान पर आ गई थी और इसके लिए वहां पर्यावरण के अलावा सांस्कृतिक गिरावट को जिम्मेदार माना गया था।
शहर कैसे भी क्यों न हों- उनकी जरूरत से अब इनकार नहीं किया जा सकता। गांव-कस्बों में रोजगार की कमी और बढ़ती आबादी के बरक्स खेत-खलिहानों का घटता आकार बीते कई दशकों से लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। आमतौर पर यह पलायन रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब रोजगार के साथ शहरीकरण देश के विकास की पहली जरूरत है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थितियों में ये समीकरण उलट गए हैं।
अब शहरों के लिए जरूरी हो गया है कि वे साफ-सफाई और मूलभूत ढांचे के अलावा स्थायी किस्म के रोजगार सृजन को भी अहमियत दें, ताकि गांव-कस्बों से यहां आने वाली आबादी को कोरोना जैसे संकट के समय सब कुछ छोड़ कर घर वापस लौटने का विकल्प अपनाने को मजबूर न होना पड़े। शहर बनाने और शहर बसाने का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि ढांचागत सुविधाओं के आधार पर वह रहने की एक शानदार जगह है, बल्कि अब जरूरी हो गया है कि वहां लोगों को वाजिब कीमत पर आवास के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के सारे साधन भी मिले।
यही वह कसौटी है जिस पर खास तौर से उत्तर भारतीय शहर पिछड़ते जा रहे हैं। रोजगार जैसे मसले पर तो राजनीति के तहत दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों के भीतर से आवाज उठने लगी है कि उन्हें अब और बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी शहर की रहन-सहन योग्य क्षमता तब तक अधूरी ही मानी जाएगी, जब तक यह साफ न हो कि वह शहर रोजगार के कितने और किस तरह के अवसर उपलब्ध करा सकता है।