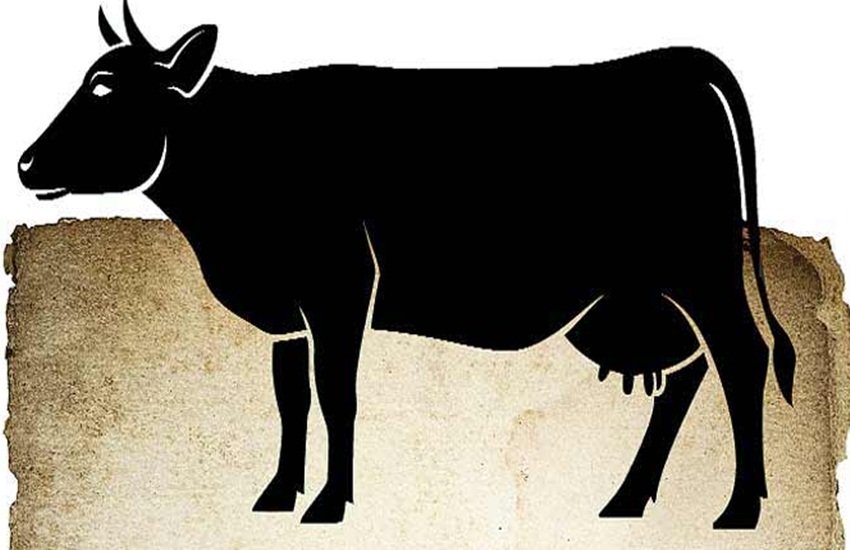जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि गोरक्षा के नाम पर हत्या स्वीकार नहीं है तो उसी समय अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान रखने वाले उनके एक मंत्री यह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि देश में मुसलमानों को किसी तरह का कष्ट है, उनकी एक मंत्री ‘मेरे नाम पर नहीं’ अभियान में शामिल हुए लोगों पर आरोप लगा रही थीं कि वे केरल और कश्मीर में भीड़ द्वारा की हुई हत्या पर क्यों नहीं बोले थे। और उसी वक्त गोमांस ले जाने के शक में झारखंड में अलीमुद्दीन मारा जा रहा था। तो उनकी सरकार के मंत्री से लेकर झारखंड के गोभक्तों तक को अब अगर प्रधानमंत्री की बात समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप जिसे आस्था का सवाल बना चुके हैं वह कानून और व्यवस्था का मसला रह ही नहीं जाता है। शीर्ष से चली आस्था की गूंज जब पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक में जगह बना चुकी है, तो नागरिक से भीड़ में तब्दील हो चुके कानों में मोदी की अपील के असर की उम्मीद क्या करें। भीड़ से पैदा हो रहे भय के खिलाफ इस बार का बेबाक बोल।
शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का अंश। मध्यकालीन युग की बर्बरता जो नाटक में दिखाई गई है वह इक्कीसवीं सदी के भारत में कश्मीर से लेकर झारखंड तक की सड़कों पर सच में घटित हो रही है। शेक्सपियर के नाटकों का अंधियारा हमारे समाज पर छाया हुआ दिख रहा है। जूलियस सीजर का एक पात्र कवि सिन्ना है। वहीं एक दूसरा सिन्ना भी है जो जूलियस सीजर की हत्या में शामिल था। भीड़ हत्यारा समझ कर कवि पर हमला करती है। कवि चीख-चीख कर अपनी पहचान बताता है, लेकिन भीड़ सिर्फ इतना ही समझती है कि उसका नाम सिन्ना है और उसे मार डालती है। क्योंकि भीड़ का मकसद समझना नहीं, सिर्फ मार डालना था।
कश्मीर में सिन्ना की जगह अयूब पंडित थे। वे भीड़ से जो भी चिल्ला कर कह रहे थे भीड़ उसे सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इस भीड़ का भी मकसद सिर्फ मारना था। दिल्ली से ईद की खरीदारी कर जाता एक किशोर। पर, वह चांद रात की तैयारी करते परिवार तक पहुंच नहीं पाया। ट्रेन में वह गुस्साई भीड़ का शिकार इसलिए बन गया कि उसकी पहचान ईद से जुड़ी थी। यात्रियों से भरी ट्रेन में इस हत्या के खिलाफ कोई नहीं बोला, किसी ने भी यह हत्या नहीं देखी और पुलिस को कोई चश्मदीद नहीं मिला।
जब कोई कुछ नहीं देखता है और कुछ नहीं बोलता है तो वह इंसान नहीं, भीड़ का हिस्सा मात्र हो जाता है। इंसान जब अपने जेहन और रूह से अलग हो जाता है तो भीड़ बन जाता है। समाज और संस्कृति से अलग हुआ – एक रक्तपिपासु। आस्था का झंडा उठाई इस भीड़ को सिर्फ इतना याद रहने दिया गया है कि वह फलां धर्म का है, वह इंसान भी है उसे यह याद रखने का वक्त और मौका तक नहीं दिया जा रहा है।
गृह सचिव यह कहते हुए उद्धृत किए जा रहे हैं कि भीड़ द्वारा हत्या को मीडिया बढ़ा-चढ़ाकर बता रहा है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है। सुना नहीं आपने कि अमेरिका के अगुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईर्ष्यालु भाषा में हमारे अगुआ से कहा कि मीडिया से तो आपका दोस्ताना संबंध है। ट्रंप साहब को अमेरिकी मीडिया परेशान कर देता है, मेरिल स्ट्रीप उन्हें आईना दिखाने लगती हैं। लेकिन ट्रंप साहब को इस बात की ईर्ष्या है कि भारत के अदाकार से लेकर पत्रकार तक उन्हें परेशान नहीं करते। तो महाशय, मीडिया इसे बढ़ाकर नहीं दिखा रहा बल्कि वह इसलिए दिखा रहा कि उसे छुपाकर नहीं रखा जा सकता था। जब पत्रकार से लेकर पुलिस तक भीड़तंत्र का शिकार होकर मारे जाएं तो फिर दोस्ती तो दरक ही सकती है।
2015 में जब दिल्ली से थोड़ी ही दूर दादरी के बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक की हत्या भीड़ ने की थी तो दहशत की पहली बयार उठी थी। अपराध समाज का हिस्सा है और हत्या जैसे अपराध होते रहते हैं। लेकिन जब बस्ती के बाशिंदे भीड़ बनकर किसी की जान लें, तो फिर डरना जरूरी है। उस वक्त जताए डर को आपने राष्टÑविरोधी और विरोध प्रदर्शन के तरीके को कागजी क्रांति कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अखलाक के बाद सूची बढ़ती गई। पुणे में मोहसिन शेख मारे जाते हैं। और, इसके बाद न्यायदंड उठाई भीड़ का शिकार झारखंड में हिंदू भी हो जाते हैं। कागजी क्रांति को ही थोड़ा सुन लिया होता तो आज सड़कों पर भीड़ हत्यारी बनने को आमादा होती नहीं दिखती।
आपने बेरोजगारी से लेकर हर समस्या को राष्टÑ और व्यवस्था से जोड़ दिया। पहली हिंसा पर आप मौन रहे और आज भी आप पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग में मरे लोगों के लिए वेदना तो जताते हैं लेकिन नफरत की हिंसा में मारे गए लोगों पर देर तक वही ‘मौनी बाबा’ बने रहते हैं, जिसका आरोप मनमोहन सिंह पर लगाते थे। जंतर-मंतर के नागरिक जुटान के बाद आप बोले जरूर हैं, पर बोलने में देरी की शिकायत तो रहेगी।आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक अवधारणा को सबसे अहम माना गया था। इसके तहत नागरिकों की सामूहिक चेतना का आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिसका परिणाम था व्यक्ति की निजता का सम्मान। निजता की यह अवधारणा उदारवाद की धुरी थी। लेकिन नवउदारवाद के ढांचे में इंसान अकेला पड़ता जा रहा था। प्रेमचंद ‘गोदान’ में किसानों की समस्या लाते हुए कहते हैं कि यह विकास नहीं, विनाश है। आजादी के बाद का दौर शोषणमुक्त समाज बनाने का दौर था। वह एक तरह से अलग किस्म के समाजवादी ढांचे का विकास था, जिसमें व्यक्ति की निजता को सामाजिक उद्धार से जोड़ा गया था। लेकिन नवउदारवाद इससे उलट ढांचा लेकर आया। इसमें व्यक्ति अकेला हो जाता है। और व्यक्ति का यही अकेलापन सामने आ रहा है। सामाजिक पायदान पर अकेला महसूस कर रहे रोहित वेमुला खुदकुशी कर लेते हैं तो बाजार में अकेला छोड़ा गया सामंती व्यवस्था के थपेड़े खा रहा किसान खुदकुशी कर लेता है।
मनमोहन काल में ही नागरिकों के बीच ऐसी सामूहिक चेतना बन रही थी कि यह जो भी ढांचा है कुछ के फायदे के लिए है। और शासक वर्ग को इसी सामूहिक चेतना को बदलने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन इस सामूहिक चेतना को बदलने में कांग्रेस सरकार नाकामयाब रही तो बाजार ने उस शासकवर्ग को ही बदल दिया। अब जनता के सामने एक ऐसी सरकार है जो अच्छे दिन का ब्रांड लेकर आई थी। अच्छे दिन आएंगे…मतलब जनता की चेतना में वह पिरोया जो वास्तविक नहीं है, जो अमूर्त है। पहले सामूहिक चेतना में जो उद्धारक थे, उसी को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया गया। सबसे पहला दुश्मन मुसलमान के रूप में खड़ा किया गया। इस नई सामूहिक चेतना में तार्किकता और बौद्धिक प्रक्रिया का अंत हो गया। इक्कीसवीं सदी का नया इंसान मध्यकालीन मानसिकता ढोने लगा। बुनियादी दिक्कतों का हल खोजने में नाकाम सत्ता के लिए बौद्धिक और तार्किक तंत्र की जगह भीड़तंत्र मुफीद था।
अब इस भीड़तंत्र में व्यक्ति की निजता के लिए कोई जगह नहीं है। वह एक सामूहिक दुश्मन की खोज करता है। याद करें नोटबंदी के दौर में राष्ट्रवाद में उलझी जनता ऐसी भीड़ बन चुकी थी जिसे अपने ऊपर हो रहे हमलों के दर्द का भी अहसास नहीं था। सरहद के दुश्मन और भ्रष्टाचार जनता के सामूहिक दुश्मन बना दिए गए थे। नोटबंदी की बड़ी मार खाए किसान आंदोलन के समय भी हम यही प्रक्रिया देखते हैं। अपने आंदोलन में किसान भी अलग पड़ गए जैसे उनका देश की सामूहिकता से कोई वास्ता नहीं था। पहचान की राजनीति के झंडाबरदार भी जातियों और उपजातियों की पहचान से ही संघर्ष को देख रहे हैं। किसानों और कामगारों को लेकर सामूहिक संघर्ष खत्म करना ही इस नवउदारवादी ढांचे की सफलता है। हर किसी के हित को अलग कर देना, यह कोशिश करना कि कोई भी सामूहिक एजंडा तैयार नहीं हो पाए।
सामाजिकता में इस सामूहिकता के खात्मे को हम दिल्ली से फरीदाबाद जाती ईएमयू ट्रेन में देख चुके हैं। कभी सहयात्रियों का पराठा-अचार मांग कर खाने वाले यात्री आज ‘ठग्गू के लड्डू’ से डर कर अपनी गठरी की चिंता में रहते हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में उद्घोषणा होती है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आज अकेला छोड़ा गया इंसान सुन रहा है कि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। और, अगर किसी जुनैद की जान ली जा रही है तो सामूहिक नजरें फेर ली जाती हैं। इतिहास गवाह है कि पक्ष के फैलाए अंधेरे के खिलाफ प्रतिरोध की रोशनी अपना मंच तैयार कर ही लेती है। जुनैद की हत्या हमारी सामूहिक चेतना की मौत का इशारा कर रही है तो वहीं इस अंधियारे के खिलाफ हम ‘मेरे नाम पर नहीं’ के सहारे बोले तो साबरमती से आपको भी बोलना पड़ा। जरूरत है इन बोलों को संगठित करने की नहीं तो इन नामों को अलग-अलग पहचानों से बिखराने की कोशिश तो जारी है ही।