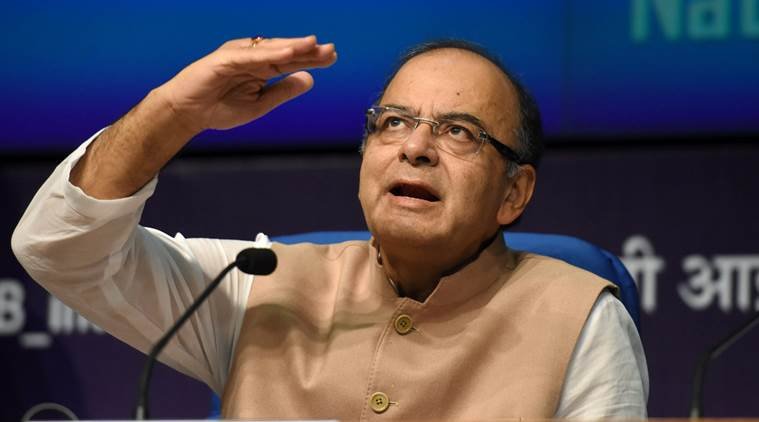केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंतजार का दौर खत्म हो गया। जैसी संभावना थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बकाया (एरियर) मिलेगा। जो सूचना है, इसमें वेतन और भत्तों में उससे कहीं ज्यादा वृद्धि है जितनी वेतन आयोग ने अनुशंसा की थी। माना जा रहा है कि इससे सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। यह बोझ हमारी कुल अर्थव्यवस्था के आकार के 0.7 से थोड़ा ज्यादा होगा। 39,100 करोड़ रुपए वेतन, 29,300 करोड़ रुपए भत्ते और 33,700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे। आम बजट पर 73,650 करोड़ रुपए और रेल बजट पर 28,450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे सैंतालीस लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के साथ करीब तिरपन लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अठारह से तीस प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केंद्र के इस निर्णय के बाद राज्यों पर भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का दबाव होगा और इससे देश के कुल खजाने पर बोझ और बढ़ेगा। इसे झेलने की कुव्वत अर्थव्यवस्था को पैदा करनी होगी।
इसके अलावा सरकारों के पास चारा क्या है। या तो वे वेतन बढ़ाएं या फिर कर्मचारियों का विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। निश्चित रूप से जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारियों को इससे प्रसन्न होना चाहिए वहीं उन लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं हो सकती जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं या किसी प्रकार की नौकरी नहीं। आखिर हम नौकरी में हों या नहीं, लेकिन वेतन-भत्ते मिलेंगे तो कर के रूप में हमारे द्वारा दिए गए पैसे से ही। तो कुल मिलाकर इसका बोझ उस आम जनता के सिर आना है जिसके लिए न कोई वेतन आयोग है न आर्थिक सुरक्षा की कोई अन्य व्यवस्था। जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं या किसी तरह सरकारें कर्मचारियों के भत्तों आदि में बढ़ोतरी करती हैं उनकी खुशियों के साथ यह प्रश्न उठता है कि आखिर उनके लिए क्या, जिनका जीवन दैनिक मजदूरी या असंगठित क्षेत्र में काम करने पर निर्भर है? या, जिनके पास कोई काम नहीं? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, पर इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। जवाब हो भी नहीं सकता। कर्मचारी संगठित हैं। अगर वेतन-भत्ते नहीं बढ़े तो काम बंद करने का विकल्प उनके पास है जिससे वे सरकार की गति को ही विराम दे देंगे। उन्होंने वर्तमान बढ़ोतरी से नाखुशी जाहिर करके ऐसा करने की धमकी दे भी दी है। इसके समांतर बेरोजगारों या असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का ऐसा संगठन नहीं, और हो भी तो उनके लिए ऐसा कोई विधान नहीं, जिससे उनको वित्तीय सुरक्षा दी जा सके।
सातवें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में किया था। इसे अपनी रिपोर्ट डेढ़ साल में सौंपनी थी। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अगुआई वाले आयोग का कार्यकाल अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ाया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री अरुण जेटली को सौंप दी थी। ध्यान रखिए, वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर रिपोर्ट बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। सिन्हा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर वित्त मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार किया तथा उसी नोट को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया जिसे मंजूर कर लिया गया। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा सात हजार रुपए से बढ़ा कर अठारह हजार रुपए करने और अधिकतम वेतन- जो कैबिनेट सचिव का है- मौजूदा नब्बे हजार रुपए से बढ़ा कर ढाई लाख रुपए करने की सिफारिश की गई थी।
आइए जरा देखें कि वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं। इससे वस्तुस्थिति को समझने में सुविधा होगी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक इजाफा करने की सिफारिश की। कुल वेतन में साढ़े तेईस प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश थी, जबकि पेंशन में औसत चौबीस प्रतिशत की। उसने कहा कि न्यूनतम वेतन सात हजार रुपए से बढ़ कर अठारह हजार रुपए किया जाए। वेतन में वार्षिक तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हो। केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन हो। इसके दायरे में दस साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी होंगे। ग्रैच्युटी की सीमा दस लाख से बढ़ा कर बीस लाख रुपए करने की सिफारिश भी वेतन आयोग ने की थी। इसके साथ महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत तक बढ़ाने और ग्रैच्युटी सीमा भी पच्चीस प्रतिशत बढ़ाने की बात थी। वेतन तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली खत्म हो जाएगी। इसने कहा कि छप्पन तरह के भत्ते खत्म किए जाएं और सभी को एक जैसी पेंशन मिले।
यह बात ठीक है कि मूल वेतन में 14.7 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक वृद्धि, सत्तर सालों में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश थी। छठे वेतन आयोग ने बीस प्रतिशत वेतन बढ़ाने की सिफारिश की थी। पर अगर कुल मिलाकर देखें तो यह कर्मचारियों के लिए समग्रता में बेहतर वेतन-भत्ते तथा सेवानिवृत्ति के बाद बढ़िया पेंशन की व्यवस्था करने वाली सिफारिशें थीं। पर केंद्रीय कर्मचारियों को यह स्वीकार नहीं था। यहां यह जानना जरूरी है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने वेतन आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन के लिए अठारह हजार रुपए मासिक के प्रस्ताव को कम मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों से भी अठारह से तीस प्रतिशत ज्यादा वेतन तय करने की बात कही थी। समिति ने 23,500 रुपए न्यूनतम और 3.25 लाख रुपए अधिकतम वेतन रखने को कहा था। यही रिपोर्ट वित्तमंत्री अरुण जेटली के पास गई थी। जाहिर है, करीब तेईस प्रतिशत की वृद्धि इन्हें नागवार गुजर रही थी। मंत्रिमंडल के निर्णय पर ये खुश नहीं हो सकते।
जरा सोचिए, सात हजार का न्यूनतम वेतन अठारह हजार हो जाएगा और नब्बे हजार वाला वेतन 2 लाख 50 हजार। यह कितनी वृद्धि है? ढाई गुनी से ज्यादा। लेकिन जिनके लिए यह बढ़ोतरी की गई वही संतुष्ट नहीं हैं। जो सूचना आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। इसी तरह रेलवे कर्मचारी संगठन भी विरोध प्रदर्शन का एलान कर चुके हैं। कैबिनेट सचिव की समिति ने जो अनुशंसा की थी, उसे ये स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं। आप संगठित हैं और आप सरकार का कामकाज ठप कर सकते हैं। वैसे भी सरकारें कर्मचारियों को नाराज करके काम नहीं कर सकतीं। कर्मचारियों के दबाव के आगे सरकारें हमेशा झुकी हैं। हो सकता है इस बार भी वैसा ही हो। हम भी मानते हैं कि जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनको उतना वेतन और भत्ता मिलना चाहिए जिनसे कि उनका जीवन आराम से चल जाए तथा वे दैनिक खर्च के दबाव से मुक्त होकर काम कर सकें। पर कहीं न कहीं तो संयम और संतुलन की रेखा खींचनी होगी। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी तुलना में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें किसी तरह का वेतन और भत्ता नहीं मिलता। आखिर उनका जीवन कैसे चलता है? इन कर्मियों को यह भी पता है कि भारत का खजाना अभी दबाव से मुक्त नहीं हुआ है। राजकोषीय घाटा अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। इसका हल भी उन्हें ही निकालना है। पर इस दिशा में कोई सोचने को तैयार नहीं है। सबको अपनी पड़ी है।
केंद्रीय या राजकीय कर्मियों से हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन उनके लिए वेतन आयोग की जिस तरह से व्यवस्था है- यह ठीक क्रम से गठित होता है, उसकी सिफारिशें आती हैं और अपरिहार्य रूप से स्वीकार भी होती हैं- वैसी कोई व्यवस्था इस देश के करोड़ों गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, मेहनत-मजदूरी से जीवन जीने वालों के लिए क्यों नहीं? क्या समय-समय पर किसी जन कल्याण आयोग जैसे नियमित ढांचे की शुरुआत नहीं हो सकती, जो यह आकलन करे कि आम लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद हुआ है, उन पर बोझ कितना बढ़ा है और उनकी राहत के लिए सरकारें कहां-कहां सहयोग कर सकती हैं। दुर्भाग्य से ऐसी कल्पना आज तक की ही नहीं गई। मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कुछ पेंशन या इन्श्योरेंस की योजनाएं आरंभ की हैं, पर ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही हैं। आखिर देश का काम केवल सरकारी कर्मचारी नहीं करते। एक किसान और खेत में काम करने वाला मजदूर भी देश का काम करता है… निर्माण क्षेत्र में मेहनत करने वाला मजदूर भी देश का ही काम करता है। तो फिर हमारी व्यवस्था इस तरह का भेदभाव क्यों करती है? कम से कम वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के समय तो ऐसे प्रश्नों पर विचार किया ही जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए कुछ रास्ता बने। इसका रास्ता भी केंद्रीय कर्मियों को सुझाना चाहिए। आखिर सरकार के आंख, कान और नाक वही हैं।