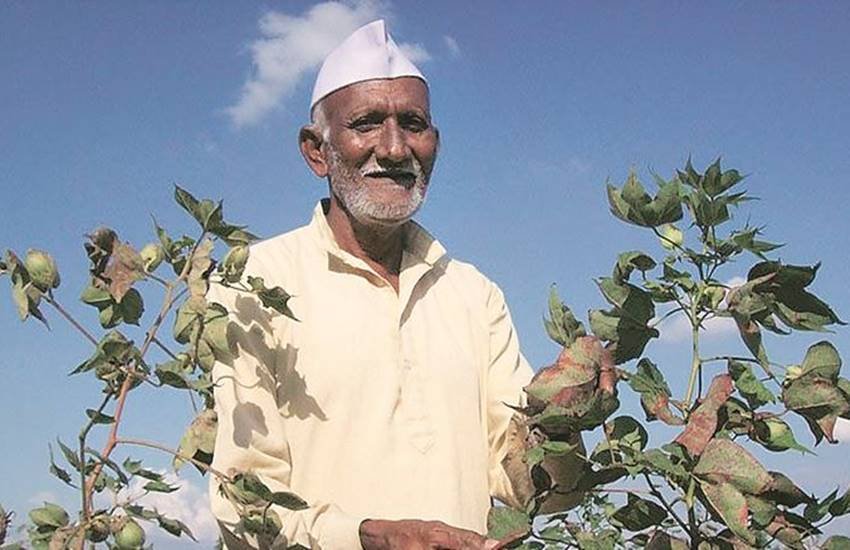सरकार द्वारा धान सहित खरीफ की चौदह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा किसानों की आय वृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। पिछले तीन वर्षों से सरकार मूल्यों में सामान्य बढ़ोतरी कर रही थी। लेकिन इस वर्ष एक साथ पच्चीस फीसद की वृद्धि की गई, जो रेकॉर्ड वृद्धि है। खरीफ की मुख्य फसल धान का मूल्य अब 1750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। रागी का मूल्य 1900 रुपए बढ़ा कर 2897 रुपए कर दिया है, तो मूंग में 1400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जैसा हम जानते हैं कि कृषि और लागत मूल्य आयोग हर वर्ष किसानों की फसलों की लागत तय कर उसके अनुसार मूल्य निर्धारित करता है। केंद्र और राज्य सरकारें एक निश्चित सीमा तक भंडार रखने और जन वितरण प्रणाली आदि के लिए इनकी खरीद करती हैं। किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। ज्यादा गिरावट को रोकने के लिए भी सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है। बाजार में अगर किसानों को फसलों का उचित भाव नहीं मिल पाता है तो सरकारी एजंसियां घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसे खरीद लेती हैं। वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) के दौरान देश का खाद्यान्न पैदावार करीब अठ्ठाईस करोड़ टन के रेकार्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।
आम कल्पना यह थी कि एक साथ इतनी बढ़ोतरी का जोरदार स्वागत होगा। किंतु प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। एक ओर जहां इसका स्वागत हुआ, वहीं कई किसान संगठन नाखुश भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें फसलों की लागत तय करने के आधार को समझना होगा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि लागत और कीमतों से संबंधित आयोग (सीएसीपी) मुख्यत: तीन आधारों पर विचार करता है। इसमें पहला है ए-2, जिसमें बीज से लेकर खाद आदि, मजदूर, मशीनरी और पट्टे पर ली गई जमीन का खर्च शामिल होता है। दूसरा है, ए-2 (एफएल), जिसमें ए-2 के साथ किसानों के परिवारों का पारिश्रमिक भी जोड़ा जाता है। तीसरा है, सी-2, जिसे कांप्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं। यह लागत के आकलन करने का सबसे व्यापक आधार है। इसमें परिवार का श्रम, जमीन का किराया और खेती के काम में लगाई गई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। किसान संगठनों का कहना है कि इसी लागत के आधार पर उनका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में बने राष्ट्रीय किसान आयोग ने सी-2 पर पचास फीसद अधिक देने की सिफारिश की थी। सरकार ने मुख्यत: ए-2 (एफएल) को आधार बनाया है।
जहां तक लागत के आकलन बदलने का प्रश्न है, तो इसके लिए मांग जारी रखने में हर्ज नहीं है। मुख्य बात है किसानों की आय बढ़ना और कृषि लाभ और सम्मानजनक जीवनयापन का कार्य बन सके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को इस दिशा में कुछ कदम और उठाने ही होंगे। वैसे भी केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। किसानों की जेब तक यह मूल्य पहुंचे, यह भी आवश्यक है। यदि किसानों को कुछ किलोमीटर के अंदर मंडियां नहीं मिलेंगी और वहां निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने की व्यवस्था नहीं होगी तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। सरकारें किसानों की कुल बिक्री योग्य सामग्रियां नहीं खरीद सकतीं। सरकारी एजंसियों ने 2017-18 में सात करोड़ दस लाख टन गेहूं और धान की खरीद की थी, जबकि पैदावार इक्कीस करोड़ टन थी। इसके अलावा करोड़ों टन दलहन, तिलहन, प्याज और आलू आदि भी पैदा हुए। दालें और तिलहन भी काफी खरीदी गर्इं। कपास की खरीद भी होती है। एक समस्या भंडारण की भी है। खाद्य मंत्रालय ने मार्च में संसद को जानकारी दी कि चावल और गेहूं जैसे अनाज के लिए केंद्रीय भंडारण की क्षमता सात करोड़ पैंतीस लाख टन की है। इसमें से भी सत्रह फीसद खुले भंडार हैं जहां अनाज को प्लास्टिक या अन्य चीजों से ढंका जाता है।
किसानों के उत्थान के लिए ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनका लाभ भविष्य में मिलेगा। इनमें राष्ट्रीय कृषि बाजार या ईनाम पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। मार्च, 2018 तक पांच सौ पिचासी मंडियों को ईनाम से जोड़ा गया है। अन्य को जोड़ने पर काम चल रहा है। इस पोर्टल पर करीब एक करोड़ किसान, सवा लाख व्यापारी और बारह सौ से ज्यादा कमीशन एजंट जुड़ चुके हैं। यह पोर्टल भारत की कई भाषाओं में है। मोबाइल ऐप भी है। इस ऐप पर आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि किस बाजार में किस चीज के कितने दाम हैं और आप वहां जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर इसका विस्तार हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर नीति आयोग एक बेहतर प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है जो यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले।
चूंकि अभी तक भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरण के लिए केवल गेहूं और चावल खरीदता रहा है, इसलिए एक नई व्यवस्था स्थापित करने पर काम किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य फसलों के मूल्यों में वृद्धि का लाभ भी किसानों तक पहुंचे। नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि राज्यों को तीन मॉडलों का विकल्प दिया जाना चाहिए- बाजार आश्वासन योजना (एमएएस), मूल्य अंतर खरीद योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। इसमें चावल और गेहूं को छोड़ कर अन्य सभी फसलों के दाम एमएसपी से नीचे जाने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार को हर वर्ष करीब बारह से पंद्रह हजार करोड़ रुपए का बोझ वहन करना पड़ सकता है। बाजार आश्वासन योजना (एमएएस) राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाएगी, जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बाजार में जाएंगे और राज्यों द्वारा अधिकृत अपनी निजी एजंसियों या किसी अन्य निजी एजंसी के माध्यम से खरीद करेंगे। मूल्य कमी खरीद योजना के तहत, यदि बिक्री मूल्य मॉडल कीमत से कम है, तो किसानों को कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ एमएसपी और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर का मुआवजा दिया जाएगा। नीति आयोग ने एक पारदर्शी ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसपी-संबद्ध खरीद के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रस्ताव भी दिया है।
सरकारों के सामने कई प्रकार की वित्तीय सीमाएं होती हैं जिनके तहत उनको फैसले करने पड़ते हैं। केंद्र सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई दर को एक सीमा से नीचे बनाए रखने की चुनौती है। पिछले तीन सालों में यदि कृषि पैदावारों के दाम में एक साथ भारी वृद्धि नहीं हुई तो इसका एक बड़ा कारण महंगाई दर था। किसानों को पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस काम हो रहा है। इन सबको पूरी तरह साकार होने में थोड़ा समय लगेगा। सरकारों द्वारा मूल्य वृद्धि की सीमाएं हैं। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसान जब चाहें, नियत मूल्य पर उनका सामान बिक जाए। किसानों की आय में मूल बात है कृषि लागत में कमी लाना। दूसरे, कृषि से जुड़े उद्योग जगह-जगह खड़े हों और उनसे अन्य वस्तुएं तैयार हों और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता विकसित हो। इन दोनों पर तेजी से काम किए जाने की आवश्यकता है।