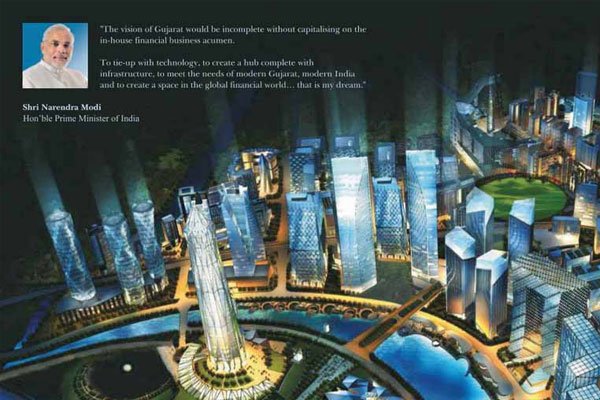तेज शहरीकरण की आपाधापी में इंसान उन बुनियादी बातों को भूल चुका है, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की हदों से वास्ता रखती हैं। धरती इंसानी आबादी की तरह अपना विस्तार नहीं कर सकती, लेकिन इस वास्तविकता को समझने के लिए इंसान तैयार नहीं है। छोटे से लेकर बड़े शहरों और महानगरों तक, अनियोजित तरीके से टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। हर अखबार में टाउनशिप के बड़े-बड़े विज्ञापन आते रहते हैं, जिनमें सभी तरह की सुविधाएं एक ही जगह मुहैया कराने के वादे किए जाते हैं। शहर से सड़क या रेलमार्ग से जुड़े नजदीकी गांवों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है। वातानुकूलित मॉल में सब्जी और किराना के सामान बेचे जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगल की कीमत खेत-खलिहान से बहुत ज्यादा है। इसलिए किसान का लालच में आना स्वाभाविक है। शहर के निकट के इलाकों में जो खेत लाख-दो लाख में बिक रहे थे, उनकी कीमत आज लाखों-करोड़ों में आंकी जा रही है। गरीबों और किसानों की जमीन को कम कीमत पर कारोबारियों को उपलब्ध कराने में सरकार भी बराबर की दोषी है।
सड़क और रेलमार्ग के निर्माण के लिए खेतीयोग्य जमीन के अधिग्रहण की जरूरत होती है। इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हर प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन किसानों को जमीन की वाजिब कीमत न मिल पाने के कारण अधिग्रहण के मसले पर सरकार और किसानों के बीच टकराव के मामले देखे जाते हैं। सिंगूर और भट्टा पारसौल विवाद इसी तरह के थे। पटना में नवनिर्मित पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का सालों से उद्घाटन न होने का कारण भी यही है। बहुत सारी सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाएं इसी कारण अधर में अटकी पड़ी हैं। वर्तमान भूमि अधिग्रहण नीति के पारदर्शी न होने और किसानों के प्रतिकूल होने के कारण किसानों और सरकार के बीच लगातार संघर्ष हो रहे हैं। कॉरपोरेट और बिल्डर आमतौर पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके प्रस्तावित परियोजना का पता पहले लगा लेते हैं और प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास की जमीन औने-पौने दाम में या तो खरीद लेते हैं या फिर उस पर कब्जा जमा लेते हैं। सारा खेल मौखिक करारनामे के आधार पर होता है, जिसके एवज में स्पीड मनी लेने का रिवाज हमारे सभ्य समाज में है।
कंक्रीट के जंगल में हर वस्तु की मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ती है। खाद्य पदार्थ और उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमत सामान्य तौर पर कस्बानुमा शहरों और गांवों से अधिक होती है। इस जंगल में सारा काम प्रायोजित तरीके से किया जाता है। इसलिए इस जंगल में छायादार वृक्ष से हर कोई परहेज करता है। दरअसल, पेड़-पौधे, जंगल आदि कारोबारियों के व्यावसायिक इरादों को अवरुद्ध करते हैं। वे मूल रूप से पूंजीवाद के वाहक होते हैं। नौकर-चाकर की जरूरत तो इन्हें होती है, लेकिन आसपास बनी झुगी-झोपड़ी उन्हें टाट का पैबंद लगती है। लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल की वजह से भूजल के उपयोग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है, जिसके कारण भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। नदी, तालाब, झील, पोखर आदि या तो मार दिए गए हैं या उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। भूजल के अंधाधुंध दोहन के चलते देश के अनेक इलाके डार्क जोन की श्रेणी में आ गए हैं, यानी वहां भूजल का भंडार पूरी तरह रिक्त हो चुका है, या भूजल इतना नीचे चला गया है कि उसकी निकासी संभव नहीं है।
पुराने शहरों में भी अपार्टमेंट महज दस से बारह फुट चौड़ी सड़क के किनारे बनाए जा रहे हैं, जबकि एक अपार्टमेंट में एक गांव बसता है। जब एक पूरा गांव तीन से चार कट्ठा के क्षेत्रफल में बसेगा तो नाली और यातायात-जनित समस्या उत्पन्न होगी ही। रास्ता बड़ा हो, इसके लिए नालियों को पाट कर सड़क बनाई जा रही है। तात्कालिक रूप से जरूर इससे जाम से निजात मिल सकती है, लेकिन नाली जब जाम होगी तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। पटना और इस श्रेणी के दूसरे शहरों की हालत अमूमन ऐसी ही है। पूरे शहर में गगनचुंबी अट्टालिकाओं का जाल बिछा हुआ है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात से जुड़ी समस्याओं में अपूर्व इजाफा हुआ है। संकरी सड़कों के किनारे, अपार्टमेंटों के कारण, नालियां अक्सर जाम हो जाती हैं, जिससे मल-मूत्र सड़कों पर बहता रहता है। इस वजह से डायरिया, पीलिया, डेंगू आदि रोगों का संचार होता है। संकरी सड़कों पर खोमचे, रेहड़ी और सब्जी वालों की उपस्थिति स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। ऐसे में अगर सड़क पर निर्माण-कार्य चल रहा हो तो हालात नारकीय हो जाते हैं। आमतौर पर इस तरह के स्थलों पर चेतावनी वाला बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया जाता।
इधर फुटपाथ बनाने की परिपाटी खत्म हो रही है। जो पहले से हैं वे भी संकरे होने की वजह से बहुत उपयोगी नहीं हैं। ऐसी हालत में पार्किंग की व्यवस्था के बारे में सोचना बेमानी है। अगर कहीं फुटपाथ को योजनानुसार विकसित भी किया गया है तो वहां पर बेरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे आम नागरिकों की जान हमेशा सांसत में रहती है।
यातायात और गाड़ियों की आंख-मिचौली में प्रतिदिन दुर्घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण सड़कों पर मरम्मत और खुदाई के काम का चलना भी होता है। कंक्रीट के जंगलों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक से नहीं की जा सकी है। सड़क पर अंधेरा होने से स्वाभाविक ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़कों पर बने बेतरतीब ब्रेकर भी अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं। व्यस्ततम सड़कों पर पैदल मार्ग न होने से भी दुर्घटनाएं होती हैं, खास करके चौराहों पर। जेब्रा क्रासिंग रहने पर भी, ट्रैफिक नियमों की जानकारी के अभाव में, लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।
अधिकतर शहरों में आज न तो खेल के मैदान हैं न बाग-बगीचे और न ही पार्क। अब तो कब्रिस्तान पर भी बिल्डरों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। समारोहों और शोकसभाओं में शामिल होने तक के लिए जगह नहीं बची है। शादी और शोकसभा सड़कों पर आयोजित की जाने लगी हैं। धरना-प्रदर्शन, वीआइपी या वीवीआइपी के काफिले आदि के चलते यातायात-व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। इस तरह के जाम के कारण कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अब तो बच्चों के लिए घर के बाहर खेलना सपना हो गया है। जगह की कमी की वजह से बच्चे शारीरिक कवायद वाले खेल खेलने के बजाय कमरे में बंद होकर खेलना पसंद करते हैं। कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल और वीडियो गेम उनके सबसे महत्त्वपूर्ण साथी बन चुके हैं। इससे बच्चों में कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। टेलीविजन और कार्टून वाले कार्यक्रम के पात्रों की नकल करने के चक्कर में वे हादसे के शिकार बन जाते हैं।
क्या विकास की ऐसी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं? शहरीकरण का उद्देश्य है संसाधनों और सुविधाओं को समुचित तरीके से सभी को मुहैया कराना। लेकिन शहरों का विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। शहरों के बेतरतीब विकास से इंसान असमय ही काल का ग्रास बन रहा है। सवाल उठना लाजिमी है कि विकास की ऐसी कीमत चुकाने के लिए क्या हम तैयार हैं। अव्यवस्थित विकास का खमियाजा अक्सर हमें जान-माल की कीमत पर भुगतना पड़ता है। नेपाल और उत्तराखंड में हाल ही में बेतरतीब विकास ने हजारों की जान ले ली। आधारभूत संरचना में क्रमिक रूप से सुधार लाना बेहतर तरीके से जीवन जीने की पहली शर्त है, लेकिन इसका पर्याय सिर्फ सड़क, टाउनशिप या गगनचुंबी इमारतों को नहीं माना जा सकता।
कहा जा सकता है कि अनियोजित विकास से किसी का भला नहीं हो सकता। बुनियादी जरूरतों को दरकिनार करके विकास की गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में गरीबों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। उन्हें विकास के मौजूदा मॉडल ने क्या दिया है? इस विकास की नीति के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। बहुत-से लोग गांव छोड़ कर शहर की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। पर शहर में उनकी समाई नहीं हो पाती। वहां वे बेगाने बने रहते हैं। मलिन बस्तियों, झुग्गियों और फुटपाथों पर गुजर करने वालों की तादाद नित बढ़ती जा रही है।
भारत एक लोकतांत्रिक और राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। हर नागरिक को दो वक्त की रोटी मुहैया कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लिहाजा, विकास का स्वरूप चाहे जैसा हो, इस कवायद में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। आधुनिक तरीके से शहरीकरण की प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति नहीं है, पर इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के क्रम में कुदरती संसाधनों की सीमाओं और उन गरीबों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कड़ी मेहनत के बावजूद बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से वंचित रहते हैं।
(सतीश सिंह)
फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta
ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/Jansatta