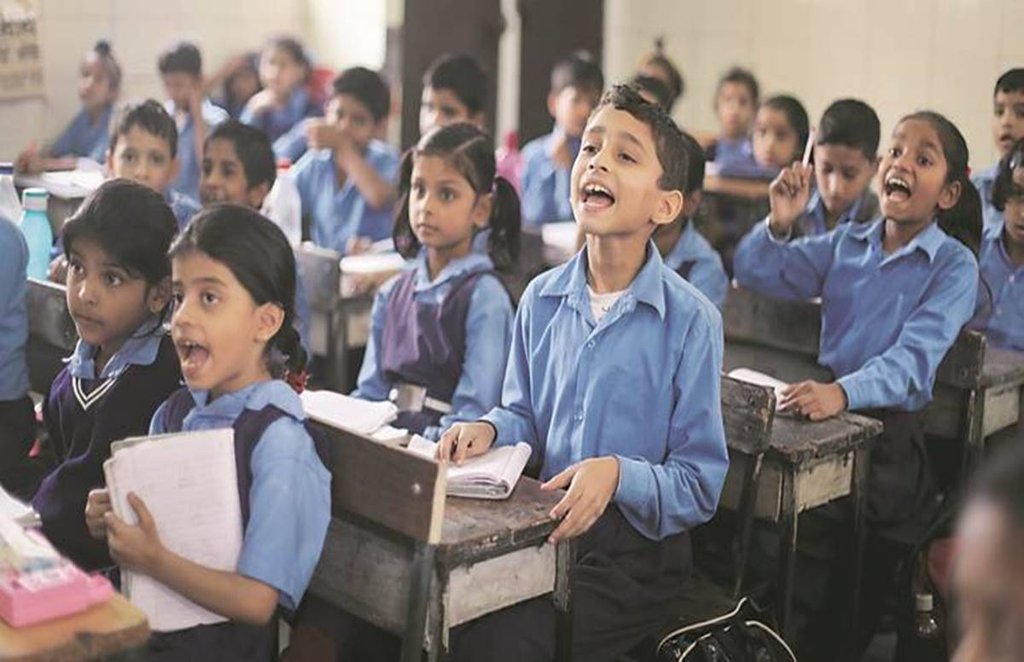हर भारतवासी की अपेक्षा है कि भारत शिक्षा, ज्ञान, कौशल और उत्कृष्टता में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि भारत अन्य देशों के छात्रों के लिए वैश्विक ज्ञान केंद्र बने और अपनी ज्ञानार्जन परंपरा की विशिष्टताओं को भी बनाए रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई-2020) के प्रारंभ में कहा गया है कि ‘प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है।
ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना जाता था।’ यह ऐतिहासिक तथ्य है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे संस्थान विश्वस्तरीय ज्ञान केंद्रों के रूप में स्थापित थे।
इनमें अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे और भारत विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। यदि भारत को फिर से वैश्विक शिक्षा केंद्र बनना है तो उसे विदेशों की तरफ देखने के पहले अपने इतिहास और संस्कृति में झांक कर देखना होगा कि वे कौनसे तत्त्व थे जो चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चाणक्य, नागार्जुन, पातंजलि, गार्गी, थिरुवल्लवूर जैसे मनीषियों को तैयार कर सके!
गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, भवन निर्माण, नौकायन, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में भारतीय बहुत पहले से ही कैसे अग्रणी रहे। स्पष्टत: यह सब ज्ञानार्जन परंपरा, विद्या और संस्थागत उत्कृष्टता से ही संभव हुआ होगा। अनेक ऐतिहासिक कारणों से उस व्यवस्था की गतिशीलता में शिथिलता आई और स्वयं भारतीय ही उससे दूर होते गए।
इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि भारत केवल पश्चिम के विश्वविद्यालयों की नकल कर उस विशिष्टता और उत्कृष्टता को प्रात नहीं कर सकेगा जो उसके संस्थान अपनी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में और नए ज्ञान के सकारात्मक पक्ष को समाहित कर प्राप्त कर सकेंगे। गुरुकुल पद्धति में ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण, और मानव ऋण की जो समझ विद्यार्थियों को नैसर्गिक वातावरण में मिल जाती थी, उसका सार तत्व यदि भारत विश्व को समझा सका होता तो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील डोर चिंताजनक स्थिति तक कमजोर नहीं हुई होती और आज का विश्व घातक प्रदूषण, बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन जैसी स्वजनित समस्याओं से जूझ नहीं रहा होता।
इक्कीसवीं शताब्दी के भारत को वैश्विक स्तर पर भी अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। इसके लिए देश को एक प्रत्यारोपित शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़ कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर अग्रसर होना होगा, जिसकी जड़ें गहराई तक भारत की मिट्टी से पोषण पा रही हों और जो नए ज्ञान को ग्रहण कर प्रगति के मार्ग पर चलने को कटिबद्ध हो। इसकी सफलता से ही भारत शिक्षा का वैश्विक आकर्षण केंद्र बन सकेगा।
आधुनिक भारत की श्रेष्ठता उसके ज्ञान, आध्यात्म और विश्व-बंधुत्व के दर्शन की धुरी पर ही स्वीकार्य होगी। अपने शांति प्रयत्नों के लिए सारे विश्व में सराहे जाने वाले महामहिम दलाई लामा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत में दुनिया के सभी बड़े धर्म, मत और पंथ एक साथ जिस समन्वय के साथ सदियों से रहते रहे हैं, उसे बढ़ाना उनकी प्रतिबद्धता है।
दुर्भाग्य से भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जो भारत की पंथ-निरपेक्षता की व्यावहारिकता से अपरिचित हैं और इसी कारण वैश्विक स्तर पर उसके अपने शुद्ध-स्वीकार्य स्वरूप में उभरने की आवश्यकता और महत्त्व को समझ नहीं पा रहे। इस समय अधिकांश देशों में आर्थिक सामजिक, सांस्कृतिक स्तर पर जो चिंताएं और तनाव पनप रहे हैं, वे स्पष्ट इंगित करते हैं कि इससे छुटकारा पाने का रास्ता एक ही है- हर देश हर प्रकार की विविधता की स्वीकार्यता के महत्त्व को जाने, उसे स्वीकारे और व्यावहारिक रूप में अपने आचरण में उतारे।
इस सोच की व्यावहारिक अनुपस्थिति में विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा, क्योंकि देशों की उर्जा और संसाधन हिंसा, हथियार, युद्ध, आतंक असुरक्षा और अविश्वास में ही नष्ट होते रहेंगे।
हर संस्कृति मनुष्य का सम्मान करने की आवश्यकता को स्वीकार तो करती है, मगर लोक-व्यवहार में उसे भुला देती है! ज्ञान और विज्ञान आवश्यक है, मगर केवल उसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। उसके साथ संस्कृति और संस्कार भी चाहिए. जिनकी अनुपस्थिति में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी में नई खोज और नवाचारों की गति से जीवन में भौतिक सुविधाएं तो बढीं, लेकिन मानवीय तत्त्व व्यवहार से दूर होते चले गए।
जहां-जहां नए ज्ञान और तकनीकी का विवेकपूर्ण उपयोग हुआ है, वहां दैनंदिन जीवन की भौतिक गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, मगर लोगों में, परिवारों में, पीढ़ियों में और देशों में संबंधों की प्रगाढ़ता घटी है, संवेदनात्मक संबंधों में जुड़ाव कम हुआ है। आज विश्व के सात अरब लोग एक दूसरे के पड़ोस में आ गए हैं, मगर पड़ोसी नहीं रहे।
प्यार, करुणा और दयालुता से ही मानव-जीवन प्रारंभ होता है, हर जन्म स्वजनों और परिवार में प्रसन्नता लाता है। यह प्यार बढ़ाते रहन चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। अन्य से अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरों से वैमनस्य रखना, अनावश्यक संग्रहण करना, भौतिकता की चकाचौंध के पीछे भागना, केवल धन प्राप्ति को सुख और आनंद मानने जैसी प्रवृत्तियां आज के भौतिकवादी समाज में गहरी पैठ बना चुकी हैं। इस नकारात्मकता पर अंकुश लगाने का काम संस्कृति और शिक्षा आपसी समन्वय से ही कर सकती हैं।
विश्व के समक्ष एक जो बहुत बड़ी चुनौती उभरी है, वह है- साथ-साथ रहना सीखना! ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था जो केवल ज्ञान देने का प्रयत्न करती है और परीक्षा के प्राप्त अंकों को ही उपलब्धि का मानक मानती है, इसमें सहायक नहीं हो सकेगी। भारत को ऐसे शिक्षित युवा तैयार करने हैं जो हर प्रकार की विविधता को स्वीकार करते हुए किसी भी क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता से युक्त हों।
पिछले कुछ वर्षों में यह तथ्य उजागर हुआ है कि विश्व के अनेक विकसित देशों में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है और वे भारत की ओर देख रहे हैं कि वे भारत में उचित प्रशिक्षण पाकर इन देशों में मानव-शक्ति की कमी को पूरा करेंगे! इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, कौशल विकास को प्रारंभिक वर्षों से ही महत्त्व देना होगा, शोध, नवाचार और नई तकनीकी के विकास पर अधिक निवेश करना होगा।
वैश्विक स्तर पर 2015 में स्वीकृत सतत-विकास लक्ष्य-2030 के अंतर्गत चौथे लक्ष्य में ‘सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने’ की हर राष्ट्र से अपेक्षा है। भारत की नई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि शिक्षा द्वारा उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए और इसी के साथ ह्यनैतिक, सामजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास आवश्यक है।
भारत ने नई शिक्षा नीति में मानवीय पक्ष विकसित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समकक्षता बनाए रखने को भी प्रमुखता दी है। इस समय स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक जो पूर्व-निश्चित खांचों में विद्यार्थी को अपनी अध्ययन-धारा को आगे बढाने की बाध्यता होती है, उसे समाप्त किया जा रहा है। सीखने वाले की रुचि के अनुसार उसे अपने अध्ययन विषय चुनने की स्वायत्तता अब उपलब्ध होगी।
शिक्षा में किया गया निवेश ही देश को सबसे अधिक लाभांश देता है। नई शिक्षा नीति में आश्वासन निहित है कि आर्थिक निवेश बढ़ेगा, संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित और होगी, निर्धारित अनुपात में प्रशिक्षित नियमित अध्यापक नियुक्त शीघ्रता से नियुक्त किए जाएंगे। इस आश्वासन के पूरा होने की ओर देश और विदेश का ध्यान बना रहेगा।