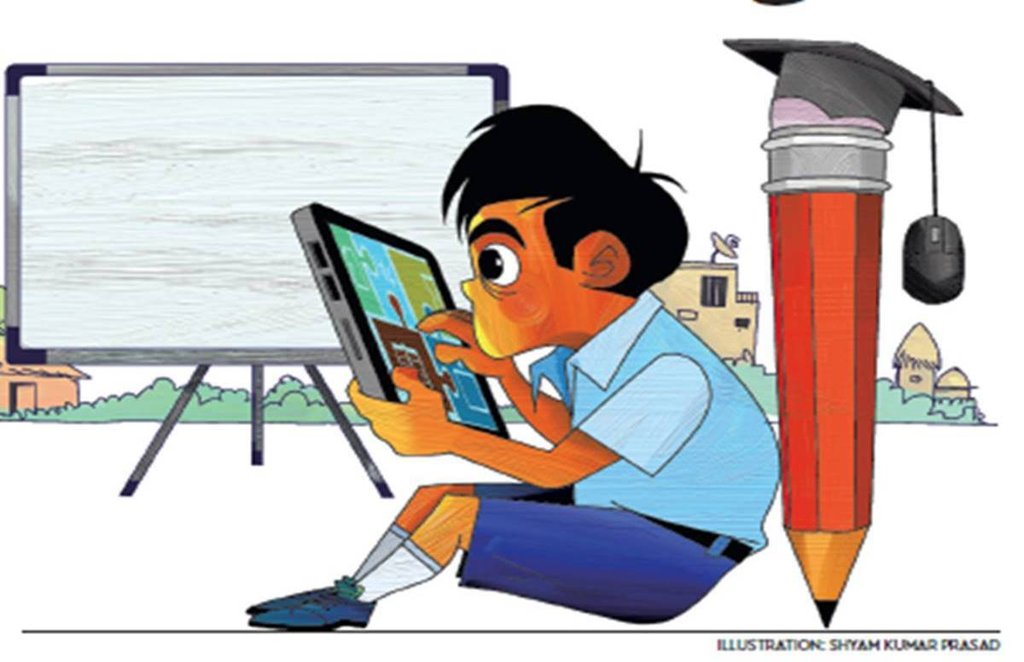प्रदीप कुमार राय
अभी तक महज अक्षर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को साक्षर मान लिया जाता था, मगर अब ‘साक्षरता’ की परिभाषा बदल गई है। एक नया विज्ञान ‘मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी’, जिसका अनुवाद भारतीय विद्वान ‘जनसंचार एवं सूचना संचेतना’ के रूप में करते हैं, को साक्षरता के नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भारत के दुर्भाग्य की गाढ़ी लकीर है कि जब संसार के एक बड़े हिस्से में इस नए विज्ञान को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, भारत की शिक्षा में इसकी चर्चा इतनी भर है, जैसी उड़द पर सफेदी।
मूलत: ज्ञान की यह शाखा विभिन्न स्रोतों से आए संदेशों का सार्थक विश्लेषण सिखाती है। यानी समूह चर्चा से लेकर किताब, टीवी, इंटरनेट आदि विभिन्न माध्यमों के संदेशों को आलोचनात्मक चिंतन की छलनी से छान कर उसमें से पक्षपात को अलग करने की प्रवीणता देती है।
संसार के विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के ठोस तर्कों पर ‘लिटरेसी’ का जो नया संस्करण संसार में आया, उसने दुनिया को बताया कि ‘साक्षरता’ वह होती है, जो आपको समाज को सही दृष्टि से समझने में मदद करे। इसका वृहद अर्थ यह है कि लिखित शब्दों के सपाट अर्थों के जरिए पाई उच्च डिग्रियां भी नई सदी की साक्षरता के लिए काफी नहीं हैं।
अमेरिकी विद्वान फ्रेंक बेकर कहते हैं- ‘यह प्रभावशाली छवियों (मूविंग इमेज) का युग है, जो अक्षरों से कहीं ज्यादा चलन में है और मानव की देश और समाज के प्रति समझ को निर्धारित करती हैं। जो व्यक्ति इन छवियों के छिपे अर्थों को पढ़ने में सक्षम न हो, वह इक्कीसवीं सदी का साक्षर कैसे हो सकता है।
क्योंकि बच्चे से लेकर वयस्क सभी अब इनसे ही अपनी सामाजिक सोच का निर्माण कर रहे हैं?’ कुछ ऐसा ही तर्क यूनेस्को की ग्रुनवाल सिंपोजियम में आया- ‘पिछले पांच सौ वर्षों से हम बोधपूर्ण और शिक्षित नागरिक की समाज में भूमिका को मुद्रित माध्यम से पढ़ने-लिखने की योग्यता के तौर पर देखते रहे, लेकिन आज परिवार, स्कूल और विभिन्न संस्थानों का साझा दायित्व है कि वे युवाओं को प्रभावशाली छवियों और ध्वनियों के इस युग में सजग संदेश ग्रहणकर्ता के रूप में तैयार करें और इसे मीडिया लिटरेसी का नाम दें।’
विद्वानों के एक वर्ग ने तर्क रखा कि यह युग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड (अतिशय सूचना) का है। इसलिए अपार सूचनाओं में से अपने लिए उपयुक्त सूचना की खुराक का चयन करने की कला को भी नए युग की साक्षरता में शामिल किया जाए। इस विषय की ख्यातिलब्ध विद्वान रेनी हॉब्स ने अपने लेख ‘वाट टू बिलीव इन ऐन ऐज इन्फॉर्मेशन एबंडेंस’ में कहा, ‘सूचनाओं की सहज उपलब्धता के इस युग में सूचना में सत्य का पुट मापना और भी कठिन काम हो गया है।’
सूचना के अपार प्रवाह और उसकी आड़ में शक्तिशाली होते ‘प्रोपेगंडा’ ने पूरे संसार में भावनात्मक और बौद्धिक संकट खड़ा कर दिया है। नवंबर, 2020 में अमेरिकी स्तंभकार थॉमस फ्रीडमैन ने अपने लेख में कहा कि ‘देश में झूठ का उद्योग (मिथ्या सूचनाओं का व्यापक प्रसार) इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी अपनी अलग जीडीपी लाइन होनी चाहिए। हमें अमेरिका के हर स्कूल में ‘डिजिटल सिविक्स’ पढ़ानी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी यह अच्छे से पहचान करना सीख सके कि इंटरनेट पर कौन-सी सूचना झूठी और कौन-सी पुष्ट है।’
उल्लेखनीय है कि जनसंचार एवं सूचना साक्षरता की उपशाखाएं ‘न्यूज लिटरेसी’ और ‘डिजिटल लिटरेसी’ के रूप में आई। यानी सोशल मीडिया पर अनजान स्रोतों से आने वाले मिथ्या समाचारों की पहचान कराने के लिए इन दो शाखाओं का अलग से निर्माण करना जरूरी समझा गया।
इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका को बीस झूठी खबरों ने खूब भरमाया। बजफीड के अनुसार इस चुनाव में अनजान स्रोतों से आई इन बीस झूठी सूचनाओं ने अमेरिका में इतनी भारी संख्या में पाठकों को आकर्षित किया जितना वहां के नामी-गिरामी अखबारों की खबरें भी उतना नहीं कर सकीं।
उसके बाद संसार के इस सबसे शक्तिशाली देश के विद्वानों ने स्वीकार किया था कि अमेरिका मीडिया एंड इन्फोर्मेशन लिटरेसी को शिक्षा का अंग बनाने में कई विकसित देशों से पीछे है। इसके बाद वहां अमुक विषय के विकास पर विद्वानों ने काफी ध्यान दिया।
एक अकादमिक विषय के रूप में संसार भर में यह विषय पूरी तरह स्थापित हो गया है। क्योंकि ‘प्रोपेगंडा’ से निपटने के लिए शायद यही सबसे कारगर विज्ञान है। ‘यूनेस्को’ जैसे संगठन पूरे संसार में इस विषय को स्थापित करने का कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को का संचार विभाग हर साल संसार के अलग-अलग देशों में जनसंचार एवं सूचना संचेतना पर बैठक आयोजित और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
संसार के बहुत सारे विकसित और विकासशील देश इस बात को समझ गए हैं कि अगर नागरिकों को तथ्यों को समझने की कला नहीं सिखाई जाती, तो सारी शिक्षा अधूरी है। विषय समाज विज्ञान का हो या शुद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग का, विद्यार्थी का ठोस ज्ञान तभी बनेगा, जब उसे तथ्यों का विश्लेषण करने आता हो। नहीं तो वह अधूरी और अधकचरी, अप्रासंगिक चीजों को भी सही मान लेगा।
कई देश तो औपचारिक शिक्षा के बाहर वयस्क लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। संसार के सबसे शक्तिशाली मीडिया नियामक इंग्लैंड के ‘आॅफ काम’ की आधिकारिक जिम्मेदारी तय की गई है कि वह अपने नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से जनसंचार एवं सूचना साक्षर बनाए। नार्कोडिक देशों ने प्राथमिक स्तर पर इस विषय को शिक्षा का हिस्सा बनाया। इस क्षेत्र में केन्या जैसे अफ्रीकी देश और कई विकासशील देश भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहां तक कि भूटान में मीडया लिटरेसी सेंटर की स्थापना की गई है।
मगर भारत का इसमें कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अव्वल तो भारत के स्कूल-कॉलेजों में इस विषय का कोई स्थान बन ही नहीं पाया है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत दुनिया का पहला देश माना जाता है, जहां ‘मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी’ से मिलते-जुलते ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ यानी आलोचनात्मक चिंतन विषय को मीमांसा, न्याय जैसे ग्रंथों के माध्यम से भरे-पूरे रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत के विभिन्न विषयों के शोध का आधार यही विषय था।
आज भी बहुत से विदेशी विद्वान मानते हैं कि अगर आलोचनात्मक चिंतन का भरपूर खजाना कहीं से मिल सकता है तो वह भारत है। प्राचीन भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में संदेशों के विश्लेषण का विज्ञान पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय के आचार्य शांतराक्षित ने उस समय के प्रोफेसरों के व्याख्यानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को फार्मूला उपलब्ध कराया था। आज वही भारत है, जहां आलोचनात्मक चिंतन विषय सिरे से गायब है।
नई शिक्षा नीति में आलोचनात्मक चिंतन को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने की बात की गई है। अगर नई शिक्षा नीति में आलोचनात्मक चिंतन और जनसंचार सूचना साक्षरता के रूप में पूर्ण विषय रख दिया जाता, तो यह और भी बेहतर होता। संभावनाएं अब भी हैं, क्योंकि दोनों का मूल ध्येय यथार्थ को जानना यानी चीजों को उनके सही भाव से समझना-सिखाना है।
यह बात गौरतलब है कि लाख तरह के विषय पढ़ाने के बावजूद विद्यार्थी को सजग, सचेत और तथ्यों को पकड़ने, स्वतंत्र सोच और अपने विवेक से निष्कर्ष निकालने वाला बौद्धिक व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि वह आलोचनात्मक चिंतन और ‘मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी’ जैसे विषयों में प्रशिक्षित न हो। भारत को अपनी शिक्षा को नए युग की जरूरत की शिक्षा बनाना है, तो इस सच्चाई को अंगीकार करना ही होगा।