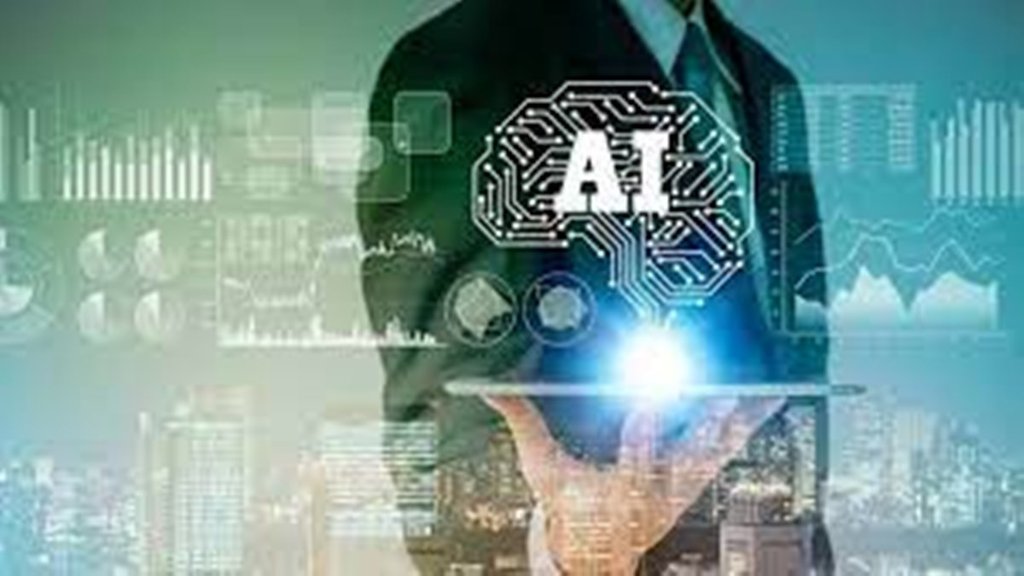कृत्रिम मेधा यानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जैसे-जैसे मानवीय जीवन की जटिलताएं बढ़ रही हैं, मनुष्य वैकल्पिक तरीकों से उनका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ देश और दुनिया की बढ़ती आबादी है, जिसके लिए संसाधनों की चिंता करनी है, वहीं मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कई काम अब कृत्रिम मेधा की मदद से किए जा रहे हैं।
आनलाइन गेम खेलने से लेकर रोगों के उपचार, सर्जरी तक में उपयोग
कृत्रिम मेधा युक्त मशीन वैसे ही काम कर रही है, जैसे मनुष्य करता है। निरंतर शोध का परिणाम है कि इस मशीन से गलती कम और काम की गति तेज हो रही है। विद्यार्थी के सीखने के तरीके के आधार पर उसको सहयोग देने, भाषा प्रसंस्करण करने, आनलाइन गेम खेलने से लेकर रोगों के उपचार, सर्जरी तक कृत्रिम मेधा की जरूरत पड़ रही है।
जान मैकार्थी ने 1956 में की थी कृत्रिम मेधा की शुरुआत
तकनीक के सहयोग से विद्यार्थियों को निर्देश और व्याख्यान दिए जा सकते हैं। कृत्रिम मेधा का उपयोग करके उत्तर कुंजी की मदद से परीक्षा का मूल्यांकन और आंकड़ों के जरिए छात्रों के परिणाम का विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है। यही नहीं, उत्तर पुस्तिका में जो गलती छात्रों से हुई है, कृत्रिम मेधा के सहयोग से उसे भी आसानी से रेखांकित किया जा सकता है। कृत्रिम मेधा की शुरुआत 1956 में जान मैकार्थी द्वारा की गई थी। इसके लिए कंप्यूटर द्वारा निर्मित रोबोटिक प्रणाली तैयार की जाती है, फिर उसे मानव मस्तिष्क के आधार पर साफ्टवेयर की मदद से प्रोग्रामिंग करके सोचने-समझने और चलाने का प्रयास किया जाता है।
कृत्रिम मेधा विश्लेषण करती है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता, समझता और सीखता है, फिर उस विश्लेषण के आधार पर अपना ‘अल्गोरिद्म’ बनाती और काम करती है। ऐसे ही यह विद्यार्थियों के कौशल और दक्षता का मूल्यांकन करके उन्हें उच्च दक्षता के लिए निर्देशित कर सकती है।
कुछ कंपनियां कृत्रिम मेधा का उपयोग करके अलग-अलग उम्र के बच्चे के लिए रुचिकर गणित-भाषा के लिए आनलाइन और वीडियो गेम बना रही हैं। भाषा के व्याकरण, शब्द और वाक्य विन्यास जैसी अशुद्धियों को ठीक कर रही हैं। इस तरह के ऐप आने से भाषा-संपादन के लिए दूसरों पर निर्भरता कम होती जा रही है।
अस्सी के दशक से पांचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर बनाने की परियोजना शुरू हुई और फिर सुपर कंप्यूटर बनने लगे। 1997 आते-आते ऐसे सुपर कंप्यूटर बन गए, जिनका मस्तिष्क सामान्य मनुष्य से तेज चलने लगा। ‘डीप ब्लू’ नामक आइबीएम के कंप्यूटर का दिमाग इतना तेज हो गया कि उसने शतरंज के एक मशहूर खिलाड़ी को हरा दिया था।
उसकी सफलता ने ऐसे कंप्यूटर बनाने का रास्ता खोला, जो कठिन गणितीय गणना, वित्तीय माडलिंग, बाजारों का रुझान, गंभीर खतरों का विश्लेषण आदि कर सकें। ‘डीप ब्लू’ के बाद की पीढ़ी के ‘वाटसन’ नामक कंप्यूटर ने फरवरी, 2011 में कृत्रिम मेधा के सहयोग से शतरंज के दो मशहूर खिलाड़ियों को लाखों लोगों के सामने हरा दिया।
आज हर जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह के कृत्रिम मेधा के माडल तैयार हैं- कुछ पूर्णत: प्रतिक्रियात्मक हैं, तो कुछ की स्मृति सीमित है। मगर जिस तरह से विकसित और विकासशील देशों में शोध जारी हैं, आने वाले दिनों में मनुष्य के मस्तिष्क को सबसे बड़ी चुनौती कृत्रिम मेधा के माडल से मिलने वाली है। नए दौर के माडल मस्तिष्क सिद्धांत और आत्म-चेतन के आधार पर कार्य करेंगे।
इसकी झलक ‘चैट बोट’ के कई विकल्पों से मिलती है। इसके कुछ प्रमुख उदहारण, अलेक्सा, गूगल का अस्सिटेंस होम, एप्पल का सीरी आदि हैं। ये सभी ‘चैट बोट’, मशीनी प्रशिक्षण और आपके दिशा-निर्देश पर काम करते हैं। ‘चैट बोट’ दो तरह के होते हैं। एक, जो मौखिक निर्देश पर काम करते हैं और दूसरे, लिखित निर्देशन पर काम करते हैं।
इन दिनों ‘चैट जीपीटी’ बहुत चर्चा में है। एक तरह का ‘कंप्यूटर साफ्टवेयर लैंग्वेज माडल’ है, जो ‘की-इनपुट कमांड’ के आधार पर जानकारी देता है। कुछ दिनों पहले इसे जारी किया गया और देखते-देखते इसकी लोकप्रियता दुनिया भर में फैल गई। आपको कोई चिट्ठी बनानी है, कोई छोटा लेख लिखना है, कोई प्रस्ताव बनाना है, यह सब काम ‘चैट जीपीटी’ दस मिनट में कर देगा! इसके आने से ऐसी आशंका है कि लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी।
इससे शोध कार्य और ‘कापी राइट’ भी प्रभावित होने वाले हैं। मान लीजिए, किसी छात्र को पर्यावरण पर एक लेख लिखना है और वह ‘चैट जीपीटी’ की मदद से वह लेख लिख दे, तो उस लेख का वास्तविक लेखक कौन हुआ, ‘चैट जीपीटी’, वह छात्र या ‘चैट जीपीटी’ ने जहां से सामग्री ली? मगर अभी यह जानना एक समस्या है कि ‘चैट जीपीटी’ कहां से सामग्री ले रहा है और वह जानकारी कितनी तथ्यपरक है?
कृत्रिम मेधा की मदद से चौबीस घंटे काम करने वाली एक मशीन मिल जाएगी। वह स्वचालित तरीके से काम करेगी और गलतियां भी कम करेगी। मगर सवाल है कि क्या यह मशीन मानवीय रचनात्मकता का मुकाबला कर पाएगी? स्कूल-कालेज-विश्वविद्यालयों के अनेक प्रशासनिक कार्य, कक्षा में हाजिरी लेना आदि कृत्रिम मेधा की मदद से होगा, लेकिन शिक्षण के लिए एक ‘हाइब्रिड माडल’ के उभरने की संभावना है।
मैथ्यू लिंच शिक्षा में कृत्रिम मेधा की बहुत संभावना देखते हैं। वे शिक्षक की पाठ योजना से लेकर भाषा सीखने, परीक्षा की तैयारी और छात्रों-अभिभावकों के साथ संवाद, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन के व्यवस्थापन आदि में इसकी उपयोगिता देखते हैं।
उच्च शिक्षा में कृत्रिम मेधा आजकल शोध कार्य में अकादमिक चोरी रोकने के लिए प्रयुक्त होती है। शोध छात्र को शोध प्रबंध के मौलिक होने का एक प्रमाणपत्र लेना होता है, तभी वह विश्वविद्यालय में अपना शोधकार्य प्रस्तुत कर पाता है। कुछ साफ्टवेयर, शोधकार्य में किसी दूसरे से ली गई एक-एक लाइन को पकड़ लेते हैं। मगर अब ‘चैट जीपीटी’ को शोध में अकादमिक लेखन के लिए उपयोगी भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके सहयोग से सामग्री का अनुवाद, लंबे लेख को संक्षेप में लिखने आदि में मदद मिल रही है। मगर इसकी सीमा यह है कि यह मौलिक विचार नहीं प्रस्तुत कर सकता। यह उपलब्ध सामग्री ही प्रस्तुत करता है और वह भी बिना संदर्भ के। इस तरह इसमें किसी और की सामग्री का इस्तेमाल होने और कभी पक्षपातपूर्ण रवैए का खतरा भी है।
भारत सरकार ने कृत्रिम मेधा के महत्त्व को पहचानते हुए शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और कुछ अन्य संस्थान अब कृत्रिम मेधा में स्नातक कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में ‘चैटबोट’, ‘रोबोटिक्स’, ‘मशीन लर्निंग’ न सिर्फ शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल हो जाएंगे, बल्कि इनके अपने काम के मूल्यांकन की एक पद्धति भी विकसित हो जाएगी। इसके बढ़ते प्रभाव से अकादमिक कार्यों की गुणवत्ता कैसी होगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
दुनिया भर में कृत्रिम मेधा, ‘रोबोटिक्स’, ‘डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग’, ‘बिग डाटा इंटेलिजेंस’, ‘रियल टाइम डाटा’ और ‘क्वांटम कम्युनिकेशन’ के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास का कार्य बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां इनका उपयोग व्यापारिक हित में कर रही हैं। कृत्रिम मेधा अब कई अरब डालर का उद्योग बन गया है।
मगर इसमें व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक की गोपनीयता भंग होने का खतरा भी है, जिसमें सुरक्षित डेटा रखना एक चिंता की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि कृत्रिम मेधा पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्य की निजता और गरिमा के लिए खतरा हो सकता है। मगर यह तो तय है कि कृत्रिम मेधा हमारे रहन-सहन, काम करने, पढ़ने-पढ़ाने, शोध के तरीकों में व्यापक बदलाव लाने वाली है।