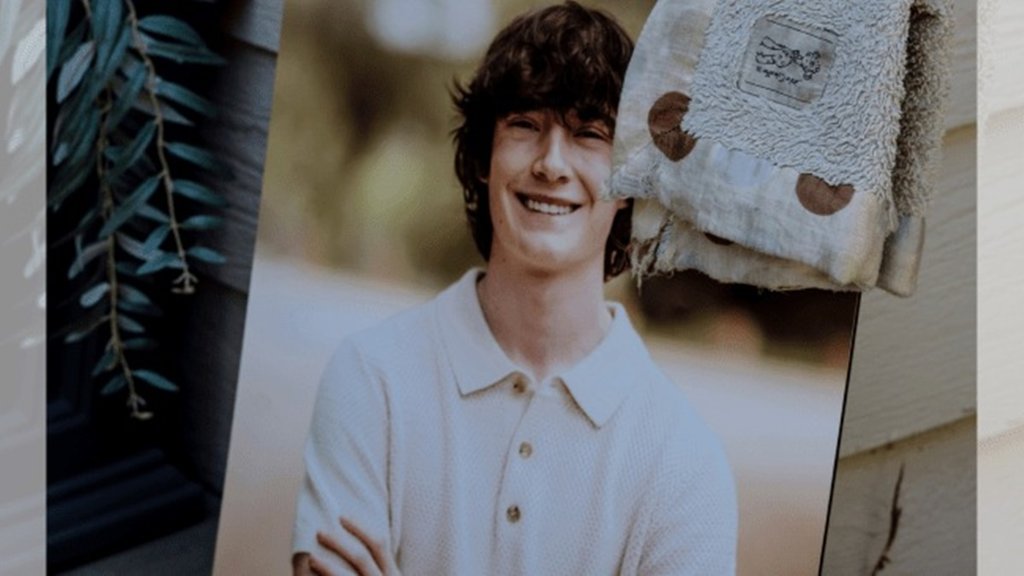वर्तमान दौर में शैक्षणिक और तकनीकी विकास की वजह से आम नागरिकों की औसत बुद्धि का स्तर दिनोंदिन तर्कसंगत होता जा रहा है। अब वह दौर नहीं रहा कि एक ने कुछ कह दिया और दूसरे ने मान लिया। हालांकि बीते समय में विभिन्न क्षेत्रों की उच्चस्तरीय शख्सियत के बोल वचन भी ‘सत्य वचन महाराज’ की मुद्रा में अकाट्य माने जाते रहे थे, लेकिन अब किसी भी तथ्य को आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता।
आम नागरिकों के जेहन में हर किसी बात पर तमाम तरह के ‘किंतु परंतु’ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो ही जाते हैं। न केवल राजनीति, बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति पाई जाती है कि किसी भी स्थापित शख्सियत की अवधारणा को सर्वमान्य नहीं माना जाता। सबकी सोचने और समझने की अपनी-अपनी क्षमता है और सबके पास अपने-अपने आधार हैं।
ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने के कारणों की पड़ताल करने पर आखिर यही साबित होता है कि नागरिकों की शैक्षणिक और तकनीकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके चलते सदियों पुरानी अवधारणाएं या तो सिरे से ही नकारी जा रही हैं या फिर उसका पालन किया भी जा रहा है तो तर्क की कसौटी पर पूरी तरह कसकर। यों भी, आज जितने अति विकसित साधन-संसाधन है, कहीं न कहीं उसके उदय में भी धर्मग्रंथों की ही कोई प्रेरणा रही होगी।
जहां तक दैनिक जनजीवन की बात है, अब आम नागरिकों को कपोलकल्पित बातों की अपेक्षा तार्किक बातों पर ही भरोसा होने लगा है। एक प्रकार से नागरिकों को अपने अच्छे-बुरे का इल्म बहुत बेहतर तरीके से होने लगा है। यह एक सुखद स्थिति है और सुनहरे कल की ओर संकेत करती है।
यह एक स्थापित तथ्य है कि राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों में किसी भी अभिमत पर हर एक की अपनी एक विशिष्ट अवधारणा हो सकती है। यह आवश्यक नहीं होता कि इन संदर्भों में हमारे दृष्टिकोण से अन्य पक्ष भी पूरी तरह से सहमत हों। प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, कभी-कभी पूर्वाग्रह की प्रबलता, दुराग्रह में तब्दील भी हो जाती है।
ऐसे में किसी भी विषय को लेकर तटस्थ दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं हो पाता। इन कारणों के चलते कालांतर में नागरिकों के बीच परस्पर वैचारिक टकराव की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। किसी भी स्थिति में असहमतियों को कुचलना आखिरकार नकारात्मक परिणाम का कारक होता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवाद से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।
कभी-कभी व्यक्ति विशेष के विचारों से अभिप्रेरित होकर हम अपने विचार निश्चित करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, नागरिकों की तर्कशक्ति में आशातीत परिपक्वता भी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति को सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी विषय पर गहन वैचारिक मंथन के बाद प्राप्त किए गए निष्कर्ष समाज की दशा और दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
मगर जब ऐसे निष्कर्ष किसी अन्य पर थोपने के प्रयास किए जाते हैं, तब वैचारिक टकराव परस्पर कटुता का कारण बन जाता है। इस स्थिति से बचने के प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि वैचारिक टकराव भी सकारात्मक परिवर्तन के कारक सिद्ध हुआ करते हैं।
इसमें संदेह नहीं कि नागरिकों की तर्कशक्ति में आमूलचूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अलग-अलग विचारधारा को देश-प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसे हम नागरिकों की राजनीतिक चेतना के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं।
आमतौर पर देश-प्रदेश के नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर आम नागरिक अपना अभिमत सुनिश्चित करते हैं, लेकिन नागरिकों का ऐसा वर्ग भी है, जो गहन वैचारिक मंथन के बाद मताधिकार के माध्यम से देश-प्रदेश की दशा और दिशा को सुनिश्चित करता है। स्पष्ट रूप से ऐसी जागृति लोकतंत्र की बुनियाद को और भी अधिक सशक्त आधार देने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन सबके मूल में मतभिन्नता की वजह से ही आखिर परिवर्तन को स्वीकार किया गया है।
सामाजिक दृष्टि से अनावश्यक रूप से जारी परंपराओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है। दरअसल, विचारधारा के टकराव से भी नए निष्कर्षों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यही कारण है कि हमने प्रत्येक रीति-रिवाज और परंपराओं का तार्किक दृष्टि से आकलन करने की शक्ति प्राप्त की है। भौतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद आम नागरिकों का विचार-दर्शन आस्था और विश्वास पर ही टिका हुआ है। यह जरूर है कि प्रगति की दौड़ में हर कोई सहभागी है। भौतिकवाद की प्रबलता नैतिकता को भी तार-तार कर रही है। इसके बावजूद, हमारी तार्किक परंपराओं का परिपालन भी बखूबी किया जा रहा है।
दुनिया में चाहे जितने परिवर्तन आए, लेकिन हम अपनी मूलभूत सभ्यता और संस्कृति से निरंतर जुड़े रहे हैं। आज भी धर्म-अध्यात्म की दुनिया में चहल-पहल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। माता-पिता के संस्कार बच्चों में परिलक्षित हो रहे हैं। हालांकि यह जरूर है कि कई बार नकारात्मकता प्रबल दिखती है, लेकिन आज भी मर्यादित जीवनशैली को बड़ी शिद्दत के साथ आत्मसात किया जा रहा है।
दरअसल, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं वैचारिक असहमतियां किसी न किसी रूप में अवश्य रही है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह कि वैचारिक मतभिन्नता का सदैव स्वागत किया जाना चाहिए।