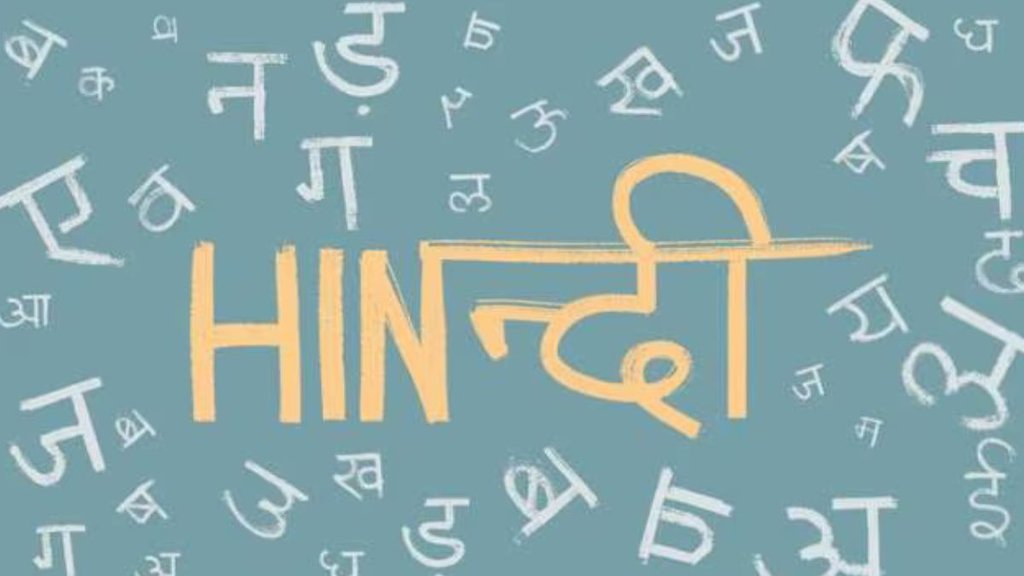भाषा और बोली के फर्क के बारे में आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि भाषा लिखी जाती है, बोलियाँ बोली जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाषा का व्याकरण होता है और बोलियों का व्याकरण नहीं होता। भाषा में साहित्य रचा जाता है और बोलियों में कोई साहित्य नहीं होता। भाषा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, बोलियाँ पढ़ी या लिखी नहीं जातीं। भाषा के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है और बोलियों के साथ हीन भावना। भाषा शुद्ध मानी जाती है जबकि बोलियाँ अशुद्ध और टेढ़ी-मेढ़ी समझी जाती हैं, वगैरह-वगैरह। लेकिन कभी आपने सोचा यह फर्क आया कहां से? इस फर्क की जड़ें क्या हैं? और क्या वाकई भाषा और बोली में कोई ऑब्जेक्टिव अंतर है भी या नहीं?
इस गुत्थी को समझने के लिए हमें चलना होगा भाषाविज्ञान के पास। भाषा विज्ञान यानी भाषाओं को वैज्ञानिक और निष्पक्ष नज़रिए से देखने की विद्या। भाषा विज्ञान के अनुसार, भाषा हमारे मस्तिष्क की वह क्षमता है जो हमारे ख्यालों और विचारों को ध्वनि या इशारों के माध्यम से प्रकट करती है। यानी हमारे मस्तिष्क की वह क्षमता जो हमें अपने ख्यालों और विचारों का इजहार करने में मदद करती है। इस परिभाषा के अनुसार, मनुष्य जाति में जन्मा हर व्यक्ति कोई न कोई भाषा बोलता है। आज तक मनुष्यता के पूरे इतिहास में कोई ऐसा कबीला, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा देश, कोई ऐसी सभ्यता नहीं मिली है, जहां भाषा का उपयोग न होता हो। अतः भाषा मनुष्य जाति का “डिफाइनिंग फीचर है”: जो मनुष्य है, वह कोई न कोई भाषा ज़रूर बोलता होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि ख्यालों और विचारों से शब्दों और वाक्यों तक का सफर कैसे तय होता है?
भाषाविज्ञान का जवाब है कि हमारे मस्तिष्क में है एक ग्रामर: मेंटल ग्रामर। ख्यालों और विचारों को शब्दों और वाक्यों में बदलने का काम यही मेंटल ग्रामर करता है, यानी मस्तिष्क का व्याकरण। और यह मेंटल ग्रामर प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में मौजूद है। यानी साफ़ बात है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, वे सब कोई न कोई भाषा बोलते हैं और उनके दिमाग में उस भाषा का मेंटल ग्रामर मौजूद है। अर्थात, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह व्याकरण, व्याकरण की किताबों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिमाग में स्टोर है। इसी व्याकरण का इस्तेमाल करके हर मनुष्य आवाज़ से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाता है। अतएव, भाषा विज्ञान ने यह साफ़ तौर पर प्रमाणित कर दिया है कि हर मनुष्य की अपनी एक भाषा है और उसके दिमाग में उस भाषा का ग्रामर मौजूद है।
तो अब सवाल उठता है कि यह भाषा और बोली का भेद पैदा कैसे हुआ? इसका जवाब है सत्ता! जी हाँ, सत्ता और राजनीति! प्रत्येक जगह के लोगों की अपनी-अपनी भाषाएं हैं, उनमें से जो भाषाएं सत्ता के केंद्र के करीब रहीं, चाहे धार्मिक सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता, उन भाषाओं को सत्ता का संरक्षण मिला, सम्मान मिला, उन भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा, कविताएं, ग़ज़लें, और कहानी-उपन्यास लिखे जाने लगे, और धीरे-धीरे वह भाषा “प्रेस्टिज” या प्रतिष्ठा का मानक बनती गई। धीरे-धीरे लोगों पर उस भाषा को सीखने का दबाव बनता गया, रोजगार के कारणों से, या खुद को “शिक्षित” और “सभ्य” दिखाने की चाह में, या कभी सिर्फ इसलिए कि सत्ता द्वारा उस भाषा के ज्ञान को ही “ज्ञान” माना जाता था।
अब हिंदी का उदाहरण लीजिए। हिंदी, खड़ी बोली का एक विकसित रूप है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (जैसे पश्चिमी यूपी) में जो भाषा बोली जाती थी, उसे खड़ी बोली कहा जाता था। वर्तमान कजाखिस्थान में जन्मे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली में सल्तनत कायम की तो उसके दरबार की भाषा (Court Language) फारसी थी। उसके बाद भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले मुस्लिम शासकों की दरबारी भाषा फ़ारसी रही।
लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद जब मुस्लिम शासक दिल्ली की स्थानीय संस्कृति के साथ घुलने-मिलने लगे, तब धीरे-धीरे उन्हें स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का ख़याल आया। शुरुआत में सिर्फ़ फ़ारसी में ही शायरी वगैरह लिखी जाती धीरे-धीरे शायरी में खड़ी बोली का भी उपयोग होने लगा। इसकी मशहूर मिसाल अमीर खुसरो की वह ग़ज़ल है, जिसका एक मिसरा फ़ारसी में है और दूसरा खड़ी बोली में। एक शेर देखा जाए:
शबान-ए-हिज्राँ दराज़ चूँ ज़ुल्फ़ ओ रोज़-ए-वसलत चूँ उम्र-ए-कोताह
सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अँधेरी रतियाँ
लोग सुनते हैं, दाद देते हैं, और धीरे-धीरे दरबार में खड़ी बोली का इस्तेमाल बढ़ने लगता है। अरबी-फ़ारसी के शब्दों की मिलावट के साथ खड़ी बोली साहित्य में, ग़ज़लों में इस्तेमाल होने लगती है। बाद में इसी अरबी-फ़ारसी मिश्रित खड़ी बोली को कभी हिंदवी, कभी हिंदी और कभी उर्दू कहा गया। खड़ी बोली के इसी रूप में मीर और मिर्ज़ा ग़ालिब जैसे बड़े-बड़े शायरों ने अपना कलाम लिखा। खुद आख़िरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने इसी भाषा में कई मशहूर ग़ज़लें कहीं। फलतः मुगल काल के अंत तक, अरबी-फ़ारसी शब्दों के मिश्रण वाली और फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, जिसे उर्दू कहा जाने लगा, एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँच चुकी थी। उसमें साहित्य रचा जाने लगा था। मुगल सत्ता के केंद्र में होने के कारण यह भाषा पूरे उत्तर भारत की लिंगुआ फ़्रैंका अर्थात संपर्क भाषा बन गई।
अगली बड़ी घटना हुई 1837 में, जब अंग्रेज़ों ने फ़ारसी के स्थान पर उर्दू को उत्तर भारत की सरकारी भाषा घोषित कर दिया। सरकारी भाषा बनने का अर्थ था कि अब सरकारी नौकरी के लिए उर्दू का जानना लाज़मी हो गया। इस तरह उर्दू पूरे उत्तर भारत में पढ़े-लिखे लोगों की भाषा बन गई। फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली इसी उर्दू को बाद में राजनीतिक और अन्य कारणों से देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा और अरबी-फ़ारसी शब्दों की जगह संस्कृत मूल के शब्दों का उपयोग होने लगा, और इस भाषा को हिंदी का नाम दिया गया।
यानी दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली, जिसे मुगल काल के अंतिम दौर में अरबी और फ़ारसी शब्दों का मिश्रण करके उर्दू बनाया गया और फ़ारसी लिपि में लिखा गया, बाद में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को लेकर हिंदी बनी, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया। शब्दों और लिपियों के इस भेद ने एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दिया, जो अपने आप में एक अलग कहानी है।
दिलचस्प बात यह है कि जब खड़ी बोली के “मानक” रूप का विकास नहीं हुआ था, उस समय उत्तर भारत के हिंदुओं के बीच साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण भाषा ब्रजभाषा थी, वही ब्रजभाषा जिसमें सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी रचनाएँ कीं। लेकिन खड़ी बोली के विकास के साथ-साथ ब्रजभाषा पीछे चली गई। और आज खड़ी बोली के विकसित रूप अर्थात हिंदी या उर्दू को भाषा कहा जाता है, जबकि खड़ी बोली के नाम में ही बोली शब्द है, और ब्रजभाषा को बोली कहा जाता है, जबकि उसके नाम में भाषा मौजूद है। यही उदाहरण इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि भाषा और बोली का विभाजन आर्टिफ़िशियल है, जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करता है।
किसी मशहूर भाषाविद् ने कहा था, “भाषा वह बोली है जिसके पास आर्मी और नेवी है।” यानी वे बोलियाँ जो सत्ता के संरक्षण में आ जाती हैं और सत्ता के क़रीब होने के कारण जिनका सम्मान बढ़ जाता है, भाषा कहलाने लगती हैं। चाहे वह हिंदी हो, बांग्ला हो या अंग्रेज़ी — सबकी लगभग एक जैसी कहानियाँ हैं।
भारत भाषाई विविधता से मालामाल देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं, मगर अफ़सोस की बात है कि सभी भाषाओं के साथ बराबरी का सुलूक नहीं होता। कुछ भाषाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो बहुत-सी भाषाओं को इस तरह हाशिए पर धकेल दिया गया है कि अब उनका अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ गया है। भाषा और बोली का यह आर्टिफ़िशियल बंटवारा इसी हाशिए पर धकेले जाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, मगही, अंगिका, बज्जिका जैसी न जाने कितनी भाषाओं को हिंदी की बोली करार देकर हाशिए पर धकेल दिया गया। इन्हें और इन जैसी अन्य भाषाओं को इतना साइडलाइन किया गया कि कई बार इन भाषाओं के बोलने वाले अपनी भाषा का नाम तक नहीं जानते, खुद अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ बंगाल और अन्य जगहों की भाषाओं के साथ भी होता रहा है।
भाषा और बोली का यह बंटवारा कितना हास्यास्पद है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट है कि मैथिली एक समय हिंदी की बोली मानी जाती थी। फिर मैथिली भाषियों के आंदोलन के बाद इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह मिली और अब मैथिली एक स्वतंत्र भाषा मानी जाती है। यही नहीं, उसी मैथिली के बोलने वाले अब अपने आसपास की भाषाओं को मैथिली की बोली करार देने के अभियान में लगे हुए हैं।
जनगणना के आँकड़ों में आप देखेंगे कि हिंदी के नीचे 50 से ज़्यादा भाषाओं को “हिंदी की बोलियाँ” बताकर हिंदी के खाते में जोड़ दिया गया है। अगर आप इन भाषाओं के बारे में जानने की कोशिश करें तो पाएँगे कि इनमें से कोई भी भाषा किसी भी एंगल से हिंदी की बोली नहीं है। जिस तरह मैथिली हिंदी की बोली नहीं है, उसी तरह ये सारी भाषाएँ भी हिंदी के दायरे से बाहर हैं और अपनी अलग पहचान की हकदार हैं।
इन तमाम बातों से यह स्पष्ट है कि भाषा और बोली का फ़र्क कोई ऑब्जेक्टिव फ़र्क नहीं है। यह फ़र्क सामाजिक और राजनीतिक कारणों से पैदा हुआ है या पैदा किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तथाकथित “भाषा” सम्मान का विषय है और “बोलियाँ” हीनता से जुड़ी हैं, या भाषाओं का व्याकरण होता है और बोलियों का नहीं। सभी भाषाएँ, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, चाहे उन्हें भाषा कहा जाए या बोली, बराबर के सम्मान और पहचान की हकदार हैं।
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 71 उम्मीदवारों का ऐलान
मैं यहाँ साफ़ करना चाहता हूँ कि मैं हिंदी के पूरे उत्तर भारत में लिंगुआ फ़्रैंका वाले किरदार का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ। हिंदी ने एक बड़े भूभाग को जोड़कर बहुत सारी सुविधाएँ पैदा की हैं, और इन सुविधाओं का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हिंदी के विकास के नाम पर बाकी भाषाओं की पहचान छीन लेना, उन्हें हाशिए पर धकेल देना — इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।
“एक देश, एक भाषा” के यूरोपीय दृष्टिकोण के विपरीत, भाषाई विविधता हमारे भारत की असली पहचान है, जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि भाषा और बोली के इस आर्टिफ़िशियल बंटवारे के आधार पर किसी भाषा को हाशिए पर न धकेला जाए, और यह बंटवारा जितना संभव हो समाप्त किया जा सके। हम ऐसा भारत बनाएं , जहां हर बच्चा अपनी मातृभाषा बोलते हुए गर्व महसूस करे, जहां बूढ़ा किसान अपनी भाषा में कहानी सुनाते हुए शर्मिंदा न हो, जहां सभी भाषाओं को बराबर का सम्मान और बराबर की पहचान मिले। यह सारी भाषाएँ हमारे देश की खूबसूरती हैं, और इस खूबसूरती को बरक़रार रखने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।
यह भी पढ़ें- ‘…तो और भी घातक होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0’, सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी
(लेखक भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं।)