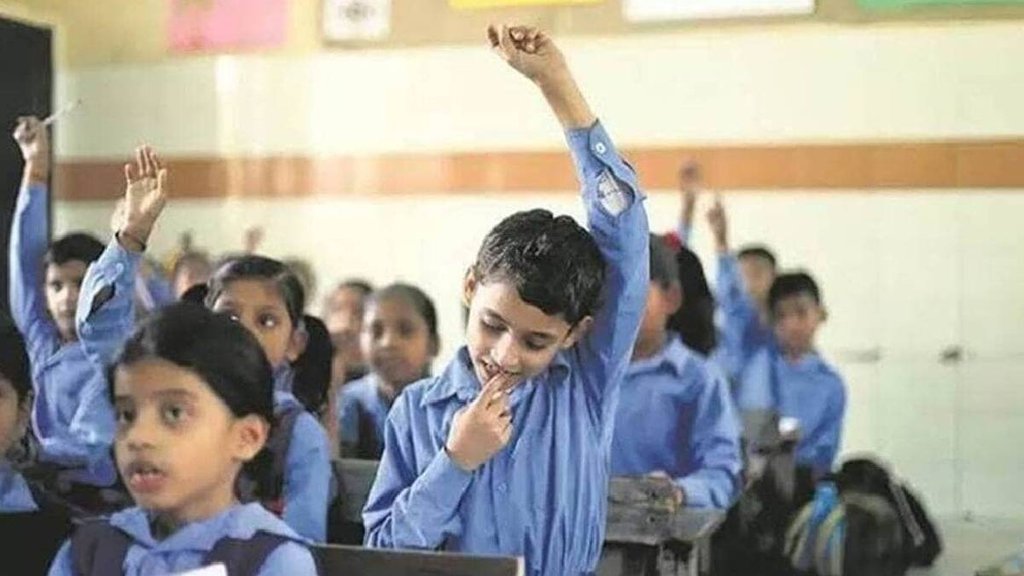दुनिया में हर वर्ष करोड़ों बच्चों और किशोरों को किसी न किसी रूप में शारीरिक दंड झेलना पड़ता है। प्राय: इसे ‘अनुशासन’ या ‘सुधार’ का उपाय कह दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि इस तरह के कृत्य बच्चों के लिए दर्द, अपमान और मानसिक आघात की वजह बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की एक हालिया रपट में कहा गया है कि बच्चों पर आक्रामक होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इससे न तो बच्चों का व्यवहार सुधरता है और न ही उनका जीवन बेहतर बनता है।
उलटे, यह उनके व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। भारत में भी बच्चों को शारीरिक दंड देना एक बड़ी समस्या है। घर से लेकर स्कूलों तक बच्चों के प्रति आक्रामक व्यवहार आम बात है। कई लोगों को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच इस तरह के व्यवहार से बच्चे सुधरते हैं, या फिर उनमें हीन भावना और हिंसा की मानसिकता घर कर जाती है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट में इस सवाल का स्पष्ट जवाब है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में अठारह साल से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे हर वर्ष किसी न किसी रूप में शारीरिक दंड का शिकार होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शारीरिक सजा को अक्सर हम केवल मारपीट तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं व्यापक है। बच्चों के कान खींचना, उन्हें घुटनों पर बैठाना, घंटों खड़ा रखना, अपमानित करना, भूखा रखना या ऐसी कोई भी सजा जो उन्हें शारीरिक या मानसिक पीड़ा देती है, सब इसी श्रेणी में आती है। बच्चों पर हाथ उठाने का मतलब उनकी गरिमा को चोट पहुंचाना भी है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा है कि यह सब केवल घरों में ही नहीं होता, बल्कि स्कूलों और छात्रावासों में भी ‘अनुशासन’ के नाम पर इस तरह की आक्रामकता अक्सर देखने को मिलती है।
बच्चों के तनाव को बढ़ा देती है पिटाई
शारीरिक दंड केवल दर्द ही नहीं देता, बल्कि यह बच्चों के दिल और दिमाग पर स्थायी घाव छोड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बच्चों को शारीरिक दंड झेलना पड़ता है, उनके विकास की राह पर आगे बढ़ने की संभावना अपने साथियों की तुलना में चौबीस फीसद कम होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पिटाई बच्चों के तनाव को बढ़ा देती है, जिससे मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रभावित होते हैं। इसका असर केवल पढ़ाई-लिखाई पर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ता है। ऐसे बच्चे अक्सर गुमसुम और सहमे हुए रहते हैं। वे अपनी बात कहने से डरते हैं और उनमें चिंता और अवसाद गहराने लगता है।
इससे एक और अहम पहलू उजागर होता है कि शारीरिक दंड हिंसा को समाज में सामान्य बना देता है। जिन बच्चों को बचपन में आक्रामक व्यवहार झेलना पड़ता है, वे बड़े होकर वही तरीका अपनाते हैं। यानी यह चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर जब खुद माता-पिता बनते हैं, तो वे भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह पेश आते हैं। कई बार यही बच्चे हिंसक प्रवृत्तियों के साथ समाज में अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। शारीरिक दंड बच्चों के अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने इसे उस सजा के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग कर बच्चों को दर्द या परेशानी पहुंचाई जाती है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में दो से चौदह वर्ष की आयु के लगभग साठ फीसद बच्चों को घर और स्कूल में नियमित रूप से शारीरिक दंड का सामना करना पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शारीरिक दंड के कई रूप बताए हैं। इनमें बच्चों को असुविधाजनक मुद्रा में खड़ा करना, सिर पर बैग रख कर बैठाना, घुटनों के बल बैठाना और उन्हें बंद करके रखना शामिल है।
कई मामलों में तो बच्चों को गंवानी पड़ी है अपनी जान
दरअसल, बच्चों की पिटाई केवल एक घर या एक कक्षा की समस्या नहीं है। यह समाज के भीतर हिंसा की संस्कृति को जड़ से सींचने का काम करती है। दुनिया के सड़सठ देशों में शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारत में भी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में बच्चों की पिटाई गैर कानूनी है। मगर कानून और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा है। इसका प्रमाण स्कूलों में आए दिन बच्चों से मारपीट की घटनाएं हैं। कई मामलों में तो बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इसी वर्ष मई में प्रयागराज के एक स्कूल में नर्सरी के एक बच्चे को शिक्षिकाओं ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बीते अप्रैल में राजस्थान के प्रतापगढ़ में निजी स्कूल में एक बच्ची को न केवल मारा-पीटा गया, बल्कि उसके हाथ-पांव बांध कर घंटों बैठाए रखा गया। वर्ष 2022 में राजस्थान के जालोर स्थित एक स्कूल में शिक्षक द्वारा मासूम की पिटाई का मामला सामने आया था। ऐसी घटनाओं की पूरी शृंखला है।
ग्रामीण इलाकों और कस्बों के स्कूलों में अब भी बच्चों को पीटना आम बात है। अफसोस है कि घरों में माता-पिता भी बच्चों को मारना ‘जरूरी’ मानते हैं। हम अक्सर इन्हें ‘सामान्य’ मान कर नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कागज पर लिखे कानून से कोई बदलाव नहीं होगा। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि पिटाई से अनुशासन आता है। अगर पिटाई नहीं की जाए तो अनुशासन कैसे संभव है? यह गलत धारणा है, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार के बिना भी उन्हें सही दिशा दी जा सकती है। सकारात्मक अनुशासन इसका विकल्प हो सकता है। इसके तहत बच्चों से संवाद कर उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं। उन्हें यह बताना जरूरी है कि कौन-सा काम क्यों गलत है। बच्चों के साथ धैर्य से पेश आना होगा। नासमझी में बच्चे गलतियां करते हैं। जब वे गलती करें, तो उन्हें डांटने- फटकारने के बजाय प्यार से समझाया जाना चाहिए।
यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे वही सीखते हैं, जो देखते हैं। अगर घर और विद्यालय में उन्हें सम्मान और प्यार मिलेगा, तो वे भी ऐसा ही आचरण करेंगे। अच्छे व्यवहार पर तारीफ और प्रोत्साहन बच्चों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। स्कूलों में नियम और सीमाएं आवश्यक हैं, पर उन्हें बच्चों को आतंकित करके नहीं, बल्कि विश्वास और समझ-बूझ से लागू करने की जरूरत है। जो शिक्षक आदतन बच्चों को शारीरिक सजा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मासूम बच्चों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में जिम्मेदारी को केवल माता-पिता अथवा शिक्षकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है। समूचे समाज को यह मानना होगा कि बच्चों के साथ आक्रामक व्यवहार अनुशासन का साधन नहीं, बल्कि हिंसा है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं। सम्मान और सुरक्षा के साथ बड़े होना उनका अधिकार है। यह अधिकार उनसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जाना चाहिए।