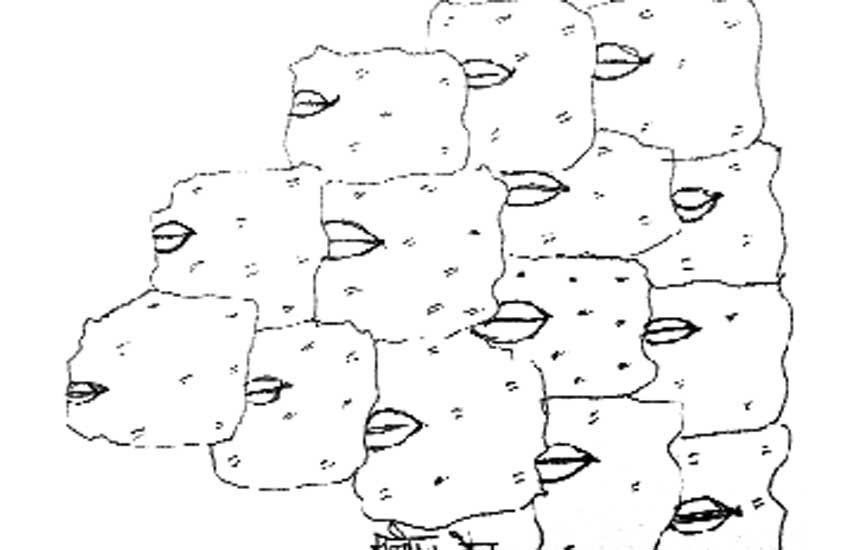भारत में बुनियादी शिक्षा की हालत चिंताजनक है। नामांकन दर तो बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता की हालत खस्ता है। आजादी के देश की साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी, 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत बढ़कर 74.04 हो गया। इन सब सफलता के बीच चिंता का विषय यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। देश में शिक्षा के लिए नीतियां, कार्यक्रम और बजट का वर्गीकरण तो अच्छी तरह से किया जाता है। मगर जब उन नीतियों के क्रियान्वयन की बात आती है तो सारा तंत्र विफल हो जाता है।
सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। इस समय हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन का प्रतिशत लगभग 96 प्रतिशत है, जबकि दूसरी ओर एनुअल स्टेट्स आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर)कहती है कि लगभग 92 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता। शिक्षा के इसी स्तर को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया की सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को काफी सराहना मिली।
लेकिन जब इसके क्रियान्वन की बात आई तो इसके विरोध में भी आवाज उठने लगी। इस तरह से यह आदेश भी कागजों की खूबसूरती बढ़ाने और लोगों की चर्चा तक सीमित रह गया। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि आज बड़ी संख्या में नेताओं, अफसरों, व्यापारियों और प्रशासनिक वर्ग लोगों के ही निजी विद्यालय चल रहे हैं, उनमें समृद्ध परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनसे मोटी कमाई हो रही है। सरकारी विद्यालयों में केवल गरीब घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। इन विद्यालयों की देखभाल का जिम्मा भी इन्हीं नेताओं और प्रशासनिक वर्गों पर ही रहता है, जिसे ये ठीक से पूरा नहीं करते। नतीजतन, शिक्षा की नींव कमजोर होती जाती है।
प्राथमिक विद्यालय संसाधनों की कमी से लंबे समय से जूझते रहे हैं। वर्तमान में छह लाख, नवासी हजार शिक्षकों की प्राथमिक विद्यालयों में है और केवल तिरेपन प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। असर-2014 के अनुसार देश में 49.3 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र-शिक्षक अनुपात ठीक है। इन विद्यालयों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी का सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।
असर के ही अनुसार कक्षा-तीन से 78 प्रतिशत और कक्षा-पांच के 50 प्रतिशत बच्चे कक्षा-दो की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। कक्षा-पांच के 26 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घटाना का प्रश्न हल करना आता है। पूर्ण साक्षारता प्राप्त करने के साथ उसके स्तर में सुधार प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा की गुणवत्ता में देश में निरंतर कमी क्यों हो रही है, इसके कारणों को खोजना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों में कहा गया है कि सरकारें चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था 26 जनवरी 1960 तक कर देगी। लेकिन आजादी के अड़सठ वर्ष बीत जाने पर भी यह सपना अधूरा है। एक और बात चिंतनीय है कि हमारे देश में लोगों को साक्षर बनाने की बात हो रही है। साक्षर का अर्थ इतना सा है जिसे अक्षर का ज्ञान हो, जो अपना हस्ताक्षर कर लेता है, उसे जनगणना में शिक्षित का दर्जा दे दिया जाता है। इससे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कोरी कल्पना ही है।
हमारी नीतियां दूरदर्शी क्यों नहीं हैं? क्यों ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती जिसमें साक्षरता के साथ-साथ गुणवत्ता का भी समन्वय हो, जो लोगों का चारित्रिक-नैतिक विकास करे सके, उन्हें रोजगार दे सके। सरकारी तंत्र भ्रष्ट व्यवस्था से व्याप्त है। मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं भी बच्चों को सरकारी विद्यालयों तक खींचने में नाकाम हैं। गुणवत्ता के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मान लिया गया है कि सरकारी व्यवस्था तो बस गई-गुजरी है। बदलाव करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो बदलता कुछ भी नहीं, लेकिन वह स्वयं बदल जाता है।
यह सही है की व्यवस्था में सुधार कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता और न ही सरकार सब कुछ कर सकती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार की नीतियों में भी दूरदर्शिता और व्यापकता का होना बहुत जरूरी है। केवल मकसद पूरा करने के लिए किया गया काम कल्याणकारी नहीं हो सकता। देश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का कर्त्तव्य है और उसे यह समझना होगा, देश में समान शिक्षा प्रणाली के बिना शिक्षा में असमानता के दुश्चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता।
देश के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि गरीब, शोषित, सर्वहारा और वंचित वर्गों को वे सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जो उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक हों। शिक्षा अधिनियम -2009 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों से गैरशिक्षण कार्य न कराया जाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बाद भी जनगणना, पोलियो ड्राप और चुनाव में इन अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। सरकारी विद्यालयों के बच्चों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी है, जो कि उन्हें नहीं मिलता। इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक भी इन बच्चों को उपेक्षा की नजर से देखते हैं। समान शिक्षा प्रणाली लागू करके, शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।