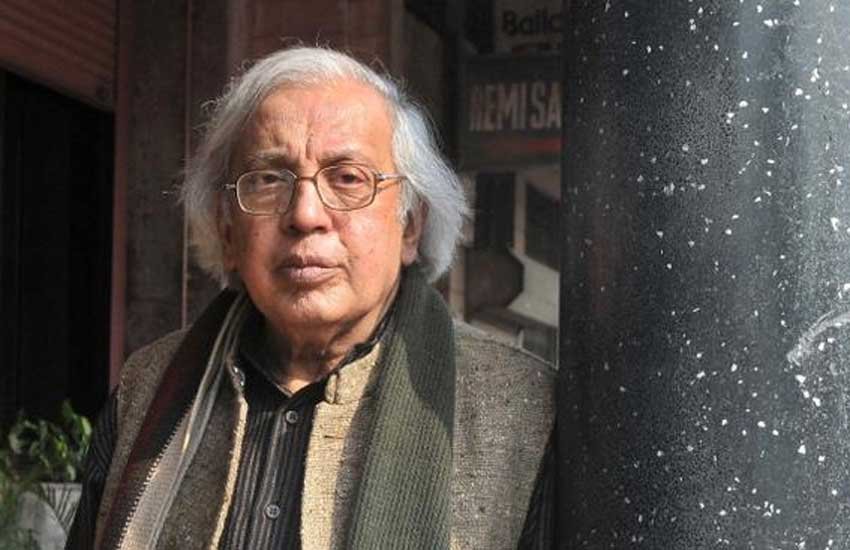हिंदी गजल को हिसाब में न लेने का आरोप जिन लेखकों पर लग सकता है उनमें मैं भी एक हूं। इसके पीछे दो पूर्वग्रह काम करते रहे हैं: पहला तो यह कि मैं उर्दू गजल से इतना मुत्तासिर रहा हूं कि मुझे हिंदी गजल की तरफ कभी ध्यान देने का प्रलोभन नहीं हुआ। दूसरे, मैं पिछले लगभग पचास वर्षों में लिखी गई तथाकथित छंदबद्ध कविता, जिसमें गीत, गजल आदि शामिल हैं, विचारणीय नहीं मानता रहा हूं, कम से कम अपनी रुचि और दृष्टि की सीमाओं के रहते। इसका एक दुष्परिणाम यह है कि मैंने हिंदी गजल को ध्यान से नहीं पढ़ा। कुछ महत्त्वपूर्ण कवियों जैसे निराला, शमशेर, त्रिलोचन आदि ने भी गजलें लिखी हैं, पर वे उनके कृतित्व का महत्त्वपूर्ण या निर्णायक हिस्सा नहीं रही हैं। अकेले दुष्यंत कुमार इसके अपवाद रहे हैं। इसलिए जब ‘अ लाव’ के कवि-संपादक रामकुमार कृषक ने मुझसे अपनी पत्रिका के विशेषांक के लिए हिंदी गजल पर कुछ लिखने का आग्रह किया तो मैंने कोशिश की, पर पर्याप्त अनुभव के अभाव के कारण कुछ बात बन नहीं पाई।
बहरहाल, समकालीन हिंदी गजल पर लगभग पांच सौ पृष्ठों की सामग्री लिए हुए ‘अ लाव’ का विशेषांक आ गया। उसमें प्रयत्न हिंदी गजलों का चयन देने पर नहीं, उन पर आलोचनात्मक ध्यान देने पर केंद्रित है। एक बात कई ढंग से सामने आती है कि उर्दू गजल का सहचर होते हुए भी हिंदी गजल का अपना स्वतंत्र और समृद्ध अस्तित्व है। और उसमें उर्दू परंपरा की अंतर्ध्वनियां भले हैं, पर असल अनुगूंज हिंदी की अपनी परंपरा की है। हिंदी गजल सिर्फ एक पारंपरिक संरचना भर नहीं है उसमें आधुनिकता की घुसपैठ भी लगातार होती रही है और हिंदी गजल में छंद के स्तर पर शायद उर्दू से अधिक विविधता है और उसमें शब्दसंपदा भी किसी हद तक अधिक विपुल है, क्योंकि वह दोनों भाषाओं से अभिव्यक्तियां, मुहावरे, बिंब, छवियां आदि लेती रही है। अच्छा यह है देखना कि शायद उर्दू गजल की ही तरह हिंदी गजल की दुनिया निरे रूमान, नास्टेल्जिया, नाउम्मीदी आदि तक महदूद नहीं रही है। भावों और अनुभवों के स्तर पर उसमें पर्याप्त विविधता है। कुल मिलाकर यह कि इस विशेषांक से हिंदी गजल को देखने-समझने की उत्तेजना होती है और उसके लिए कई दिशाओं के संकेत भी मिलते हैं।
अलबत्ता एक बात थोड़ी अखरती है। गजल को समझने के जो औजार इतने सारे आलोचकों ने अपनाए हैं उनमें प्राय: कोई नयापन या किसी विधि या सिद्धांत का पुनराविष्कार नजर नहीं आता। अगर गजल ने हिंदी कविता में कुछ जोड़ा है जो उसके पास अन्यथा नहीं था, तो उसे समझने-समझाने-सराहने वाली आलोचना हमारी आलोचना में कुछ नया जोड़ने में क्यों कोई दिलचस्पी नहीं रख पाई है? हो तो यह भी सकता है कि इस दिलचस्पी के निशान मेरी निगाह देख पाने से चूक रही हो।
पुणे में ‘कलाछाया’
हम इन दिनों एक के बाद एक सार्वजनिक संस्थान के धूमिल या ध्वस्त होते देखने के इतना अभ्यस्त और उससे इस कदर त्रस्त रहते हैं कि कई बार कुछ लोग निजी पहल और प्रयत्न से सांस्कृतिक संस्था-व्यवस्था में जो उजला-अच्छा कर पाते हैं उसे हिसाब में लेने से चूक जाते हैं। यह अनुभव गहराई से हुआ, जब पुणे की संस्था ‘कलाछाया’ की अर्द्धशती के समापन समारोह में मूर्धन्य कथक-नर्तक गुरु बिरजू महाराज के साथ शिरकत करने का अवसर मिला।
उनकी शिष्या नर्तक प्रभा मराठे ने तबला-वादक भरत जंगम के साथ लंबा संघर्ष कर अपनी मूलत: नृत्य-संस्था का कई दिशाओं में विस्तार करते हुए उसका एक सुकल्पित-नियोजित परिसर बना लिया है, जिसमें नृत्य के अलावा संगीत आदि की शिक्षा की व्यवस्था है; एक कलादीर्घा है और एक आत्मीय सभागार भी: रिहर्सल के लिए अलग जगह भी है। प्रभा को शुरू से ही पंडित भीमसेन जोशी संगीत-रचनाकार भास्कर चंदावरकर, वास्तुकार जयंत नचिकेता आदि का सहयोग मिला। शायद ही भारत में कहीं और ‘कलाछाया’ जैसा अपना परिसर किसी नृत्य संस्था के पास हो। यह निश्चय ही सांस्कृतिक आशा और संभावना का एक उजला मुकाम है। अपनी आयु के अस्सी वर्ष पर पहुंची प्रभाजी ने अब जिम्मेदारी युवतर पीढ़ी के अपने विश्वसनीय कलाकारों को सौंपने की घोषणा भी की। इस तरह उन्होंने व्यवस्थित, दृष्टि और नई ऊर्जा से संपन्न उत्तराधिकार भी सुनिश्चित कर लिया है।
समारोह में कलाछाया के युवा नर्तकों के काम को देखने का अवसर मिला। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कीर्तन परंपरा का सुघर और कल्पनाशील उपयोग करते हुए रामकथा पर एकाग्र एक नृत्यनाटिका प्रभावशाली थी: उसमें कीर्तनकार सूत्रधार की तरह व्यवहार करता है और कथा को वचनों और उद्धरणों द्वारा आगे बढ़ाता-जोड़ता चलता है। मराठी कविता पर केंद्रित एकल नृत्य भी मर्म भरा था। अगली शाम शाश्वती सेन का एकल प्रदर्शन और बिरजू महाराज का गायन और भाव-प्रदर्शन हुए। चूंकि सभागार में नजदीक से देख-सुन पाना संभव है और कलाछाया ने इतने वर्षों से प्रयत्नरत रहने से एक अच्छा-खासा रसिक समाज विकसित कर लिया है।
शाश्वती के नृत्य में बारीकी के अलावा ऊर्जा और कई ऐसी चीजें थीं जो आमतौर पर बड़े रंगमंच पर दिखाई-नाची नहीं जा सकतीं। बिरजू महाराज इस उमर में भी लय पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं और उससे लगातार खेलना उन्हें बखूबी आता है। कथक एक स्तर पर शारीरिक अंगों का विस्तार करता है: वह जैसे देह की सीमाओं को लांघ लेता है। बिरजू महाराज ने अपने पिता अच्छन महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। तबला-वादक अल्ला रक्खा खां की एक मूर्ति पहले से ही प्रतिष्ठित है। अब मंच के दोनों ओर दो मूर्धन्य हैं, जो इस मंच को सच्ची गरिमा देने का एक अच्छा उपक्रम है।