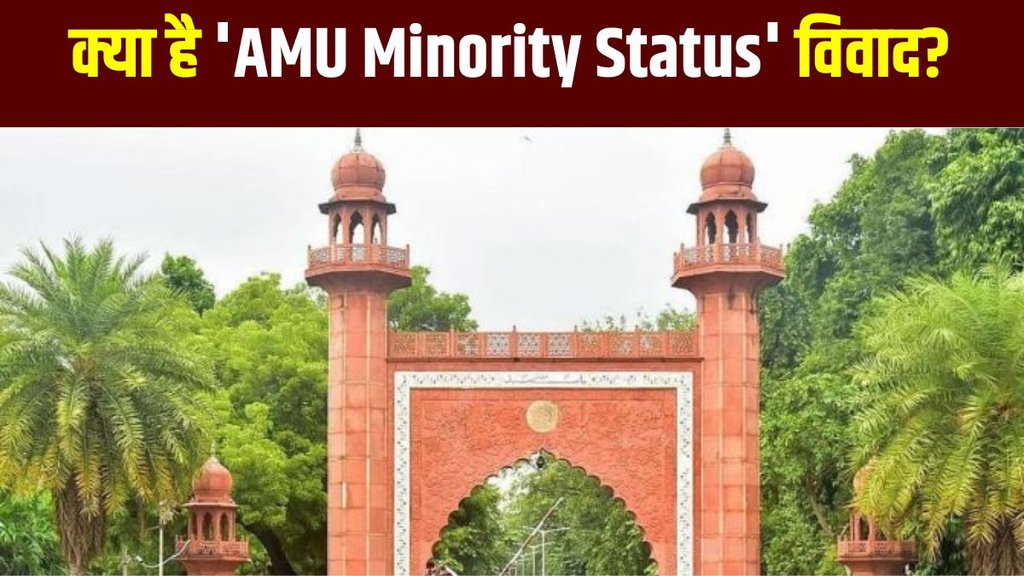अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के ‘अल्पसंख्यक दर्जे’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जहां बीते दिन केंद्र सरकार ने कहा है कि 1920 में गठन के समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा (Minority Status) छोड़ा था।
केंद्र सरकार के इस दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या जब इसे 1920 एएमयू अधिनियम के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया था तब संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो गया था या नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
क्या है पूरा मामला?
संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को यह तलकीन की जाती है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने की नजर से ऐसे संस्थानों को फंड उपलब्ध कराएगी और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से की थी। इसे शुरुआत में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एमओए) भी कहा गया। 1920 में संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और एमओए कॉलेज की सभी संपत्तियां इसे ट्रांसफर कर दी गई। इसे एएमयू एक्ट कहा गया-1920 कहा गया।
कब शुरू हुआ कानूनी विवाद?
एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति (Minority Status) पर कानूनी विवाद 1967 से शुरू होता है जब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केएन वांचू के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट (एस. अज़ीज़ बाशा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में) 1920 के एएमयू एक्ट में 1951 और 1965 में किए गए बदलावों की समीक्षा कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर समीक्षा कर रहा था कि एएमयू एक्ट में संशोधन कितने सही थे और कितने गलत? उदाहरण के लिए मूल रूप से 1920 के अधिनियम में कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। लेकिन 1951 में इसे बदलकर ‘लॉर्ड रेक्टर’ के स्थान पर ‘विज़िटर’ कर दिया गया और माना गया कि यह विज़िटर भारत का राष्ट्रपति होगा। एक प्रावधान ऐसा भी आया जिससे गैर-मुसलमानों को भी एएमयू कोर्ट में शामिल होने की अनुमति मिल गई।
ऐसे बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस आधार पर तर्क दिया कि मुसलमानों ने एएमयू की स्थापना की और इसलिए उन्हें इसका प्रबंधन करने का अधिकार है। इन संशोधनों की चुनौती पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर, 1967 को कहा कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा की गई थी और न ही इसका संचालन उनके द्वारा किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसका असर यह हुआ कि 1981 में एएमयू अधिनियम में एक संशोधन पेश किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से इसकी अल्पसंख्यक स्थिति की पुष्टि की गई। संशोधन में धारा 2(एल) और उपधारा 5(2)(सी) पेश की गई। जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान था और बाद में इसे एएमयू के रूप में शामिल किया गया।
अब क्या विवाद है?
साल 2005 में एएमयू ने एक आरक्षण नीति लागू की जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की गईं। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में में चुनौती दी गई। जहां यह फैसला पलट दिया गया और अदालत ने तर्क दिया कि एएमयू विशेष आरक्षण बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है। इसके बाद 2006 में केंद्र सरकार की एक याचिका सहित आठ याचिकाओं के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई।
12 फरवरी, 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के पास भेज दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।