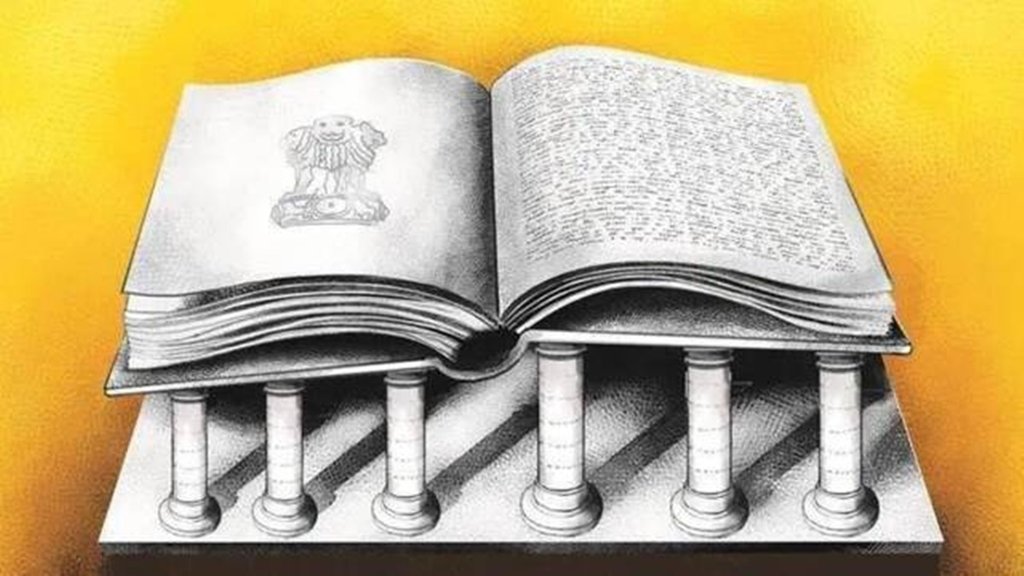भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर एक पूरा अध्याय है। अध्याय चार में दिए गए अट्ठारह अनुच्छेदों में अनुच्छेद 44 भी एक है। समानता और भेदभाव दूर करने की दृष्टि से अनुच्छेद 38(2) में वर्णित निर्देशों के बिंदु आय में असमानता को कम करने, ओहदों, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण हैं।
सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि से अनुच्छेद 39 में वर्णित निर्देश इस अध्याय का केंद्रीय स्तंभ हैं। अनुच्छेद 43 राज्य को ‘जीविका के साधन’ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, और इससे लाखों कामकाजी लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हैं।
मगर अफसोस कि इन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर शायद ही कोई बहस होती है। वे सरकार के एजंडे में ही नहीं हैं। आरएसएस-भाजपा के एजंडे और सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों की बदौलत अकेले अनुच्छेद 44 ने ही पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर कब्जा कर लिया है।
शब्दों का अर्थ होता है
आइए, पहले अनुच्छेद 44 की भाषा पर नजर डालते हैं: ‘राज्य संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।’ शब्दों का अपना अर्थ होता है। ऐलिस को दिए हंप्टी डंप्टी के जवाब की तरह ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ‘इसका अर्थ वही होगा, जो मैं निकालूं’। ‘समान’ का अर्थ ‘आम’ नहीं है।
इसमें कहा गया है कि ‘सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा’ न कि ‘सुनिश्चित करेगा’। बाबा साहेब आंबेडकर और उनके सहयोगी नासमझ नहीं थे। उन्हें भारतीय जन के इतिहास, धर्म, जातीय विभेद, सामाजिक और पारिवारिक बनावट, सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति-रिवाज आदि की गहरी समझ थी, और उन्होंने चौथे अध्याय के शब्दों को बड़ी सावधानी से चुना था।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ‘पर्सनल ला’ का संक्षिप्त रूप है। इसमें चार विषयों से संबंधित कानून हैं: विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, अल्पसंख्यक और संरक्षकत्व तथा दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण। इस देश में सदियों से, विभिन्न वर्गों के लोगों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग ढंग से व्यक्तिगत कानूनों का विकास हुआ है। शासकों ने इनके विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक बनावट, उर्वरता, प्रवासन और विदेशी प्रभावों का भी व्यक्तिगत कानूनों पर असर पड़ा।
सुधारों की शुरुआत
आज ‘पर्सनल ला’ जिस रूप में मौजूद है, उसमें लैंगिक भेदभाव और गैर-लैंगिक भेदभाव भी हैं। उसमें अवैज्ञानिक और हानिकारक व्यवहार भी मौजूद हैं। कुछ निंदनीय सामाजिक प्रथाएं और रीति-रिवाज भी हैं। निस्संदेह, व्यक्तिगत कानूनों के इन पहलुओं में सुधार की जरूरत है।
‘पर्सनल ला’ में सुधार कोई नई बात नहीं है। संविधान निर्माण के बाद से ही यह राष्ट्रीय एजंडे में रहा है। यह भारत की पहली संसद (1952-57) की शीर्ष चिंताओं में से एक था। इसमें सुधार का समर्थन करने वालों में जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब आंबेडकर भी थे। तब रूढ़िवादी लोगों और विपक्ष के विरोध का सामना करते हुए हिंदू कानून में सुधार करके चार प्रमुख कानून पारित और संहिताबद्ध किए गए:
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- हिंदू अल्पसंख्यक तथा संरक्षकत्व अधिनियम, 1956
- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
एक युवा राष्ट्र ने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार का उल्लेखनीय काम किया था। यह एक क्रांतिकारी काम था, लेकिन कुछ पहलुओं पर क्रांति होनी बाकी रह गई। उसमें से सभी भेदभावपूर्ण प्रावधान नहीं हटाए गए। उसमें हिंदू अविभाजित परिवार को एक कानूनी इकाई के रूप में स्वीकार किया गया; विवाहों में अपनाए जाने वाले रीति-रिवाजों और व्यवहारों को अपवाद मान लिया गया। अंतिम उल्लेख महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अधिकांश विवाह रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न होते हैं।
इसके बाद 1961, 1962, 1964, 1976, 1978, 1999, 2001 और 2003 में कुछ और संशोधन किए गए। 2005 से 2008 के बीच, यूपीए सरकार ने कई सुधार किए। चार अधिनियमों (ऊपर वर्णित) में से तीन में संशोधन किया गया। उनमें सबसे क्रांतिकारी संशोधन था संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार प्रदान करना।
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और भरण-पोषण तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 जैसे नए कानून पारित किए गए। इस तरह न्यायालयों के कदम उन जगहों पर भी पड़े, जहां विधायी निकाय जाने से झिझकते थे। 22 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘तलाक-ए-बिद्दत’ (तीन तलाक) की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर आघात किया।
इक्कीसवें विधि आयोग की सिफारिशें
जब हमारा सामना जनजातीय लोगों के व्यक्तिगत कानूनों से हुआ, तो हमें ठिठकना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 366, खंड 25 के तहत ऊपर वर्णित चार अधिनियमों में से कोई भी अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की छठी अनुसूची को जोड़ा गया, और उसमें एक पैराग्राफ में इन राज्यों की जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को विरासत, विवाह और तलाक तथा सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गईं।
उसमें धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करने के मकसद से नगालैंड (अनुच्छेद 371 ए), सिक्किम (अनुच्छेद 371 एफ) और मिजोरम (अनुच्छेद 371 जी) के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ऐसे ही विशेष प्रावधानों की मांग छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी निकायों द्वारा भी उठाई गई है।
निश्चित रूप से व्यक्तिगत कानूनों में और अधिक सुधार की जरूरत है। इक्कीसवें विधि आयोग ने सलाह दी थी कि: ‘‘विभेदकारी कानूनों को सुधारने की जरूरत है, न कि यूसीसी लाने की, इस स्तर पर न तो इसकी कोई जरूरत है और न ही यह वांछनीय है… सांस्कृतिक विविधता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एकरूपता का हमारा आग्रह देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है।’’
माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को दो हिस्सों में बांट दिया है- यूसीसी पर आप ‘सहमत’ हैं या ‘असहमत’। यह दृष्टिकोण यही साबित करता है कि भारत के लोग गूंगी भेड़ों की तरह हैं। सुधारों को लेकर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित करना होगा, मुसलिम कानूनों सहित सभी व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों को लेकर सार्थक बातचीत शुरू करने की जरूरत है। मुख्य शब्द है ‘सुधार’, न कि ‘एकसमान’।