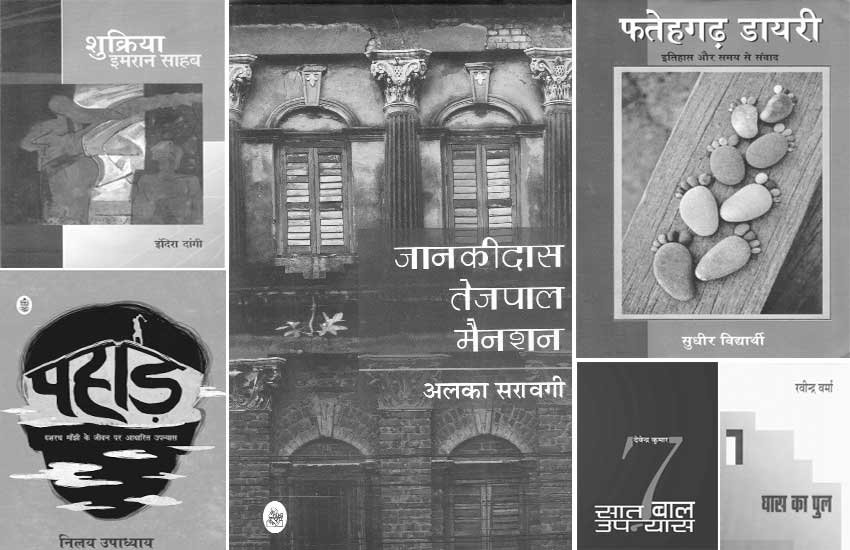असहमतियों और प्रतिरोध के सुर का खिताब पा चुके जेएनयू परिसर में जब ‘सामाजिक बदलाव में साहित्यिक पत्रकारिता की भूमिका’ पर बात करने का बुलावा आया तो सबसे पहले विषय से ही असहमति और प्रतिरोध की भावना आई। माहौल और संस्थागत संस्कृति का असर कहें कि जेएनयू परिसर में कदम रखते ही आप उम्मीदों से लबरेज होते हैं। और खासकर, तब जब सोशल मीडिया ने युवाओं को इस बात में उलझाए रखा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तो साहित्य और समाज पर चर्चा सुनने के लिए बैठे युवा चेहरे एक भरोसा पैदा करते हैं जो हालिया चुनावों के बरक्स इस मंथन में जुटे हैं कि भारतीय राजनीति में विकल्प को किसने मारा? पत्रकारिता और साहित्य को आखिर एक तराजू पर तौलने की कोशिश क्यों? अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों में बात करें तो साहित्य की तुलना में पत्रकारिता एक आधुनिक विधा है। साहित्य की एक लंबी परंपरा रही है, पत्रकारिता का इतिहास बहुत ही छोटा है। पत्रकारिता का संबंध माध्यम से है। प्रिंट माध्यम के विकास के बाद ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई। प्रिंट के माध्यम से पत्रकारिता आने के बाद गद्य के नए माध्यम की भी शुरुआत होती है। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने साहित्य की कई विधाओं को जन्म भी दिया। इसलिए साहित्य की कई विधाओं को पत्रकारिता का हिस्सा मान लिया जाता है लेकिन वह पत्रकारिता नहीं है।
साहित्य से इतर पत्रकारिता का एक लक्ष्य है। और यह लक्ष्य देश और काल से संबंधित है। देश और काल से पत्रकारिता का संबंध ठोस रूप में है काल्पनिक नहीं। और इसके उलट साहित्य का सारा कार्यकलाप ही कल्पना पर आधारित है। देश-काल सापेक्ष वह भी है, लेकिन काल्पनिक। पत्रकारिता के साथ कल्पनाशीलता संभव नहीं है। यह ठोस जीवन की सच्चाई है। सूचना पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। और, साहित्य का मूल भाव संवेदना है। साहित्य भाव प्रधान है तो पत्रकारिता तथ्य प्रधान। हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता की छवि क्या है? वह अखबार, जिसके संपादक साहित्यकार हैं या साहित्य पर लिखते हैं। या वह अखबार जहां रविवार को साहित्य के पन्ने पर कविता, कहानी और संस्मरण छपते हैं। परिचर्चा में कहा गया कि आजादी के पहले पत्रकारिता बड़ी जिम्मेदारी का काम थी। तो आज यह ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी का काम है। औपनिवेशिक काल में आपका शत्रु आपके सामने मूर्त रूप में खड़ा था। लेकिन आज हमारे इतने दुश्मन हैं कि आप उसे एक मूर्त रूप नहीं दे सकते। हमें अपने दुश्मन का अंदाजा नहीं होता। हम जिसे विकल्प, दूसरी, तीसरी और चौथी आजादी का नाम दे जिसकी मशाल उठा बैठते हैं पता चलता है कि वही हमारी आजादी का दुश्मन बन बैठा। यह नवउपनिवेशवाद का दौर ज्यादा कठिन है।
रानी के राज में सूरज नहीं डूबता था तो आज हम राष्टÑभक्त हैं या नहीं यह दूसरे तय कर रहे हैं। हमारा लिखा कब राष्टÑद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा यह नहीं पता। पहचान की राजनीति से सत्ता मिलने के बाद वे कहते हैं कि दुर्घटना करने वाली बीएमडब्लू को पता नहीं था कि मरने वाला दलित है। आप शीर्षक में दलित लिख कर आग लगा देते हैं जी। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार की स्याही की पहचान खोजी जाने लग जाती है कि वामपंथी, दक्षिणपंथी या आबंडेकरवादी है।साहित्यकार को यह छूट है कि वह अपने किरदार को संवेदनशील बनाए या कू्रर, उसे नीरो कहे, फासीवादी कहे। एक पत्रकार बिना तथ्यों के कुछ कह सकता है क्या? महाकाव्य, महागाथा और मिथकीय चरित्र साहित्य का हिस्सा हो सकते हैं पत्रकारिता का नहीं। कथा सम्राट प्रेमचंद का मानना है कि इतिहास की किताबों में तारीखों के अलावा सब कुछ कल्पना होती है और उपन्यासों में तारीख काल्पनिक होती है और बाकी सब सच होता है। साहित्य, इतिहास के इतर बात करें पत्रकारिता की। अगर इसमें तारीख और तथ्य दोनों गलत साबित कर दिए जाएं तो यह अपराध बन जाता है। तारीख और तथ्यों के भरोसे को ही पत्रकारिता कहते हैं।
हिंदी पट्टी के विमर्श का एक दुखद पक्ष यह है कि हिंदी अखबारों के संपादक में पत्रकार नहीं साहित्यकार खोजा जाने लगता है। अंग्रेजी अखबारों के संपादक अपने अकूत संसाधनों के बावजूद यह दबाव नहीं झेलते हैं। आज हम गुलामी के दिनों में अंग्रेजों से छुपकर चंदे के पैसे से लालटेन की रोशनी में अखबार नहीं निकालते। हमारी एक जिम्मेदारी है रोजगार की भी। एक संपादक और उसकी टीम से जुड़े जितने लोग हैं उनकी नमक-रोटी का इंतजाम इससे ही होना है। एक पत्रकार के तौर पर पहली चिंता यह होती है कि अपने युवा और जुनूनी साथियों को कंप्यूटर और गूगल के अलावा कुछ दे सकें। यकीन मानिए, यह छोटी सी चाह हम हिंदीवालों के लिए बड़ी चुनौती है।‘इंदू जी इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गर्इं बाप को…’ नागार्जुन ने अपनी यह कविता लिख कर साहित्यकार का फर्ज पूरा किया। तो हमारी पत्रकारिता की विरासत यह है कि हमने श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके बाद की सत्ताओं से लोहा लिया और जिंदा बचे। नागार्जुन की कविता और पत्रकारिता दोनों का तरीका अलग है और प्रभाव अलग है और हम दोनों एक नहीं हो सकते।
एक हिंदी अखबार के संपादक की चिंता यह नहीं होती है कि सहयोगी अच्छी कविता और कहानी लेकर आएं। आज चिंता यह है कि हिंदी अखबारों में भागलपुर का आंखफोड़वा कांड, तेलगी घोटाला, हवाला, टूजी, कोयला घोटाले जैसी खोजी रपटें आनी बंद हो गई हैं। विद्वान मैथ्यू अर्नाल्ड पत्रकारिता को जल्दी में रचा साहित्य कहते हैं। लेकिन यहां यह ध्यान देने की बात है कि पनामा कांड जैसी पत्रकारिता के लिए बहुत समय, संसाधन और सावधानी की जरूरत होती है। दस से ज्यादा देशों की खाक छानना और पत्रकारों को महफूज रखना कोई जल्दी का और साहित्यक काम नहीं है।पत्रकारिता जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का काम है। हम आपकी कविता, कहानी, नज्मों से हौसला लेंगे और आपको ऐसे तथ्य देंगे जिस पर आप अपने-अपने तरीके से रच सकें। कुंवर नारायण ने जो शब्द कविता के लिए कहे हैं उसे पत्रकारिता के लिए उधार ले कहा जा सकता है, ‘उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके/जुलूसों की तरह निकले/नारों की तरह लगे/और चुनावों की तरह जीते’। पत्रकारिता एक तारीख के बाद पुरानी हो जाती है और इसके लाए पर साहित्य जो रचता है वह तारीखी होती है। पत्रकारिता और साहित्य का फर्क तारीख और तारीखी का फर्क है।