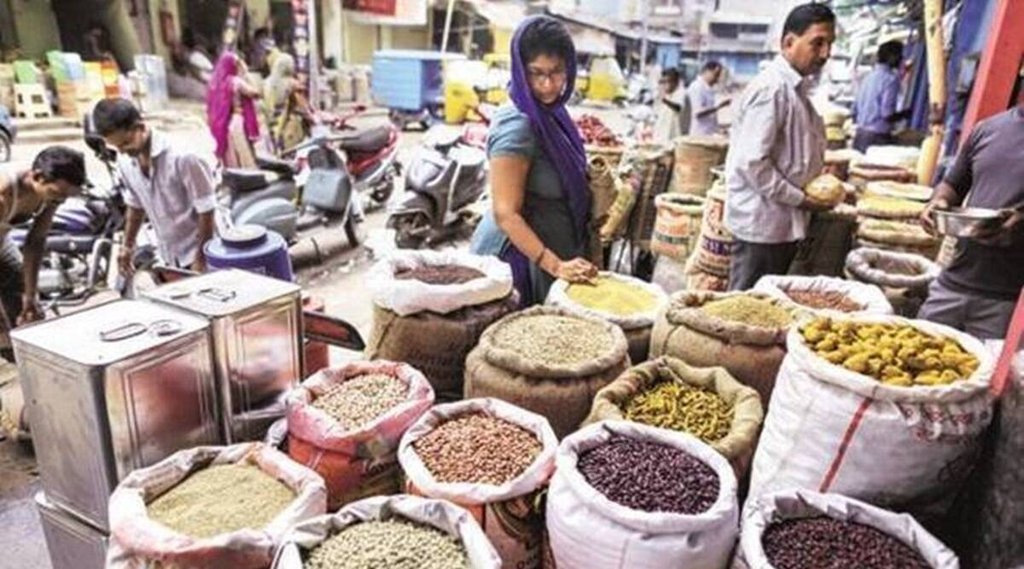वह चुनौती है आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटाए बगैर महंगाई पर लगाम लगाने की। इस दिशा में चार उपायों- घरेलू ब्याज दरें तय करना, करंसी की तरलता का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल और बैंक से जुड़े क्रियाकलापों को नियमित करने का अधिकार। बैंक से जुड़े क्रियाकलापों का अधिकार आरबीआइ के पास है। यहीं पर राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में तालमेल को लेकर सवाल उठने लगते हैं।
राजकोषीय नीति को लेकर चुनौती अहम है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कटौती से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। घूम-फिरकर इसका असर महंगाई दर पर हो रहा है। महंगाई से जुड़े दबाव बढ़ रहे हैं। नीतिगत मसलों से मुद्रास्फीति का दबाव ऊंचे आयात करों से पैदा होता है। सरकार के विस्तृत राजकोषीय घाटे के आंकड़ों से ये दबाव जाहिर होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त स्तर पर यह आंकड़ा जीडीपी के 10 फीसद से भी ज्यादा है।
ब्याज दर में बढ़ोतरी
एक ही समय में ब्याज दर के मोर्चे पर कई कार्रवाई की गई है। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को संकेत दिया जा रहा है कि आरबीआइ स्थायित्व के बचाव के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘केंद्रीय बैंक दरों में आक्रामक बढ़ोतरी जारी रहेगी, चाहे इससे निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े।’
आरबीआइ के गवर्नर ने मजबूरी स्पष्ट कर दी है। दरअसल, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहनकारी वित्तीय नीतियों का लाभ नहीं मिल पाया है। इस कारण मुद्रास्फीति की ऊंची दर लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर, राजकोषीय घाटे की चुनौती है। राजकोषीय जवाबदेही और बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2004 के तहत राजकोषीय घाटे का अनुमानित लक्ष्य तीन फीसद तय किया गया है, लेकिन राजकोषीय घाटा का आंकड़ा लगभग सात फीसद के इर्द-गिर्द बना हुआ है।
राजकोषीय नीति पर आशंकाएं
महामारी और यूक्रेन संकट के तौर पर दोहरी मार झेलने के पहले से ही ढीली-ढाली राजकोषीय नीति में मुद्रास्फीति से जुड़ी आशंकाएं जुड़ी हुई थीं। धीरे-धीरे प्रोत्साहनकारी उपायों पर अमल करने की वित्तीय क्षमताएं (विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह) कमजोर हुर्इं। लिहाजा, महामारी के दौरान बेहद नियंत्रित और लक्षित वित्तीय नीति अपनाने की ही छूट मिल पाई। आंशिक तौर पर इसकी वजह पूंजी का पलायन रोकने के लिए घरेलू ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की कवायद है।
दूसरी ओर, आपूर्ति पक्ष से कीमतों से जुड़े झटके मुख्य महंगाई के साथ जुड़ गए हैं। घरेलू मोर्चे पर मूल्य वर्धन और नौकरियों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है। दरअसल, ढीली-ढाली राजकोषीय नीति के चलते ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी की मुद्रास्फीति को कुंद करने की ताकत मंद पड़ जाती है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 फीसद के स्तर से ऊपर ही बना रहेगा। राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त दो फीसद वित्तीय घाटे की छूट दिए जाने से संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी के छह फीसद के स्तर के आस-पास पहुंच जाता है, जो तय तीन फीसद की सीमा से काफी ऊपर है।
घरेलू मुद्रा की संरक्षा
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 30 सितंबर 2022 को रेपो रेट (वो दर जिसपर वाणिज्यिक बैंक आरबीआइ से ऋण ले सकते हैं) में 0.5 फीसद अंक की बढ़ोतरी (5.40 से 5.90 फीसद) कर दी। आशिंक तौर पर इसकी वजह पूंजी का पलायन (जिससे मुद्रा पर दबाव बढ़ता है) रोकने के लिए घरेलू ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की कवायद है।
भारत में रेपो रेट अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर (3.75 फीसद) से दो फीसद अंक से भी ज्यादा है। वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान ब्याज दरों में अंतर 4.75 से लेकर 6.25 फीसद के बीच बदलता रहा था। भारत में फिलहाल महंगाई दर सात फीसद है, जो अमेरिका और यूरोप के अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से एक फीसद कम-ज्यादा होती रहती है। ऐसे में भारत में पूर्व के मुकाबले इस वक्त इन दरों में निम्न अंतर जायज दिखाई देता है। इस कारण संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा अंतर को बरकरार रखने के लिए इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले रेपो रेट बढ़कर 6.5 से सात फीसद तक पहुंच सकता है।
आर्थिक वृद्धि की हिफाजत
रेपो रेट में बदलाव के पीछे मुद्रा के प्रबंधन, महंगाई की रोकथाम और आर्थिक वृद्धि के बचाव में कुशलतापूर्वक संतुलन साधने का लक्ष्य रहता है। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालते वक्त रेपो रेट आठ फीसद के स्तर पर था। अगले तीन वर्षों यानी अगस्त 2017 तक यह छह फीसद तक घट गया। अप्रैल 2019 से इसमें धीरे-धीरे गिरावट का दौर देखा गया। मई 2020 तक यह दर चार फीसद तक आ गया और अप्रैल 2022 तक इसी स्तर पर बना रहा। मई 2022 से सितंबर 2022 के बीच पांच महीनों में इसमें 1.9 फीसद अंकों की बढ़ोतरी हुई और रेपो रेट 5.9 फीसद पर पहुंच गया।
क्या कहते हैं जानकार
पूंजी की आवक दोबारा शुरू होने से रुपए को मजबूती मिलेगी। पांच हजार अरब डालर (पांच ट्रिलियन यूएस डालर) की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए भारत को अगले पांच साल तक आठ-नौ फीसद की सालाना वृद्धि दर हासिल करनी होगी। इसके लिए मौजूदा नीतिगत रुख जारी रहना चाहिए।
सी रंगराजन, पूर्व गवर्नर, आरबीआइ
बुनियादी दर में बढ़ोतरी किस हद तक विकास की रफ्तार रोकेगी, यह अभी साफ नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चमकीले तो कई काले धब्बे हैं और सरकार को अपने खर्च को सावधानीपूर्वक लक्षित करना चाहिए ताकि कोई बड़ा घाटा न हो। मेरी सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, छोटे और मध्यम क्षेत्र हैं।
रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, आरबीआइ