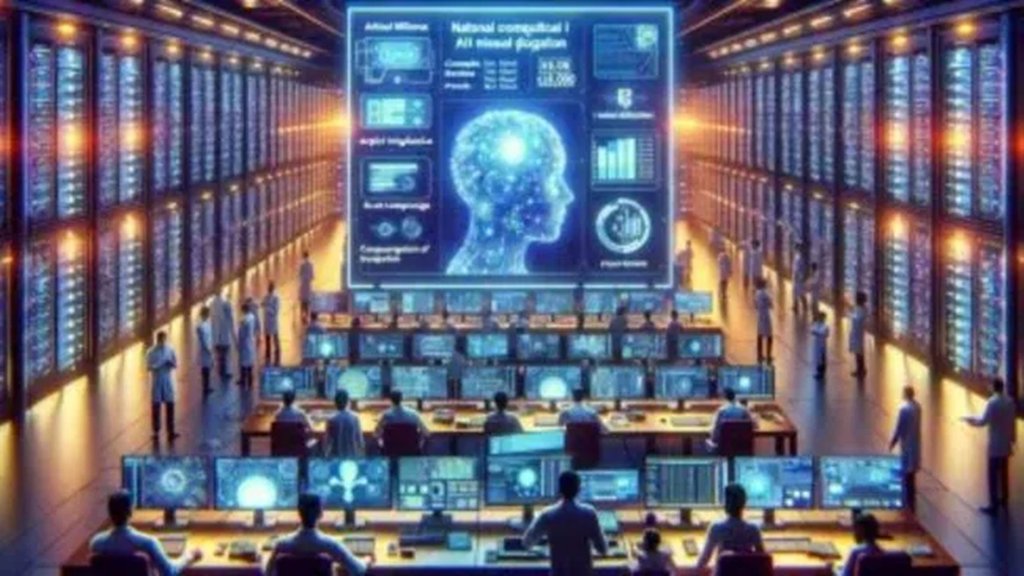भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस वृद्धि में अन्य घटकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह कि मशीनें खुद से सीख और समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। चेहरे पहचानना, वस्तुओं को वर्गीकृत करना और सवालों के जवाब देना आदि जैसे बहुत से कार्य एआइ से संभव हो सकते हैं।
नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सामाजिक और समावेशी विकास में परिवर्तनशील तकनीकों का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा बाजारों तक पहुंच, सामर्थ्य, कुशल विशेषज्ञता की कमी और असंगतता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना संभव हो सकता है। एआइ तकनीक सड़कों पर सुरक्षित रूप से रास्ता बताने, बाधाओं से बचने और स्व-संचालित कारों में उपयोग की जा रही हैं। कृत्रिम मेधा ‘एलेक्सा’ और ‘गूगल असिस्टेंट’ जैसे आभासी सहायकों को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जो व्यक्ति के निर्देशों का पालन कर सकते हैं और उसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। एआइ मानव को अपनी भूमिका उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जो सबसे अधिक मूल्यवान हों, मानवीय क्षमताओं के पूरक हों और जिनसे पूंजी दक्षता में बढ़ोतरी होती हो।
वर्ष 2035 तक एआइ भारत की वार्षिक विकास दर एक से तीन फीसद तक बढ़ा सकता है
एक रपट के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2035 तक एआइ भारत की वार्षिक विकास दर एक से तीन फीसद तक बढ़ा सकता है। सरकार ने एआइ क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। ‘इंडिया एआइ फ्यूचर स्किल्स’ पहल के तहत एआइ शिक्षा को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों तक बढ़ाया जा रहा है। एआइ कार्यस्थलों में परिवर्तन ला रहा है। ‘रैंडस्टैड एआइ एवं इक्विटी रपट 2024’ में कहा गया है कि वर्ष 2024 में दस में से सात भारतीय कर्मचारी कार्यस्थल पर एआइ का उपयोग करते हैं, जबकि एक वर्ष पहले 2023 में यह आंकड़ा दस में से पांच था। यह कार्यस्थलों में एआइ के तेजी से विस्तार को दर्शाता है।
यह सब होते हुए भी एआइ से जुड़ी कई समस्याएं हैं। इसका व्यापक उपयोग होने से नौकरी की कमी की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके कारण कई नौकरियों में स्वचालन हो सकता है, जिससे रोजगार कम हो सकता है। ‘ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस’ की ओर से हाल ही में जारी रपट में कहा गया है कि आने वाले तीन से पांच वर्षों के बीच करीब दो लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। बैंकों द्वारा भारी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। बैंकों में कार्यरत लोगों द्वारा किए जा रहे काम को आसानी से एआइ से कराया जा सकता है। एआइ का दायरा बढ़ने के साथ ही नौकरी-पेशा लोगों में चिंता भी बढ़ रही है। विश्व आर्थिक मंच के एक सर्वेक्षण से जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार 41 फीसद नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते हैं। बावजूद इसके, एआइ कौशल वाले रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है।
‘AI के युग में मानवता बनाए रखना जरूरी’, DG इन्फॉर्मेशन बोले- इसका जिम्मेदार उपयोग हमारा कर्तव्य
पिछले वर्ष किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, करीब 70 फीसद कंपनियां एआइ उपकरण और संवर्द्धन डिजाइन करने के कौशल वाले नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही हैं और 62 फीसद कंपनियां एआइ के साथ बेहतर काम करने के कौशल वाले अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करने का इरादा रखती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि नौकरियों पर ‘जेनरेटिव एआइ’ जैसी प्रौद्योगिकियों का प्राथमिक प्रभाव मानव-मशीन सहयोग के माध्यम से मानव कौशल बढ़ाने की उनकी क्षमता में निहित हो सकता है। इससे देश में भी रोजगार परिदृश्य बदल रहा है। छोटे नवउद्यम से लेकर बड़ी कंपनियों तक एआइ से जुड़ी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और साथ ही पुरानी नौकरियां करने के तरीके को भी बदल रही है। कंपनियां अब डेटा विश्लेषण, स्वचालन और यहां तक कि रचनात्मक कार्यों के लिए एआइ विशेषज्ञों को नियुक्त कर रही हैं। एआइ कुछ नौकरियों की जगह ले सकता है, तो यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ‘एआइ डेवलपमेंट’ जैसे उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कुशल पेशेवरों की मांग पैदा कर रहे हैं।
एआइ के उपयोग से गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। एआइ माडल में पक्षपात और पूर्वाग्रह हो सकता है, जिससे अनुचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका उपयोग मानव संबंधों में बदलाव ला सकता है, जिसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। एआइ माडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध होना संभव नहीं है। कई बार एआइ जटिल समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो सकती है। कई मामलों में एआइ की भाषा और सामग्री मशीनी हो सकती हैं, जिनमें कृत्रिमता साफ झलकती है।
‘चंपक’ नाम पर भिड़े BCCI और कॉमिक ब्रांड, हाईकोर्ट ने पूछा– दूसरे के ट्रेडमार्क को कैसे अपना लिया?
एआइ के उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक है। एआइ माडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्राप्त करने और डेटा सुरक्षा भी जरूरी है। इसके उपयोग के लिए नियमन और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, एआइ की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। एआइ के उपयोग के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल किया जा सके।
बीते कुछ समय में एआइ का उपयोग करके ‘डीपफेक फ्राड’ करने के काफी मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एआइ के कारण शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिससे मानव श्रम को नए कौशल सीखने की आवश्यकता हो सकती है। भावनात्मक कौशल पर निर्भर करने वाली नौकरियों में चिकित्सकों और शिक्षकों की अभी भी मांग बनी रहेगी।
यह सही है कि कृत्रिम मेधा से जुड़े बहुत से खतरे हैं और इनका समाधान भी बेहद जरूरी है। इस दिशा में कई स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसको रोका नहीं जा सकता। भविष्य में इसके जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से बदलाव आने तय हैं। वर्ष 2023 एआइ का साल था, वहीं 2024 में इसका विस्तार हुआ। अब एआइ आवाज और वीडियो के माध्यम से संवाद करने लगे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होगा।
दुनिया भर के एआइ के विकासकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए इनका नियमन भी करेंगी। यूरोपीय संघ ने एआइ एक्ट लागू किया है, जो ‘एआइ डेवलपर्स’ के लिए पहला बड़ा कानून है। दूसरे देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ‘गूगल-ओपन एआइ’ ने वीडियो माडल निकाले हैं। यह सत्य है कि तकनीकी विकास अपनी उपयोगिता के साथ खतरे भी लाता है। इन खतरों से बचाव के प्रयासों और उपयोग में संतुलन के साथ इसको अपनाना ही पड़ेगा।