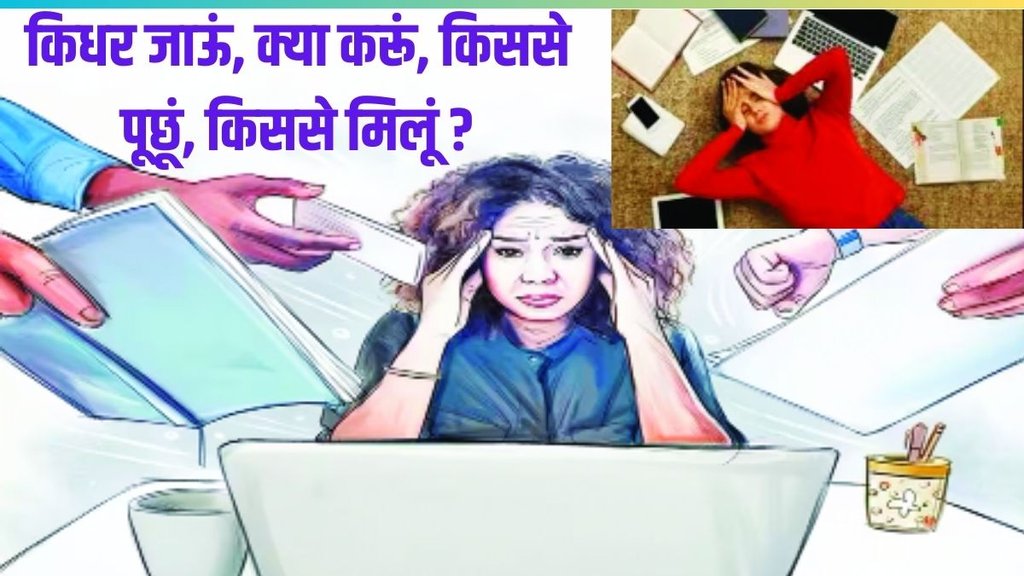जयप्रकाश त्रिपाठी
एक अध्ययन के मुताबिक, हमारे देश में छात्रों द्वारा आत्महत्या का कारण केवल मानसिक विकार अथवा अवसाद नहीं है। देश-समाज का पारंपरिक दृष्टिकोण भी युवाओं की सोचने-समझने की वैज्ञानिक क्षमता को बाधित कर रहा है। अपने भविष्य की चिंता में अभिभावक छात्रों पर अधिक मेहनत और लक्ष्य हासिल करने का अनुचित दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। गलाकाट प्रतियोगिता में पिछड़ने और घरवालों के तिरस्कार का डर छात्रों की जिंदगी छीन रहा है। ऐसा ज्यादातर खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों के साथ हो रहा है।
वंचित युवा हीन ग्रंथियों का हो रहे हैं शिकार
लिंग-जाति के भेदभाव भी दबाव बना रहे हैं। बाजार की चमक-दमक तक पहुंच से वंचित वर्गों की बुनियादी संसाधनों की प्रतिस्पर्धा भी इस आग में घी डाल रही है। बाजारवादी (और राजनीतिक भी) शक्तियों का प्रचारतंत्र निम्न आयवर्ग को लगातार कुंठित और अवसादग्रस्त कर रहा है, जिनके पहुंच से वंचित युवा हीन ग्रंथियों का शिकार हो रहे हैं।
आत्महत्या से पहले मन में उभरते हैं तरह-तरह के सवाल
सैकड़ों छात्रों की एक मीडिया काउंसलिंग से पता चलता है कि आत्महत्या से पहले ऐसे छात्रों के मन में तरह-तरह के सवाल उभरते हैं, मसलन, उनके अभिभावक समय से कालेज या कोचिंग की फीस क्यों नहीं चुका रहे, सबसे ज्यादा वह किस गतिविधि से विचलित है, परीक्षा में सफलता नहीं, किसी छात्रा की निगाह में उसकी हीरो जैसी छवि नहीं तो फिर उसके जीवन में अब बाकी बचा ही क्या है!
बात-बात पर खुद को कोसते रहते हैं छात्र
काउंसलिंग में कई ऐसे भी छात्र मिलते हैं, जो बिना किसी वजह के आत्महत्या करना चाहते हैं, उन्हें खुद पता नहीं कि आखिर किस तरह की उत्तेजना उन्हें मौत की ओर खींचे लिए जा रही है! चिकित्सक ऐसे छात्रों को मनोरोगी करार देते हैं। ऐसे छात्र बात-बात पर खुद को कोसते रहते हैं। वे निजी डायरी या सोशल मीडिया में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहते हैं। नियमित रूप से खाना नहीं खाते हैं। दोस्तों से नहीं मिलते हैं। अकेले रहना चाहते हैं। अपनी हरकतों के कारण वह परिजनों से स्वत: अलगाव में पहुंच जाते हैं।
निदान की दिशा में, अनेक शिक्षाविद ‘काउंसिलिंग’ को अपर्याप्त मानते हैं। वह दूसरे तरह के व्यावहारिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरतों पर बल देते हैं। मसलन, छात्र के आत्मविश्वास को हवा देते रहना, उसकी हर तरह की कुसंगति, व्यसन और ‘साइबर बुलिंग’ से हिफाजत करते हुए उसकी किसी खास सकारात्मक अभिरुचि, उसकी खेल, सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रेरक गतिविधियों को प्रोन्नत करना, संवादहीनता-अलगाव और अकेलेपन से बाहर रखना, उसके स्वास्थ्य का हर तरह से ध्यान रखना, परीक्षा आदि अकादमिक और कोचिंग के दबावों से शिथिल करते रहना, लगातार पढ़ाई न करने देना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जैसे मौकों पर ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन फार सुसाइड प्रिवेंशन’ (आइएएसपी) की गतिविधियों से वाकिफ कराना, मानसिक चिकित्सक के संपर्क में रहना, अभिभावक स्तर पर उनके व्यक्तित्व की समग्रता को विकसित करना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन ‘किरण’, शिक्षा मंत्रालय के ‘मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की पहल से जुड़े रहना, स्कूल-कालेजों में वरिष्ठों की अवांछित हरकतों और रैगिंग से सुरक्षित रखना आदि।
नीतियों का चक्र
तंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी। करीब तीन दशक बाद वर्ष 2020 में देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब मंजूरी मिली, उससे पहले वर्ष 1986 में बनी थी। उसके बाद वर्ष 1992 में उसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्वीकृत होने से पहले देश के विभिन्न वर्गों से उस पर रचनात्मक सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया था।