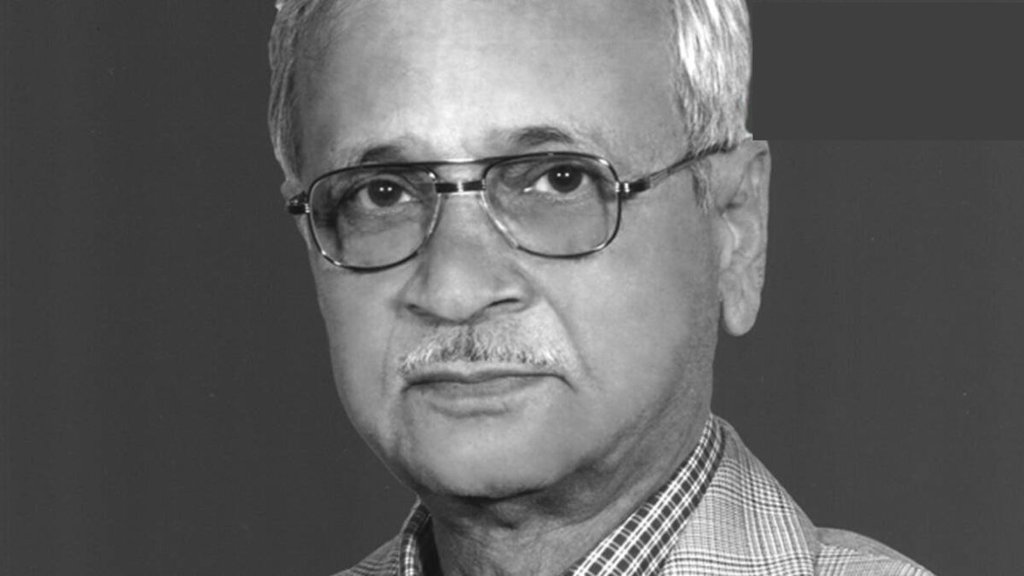26 जनवरी की पूर्व संध्या पर उन नामों की घोषणा हुई, जिन्हें पद्म सम्मानों (Padma Awards) से नवाजा जाना है। जारी सूची के मुताबिक, कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। इसी लिस्ट में एक नाम दिलीप महालनोबिस (Dilip Mahalanabis) का है। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) से सम्मानित किया जाएगा।
कौन हैं दिलीप महालनोबिस?
पश्चिम बंगाल के डॉ. दिलीप महालनोबिस का जन्म 12 नवंबर, 1934 को हुआ था। उन्होंने कोलकाता और लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। दिलीप महालनोबिस ने 1960 के दशक में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का हिस्सा रहे। वहीं उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पर शोध किया।
बाद में महालनोबिस ने मॉडर्न ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए डॉ. दिलीप महालनोबिस ने ही सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) का इस्तेमाल किया था।
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दिलीप महालनोबिस
पूर्वी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आज़ादी के बाद 1971 में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है।
तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) पर सैन्य कार्रवाई कर रहा था। इससे भारी शरणार्थी संकट पैदा हो गया था, जिसका असर पड़ोसी देश भारत पर भी पड़ा था। करीब 10 मिलियन लोग भारत भाग आए थे। उन्हीं शरणार्थी शिविरों में काम करने के दौरान डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने ORS का प्रयोग किया गया था।
दरअसल 1964 में भारत में हैजा फैल गया था। 1971 में सुरक्षा और वित्तीय संकट के कारण ढाका स्थित कॉलरा रिसर्च लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया था। महालनोबिस एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित थे। वह साल 1966 में कलकत्ता में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (JHCMRT) के हैजा अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल हुए।
उनकी टीम पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक शरणार्थी शिविर में हैजा महामारी से पीड़ितों का इलाज कर रही थी। लेकिन इस बीच हैजा से बचाव के लिए दी जाने वाली दवा खत्म हो गयी। उधर रिसर्च लेबोरेटरी पहले ही बंद हो चुका था।
तब डॉक्टर महालनोबिस ने लोगों की जान बचाने के लिए ओआरएस का उपयोग करना उचित होगा। हालांकि ओआरएस पैकेट उपलब्ध नहीं था, उन्होंने ड्रम में नमक और चीनी का घोल (ओआरएस) मिलाया और शिविरों में हैजा के रोगियों को दिया।
JHCMRT के पुस्तकालय को कारखाने में बदल दिया गया। यह उपचार का एक अनिवार्य तरीका नहीं था। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत जोखिम को उठाते हुए इस मानवीय संकट का जवाब देना चुना। दो से तीन सप्ताह के समय में यह स्पष्ट हो गया था कि चिकित्सा काम कर रही है।
उपचार का गुप्त तरीके से बांग्लादेश में हुआ प्रचार
बाद के विश्लेषण से यह साबित हुआ कि ओआरएस ने शिविरों में हैजा से होनी मृत्यु दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था। लोगों की जान बचाने के लिए उपचार के इस तरीके को पर्चा पर लिखा गया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांटा जाने लगा। इसे एक गुप्त बांग्लादेशी रेडियो स्टेशन ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बचाने के लिए प्रसारित किया।
हालांकि, इस जन अभियान के परिणामों के बारे में संशय बना रहा, कई पत्रिकाओं ने शुरू में महालनोबिस की पांडुलिपियों को खारिज कर दिया था। उनके योगदान को डब्ल्यूएचओ-मुख्यालय में जीवाणु रोगों के तत्कालीन प्रमुख धीमान बरुआ के समर्थन से मान्यता मिली। बरुआ खुद चटगाँव में 1932 की हैजा महामारी से बचे थे और शरणार्थी शिविरों में देखे गए परिणामों से आश्वस्त थे।
दिलीप महालनोबिस का प्रयोग सफल हो गया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद उन्होंने हैजा नियंत्रण के लिए WHO के साथ काम किया। वर्ष 1975 से 1979 के बीच उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र और यमन में लोगों को हैजा से बचाया। 1980 के दशक के मध्य और 1990 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर महालनोबिस WHO के डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी रहे थे।