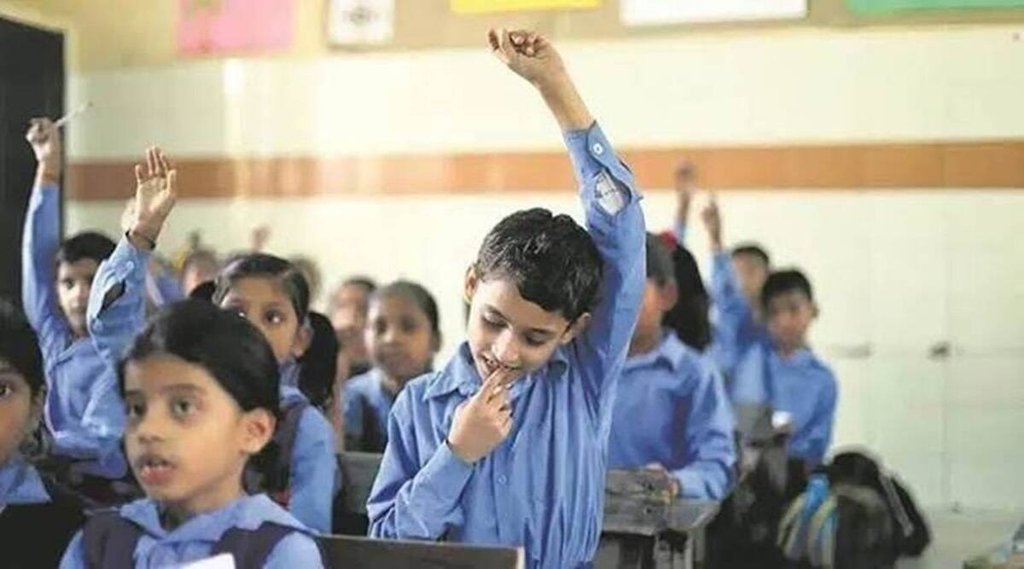नई शिक्षा नीति से जन्मा कोई भी पाठ्यक्रम अपने उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकता है, जब हर अध्यापक अपनी भूमिका को न केवल समझ, बल्कि आत्मसात कर चुका हो। ऐसा तभी संभव होगा, जब शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान युवा अध्यापक यह अंतर्निहित कर चुका हो कि देश के भविष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्माता वही है, वह सैकड़ों-हजारों के जीवन को दिशा दे सकता है। यह भी तभी होगा जब देश का हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संस्थागत आदर्श उपस्थित करता हो।
किसी भी क्षेत्र में नीतियों के क्रियान्वयन में सफलता की अपेक्षा तभी की जा सकती है, जब वे गहन, विस्तृत विमर्श और परामर्श का निष्कर्ष हों। नीति-निर्माण की इस प्रक्रिया में वर्तमान स्थिति का वस्तुनिष्ठ जमीनी आकलन तथा भविष्य-दृष्टि का समुचित सम्मिलन हो। जब भी नीतियों के पुनरवलोकन का समय आता है, व्यवस्था की कमियों, अवरोधों और पीछे की विफलताओं का वस्तुनिष्ठ, तार्किक और तथ्य-आधारित विश्लेषण केवल उपलब्धियों की सराहना से अत्यंत अधिक सहायक होता है।
जुलाई 2020 में भारत ने चार वर्ष के राष्ट्रीय विमर्श तथा अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अध्ययन के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति निर्माण में संस्थाओं से लेकर व्यक्ति तक को अपने विचार देने का प्रावधान किया गया था। लोगों की भागीदारी भी अभूतपूर्व रही। अपेक्षा तो यही है कि इसमें सम्मिलित अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण नीतिगत स्वीकार्यताएं इसकी उपयोगिता ही नहीं, सार्थकता को भी स्थापित करेंगी।
इनमें से एक है: ‘प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था।’ आज के विश्व में इससे अधिक सराहनीय लक्ष्य कोई और हो ही नहीं सकता है।
वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार्य है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था वहां के लिए तभी उपयोगी होगी, जब उसकी जड़ें उस देश की संस्कृति और ज्ञान परंपरा यानी देश की मिट्टी में गहराई तक जा चुकी हों। मगर इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि हर देश की किसी भी क्षेत्र की नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए उनकी प्रतिबद्धता नए ज्ञान-विज्ञान-तकनीकी के प्रति भी होनी चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यही नहीं, आगे वे देश और लोग ही बढ़ेंगे, जो नए ज्ञान के सृजन में भागीदारी करने में भी सक्षम होंगे। दूसरा विचारणीय बिंदु है: ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।’
यहां एक अत्यंत वैचारिक प्रश्न उभरना चाहिए कि क्या पहले की शिक्षा नीतियों में ये लक्ष्य शामिल नहीं थे? इसका उत्तर आसान नहीं है। जो लोग 1968, 1986/92 की शिक्षा नीतियों और उनके क्रियान्वयन से परिचित हैं, वही कहेंगे कि यह तो शास्वत लक्ष्य या अपेक्षाएं हर बार दोहराई गई हैं, यह अपेक्षित ही है कि हर बार वे नए और समसामयिक शब्द विन्यास में ही कही जाएंगी।
अगर वे लक्ष्य पहले से भी स्वीकार्य और नीतियों में शामिल थे, तो प्राप्त क्यों नहीं किए जा सके? इसका उत्तर हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए, जो इस समय या आगे के कुछ वर्षों में नई नीति के क्रियान्वयन में हिस्सेदरी करेगा। एक उदाहरण। पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं 1960 तक वैज्ञानिकों और विद्वानों के संज्ञान में पूरी तरह आ चुकी थीं। यह भी अनुमान लगा लिया गया था कि अगर तुरंत और दीर्घकालीन कदम न उठाए गए, तो ये समस्याएं कुछ दशकों में ही विकराल रूप ले लेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की संस्तुतियों पर बनी 1968 की शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
एनसीईआरटी ने लगातार पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम और पुस्तकों में सकारात्मक परिवर्तन किए, नई पाठ्य पुस्तकें बनार्इं, राज्यों के संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षित किया कि वे स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण पर पुस्तकें बनाएं। मगर सकारात्मक परिणाम सीमित ही रहे!
नई शिक्षा नीति से जन्मा कोई भी पाठ्यक्रम अपने उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकता है, जब हर अध्यापक अपनी भूमिका को न केवल समझ, बल्कि आत्मसात कर चुका हो। ऐसा तभी संभव होगा, जब शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान युवा अध्यापक यह अंतर्निहित कर चुका हो कि देश के भविष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्माता वही है, वह सैकड़ों-हजारों के जीवन को दिशा दे सकता है।
यह भी तभी होगा जब देश का हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संस्थागत आदर्श उपस्थित करता हो। शिक्षक प्रशिक्षक, प्रशिक्षु अध्यापक, कार्यरत अध्यापक, छात्र मिलकर जो शृंखला निर्मित करते हैं उसकी हर कड़ी को नैतिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। किसी भी कड़ी की शिथिलता पूरी शृंखला को अशक्त बना देगी।
जब 1986/92 की शिक्षा नीति को सारे देश में लागू कराने की तैयारी अपने चरम पर थी, तभी शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में पत्राचार से बीएड की डिग्री देने का कार्य कुछ जाने-माने विश्वविद्यालय कर रहे थे। इस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता से सजग और सक्रिय विद्वत वर्ग चिंतित था। कुछ वर्षों बाद बड़ी संख्या में बीएड की उपाधि देने वाले निजी संस्थान खुले और इस डिग्री का व्यापारीकरण शुरू हुआ। दूसरी तरफ, राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों में थोड़े से मानदेय पर संविदा अध्यापक नियुक्त करना प्रारंभ किया।
एनईपी-2020 ने इस संबंध में अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्तुतियां की हैं। इनमें चार-वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू करना और केवल नियमित अध्यापकों की नियुक्ति शामिल हैं। क्या यह 2030 तक संभव हो सकेगा! देशहित में ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में प्रत्येक राज्य सरकार को जी-जान से लगना होगा, और साथ ही हर स्तर पर उपस्थित और ‘व्यवस्थित’ भ्रष्ट आचरण से मुक्ति दिलाने के पारदर्शी प्रयास करने होंगे!
एवजी अध्यापकों की प्रथा लगभग चार दशकों से चल रही है, कोई इसे रोक नहीं पाया है। जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लाक शिक्षा अधिकारी इसे रोक सकता है, अगर वह स्वयं ईमानदार हो और उस पर कोई राजनीतिक दबाव न हो। केंद्र सरकार ने अभी तक केवल प्रशासनिक सेवा के लिए निश्चित पदों पर विशेषज्ञता की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिनियुक्ति पर ऐसे लोगों को लेने का निर्णय किया है।
आज से चार-पांच दशक पहले तक राज्यों में भी स्कूल बोर्ड, राज्य शिक्षा संस्थान, पाठ्यपुस्तक निगम, शिक्षा निदेशक जैसे पदों पर शिक्षा के क्षेत्र में जीवन लगा रहे लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। अब पाठ्यपुस्तक निगम का मुख्य अधिकारी प्रशासनिक सेवा से ही आता है, वह लगातार मुख्य-धार के पदों पर जाने के प्रयास में लगा रहता है।
वैसे भी उससे वह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो एक शिक्षा जगत में शोध और अध्ययन से अपनी साख बना चुके शिक्षाविद से की जा सकती है। आज यह लगभग एक सामान्य स्थिति बन गई है कि स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रचार्य जैसे पद वर्षों रिक्त रहते हैं। इस शैथिल्य से छुटकारा पाना आवश्यक है।
हर क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन को समझने वाले संस्थान जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उच्च पद के लिए अर्हताएं पूरी कर चुका है, तो उसे- अगर वह उपयुक्त पाया जाए- पद देने में देरी उसकी उत्पादकता और लगनशीलता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। तीन-चार दशक सेवा कर चुका अध्यापक अगर प्राचार्य पद पर केवल विभागीय अन्यमनस्कता के कारण प्रोन्नति नहीं पाता है, तो उसका मनोबल टूटेगा ही।
नीति के क्रियान्वयन में जमीनी स्तर के कर्मचारी और अधिकारी अप्रत्याशित सुधार ला सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं, जहां एक प्राचार्य ने अपने सहयोगियों का दृष्टिकोण परिवर्तन करने में सफलता पाई, या किसी शिक्षा अधिकारी ने सारे स्कूलों की कार्य-संस्कृति परिवर्तित कर दी।
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो व्यक्ति अपने ‘कर्म’ के दूरगामी प्रभाव का अनुमान लगा लेता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है, वही किसी भी सकारात्मक परिणाम को प्राप्त कर सकता है। चुनौती तो व्यक्ति निर्माण की ही है।