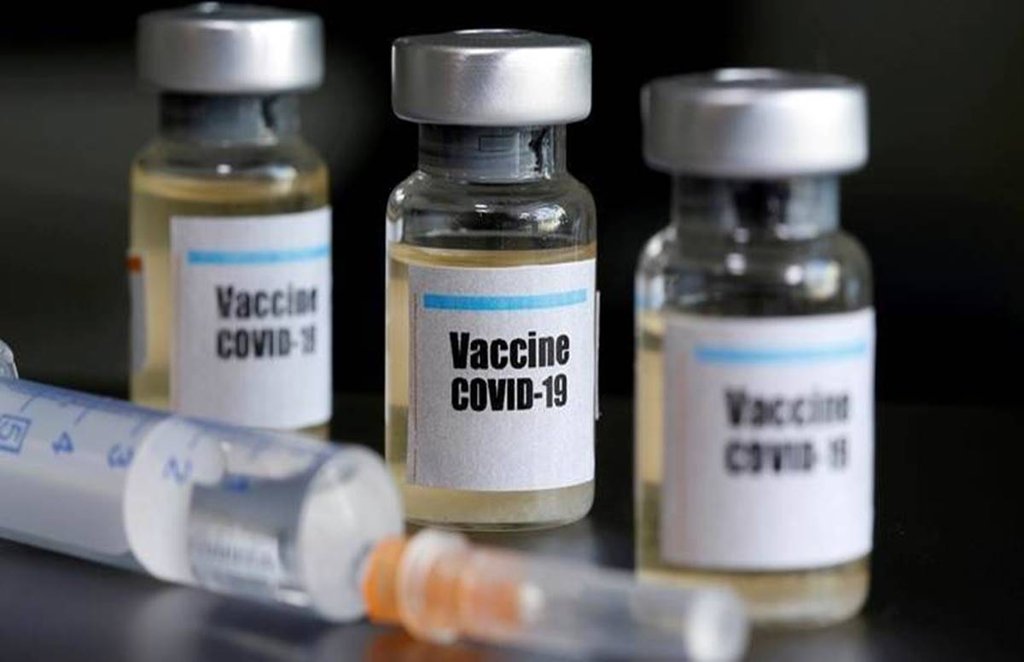मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते से ही देश में डेढ़ महीने की सख्त पूर्णबंदी की गई थी, ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसमें काफी हद तक सफलता मिली भी, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने का प्रतिकूल परिणाम भी सामने आया। पूर्णबंदी में देश की सभी छोटी-बड़ी औद्योगिक गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लग गया था।
अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे- कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट, उर्बरक, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तक का उत्पादन ठप-सा हो गया था। औद्योगिक गतिविधियां बंद रहने से बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई। बिजली नहीं बनने से कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा।
छोटे उद्योग और कारखाने बंद रहने से इस्पात के कारखानों में भी उत्पादन ठप रहा। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी नहीं के बराबर रही। ऐसे में अर्थव्यवस्था में ठहराव तो आना ही था। पहली तिमाही में जीडीपी शून्य से चौबीस फीसद नीचे चली गई थी। जाहिर है, जब इतनी भारी गिरावट रही है तो नतीजे भी लंबे समय तक भुगतने होंगे।
हाल में रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसे अनुमान और आकलन अब नए नहीं रह गए हैं। पिछले एक साल में देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां ऐसे ही अनुमान व्यक्त करती रही हैं। फिच का कहना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था में ग्यारह फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद अगले चार साल तक देश की जीडीपी साढ़े छह फीसद के आसपास ही रहेगी।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भयानक मंदी से जूझ रही हैं और इससे इन अर्थव्यवस्थाओं में भारी संकुचन पैदा हुआ है। यह सभी के लिए बड़ी चुनौती है। इस संकट से वही निकल पाएगा जो तात्कालिक कदमों के साथ दूरगामी नतीजे देने वाली नीतियों का निर्माण और उन पर अमल करेगा।
हालांकि भारत ने हालात को संभालने के लिए अब तक कई तरह के राहत पैकेज जारी किए हैं, ताकि मंदी की मार झेल रहे छोटे-बड़े उद्योग फिर से खड़े हो सकें। उद्योगों को करों में छूट जैसी कई रियायतें भी दी गई हैं। लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। कारण साफ है कि संकट के मुकाबले राहत बहुत ही न्यून है।
भारत में इस वक्त सबसे बड़ा संकट बाजार में मांग का है। इसके मूल में महंगाई और बेरोजगारी जैसे कारण हैं। पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े उत्पादों के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे भी मांग कमजोर पड़ी है। दूसरा बड़ा संकट लोगों के पास काम-धंधा नहीं होना है। पूर्णबंदी के दौरान जिन लोगों का रोजगार चला गया था, उनमें से अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। असंगठित क्षेत्र की हालत तो बहुत ही खराब है।
अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं, इसलिए जो पैसा पास में है उसे बचा कर रख रहे हैं। बढ़ते एनपीए के कारण बैंकिंग क्षेत्र अलग संकट में है। ऐसे में अब सबकी निगाहें आम बजट पर हैं। देखना होगा कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले वक्त की चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर हैं।