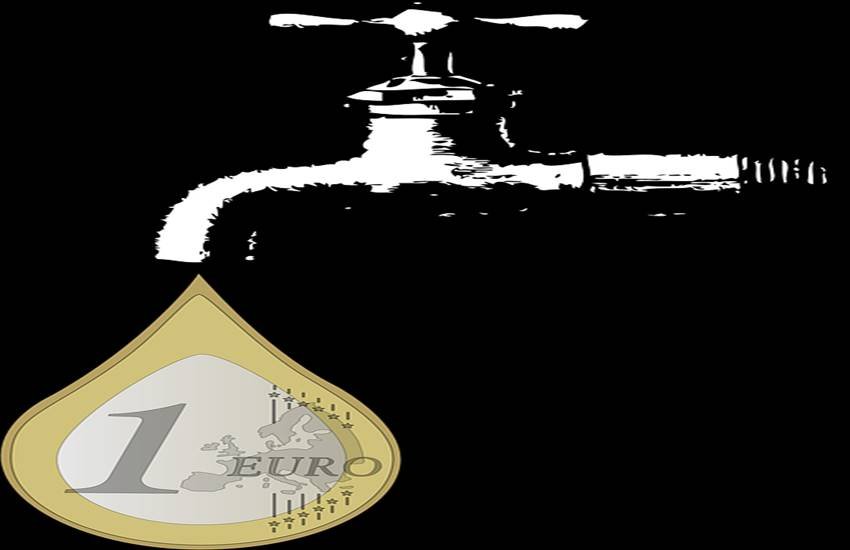आमतौर पर हर साल ही यमुना में प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पेयजल तक का संकट जब गहरा जाता है, तब जाकर सरकार इस दिशा में सक्रिय होती है और इसे दुरुस्त करने का आश्वासन देती है। लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद जब मसले का तात्कालिक तौर पर हल निकल जाता है तो संबंधित महकमे के लोग इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं। इसी तरह की उदासीनता की वजह से हर कुछ समय के बाद दिल्ली के निवासियों के सामने पीने के पानी तक की मुश्किल खड़ी हो जाती है। खासतौर पर जाड़े का मौसम शुरू होने के वक्त यह समस्या ज्यादा गहरा जाती है। लेकिन इस बार करीब दो महीने पहले ही यमुना में लगातार औद्योगिक कचरा प्रवाहित किए जाने की वजह से इसके पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है।
जल बोर्ड के मुताबिक सोमवार को यमुना में अमोनिया का स्तर 3.2 पीपीएम तक पहुंच गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पानी लोगों की सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड के तीन संयंत्रों को पूरी तरह बंद कर देना पड़ा और कई इलाकों के लोगों को पानी की कटौती का संकट झेलना पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा के सोनीपत से यमुना में औद्योगिक कचरा प्रवाहित हो रहा है, जिससे इसके पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा। लेकिन यह कोई पहली बार खड़ी हुई समस्या नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद सरकारों के सामने कौनसी मजबूरियां हैं जिनके चलते वे जहरीला पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्ती नहीं बरत पाती हैं? यमुना की सफाई के नाम पर अब तक अरबों रुपए बहाए जा चुके हैं।
लेकिन अगर इसमें घुलते जहरीले रसायनों से एक ही तरह की समस्या खड़ी हो जाती है तो आखिर वे पैसे किस काम पर खर्च किए गए? सालों पहले से यह दावा किया जाता रहा है कि सफाई अभियान चला कर यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह स्वच्छ बना दिया जाएगा। लेकिन आज भी यमुना की हालत देखी जा सकती है कि कई बार इसका पानी नहाने तक के लिहाज से जोखिम भरा माना जाता है। ऐसी स्थिति में पीने की जरूरत के लिए पानी के संकट का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।
दरअसल, बरसात के दिनों को छोड़ दिया जाए तो यमुना वैसे ही प्रदूषण की वजह से किसी नदी के बजाय एक बड़े नाले के रूप में बची दिखती है। इसके बावजूद इसके बचे हुए हिस्से से ही जलशोधन संयंत्रों के जरिए दिल्ली में पीने के पानी की बड़ी जरूरत पूरी होती है। मगर जब समूची दिल्ली में पीने तक के पानी पर संकट आ खड़ा होता है तब जाकर आनन-फानन में तात्कालिक उपाय किए जाते हैं।
सवाल है कि यमुना जिन इलाकों से गुजरती है, उन राज्यों के संबंधित महकमे यह सुनिश्चित कर पाने में नाकाम क्यों हैं कि नदी में औद्योगिक इकाइयों से निकले जहरीले रसायन नहीं बहाए जा सकें। अगर दिल्ली में यह समस्या हर साल गहरा जाती है तो हरियाणा के साथ मिल-बैठ कर इसके किसी स्थायी हल तक पहुंचने की जरूरत क्यों नहीं लगती है? फिर यमुना में अगर अब भी औद्योगिक कचरा घुल रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? नदी समूचे समाज के लिए जीवन होती है। लेकिन अरबों के खर्च के बावजूद उसे बचाने का काम अब तक कागजों पर ही दिखता रहा है।