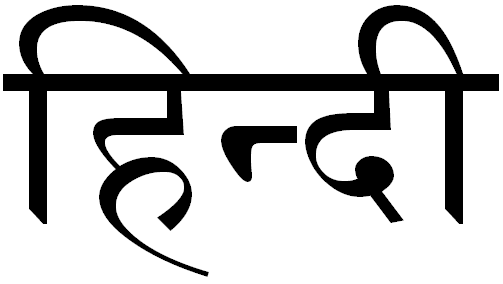हिंदी अभी न तो प्रौद्योगिकी की भाषा है और न रोजगार की। फिर भी वह अंग्रेजी से आगे निकल रही है। उसे यह गति भारतीय मीडिया ने दी है। हम इस नई हिंदी को समकालीन भाषा कह सकते हैं, जिसे पूरा भारत बोलता औरसमझता है। अब हिंदी के पास अंग्रेजी से निरर्थक लड़ने का वक्त नहीं है। उसका तो किसी से और कभी बैर था भी नहीं। वह इतनी उदार है कि उर्दू और फारसी से लेकर अंग्रेजी तक के शब्दों को आत्मसात करती रही है। फिर हिंदी के प्रति उपेक्षा और द्वेष का भाव कहां से आया, यह सोचने का विषय है। दरअसल, बरसों तक हिंदी की दुर्गति के लिए और कोई नहीं, इस भाषा के कट्टरपंथी पैरोकार जिम्मेदार रहे। उन्होंने पाठ्यक्रमों की चारदिवारी और जरूरत से ज्यादा व्याकरणिक पाबंदियों के बीच हिंदी की रसधारा को सूखने दिया। साहित्य के मठाधीशों ने तो इसे ऐसी विशिष्ट भाषा बना दिया कि एक समय में यह उपहास का पात्र बनी रही।
हिंदी पर साहित्य के इस अनावश्यक आवरण को सबसे पहले सिनेमा और फिर मीडिया ने उतार फेंका। हिंदी के इस नए रूप का परंपरावादियों ने यह कह कर विरोध किया कि यह तो बाजार की भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा देशज शब्दों और मुहावरों से समृद्ध हुई हिंदी कोई एक दिन नें नहीं बनी है। भाषा के बनने की एक सतत प्रक्रिया होती है। वह समय और स्थान के हिसाब से बनती-बिगड़ती रहती है। पिछले दो दशक में मीडिया और बाजार ने एक नई हिंदी बनाई है। यह कुछ को भली लगती है, तो कुछ को अखरती भी है। आप देश में कहीं भी चले जाइए, इस भाषा को बोलने वाले मिल ही जाएंगे। यही वजह है कि गैर हिंदीभाषी राज्यों में भी हिंदी के चैनल और अखबार पहुंचे हैं और वहां के लोगों की आवाज बन रहे हैं। पाठकों के सरोकार के साथ उनकी बोलियों के शब्दों को भी बखूबी स्वीकार किया है।
लेकिन पिछले एक दशक में हिंदी मीडिया ने भाषा को एक बार फिर परिमार्जित किया है। इससे हिंदी जरूरत से ज्यादा चमकी है। मीडिया का प्रभु वर्ग इसे युवा भारत की भाषा बनाना चाहता है। इसका समर्थन भी है और विरोध भी, लेकिन इस पर चिंता जताने वाले यह नहीं बताते कि ‘हिंग्रेजी’ बनती हिंदी अपने सामान्य रूप में कैसे बरकरार रहे! कैसे वह नई तकनीक से जुड़े शब्दों को अंगीकार करे और इससे जुड़े नए शब्द तैयार कर उन्हें प्रचलित किया जाए! टीवी और अखबार के साधारण दर्शकों और पाठकों की भाषा आज भी सामान्य ही है। लेकिन ताबड़तोड़ खबरें देने और ब्रेकिंग न्यूज के इस दौर में हिंदी की टांग तोड़ी जाती है। अंग्रेजी के शब्दों का जिस कदर बेधड़क प्रयोग होता है, उससे समझ नहीं आता कि यह संवाद क्या केवल ‘इंडिया’ के ‘प्रभु वर्ग’ से किया जा रहा है, जो सिर्फ अंग्रेजी में सोचता है!
जबकि मोबाइल फोन पर एसएमएस और वाट्सऐप पर रोमन में संदेश भेज रही नई पीढ़ी भी पहले हिंदी में सोचती है। यह हिंदी की ही ताकत है कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने मोबाइल फोन को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समर्थ बना रही हैं। वे जानती हैं कि नई पीढ़ी अपनी भाषा में संंवाद करना ज्यादा पसंद करती है। फिर क्षेत्रीय भाषाओं का अपना एक विशाल वर्ग भी है, जिसकी उपेक्षा करके बाजार में नहीं टिका जा सकता। मगर सवाल है कि हमारा मीडिया यह जिद किए क्यों बैठा है कि हमारी नई पीढ़ी को ‘हिंगलिश’ ही पसंद है! पहले इस पर अनुसंधान या सर्वे कीजिए, फिर देखिए कि युवाओं की भाषा अंग्रेजी है या हिंग्रेजी या फिर तेज-तर्रार हिंदी, जिसमें जरूरत भर के और बोलचाल में शामिल अंग्रेजी के शब्द हैं, जो आम आदमी को भी स्वीकार्य हैं।
आज जरूरत इस बात की है कि मीडिया की भाषा का एक मानक तय हो। मगर आलम यह है कि एक ओर जहां खबरों की विश्वसनीयता का संकट है, तो दूसरी ओर भाषा की सहजता, निश्छलता और भावप्रवणता खतरे में है। अब वह दिल को नहीं छूती। मीडिया की अभिव्यक्ति हर प्रकाशन और समाचार चैनल में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य व्याकरण और शब्दों के मामले में एकरूपता होनी चाहिए। नई हिंदी का स्वरूप आधुनिक तो हो, लेकिन अगर हम समाधान को ‘सोल्यूशन’ लिखेंगे तो हिंदी में बोलचाल के अपने शब्द ‘उपाय’ या ‘हल’ को धीरे-धीरे गायब कर देंगे। हिंदी का अपना व्याकरण है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों से हिंदी का किला इतना मजबूत है कि अंग्रेजी के तमाम शब्द सेंध लगा लें, इसे कमजोर नहीं कर सकते। समकालीन लेखकों और पत्रकारों का यह दायित्व है कि वे हिंदी को परिमार्जित तो करते रहें, मगर इसकी शब्द-संपदा का भरपूर प्रयोग करते हुए इसके मूल चरित्र को बनाए रखें, तभी मीडिया की हिंदी सभी को सहज और अपनी लगेगी।