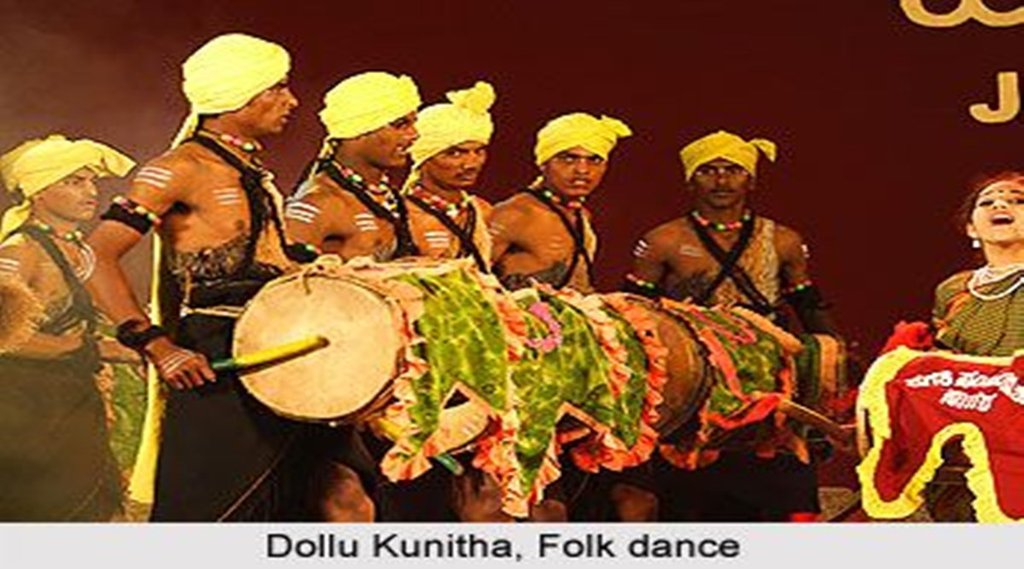खेती-किसानी वाले परिवार में जिसका बचपन बीता हो, उसके लिए एक गीत अनुभवों का पुनर्पाठ जैसा हो सकता है। शहरीकरण और मशीनीकरण की प्रक्रिया से गांव कैसे बदले हैं, इसका अंदाज तब लगता है जब हम हल-बैल-पगहा, जुआठ-जाबा, पैना-हेंगा, खरिहान, दवंरी-कटिया, रोपनी-बोअनी, जांता-ओखरी, ढेंकुल-इनार जैसे शब्दों से रूबरू होते हैं। दरअसल, ये मात्र कुछ भावनात्मक शब्द ही नहीं हैं, बल्कि बदल चुकी प्रक्रियाओं और उसके साथ बदले पारिवारिक-सामाजिक ताने-बाने का एक समकालीन इतिहास और समाजशास्त्रीय लेखा-जोखा भी देते हैं।
पारंपरिक गीतों को गाया जाता रहा है और ये इतिहास की लंबी यात्रा करके समय की बहती धारा में एक अनमोल रत्न की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिमार्जित और परिष्कृत होते रहे हैं। शहर में लोकगीत तपती दोपहरी में एक छरकका पानी बरसने जैसा एहसास देते हैं। देश या विदेश में रहते हुए भी ऊर्जा की कमी महसूस हो तो उन क्षणों में भोजपुरी लोकगीतों से ऊर्जा मिल सकती है!
विवाह के गीत से लेकर, बिरहा, लाचारी, बिदेसिया, फगुआ, झिझिया, बारहमासा, निर्गुण एक विविधता का इंद्रधनुष बनाते हैं। हालांकि गांवों में भी अब तेजी से बहुत कुछ बदलता जा रहा है। मोबाइल से लेकर अन्य तकनीकी संसाधनों के झोंके गांवों में बसे जीवन-तत्त्व को तेजी से बहा कर कहीं और ले जा रहे हैं। लोग इसमें बिना किसी शिकायत के बहे चले जा रहे हैं।
गांव में लोग जो वस्तुएं हाथ से बनाते थे, आज बाजार में वह करोड़ों का कारोबार बन गया, लेकिन गांव से वह बनना छूट गया। 1970 के उत्तरार्द्ध में और 1980 के पूर्वार्द्ध तक गांव में कुछ महिलाएं अपने हाथ से मौनी-डाली, दउरी, सिकहुता आदि बनाती थीं। जैसे-जैसे इनका आकार बड़ा होता जाता, इनका नाम बदल जाता। मौनी से बड़ी डाली, जिसमें गांव में लोग शाम को भुना हुआ चना-चावल-गेहूं का भुजा खाते थे।
सब्जी बेचने वाले दउरी सिर पर रख कर गांव में घूम कर बेचते थे। दउरी में रख कर ही शादी-तिलक-गौना में आए लड्डू-खाजा-इमरती, आस-पड़ोस के परिवारों में बांटा जाता था। अब शादियों में खाजा-इमरती का चलन बहुत कम हो गया है और दउरी की जगह पालीथिन और कागज के डिब्बों ने ले लिया है।
परिवारों के इतिहास और समाजशास्त्र के नजरिए से लोकगीतों को देखें तो इसमें जीवन की कशमकश और उत्सवधर्मिता का संगम है। संयुक्त परिवार में केवल एक बच्चे का जन्म नहीं रहा है, इससे नए संबंधों का सृजन भी होता है। एक दुल्हिन का मां के रूप में, पति का पिता के रूप में, आजी-बाबा, नानी-नाना, फुआ-फूफा, भइया-बहिन सबका नयापन होता है!
आज भी समाज में विवाह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय और संक्रमण होता है। तो इसकी एक-एक प्रक्रिया सामूहिकता से जुड़ी हुई है। यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं होता है! समाज में लड़की के लिए उपयुक्त वर खोजने पर भी पारंपरिक गीत हैं। अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन वाले पृष्ठ और वेबसाइट के पहले उपयुक्त वर खोजना एक तरह का व्यापक शोध का मामला होता था।
लड़की के घर वालों की उस पीड़ा की झलक भी लोक गीतों में मौजूद है। लेकिन लोक परंपरा के सामने औद्योगीकरण और शहरीकरण की चुनौती एक तरह से परती जमीन के रूप में उभरती है जो उनके फलने-फूलने को चुनौती देती हैं। इन्हीं दो कारकों ने सामाजिक-पारिवारिक ढांचे को सबसे अधिक प्रभावित किया है।
औद्योगीकरण के साथ पारिवारिक मामले में आधुनिक राज्य की भूमिका भी पिछले दो सौ वर्षों में बढ़ी है। आधुनिक राज्य के दखल से ही पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों में समानता की बात उठने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में जापान, जर्मनी, न्यूयार्क, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को लेकर कानून बने। उसी समय भारत में सती प्रथा के विरोध में बने कानून (1829), विधवा-विवाह के कानून, शादी की उम्र, भ्रूण हत्या संबंधी कानून (1870) ने भी पारिवारिक ढांचे में पिता की भूमिका को सीमित किया। इन सभी का असर आज हमारी सामाजिक-पारिवारिक प्रक्रिया पर दिखता है।
परंपरागत गीत, परंपरा और पुरखों की जमीन से भावनात्मक और मानसिक साहस देने का काम करते हैं। इसीलिए आज भी मारीशस के लोग गाते हैं- ‘कलकत्ता से छूटल जहाज, पवनिया धीरे बहो’ और सूरीनाम से नीदरलैंड गए भारतवंशी लोग भूजल-भात नाम से सलाना कार्यक्रम करते हैं! वैश्विक स्तर पर तकनीक के कारण लोक गीत प्रभावित हुए हैं, लेकिन तकनीक के द्वारा ही उनका संरक्षण और प्रसार भी संभव हुआ है।
हालांकि इसी दौर की तकनीकी सुविधा ने लोकगीतों के नाम पर कुछ अवांछित गीत भर कर एक गहरी चिंता पैदा की है। लेकिन यह भी थोड़ी राहत की बात है कि इसी दौर में इन पर तीखे सवाल भी उठे हैं और इसमें परिष्कार की मांग भी जोर पकड़ रही है।