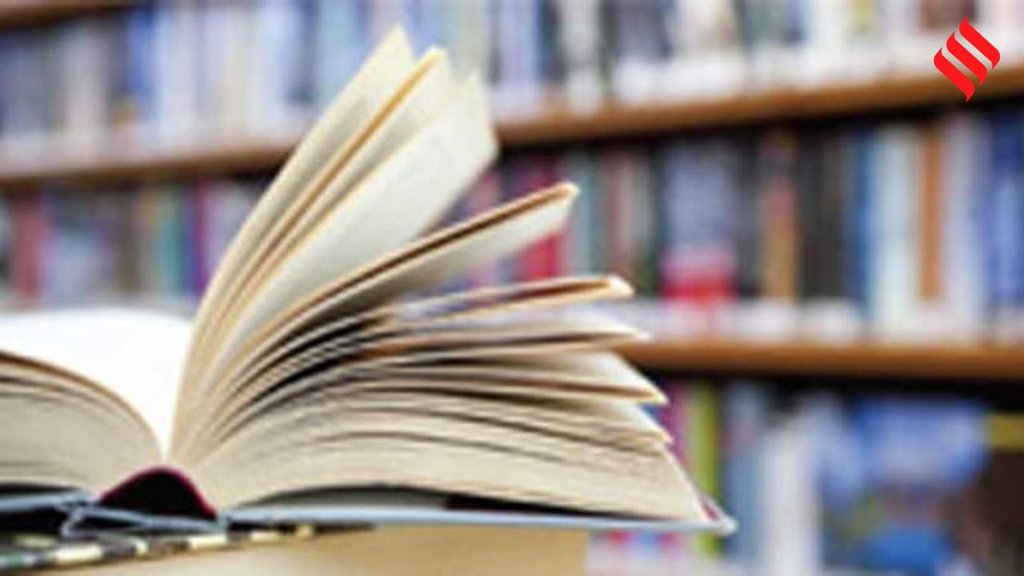कुछ दशकों पहले तक घर में पुस्तक का एक कोना किसी कक्ष में अवश्य होता था, लेकिन अब यह स्थान सीडी और ‘म्यूजिक प्लेयर’ ने ले लिया है। पुस्तकें सिर्फ हम अपने करिअर या भविष्य बनाने से संबंधित रखते हैं, जिनसे रोजी-रोटी का प्रबंध होता रहे। जो देश कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में अपने समृद्ध पुस्तकालयों के लिए प्रसिद्ध था, वहां गांवों में बारह हजार लोगों पर एक पुस्तकालय और शहरों में अस्सी हजार लोगों पर एक पुस्तकालय है, जो हमारे समाज की बौद्धिक विपन्नता और पाठकीय रुचि में ह्रास को दर्शाता है। हममें से जाने कितने तमाम लोगों ने विगत वर्षों में एक भी ढंग की पुस्तक नहीं खरीदी होगी।
जब समाज में बिना पढ़े-लिखे लोग ही सुविधा संपन्न जीवन यापन कर रहे हों, उनका पर्याप्त मान-सम्मान हो रहा हो तो पढ़ने-लिखने की जहमत कौन उठाए। यों छपे हुए शब्द की अर्थवत्ता और प्रभाव ही समग्र रूप से क्षीण हुआ है और पढ़े-लिखे व्यक्ति की सामाजिक हैसियत में गिरावट आई है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, शिक्षित लोगों के प्रति अनादर के भाव ने पुस्तक के महत्त्व और उसकी चमक को फीका किया है। यह अलग बात है कि लुगदी साहित्य और तथाकथित मनोरंजक साहित्य आज धड़ल्ले से बिक रहा है। नए लेखक अपनी बात को नई हिंदी और नई समझ के साथ पेश कर रहे हैं और युवा लेखकों ने अधुनातन समस्याओं को उठाकर अपनी जगह युवा पाठकों के बीच बनाई है। करिअर, कालेज के प्रेम प्रसंग और थोड़ी चटपटी वेब सीरिज जैसी भाषा स्थापित लेखकों को पदस्थापित कर रही है।
हमारे प्रकाशक पुस्तकों की बिक्री का रोना और पाठकों की कमी का रोना रोते रहते हैं। पाठक भी पुस्तकों के महंगे दामों की शिकायत करते पाए जाते हैं। लेकिन तीन सौ रुपए का पिज्जा और दो सौ रुपए का मल्टीप्लेक्स का टिकट लेते हुए उनको कोई मलाल नहीं होता, बस किताबों के नाम पर यह रोना शुरू हो जाता है। पुस्तकों के प्रति वह अनुराग और सम्मान भाव हिंदी पट्टी में फिलहाल बचा नहीं है। बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी प्रकाशक और समाचार पत्र बड़े-बड़े विशेषांक निकालते हैं।
पुस्तकों की खरीद का अलग से बजट रखा जाता है। दक्षिण भारत में भी पुस्तकों की अच्छी-खासी बिक्री होती है। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में एक पुस्तक का संस्करण दस हजार का होता है और देखते ही देखते बिक जाता है। जबकि हमारे यहां स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। दरअसल, शिक्षित समाज में उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रचलन बढ़ा है। किताबें हम वही खरीदना चाहते हैं जो हमें रोजगार दिला दे। बाकी नैतिक मूल्य और संबंधों की समझ, मानवीय संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को विकसित करने वाली साहित्यिक, प्रेरणादायी पुस्तकें हम खरीद कर पढ़ना नहीं चाहते।
डिजिटल युग में किताबें इंटरनेट पर ई-बुक या मौजूद संसाधनों या ऐप के जरिए पढ़ी भी जा सकती हैं और चलते-फिरते आसानी से सुनी भी जा सकती हैं। व्यस्त या बुजुर्गों के द्वारा इनका उपयोग भी हो रहा है। लेकिन जो बात मुद्रित पुस्तक में होती है, वह आनंद और अनुभूति इन ई-बुक में नहीं है। कोरी किताब के कागज की सोंधी गंध और उसके पन्नों को छूने, अपने सिराहने रखने, मनचाही पंक्तियों के रेखांकित करने का जो अनिवर्चनीय आनंद है, वह अद्भुत है।
पुस्तकों का स्वाध्याय न केवल हमारी स्मृति को दुरुस्त रखता है, बल्कि हमारे शब्द ज्ञान में भी वृद्धि करता है। हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाता है। पढ़ने से हमारा अवसाद दूर होता है, हमारी संवेदनाओं का संसार विस्तृत होता है। हम और मानवीय और विमर्श के योग्य बनते हैं। इसलिए पुस्तकें न केवल हमारी साथी हैं, बल्कि हमारी मार्गदर्शक भी हैं। विवाह, जन्मोत्सव आदि में पुस्तकें भेंट करने का पुण्य कर्म कुछ लोग करते हैं। यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए। अपने स्तर पर और प्रदेशों की ग्रंथ अकादमियां पुस्तक मेले आदि का आयोजन करती रहती हैं, लेकिन ये प्रयास पुस्तक संस्कृति के प्रचार प्रसार में मात्र ऊंट के मुंह में जीरा हैं।
व्यक्तित्व विकास, कल्पना और तर्कशक्ति के विकास में युवाओं को ही नहीं, नन्हे बालकों के जीवन में पुस्तकें अहम भूमिका निभाती हैं। ये हमारे बौद्धिक मोक्ष का द्वार हैं। हमें यह पुनीत संकल्प लेना चाहिए कि हम देश को आंकड़ों में ही साक्षर न बनाएं, बल्कि एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत समाज भी बनाएं, जहां पुस्तकें खुल कर सांस ले सकें, खिलखिलाकर ज्ञान बांट सकें।