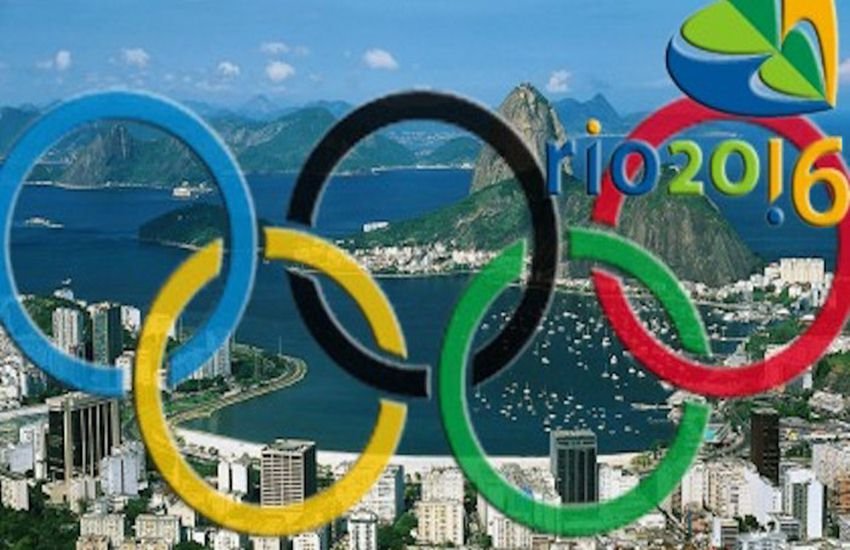आम भारतीय और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर 125 करोड़ की जनसंख्या का जिक्र करते हैं तो इसमें गर्व का भाव निहित रहता है। लेकिन रियो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन ने एक बार फिर सोचने को विवश किया है कि जनसंख्या का आकार उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रकार। पदकों की जिन उम्मीदों के साथ भारतीय खिलाड़ियों का भारी-भरकम दल रियो गया था, उन पर पानी ही फिर गया। यदि साक्षी मलिक और पीवी सिंधू पदक जीतने में सफल नहीं रहतीं तो खाली हाथ ही वापसी होती। यहां पुरानी मान्यता है कि ‘बहू-बेटियां घर की इज्जत हंै’ और इसके चलते उन्हें घर की चहारदीवारी में कैद रखा जाता रहा है। लेकिन अब, जब उन्हें पहले से थोड़े अधिक अवसर मिल रहे हैं, वे स्वयं को देश की इज्जत बचाने वाली साबित कर रही हैं।
इन दिनों लोगों के बीच और मीडिया में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों पर चर्चाएं होती रही हैं। एक मंच पर सवाल पूछा गया कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर इतनी भारी धनवर्षा होने के बावजूद क्यों पदक नहीं आ रहे हैं? इसका जो उत्तर मुझे सूझता वह यह कि किसी पौधे को खाद व पानी तब चाहिये जब वह बढ़ रहा होता है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को बचपन से ही पहचानने और तभी से गहन तैयारी व प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौर में उन्हें पौष्टिक भोजन और जरूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलते। यह बिल्कुल सही है कि जितने खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने गए वे अपनी प्रतिभा के बलबूते पर ‘क्वालिफाई’ करके गए। लेकिन पहले से उन्हें सुविधाएं मिलतीं तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।
भारत में हाल के वर्षों में अभिभावकों में बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का रुझान बढ़ा है। पिछली पीढ़ी तो ‘खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब’ की सोच में पक्का यकीन रखने के कारण बच्चों को खेलों से दूर ही रखती थी और उनकी स्वाभाविक रुचि का दमन करती थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अच्छे खिलाड़ी बनते थे। आज जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनमें से बहुतों को अपने बाप-दादा से खेलना विरासत में मिला है। लेकिन बच्चों को खेलों के लिए केवल इसलिए प्रोत्साहित करना कि इनमें दौलत-शौहरत बरसता है, उचित नहीं जान पड़ता। खेल बच्चों और बड़ों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और हार-जीत से ज्यादा महत्त्व खेल भावना का है।
भारतीय खिलाड़ियों को हरेक स्तर पर चयन के लिए ‘बाधा दौड़’ में भाग लेना अनिवार्य-सा हो जाता है, जो समाज में व्याप्त भेदभाव, पक्षपात या भ्रष्टाचार की देन है। इससे खिलाड़ियों की ऊर्जा बर्बाद होती है और उनमें कुंठा व निराशा पैदा होती है। खेलों से खिलवाड़ के इस माहौल में कभी-कभी खिलाड़ियों द्वारा आत्महत्या कर लेने के दुखद समाचार भी आते हैं। खिलाड़ियों के साथ जाने वाले प्रशिक्षकों, चिकित्सकों, प्रबंधकों के चयन पर अक्सर सवाल व विवाद उठते रहे हैं। खेल संघों की कार्यप्रणाली में भी सुधार अपेक्षित हैं।
रियो से क्या सीख ली जाएगी और कितनी चीजें बदलेंगी, कह पाना मुश्किल है।
’कमल जोशी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड</p>