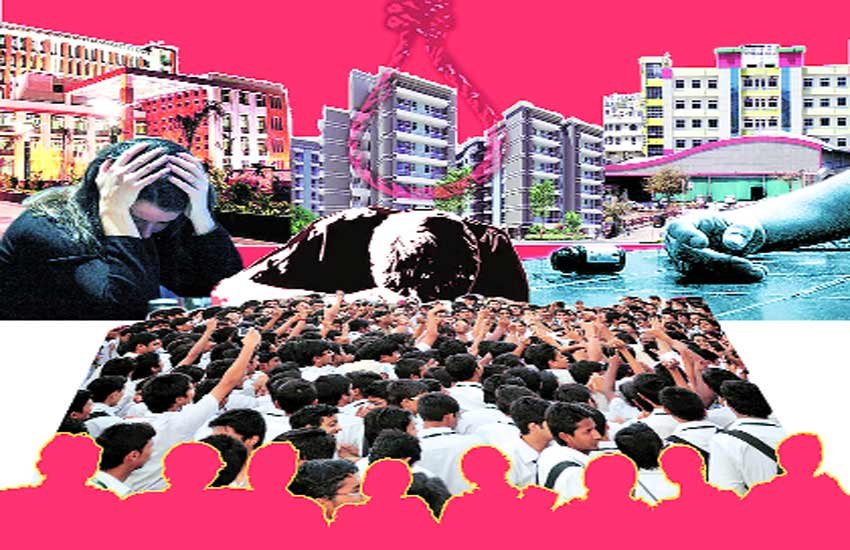बात मैं अपने उदाहरण से शुरू करता हूं। मेरी कोचिंग नब्बे दिन की है जिसमें अस्सी से एक सौ तीस विद्यार्थी तक होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी 36000 रुपए देता है। मतलब अगर हम औसत सौ विद्यार्थी भी प्रत्येक कक्षा में मानें तो चालीस हजार रुपए प्रतिदिन एक क्लास का और दिन में हमारा टीचर तीन क्लास लेता है, मतलब एक लाख बीस हजार रुपए प्रतिदिन की कमाई! यह मैं एक बहुत छोटी कोचिंग का उदाहरण दे रहा हूं जबकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग मौजूद हैं जिनके विद्यार्थियों की संख्या तीन से चार हजार हजार तक है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उद्योग मौजूद है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर। लेकिन पिछले साल महज छब्बीस बच्चों का चयन हुआ था संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में हिंदी माध्यम से और इस साल बावन का बताया जा रहा है। जबकि दिल्ली के मुखर्जी नगर का यह पूरा उद्योग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों पर ही आधारित है। पुलिस के आंकड़ों (सीसैट आंदोलन के दौरान) के हिसाब से मुखर्जी नगर के इस पूरे इलाके में 70-80 हजार विद्यार्थी मौजूद हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां एक बड़ा सवाल है कि सिविल सर्विस में हिंदी माध्यम के गिरते रिजल्ट का कारण क्या है? सरकार की नीतियां एक वजह हो सकती हैं जो युवाओं को देश का भविष्य तो मानती हैं पर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के युवाओं को। लेकिन एक बड़ी वजह यह कोचिंग उद्योग भी है जो हिंदी प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच एक भ्रम फैलाता है कि बिना कोचिंग के वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी क्षमता अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से बहुत कम है और जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वही अंतिम सत्य है और यही सफलता की आखिरी कुंजी है! अगर आप कोचिंग नहीं करते तो आपकी सफल होने की संभावना नगण्य है!
इस भ्रम और डर से अधिकतर विद्यार्थी कोचिंग का सहारा लेते हैं। ये छात्र अपनी विफलता की बड़ी वजह खराब कोचिंग को मानते हैं और फिर किसी नई कोचिंग में दाखिला लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों को यह अहसास होता है कि उन्हें ठगा और छला गया है तब तक दो-तीन साल निकल चुके होते हैं। जिस आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से ये छात्र आते हैं वहां उनके पास अब न इतने पैसे होते हैं और न वक्त कि और कुछ साल तैयारी कर सकें।
’अब्दुल्लाह मंसूर, जामिआ, नई दिल्ली</strong>
समान शिक्षा
एक तरफ राजधानी में दिल्ली पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय सरीखे स्कूल हैं तो दूसरी ओर नगर निगम और राजकीय विद्यालय हैं। इनकी सुविधाओं में भयंकर असमानता है। यह असमानता दूर करने के लिए हमें ‘सबको समान और निशुल्क स्कूली शिक्षा’ की मांग उठानी होगी। हर बच्चे के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। 1990 के दौर से जारी उदारीकरण और निजीकरण की जनविरोधी नीतियों ने सरकारी और निजी स्कूलों में खाई को और चौड़ा कर दिया है। ऐसे में हमें आम नागरिकों के बच्चों के भविष्य की खातिर संघर्ष करना होगा।
’प्रेम प्रकाश, बुराड़ी, दिल्ली
बधाई के साथ
एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा में विफल होने या कम अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं अपना उत्साह और यह विश्वास बनाए रखें कि जिंदगी का पूरा खेल सिर्फ अंकों के आधार पर तय नहीं होता है। दूसरी तरफ परीक्षाओं के परिणाम आते ही पूरा मीडिया उन छात्रों को मुबारकबाद देने में जुट जाता है जो लगभग शत-प्रतिशत अंक पाकर अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं। फेसबुक पर आजकल ऐसे सभी छात्रों को बधाई देने का दौर चल रहा है। उधर परीक्षा परिणामों से खिन्न होकर जब कोई छात्र दुखद कदम उठाता है तो हम दुनिया की उन मशहूर हस्तियों के नाम गिनाने लगते हैं जो परीक्षाओं में फेल होने अथवा कम अंक लाने के बावजूद जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष स्थानों पर पहुंचे। कोचिंग सेंटर वाले ऐसे प्रत्येक छात्र को, जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, अपने सेंटर से जुड़ा बताते हैं। सुना है, उनमें से कुछ ऐसे छात्रों को पैसा देकर खुद से जोड़ते हैं। यह सही है कि छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा जाए लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि इसकी एक सीमा होनी चाहिए।
आज हमारे प्रदेशों में जितने मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां रही होंगी। यही बात बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर भी लागू होती है। अधिकतम अंक पाने वाले सभी विद्यार्थी अंतत: इन्हीं के अधीन काम करते हैं। प्रशंसा तब होनी चाहिए जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे देश-विदेश यानी पूरी मानवता लाभान्वित हो। आप कोई ऐसा आविष्कार या खोज करें जिससे देश को भी लाभ हो या आप कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आपने समाज को एक नई दिशा और दृष्टि दी हो। अगर कोई पूरे अंक लाकर इंजीनियर, डॉक्टर, आइएएस जैसा कुछ बन कर बाद में सिर्फ अपना घर भरता है तो उसकी उपलब्धियों पर इतना हो-हल्ला क्यों?
’सुभाष चंद्र लखेड़ा, द्वारका, दिल्ली
नया मीडिया
न्यू मीडिया मतलब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि का चलन तेजी से बढ़ रहा है जिसने मीडिया को खबरें परोसने का एक नया और बढ़िया विकल्प दिया है। रोज नए आॅनलाइन समाचार चैनल खुल रहे हैं। समाचार देने वाली वेबसाइटों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हर अखबार का अपना ई-संस्करण है। खबर कैसी भी हो, तुरंत सोशल साइट्स पर आ जाती है और फिर शुरू होता है प्रतिक्रियाओं (कमेंट्स) का दौर। जिस तरह कई बार खबरों का सिर-पैर नहीं होता वैसा ही हाल कमेंट करने वालों का होता है। अक्सर ये कमेंट धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिए जाते हैं और इनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो आम बात है।
यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि लोग खुल कर अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन जिस तरह सांप्रदायिक नजरिए या अशालीन अंदाज में विचार रखे जाते हैं वह कहीं न कहीं सोशल मीडिया का नकारात्मक इस्तेमाल है जो धीरे-धीरे समाज में नफरत घोल रहा है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इस मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें कि दूरियां कम हों, न कि बढ़ें।
’अंकित श्रीवास्तव, नोएडा