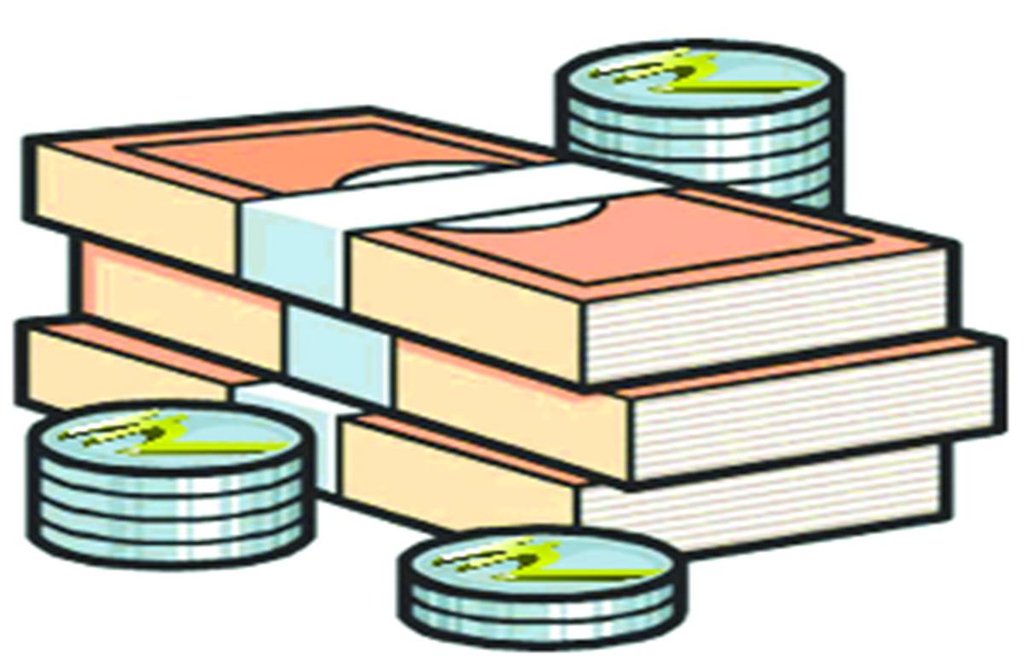वित्त वर्ष : यह वित्तीय साल होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। फिलहाल सरकार वित्त वर्ष को बदलने पर विचार कर रही है।
कर निर्धारण साल : यह कर निर्धारण साल होता है, जो किसी वित्तीय साल का अगला साल होता है। जैसे 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 अगर वित्तीय वर्ष है तो कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा।
मुद्रास्फीति : मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति का विपरीत अपस्फीति होता है, यानी वह स्थिति जिसमें समय के साथ-साथ माल और सेवाओं की कीमतें गिरती हैं।
अंतरिम बजट : अंतरिम बजट हर साल पेश होने वाले पूर्ण बजट से काफी अलग होता है। अंतरिम बजट एक खास समय के लिए होता है। चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होती है।
पिछला वित्त वर्ष : यह वित्तीय साल है, जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले आता है। यह एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। इस दौरान कमाई गई रकम पर कर निर्धारण साल में टैक्स देना होता है। यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 अगर वित्तीय साल है तो कर निर्धारण साल एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा।
विकास दर : सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक वित्त वर्ष के दौरान देश के भीतर कुल वस्तुओं के उत्पादन और देश में दी जाने वाली सेवाओं का जोड़ होता है।
वित्त विधेयक : इस विधेयक के माध्यम से ही आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सरकारी आमदनी बढ़ाने के विचार से नए करों आदि का प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही वित्त विधेयक में मौजूदा कर प्रणाली में किसी तरह का संशोधन आदि को प्रस्तावित किया जाता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाता है।
उत्पाद शुल्क : उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) उन उत्पादों पर लगता है जो देश के भीतर बनते हैं। यह शुल्क उत्पाद के बनने और उसकी खरीद पर लगता है। फिलहाल देश में दो प्रमुख उत्पाद हैं, जिनसे सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है। पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डीजल आदि) और शराब इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं।
राजकोषीय घाटा : सरकार की ओर से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्ज राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ है। इससे सरकार आय और खर्च के अंतर को दूर करती है।
प्रत्यक्ष कर : प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, जो व्यक्तियों और संगठनों की आमदनी पर लगाया जाता है, चाहे वह आमदनी किसी भी स्रोत से हुई हो। निवेश, वेतन, ब्याज, आयकर, कंपनी कर आदि प्रत्यक्ष कर के तहत ही आते हैं।
शार्ट टर्म कैपिटल असेट : 36 महीने से कम समय के लिए रखे जाने वाले पूंजीगत संसाधन को शार्ट टर्म कैपिटल असेट कहते हैं। शेयर, सिक्योरिटी और बांड आदि के मामले में यह अवधि 36 महीने की बजाय 12 महीने की है।
अप्रत्यक्ष कर : ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने और सेवाओं का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर लगाया जाने वाला कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है।
जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी आदि अप्रत्यक्ष कर के तहत ही आते हैं।
कैपिटल असेट : जब कोई व्यक्ति कारोबारी या पेशागत- किसी भी उद्देश्य से किसी चीज में निवेश करता है या खरीदारी करता है तो इस रकम से खरीदी गई संपदा कैपिटल असेट कहलाती है। यह बांड, शेयर मार्केट और कच्चा माल में से कुछ भी हो सकता है।
कैपिटल गेन्स : पूंजीगत एसेट्स को बेचने या लेन-देने से होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन्स कहलाता है।
असेसी : ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के तहत कर भरने के लिए उत्तरदायी होता है।
ग्रॉस इनकम : ग्रॉस सैलरी वह धन होता है, जो कंपनी की तरफ से आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है। इसमें मूल वेतन, किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता या डीए, विशेष भत्ता, अन्य भत्ते, छुट्टी के एवज में नकदी आदि शामिल होते हैं। ग्रॉस सैलरी को टेक होम सैलरी भी कहा जाता है। कर योग्य आय की गणना के लिए ग्रास इनकम का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पहला चरण होता है। कंपनी की तरफ से दिए गए फॉर्म-16 में ग्रॉस इनकम लिखा होता है।
नेट इनकम : ग्रॉस सैलरी में से जब एलटीए, एचआरए, ईएल इनकैशमेंट जैसे तमाम भत्तों को घटा दिया जाता है, तो ये आपकी नेट सैलरी बन जाती है।
कर योग्य आय : जब आपकी नेट सैलरी निकल आती है तो उसमें से आपकी सेविंग्स और डिडक्शन को घटाया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये का कम किया जाता है, आपकी तरफ से टैक्स बचाने के लिए 80सी के तहत किए गए निवेशों को घटाया जाता है, आपकी तरफ से दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को घटाया जाता है, किसी तरह के मेडिकल खर्च को आप दिखाते हैं तो उसे भी घटाया जाता है।
साथ ही इसमें किसी प्रॉपर्टी से हुई कमाई या फिर किसी अन्य सोर्स से हुई आमदनी को भी जोड़ा जाता है। ये सब होने के बाद सीधे-सीधे आयकर में मिलने वाली छूट की रकम को घटाया जाता है। (मौजूदा समय में यह 2.5 लाख रुपए है)। इन सब के बाद बची आय कर योग्य आय होती है।