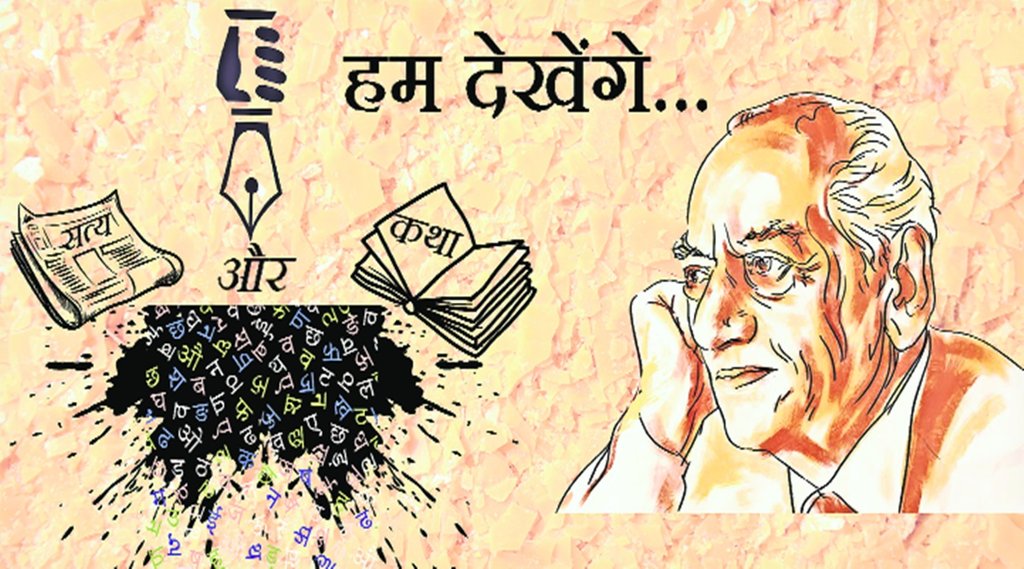Internet Age And Literary Creation: इंटरनेट की विडंबना है कि यह जिसका निर्माण करता है उसके विध्वंस के औजार को भी इसी से जन्म लेना होता है। इंटरनेट से उपजे साहित्य से लेकर नायकों तक का यही हासिल था। ‘सब याद रखा जाएगा’ कविता से लेकर कन्हैया कुमार जैसे प्रतिरोध के रूप को जनता ने याद नहीं रखा। किसी भी साहित्य या नायक का इंटरनेट से विस्तार का आयतन अपार है तो लोगों के जेहन में उसके जिंदा रहने की उम्र बहुत कम। इस दौर में जो हालात हैं उनमें शब्द और अर्थ गुम हो जाएंगे। कुछ रहा तो बस शोर ही रह जाएगा। पत्रकारिता बनाम साहित्य के संदर्भ में ‘सत्य और कथा’ की दूसरी कड़ी।
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे
फरवरी, 1986 में लाहौर के स्टेडियम में इकबाल बानो के गले से जब यह नज्म शुरू हुई तो इसे खत्म करना मुश्किल हो गया। इकबाल बानो के खत्म करते ही नज्म श्रोताओं के गले से उठ जाती थी। हम देखेंगे…कहते हुए हर दर्शक मंच पर बैठा इकबाल बानो हो जा रहा था। यह नज्म फैज अहमद फैज की थी, लेकिन मुखालफत इकबाल बानो की थी।
जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान में हर तरह की तानाशाही लागू करने के साथ पाकिस्तानी औरतों के साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। साड़ी पहनने की आजादी पर जिया की हकमारी के खिलाफ इकबाल बानो काली साड़ी पहन कर इस नज्म को गाने पहुंची थीं। तख्त पर बैठे तानाशाह को साड़ी पहन कर दिखाया…हम देखेंगे। इस कार्यक्रम की रिकार्डिंग को आज भी यू-ट्यूब पर देखना एक अतीतव्यामोह में पहुंचा देता है।
हम देखेंगे…नज्म भारत और पाकिस्तान के साझा राजनीतिक प्रतिरोध का हिस्सा बन गई। विश्वविद्यालयों से लेकर सड़क की राजनीति का बिसमिल्लाह इसी से होता था। इसके साथ ही फैज की अन्य नज्में, ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे…’ और ‘निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन कि जहां/चली है रस्म कि कोई न सिर उठा के चल सके’ आज भी मुखालफती जुबान का पसंदीदा नारा है।
क्या आज के हालात में भी हम साहित्य या अखबार को क्रांति का औजार कह सकते हैं
साहित्य और पत्रकारिता दोनों को क्रांति का सबसे बड़ा औजार कहा जाता है। लेकिन, इक्कीसवी सदी के खत्म होते 22वें साल में हमारा सवाल यह है कि क्या आज के हालात में भी हम साहित्य या अखबार को क्रांति का औजार कह सकते हैं? क्या आज किसी दस या बारह पंक्ति की रचना से उम्मीद कर सकते हैं कि वह आधी सदी तक लोगों के जेहन पर तारी रहे। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन से निकले इंटरनेट साहित्य को देख कर हम इसके जवाब में नहीं का विकल्प चुन सकते हैं।
चाहे वरुण ग्रोवर का लिखा ‘कागज नहीं दिखाएंगे’ हो या आमिर अजीज का लिखा ‘सब याद रखा जाएगा’ ये पंक्तियां उतने ही दिनों तक लोगों की जुबान पर रहीं जब तक इन्हें ‘लाइक’ और ‘शेयर’ मिलते रहे। इंटरनेट के असीमित विस्तार की विडंबना यही है कि उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। नागरिकता संशोधन कानून विरोध का कोई असर चुनावों में नहीं दिखा।
व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया लेकिन उस लखीमपुर में अजय टेनी की अगुआई में भाजपा आठों विधानसभा चुनाव जीत गई जहां मंत्री-पुत्र की गाड़ी से किसानों की कुचलने से हुई मौत के बाद सबसे ज्यादा ‘याद रखा जाएगा’ बोला गया था। चुनाव तक जनता सब कुछ भूल चुकी थी।
साहित्य विभिन्न माध्यमों से ही लोक तक पहुंचता है
कोई रचना कितनी कालजयी है यह तो काल विशेष के बाद ही पता चल सकता है। किसी भी रचना के प्रसार की गति में संचार के माध्यम की अहमियत होती है। साहित्य विभिन्न माध्यमों से ही लोक तक पहुंचता है। कागज से पहले भी साहित्य था, कागज के दौर में भी साहित्य था और आज कागज रहित इंटरनेट की दुनिया में भी साहित्य है। साहित्य का दायरा कितना बड़ा होता है यह उसके माध्यम पर ही निर्भर करता है।
पहले साहित्य का दायरा से लेकर उसके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की गति बहुत धीमी थी। तुलसीदास के लोक तक पहुंचने की गति अपनी थी, तो कबीरदास उस गति से नहीं पहुंचे जिस गति से आज पहुंचा जा सकता है। यहां माध्यम के साथ उसके प्रसार के आयतन व उसके असर को तुलनात्मक रूप से देखना होगा। आज तुलसीदास के ‘श्रीरामचरितमानस’ के पास यह कीर्तिमान है कि वह लोक के बीच एक समय में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला साहित्य है।
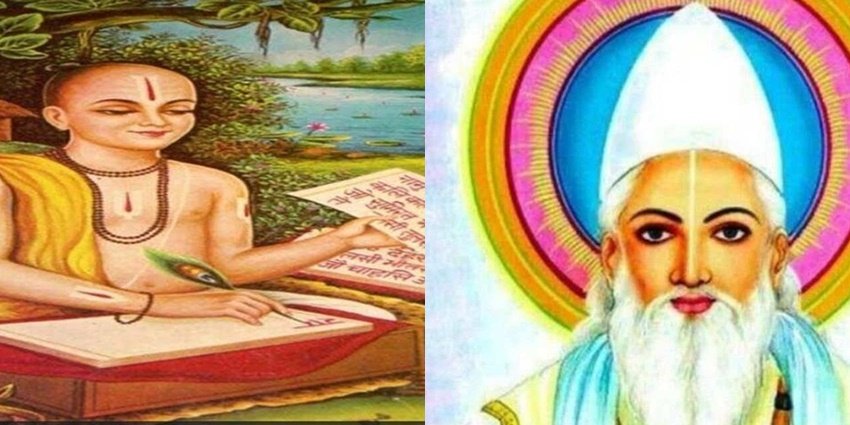
अक्षरज्ञान से विहीन कोई व्यक्ति उसे अपनी स्मृति से गुनगुनाता है तो देश के स्कूल, कालेज से लेकर विश्वविद्यालयों में शिक्षक उसकी चौपाइयां लिख कर विद्यार्थियों के साथ उसके साहित्यिक महत्व पर चर्चा करते हैं। तुलसीदास और कबीरदास के समय में इंटरनेट नहीं था। उस समय का बहुत कुछ एक की स्मृति से ‘कापी’ होकर दूसरे की स्मृति में ‘पेस्ट’ हुआ। आज तुलसी से लेकर कबीर और फैज तक हमारी स्मृति का हिस्सा हैं। लेकिन, ‘सब याद रखा जाएगा’ को आम लोग जल्द ही भूल गए क्योंकि इंटरनेट हमारी स्मृति को किसी और चीज के साथ संक्रमित कर रहा है।
इंटरनेट के इस युग में क्षणभंगुरता की भावना आई है।
इंटरनेट के इस युग में क्षणभंगुरता की भावना आई है। आज का साहित्य तुरंत छप सकता है और लोगों के बीच उसका दायरा भी विस्तृत होता है। लेकिन, कोई एक रचना स्क्रीन पर नीचे जाते ही दूसरी रचना सामने आ जाती है। एक घंटे में हम साहित्य की सैकड़ों पोस्ट से गुजर जाते हैं। साहित्य की किसी एक रचना को पढ़ना और उसे लंबे समय तक जेहन में रखना दोनों विरोधाभासी चीजें हो गई हैं। माध्यम का आयतन हमारे भावना-क्षेत्र के आयतन को पार कर जाता है।
मात्रात्मक रूप से देखें तो इतनी बड़ी संख्या में रचनाकार कभी नहीं थे, जितने आज हैं। आज छपने का कोई संकट नहीं है, दायरे के विस्तार का कोई संकट नहीं है। संकट है बस शब्द के स्मृति में रहने की समय-सीमा का। अरब वसंत से लेकर जेएनयू के वसंत बने कन्हैया कुमार के भाषण तक हम इस सिकुड़ती स्मृति-सीमा को देख सकते हैं।
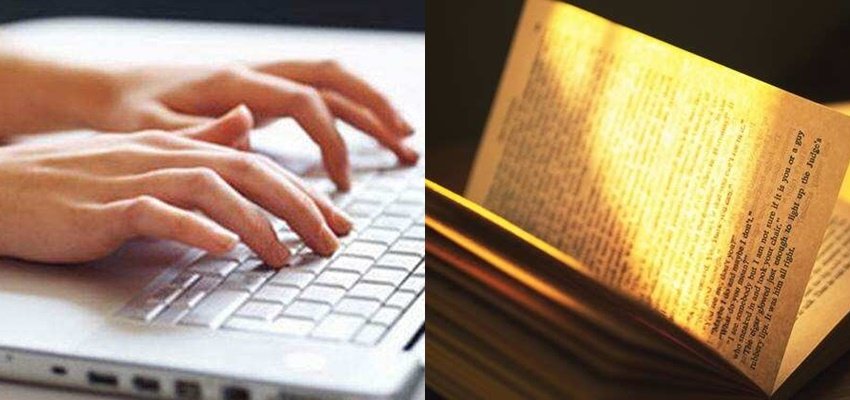
इंटरनेट पर जिस तरह कन्हैया कुमार के भाषण वायरल होते थे, उन्हें केंद्र के चेहरे का ही विकल्प करार दे दिया गया। लेकिन, बिहार के बेगूसराय से चुनाव हारने के बाद कन्हैया कुमार भी क्षण-भंगुर स्मृति-लोप के शिकार हो गए। यही कारण है कि इससे जिसका सृजन होता है उसके विखंडन का भी यही जिम्मेदार होता है। इसके भस्मासुर वाले रूप को देखते हुए दुनिया भर में जो सरकारें इंटरनेट के भरोसे आती हैं वह सबसे पहले इस पर ही नियंत्रण करना चाहती हैं, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है परतदार निर्माण।
कहा जाता है कि एक बार जो चीज इंटरनेट पर आ जाती है वह अमिट है, वह इस नई संजालीय सृष्टि का हिस्सा हो जाती है। लेकिन, यह अमिट सहज रूप से स्मृति का हिस्सा नहीं रहता हां, विशेष अवसरों पर इसे इंटरनेट की खुदाई कर निकाला जा सकता है। एक स्मृति के ऊपर चंद मिनटों में स्मृति की इतनी परतें चढ़ती हैं कि उस स्मृति-मीनार के सामने हमारी चेतना बौनी हो जाती है।
कथित वैश्विक इंटरनेट के साथ वही दिक्कत है जो आज हमारे खान-पान के साथ है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी सेहत के लिए वही अच्छा होता है जो हमारी जलवायु में मिलता है। एक उत्तर भारतीय के लिए ड्रैगन फल या अवाकाडो से ज्यादा सेहतमंद और इसकी तुलना में काफी सस्ते अमरूद होंगे। सरसों पैदा होने की जलवायु में जैतून के तेल से ज्यादा सेहतमंद सरसों का तेल होगा।
इंटरनेट के जरिए आयातित विमर्श हमारी मानसिक सेहत को तितर-बितर कर रहा
उसी तरह इंटरनेट के जरिए आयातित विमर्श भी हमारी मानसिक सेहत को तितर-बितर करता है। जब नोएडा की अमीर रिहाइशों में महिलाओं के सुरक्षाकर्मियों को पुरुषवादी गाली देने के मामले आ रहे थे तो इंटरनेट पर वहीं की खास वर्ग की महिलाएं ईरानी महिलाओं के हिजाब को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में बाल काट कर वीडियो डाल रही थीं।
‘मैं भी अर्बन नक्सल’ से लेकर बाल काटने के वीडियो तक के सफर को देखें तो किसी का भी लंबे समय तक कुछ भी हासिल नहीं है। हम बस एक हैशटैग से दूसरे हैशटैग पर मानसिक छलांग लगा देते हैं। इस क्षणिक छलांग से न तो कोई क्रांति संभव है और न कोई बदलाव।
ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क के हाथों में जाना वह परिघटना है जो भविष्य की क्रांति और बदलाव के मुहिमों को प्रभावित कर सकती है। ट्विटर के नीले निशान के भुगतान की बात शुरू हो चुकी है। मस्क उन लोगों में से हैं जो मसखरी का रूप धरते हुए बहुत संजीदगी से इस दुनिया को अपने हिसाब से बदल रहे हैं। अखबार, साहित्य, क्रांति पर यह चर्चा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। (क्रमश:)