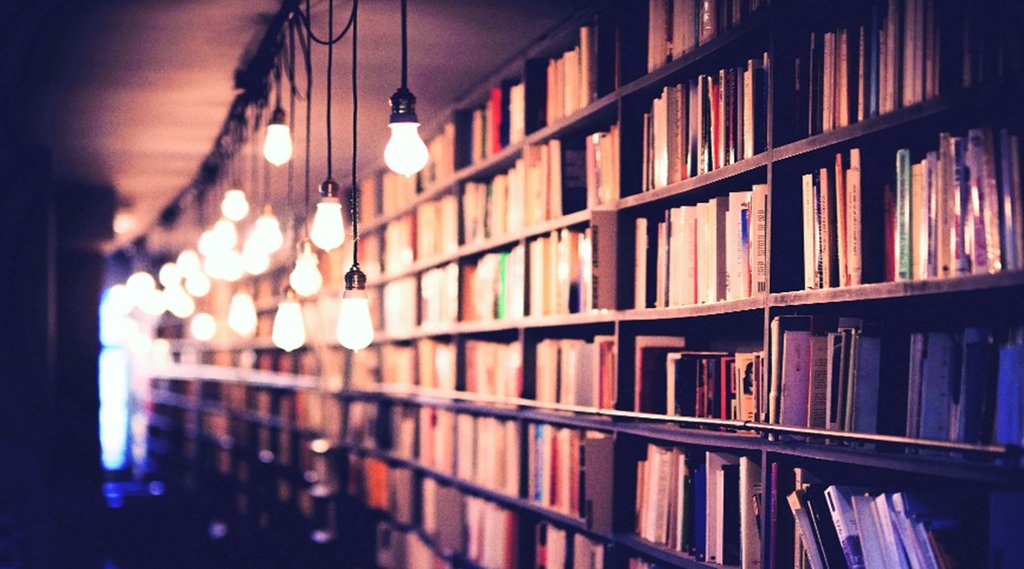प्रेम प्रकाश
कविता को संस्कृति का सबसे प्रामाणिक रचनात्मक दस्तावेज माना गया है। यह दस्तावेज समय के साथ जर्द नहीं पड़ता बल्कि हमारी चेतना का ‘कंपास’ बन जाता है। टीएस इलियट की लंबी कविता ‘द वेस्ट लैंड’ आज दुनिया के आगे इसी कंपास की तरह है। तारीफ है कवि और उसके रचनात्मक सरोकारों की कि यह कविता बीसवीं सदी की उत्कृष्ट लिखावट से आगे आज भी कई प्रासंगिक सवालों और दरकारों के सामने रचनात्मक निर्भीकता और दमखम के साथ खड़ी है। इस कालजयी रचना पर विशेष।
अजकल समय प्रबंधन की खूब चर्चा होती है। यह प्रबंधकीय दृष्टि जीवन और समय से जुड़े भौतिकीय दरकारों और उपलब्धियों को महत्व देती है। इससे उलट भारतीय अध्यात्म और दर्शन परंपरा में काल चिंतन को लेकर आधारभूत बातें कही गई हैं। साहित्यिक आलोचना के भारतीय संदर्भ में भी काल को महत्व दिया गया है।
तत्काल और समकाल के धुंध से बाहर निकलने की दरकार के बीच जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि कोई रचना तभी बड़ी है जब वह सार्वकालिकता और सार्वदेशिकता के निकष पर खरी उतरती हो। इस लिहाज से सृजन और काल का जो साझा संदर्भ सामने आता है, वह हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटने को विवश करता है। ओशो ने इसके लिए कहा है कि रौशनी हमेशा पीछे से आएगी, तभी हम आगे का रास्ता चुन सकते हैं, उसे तय कर सकते हैं। सामने से आती रौशनी तो चौंध पैदा करती है, जिसमें कुछ दिखता नहीं है।
रचना और कृति
रचना और काल से जुड़ी इस समझ के साथ इतिहास की तरफ देखें तो शताब्दी यात्रा तय कर चुकी एक महान कृति हमारा हाथ थामने के लिए सामने आती है। दरअसल, हम चर्चा कर रहे हैं महान कवि टीएस इलियट की। ‘द वेस्ट लैंड’ उनकी महानतम कृति है। इसके औपचारिक प्रकाशन का वर्ष 1922 माना गया है। यह लंबी कविता उद्योग, विकास और समृद्धि के बीच आकार लेती दुनिया में मानवीय सभ्यता के सफर और हश्र को बहुत गहराई से व्याख्यायित करती है।
आज जब दुनिया विश्वयुद्ध की आहट से एक बार फिर डरी हुई है, विकास और वर्चस्व की नई औपनिवेशिक ललक ने मानवीय संवेदना की हर दरकार को बेमानी साबित कर दिया है, तो इलियट की यह कविता हमें नए सिरे से विवेक और सामर्थ्य के उन तमाम दमदार दावों को परखने के लिए बाध्य करती है, जिसका झांसा हर लिहाज से हिंसक है, अमानवीय है।
हिंद स्वराज
दिलचस्प है कि ‘द वेस्ट लैंड’ से पहले 1909 में गांधी एक छोटी पुस्तिका ‘हिंद स्वराज’ के साथ दुनिया के सामने नए सभ्यता विमर्श के साथ प्रस्तुत होते हैं। इलियट अपने समय में रची जा रही आधुनिकता को बड़े उद्योगों के धुंओं में डूबी मानवता और दिशाहीन अंधकार में बढ़ते कदम के तौर पर देखते हैं तो गांधी सीधे-सीधे भारी उद्योग और भारी खपत के सभ्यतागत अनुशीलन पर सवाल उठाते हैं।
इलियट की चिंता मानवीय संवेदना की सजलता नष्ट होने और उसके भीतरी उजास के कालिख में बदलने की है तो गांधी प्रेम और करुणा के साथ विकास के विकेंद्रित माडल की दलील देते हैं। इन दोनों की चिंता को साझे तौर पर देखें तो हमें अपने मौजूदा हश्र पर एक तो आश्चर्य नहीं होगा, वहीं हमें यह भी दिखेगा कि आगे का रास्ता कहां और किधर है।
जटिल शिल्प
काव्यशिल्प के लिहाज से ‘द वेस्ट लैंड’ पहले भी जटिल मानी गई और आज भी इसकी व्याख्या को लेकर आलोचकीय सहजता नहीं दिखती है। यह असहजता कैसी है, इसे हम हिंदी में मुक्तिबोध की लंबी कविता ‘अंधेरे में’ के संदर्भ में समझ सकते हैं। दरअसल, जब चिंतन का आधार गहरा और व्यापक हो और उसके सामने चिंता अखिल मनुष्यता की हो तो रचना कीशिल्पगत चुनौती स्वाभाविक है।
इस स्वाभाविकता से रचनात्मक अपरिचय ऐसी कृतियों को जटिल मान लेने की नियति को जन्म देती है। यही कारण है कि न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद इलियट लंबे समय तक इस दुविधा में रहे कि उनकी इस कृति का अतिशय विस्तार और जटिल शिल्प इसे कहीं अंतिम रूप से अभाष्य या दुरूह मानने की नौबत तक न धकेल दे।
रचनाकाल के लिहाज से इलियट की यह कविता पहले विश्वयुद्ध की नियति के बीच लिखी गई। इससे पहले दुनिया के आगे अकूत उत्पादन और विज्ञान के चामत्कारिक उपक्रम के जरिए वर्चस्व और सत्ता की भोगवादी संरचना का औपनिवेशिक आख्यान सामने आ चुका था। यही नहीं, धर्म और संप्रदाय के तौर पर ईसाइयत ने भी इस दौरान अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि वह खुद में वर्चस्व का बड़ा और तकरीबन अभेद ढांचा बन गया। एक ऐसा ढांचा जो अराजकता और राजसत्ता दोनों को एक साथ आशीष दे रहा था।
असुकुमार बिंब
इलियट की 434 पंक्तियों की यह कविता दरअसल अपने समकाल से मुठभेड़ के बीच मनुष्य और उसके सभ्यतागत विकास पर एक कवि हृदय की व्यथित और विस्तृत टिप्पणी है। यह टिप्पणी हमें जहां शोकाकुल करती है, वहीं संवेदनात्मक तकाजों से दूर होते जाने की नियति के प्रति पुरजोर तरीके से आगाह भी करती है।
इसके प्रसिद्ध मुहावरों में ‘अप्रैल इज द क्रुअलेस्ट मंथ’, ‘आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल आफ डस्ट’ से लेकर ‘ओम शांति: शांति: शांति:’ तक शामिल हैं। साफ है कि इलियट अपने बिंब विधान में किसी सुकुमारता के मोह से मुक्त हैं। मुक्त छंद में लिखी और विभिन्न साहित्यिक संदर्भों एवं उद्धरणों से भरी इस लंबी कविता में देश-समाज की तत्कालीन परिस्थिति का अत्यंत नैराश्यपूर्ण चित्र खींचा गया है।
एक द्रष्टा की भविष्यवाणी
इलियट काफी क्षुब्ध मन से अनाकर्षक एवं कुरूप रूपकों-उपमाओं का प्रयोग करते हैं ताकि पाठकों को वे अपनी उस चिंता से जोड़ सकें जो उन्हें एक कवि होने के नाते युगसत्य को उद्घाटित करने के लिए प्रेरित करती है। जाहिर है कि वे पाठकों की भावना को ठेस पहुंचाने की हद तक रचनात्मक जोखिम लेते हुए यह सब करते हैं।
दिलचस्प है कि जिस जोखिम के साथ इलियट ने ‘द वेस्ट लैंड’ को पूरा किया, वह जोखिम उन्हें हमारे सामने एक ऐसे द्रष्टा के तौर पर सामने लाता है जो शताब्दी पूर्व यह कह-लिख चुका है कि उद्योगों की चिमनी से उठने वाले धुएं और जंग के मैदान में उठने वाले गुबार के बीच मनुष्य और उसके सभ्यतागत तकाजों का निढाल पड़ते जाना तय है।