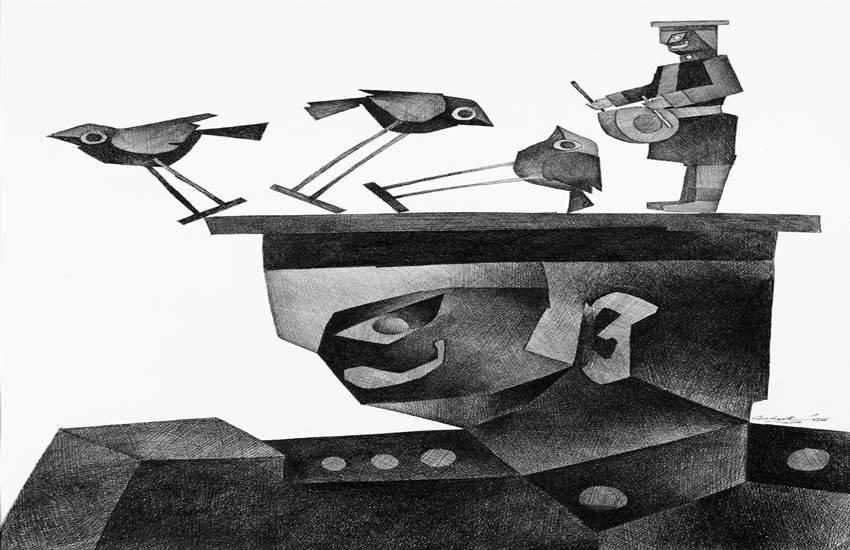आनंद कुमार सिंह
कहानी अपने ढांचे में पुरानी होते हुए भी एक नई विधा है, जिसे अंग्रेजी में ‘शॉर्ट स्टोरी’ कहते हैं। हिंदी में इसका आगमन हुए लगभग सवा सौ साल होने को आए, लेकिन इसे समझने के मानक ठीक तौर पर अभी तक विकसित नहीं हो सके हैं। यहां तक कहा जाता है कि हिंदी में कहानी की आलोचना का विकास ही नहीं हुआ है। कुछ हद तक यह बात इसलिए ठीक लगती है कि कविता जैसी विधा, जो परंपरिक होते हुए भी नवीन है और जिसमें विगत पचास सालों में ही कितना उछाल आ चुका है, उसे समझने के लिए पारंपरिक दृष्टि के साथ-साथ आधुनिक दृष्टि का विकास हिंदी में दिखाई देता है। कह सकते हैं कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नई कविता भी आलोचकों की जद से बाहर नहीं जा सकी, इसलिए सभी महत्त्वपूर्ण आलोचकों ने अपने विचार-विमर्श के केंद्र में कविता को ही महत्त्वपूर्ण मान कर रखा है। लेकिन यही बात कहानी, बल्कि नई कहानी के बाबत नहीं कही जा सकती। दिलचस्प यह भी है कि नई कहानी ने अपनी शुरुआत में मूर्धन्य आलोचकों को अपनी ओर खींचा था, लेकिन बाद में उनमें से कुछ कविता की ओर मुड़ गए। कुछ ने आलोचना का काम ही छोड़ दिया और कुछ की पकड़ से कहानी ही बाहर चली गई।
मगर यह भी सच है कि नामवर सिंह, धनंजय वर्मा, मधुरेश और विजय मोहन सिंह, देवीशंकर अवस्थी जैसे समीक्षकों के काम को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहानी के नएपन को पुराने छिलकों से बिलगा कर देखा और रूप, अंतर्वस्तु, संगठन, अंतर्विरोध, तनाव, पठनीयता और कहानीपन जैसे प्रतिमानों की चर्चा चलाई। न केवल यही, बल्कि उन्होंने नई कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी आदि के जुमलों को, जिसे मोहन राकेश-राजेंद्र यादव-कमलेश्वर की त्रयी ने खूब उछाला था उसे, कहानीकारों की मंशा से अलग केवल प्रवृत्ति विशेष के रूप में ही स्वीकार किया। वह नामवर सिंह थे, जिन्होंने प्रगतिवाद की सीमाओं से बाहर जाकर कहानी के रूप-संगठन और शिल्प की तरलता की चर्चा की और निर्मल वर्मा की ‘परिंदे’ कहानी को हिंदी की पहली आधुनिक या नई कहानी मानने का खतरा मोल लिया। वह बात अब भी कहानी की चर्चा करते हुए अनायास सामने आती है। बाद में उदय प्रकाश की कहानियों को लेकर विजय बहादुर सिंह ने भी इसी तरह की पहल की थी। गोपाल राय, परमानंद श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने नए, पुराने और बिल्कुल नए कहानीकारों पर ढेर सारी बात की है, लेकिन कहानी आलोचना के प्रतिमानों का स्वरूप स्थिर नहीं हो सका। परिणाम यह हुआ कि कहानी को लेकर हिंदी में एक अराजकता का माहौल है।
अस्सी के दशक और उसके बाद अनेक महत्त्वपूर्ण कहानियां लिखी गर्इं, जो आलोचकों की दृष्टि से ओझल रहीं। उन्हें पाठकों ने अपनाया, जिसे समीक्षकों ने नजरअंदाज किया। इन कहानीकारों ने अपने जिए गए जीवन के सापेक्ष बाहरी जीवन की विविधता और उसकी अनगढ़ता को बाकायदा कथाशिल्प में ढाला है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आज भी जबकि कहानी का वर्तमान परिदृश्य सर्जना के लिहाज से बहुत उर्वर और उपजाऊ है, वहीं पर आलोचना के औजार वर्तमान कहानी को समझने-समझाने के लिए नाकाफी नजर आते या छोटे पड़ते हैं। स्वयं कहानीकार इसे अनेक बार कहते ही हैं, समीक्षकों को भी इस अपूर्णता का बोध होता रहता है। इसका आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या कहानी एक अधूरी और अपूर्ण विधा है या कि आलोचना ही अधूरी है, जो कहानी को पकड़ नहीं पाती! क्या जीवन-दृष्टि को अपने समूचेपन में अभिव्यक्त करने में कहानी लाचार है, पंगु है या कि उसे आलोचकों द्वारा वह भूमिका ही अदा नहीं करने दी गई? क्या कारण है कि समकालीन कहानी की आक्रामकता को भी देख पाने में आलोचक विफल रहे। पिछले तीस-पैंतीस सालों में कहानी का भूगोल और अक्षांश ही खिसक गया है। कहानी अपने घाट-बाट से बहुत दूर बह कर आ चुकी है। आलोचक के लिए जरूरी है कि वह उस यथार्थ को पकड़ने के नए उद्यम करे। नए यथार्थ की कहानी, ग्रामीण संवेदना की कहानी, स्त्री-पुरुष के मौलिक अंतर्द्वंद्व की कहानी और तकनीकी उलझनों में रचे-बसे जीवन की सच्चाइयों की कहानी, पिछले तीन दशकों में बहुत त्वरा से चीजें आपस में संगुंफित होती चली गई हैं। भाषा-शैली, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन आदि जंग लगे और घिस चुके प्रतिमानों के आधार पर आज की कहानी को समझना बहुत कठिन है। वह कोई जैविक प्रतिमान नहीं है। वह कहानी को खंड-खंड करके देखने का उपक्रम है, जिस प्रक्रिया में कहानी ही मर जाती है। क्या ऐसा प्रतिमान नहीं विकसित होे सकता, जिससे हम कहानी के जीवित होने के क्षण में ही उसके साथ न्याय कर सकें? हमारे बड़े आलोचकों ने खतरे उठा कर जो बातें बहुत पहले कही थीं, क्या वहां से आगे हिंदी कहानी को नहीं ले जाया जा सकता? क्या पश्चिमी प्रतिमानों की मुंहदेखी करते हुए ही हम आलोचना के औजार बनाएंगे? क्या हमारे देश की परंपरागत कहानी के मलबे में ऐसा कुछ नहीं जिसको ‘रिसाइकिल’ किया जा सके? सवाल तो और भी हैं।
हम जानते हैं कि अब मामला बिल्कुल दूसरी ओर जा चुका है। अब हम एक ऐसी मांग कर रहे हैं, जो उत्तर-आधुनिक समय में संभव ही नहीं है। हम आज कहानी की आलोचना का वृहद आख्यान ही क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसे ‘नैरेटिव’ संकटग्रस्त हो चुके हैं? बनना ही था, तो प्रतिमान पहले ही बन जाने थे। अब तो कहानी भी उपशीर्षों में लिखी जाने लगी है, विधाएं गड्डमड्ड हो गई हैं और उनका ढांचा ही बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी मांग करते हुए हम किसी शाश्वत प्रतिमान की जकड़बंदी में कहानी जैसी जीवित विधा को कैद करना चाहते हंै? अभी तक तो यही कहा जाता रहा है कि आलोचना के निकष स्वयं विधाओं के भीतर से निकलते हैं। लेकिन सवा सौ सालों की हिंदी कहानी यात्रा में अब तक कहानी के भीतर से भी कोई शास्त्र बन कर तैयार नहीं हो सका। क्या इसका कारण केवल इतना है कि हिंदी कहानी को मुकम्मल आलोचक नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी की विधागत सीमा में ही चुनौती निहित हो कि इसका समीक्षक खंड-खंड समीक्षक होगा, वह हमेशा अधूरा होगा और पूरा होते ही कविता की ओर चला जाएगा। अब तक यही होता आया है।
क्या कहानी जीवन की बड़ी अर्थवत्ताओं को उस कौशल और बल से उठाने में न्यून रह जाती है, जिसे कविता बहुत हल्के प्रयत्न से उठा लेती है? कहानीकार तो यही कहते हैं कि कविता की रचना से कहानी लिखने की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि कहानी को देश-काल की जमीन पर ठीक से पैर जमा कर चलना पड़ता है, जबकि कविता ऐसे दलदलों के सामने आने पर उड़ान भरने का विकल्प खुला रखती है।
जाहिर है कि यह एक पुरानी बहस है, पर इस दृष्टि से भी इस पर सोचा जाना चाहिए। केवल समीक्षक क्यों, स्वयं कहानीकारों ने भी कहानी से दूरी बना ली। जब अज्ञेय ने कहानियां लिखनी छोड़ दी, तो यही इल्जाम लगाया गया कि कहानी उनसे छूट गई। संभवत: जीवन का बदला हुआ यथार्थ उनसे छूट गया। एक बार फिर यह बात केंद्र में लगती है कि सचमुच ही जिसे कहा गया कि ‘टाइम इज आउट आफ ज्वाइंट’ यानी काल की चूलें उखड़ गई हैं, वही बात आज कहानी के यथार्थ के साथ घटित हो रही है। आज की कहानी बड़े जीवनादर्शों और सामाजिक सत्यों को सर्वथा नए शिल्प में उकेर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर आलोचकों की पूरी दृष्टि नहीं पड़ रही। आजकल आख्यानों के संकटग्रस्त हो जाने से कहानी ने अपना आलोचकीय विवेक खुद कहानी के शिल्प में ही प्रतिष्ठित करने का काम किया है। लगभग हर कहानी एक सुरंग बनाती है, जो दूसरे छोर पर पाठक की आंख की पुतली में खुलती है। समकालीन कहानी का लेखक एक समांतर आलोचना अपनी कहानी में स्वयं ही करता चलता है। उसे ऐतिहासिक हड़बड़ी और जल्दी भी है। जाहिर है कि समीक्षा को ही अपना दायरा बड़ा करना होगा, क्योंकि कहानी ने अपना तेवर, अंदाज और अपनी राजनीति बदल दी है। इसलिए आलोचना को अपने देसी औजार विकसित करने चाहिए। समीक्षकों के सामने असल चुनौती यही है।