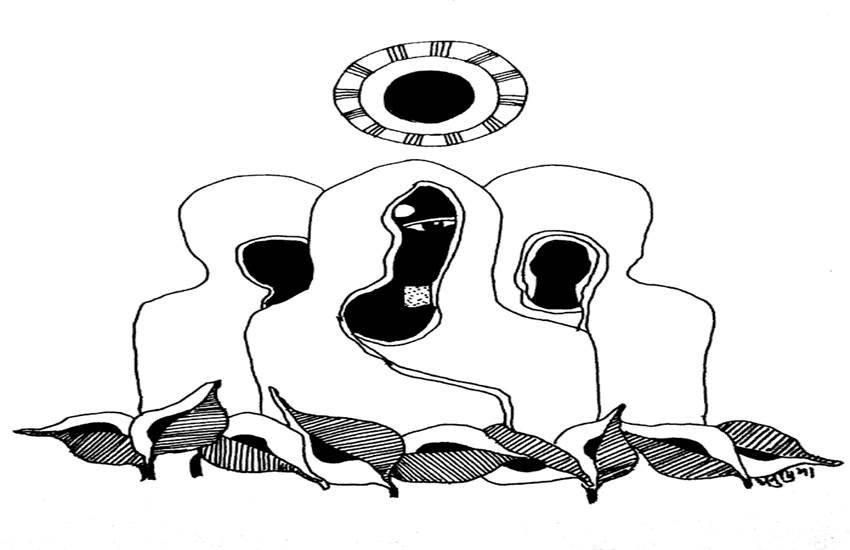जब एक लड़की जन्म लेती है, तो भविष्य की एक मां, एक बहन और एक पत्नी जन्म लेती है। वह चिंता की तरह क्यों आए, चेतना की तरह क्यों नहीं? भारतीय समाज तो लड़की के जन्म को लक्ष्मी या सरस्वती का जन्म कहते हैं, वही लक्ष्मी, सरस्वती आगे चलकर परिवार में बोझ की तरह क्यों देखी जाती है? उसे हमारे बौद्धिक विमर्शों में समानता के नाम पर पुरुष-छवि देने की कोशिश की जाती है। पर वह पुरुष क्यों बने, प्रति-पुरुष क्यों नहीं, पुरुष से बेहतर क्यों नहीं? उसकी छवि को आंसुओं के आईने में ही क्यों देखा जाए, अग्नि-धर्मा के अग्नि-चैतन्य रूप में क्यों नहीं? कवि-लेखक उसका नख-शिख वर्णन ही क्यों करें, उसकी मानवीय संवेदना का क्यों नहीं। उसके अंदर के उस मर्म का क्यों नहीं, जो अपने पति या पिता को भी मातृत्व-भाव से देखती है, निस्वार्थ सेवा करती है। उसे कोई भी अंकशायिनी बना कर आनंदित या गर्वित क्यों होता है, उसे प्राणदायिनी या वीर-प्रसूता क्यों नहीं माना जाता? सच पूछा जाए तो वह सृष्टि है, सृष्टि पर कुदृष्टि का कोप क्यों, जबकि स्त्री पुरुष से अधिक मानवीय है।
एक लड़की परिवार में जैसे-जैसे बड़ी होती है, उसे संस्कार-दीक्षा दी जाती है। उसे एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी बनने के कई मंत्र दिए जाते हैं। यहां तक कि उसे पिता और पति के परिवार में एक निर्विरोध और आज्ञाकारी सेविका बनने की भी हिदायतें और मर्यादाएं सिखाई जाती हैं। मगर वह एक स्वतंत्र, स्वायत्त, स्वावलंबी, स्वाभिमानी और वक्त आने पर निर्भीकता पूर्वक अपनी आत्मरक्षा की शक्ति बनने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। एक लड़की को हम परिवार में शक्तिरूपा न मान कर, पराया धन मानते हैं और पति के परिवार के लिए तो वह मानवीय-धन भी न होकर दहेज-धन हो जाती है। कितनी मानसिक यंत्रणाओं और वर्जनाओं में जीना होता है एक लड़की, स्त्री या पत्नी, मां, बहन को! अगर वह नौकरी करती है तो नौकरी के संदेहों और लांछनों में भी क्या यही नारी का ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यंते’ रूप है? अगर उसकी पूजा में देवता का निवास है, तो पुरुष उसे पूजा का देवता बनने के बजाय उसका शोषक क्यों बन जाता है? वह देह से शोषित होती है, मन से शोषित होती है और अगर कमाती है तो कमाई से या दहेज से शोषित होती है। इतने शोषणों में जीते हुए स्त्री समाज की बनाई गुलामी की जटिल रस्सी से मुक्त हो तो कैसे! उसके लिए हर दिशा का दरवाजा या तो बंद है या वहां समाज का तथाकथित पहरेदार सिपाही बैठा है।
कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्रियों को लेकर एक ओर समानता और सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक उत्तेजित और आक्रोशभरी बहसें होती हैं, जिनमें पढ़ी-लिखी, सजी-धजी, ऊंचे ओहदे या स्वदेशी-विदेशी संगठनों से जुड़ी विदुषियां शमिल होती हैं। कम्प्यूटर पर प्रेजेंटेशन बड़ी चमक-दमक के साथ दिए जाते हैं। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के पाठ्यक्रमों में स्त्री सशक्तिकरण के विषय शामिल किए जाते हैं। वे सब दिखावटी काम केवल ऐसी स्त्रियों के हैं, जो शहरी, संभ्रांत और अन्य मध्यवर्गीय जीवन जीती हैं और उनमें ऐसे पुरुष भी शरीक होते हैं, जो एनजीओ और तथाकथित प्रतिष्ठा-प्राप्त संस्थाओं के पदों पर रह कर दफ्तर में स्त्री का कभी अपमान करते हंै, तो कभी स्त्री के कथित यौन शोषण के आरोप से देश भर के मीडिया और सोशल मीडिया में रोचक समाचार बन जाते हैं। उनका बिगड़ता कुछ नहीं, स्त्री को ही बिगड़ने और बिगाड़ने का दोषी मान लिया जाता है।
अब प्रश्न यह है कि स्त्री-पुरुष बराबरी या उनके सशक्तिकरण की यह नगाड़ेबाजी क्यों? इस देश की साठ-सत्तर प्रतिशत स्त्रियां ग्रामीण, आदिवासी, दलित और परिवारों की गृहिणियां हैं। क्या इन महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ? क्या इनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक समानता मिली? क्या सशक्तिकरण के शक्ति-मंचों से स्त्रियों के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया कि स्त्री पारिवारिक हिंसा से मुक्त हो, देहशोषण के अपराध से मुक्त हो, आर्थिक निर्धनता के कारण देह-व्यापार से मुक्त हो और पुलिस-स्टेशनों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थलों की देह-हिंसा से मुक्त हो। अंगुलियों पर गिने जाने वाले अपवाद कई हैं, पर पद और प्रतिष्ठा-प्राप्त प्रभावशाली स्त्रियां भी कम हैं। मगर ये स्वयं स्त्रियां भी स्त्री-शोषण, उत्पीड़न और अपमान का जब प्रयोग करती हैं, तो पीड़ित स्त्री की जबान ही बंद हो जाती है। अपने जीवन और अस्तित्व की रक्षा में गरीब स्त्रियों को कितनी-कितनी मजबूरियों के आगे समर्पण करना पड़ता है, यह सब सरकारें भी जानती हैं, संगठन और समाज भी जानते हैं। केवल व्याख्यानों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों से स्त्री सशक्त नहीं होती। उसे उसकी प्रारंभिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक, नौकरियों तक ऐसे कार्य से जोड़ना होगा, जो उसका आर्थिक आधार भी बने, उसकी स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की आजादी भी बने।
सशक्तिकरण एक प्रतिष्ठासूचक शब्द तो है, लेकिन वह इतना घसीटा गया कि उसका तेज और प्रभाव ही समाप्त हो गया। बराबरी या समानता अच्छा विचार है, लेकिन वह केवल व्याख्या-वीर बन कर रह गया। स्त्री स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, निर्णायकता, न्याय और अन्याय के विरुद्ध आक्रोश शब्द भी तो अच्छे हैं, लेकिन वे अगर स्त्री शब्द को नकली सशक्त बनाने के बजाय स्त्री के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके कार्य को सशक्त बना देते, तो स्त्री पुरुष-पराधीन होने के बजाय स्वाधीन होती। भारत पूजाओं, साधनाओं, मंत्र-तंत्रों, प्रवचनों का एक मंच-मार्गी तेजस्वी देश है, जहां पाखंड का सार्वजनिक प्रदर्शन अधिक है, वास्तविक आस्था की स्थापना का कम। ऐसे में साधु-संत, साध्वी और स्वयं स्त्री एवं स्त्री-संगठन तथाकथित आश्रमों के अंधेरे ध्यान-गृहों से निकल कर लोक-जीवन के अंधेरों को उजालों में बदलने की ताकत लगा दें, तो स्त्री-सेवा प्रभावशाली होगी और भारतीय नारी के नए स्वाभिमान की स्थापना होगी। स्त्री को लेकर साहित्य और कलाओं का संसार पूरी तरह आच्छन्न है, लेकिन साहित्य और कलाओं के पीछे का प्रच्छन्न सत्य क्या किसी रचनाकार ने उद्घाटित किया? साहित्य, कलाएं, खेल प्रतियोगिताएं लड़कियों और स्त्रियों को एक भावुक मैदान देती हैं, जहां वे अपनी हसरत को ही अपनी कसरत मान लेती हैं। कठोर से कठोर यथार्थवाद भी स्त्री का यथार्थ न तो लिख पाता है, न स्वयं स्त्रियों से उनका सत्य लिखवा पाता है।
स्त्री की शक्ति स्त्री के अपने होने में है। वह मां है तो उसके पास मां की ताकत है, वह बहन है तो बहन की ताकत है, जहां भी जो भी है वहां उसकी वही ताकत है। कमी है तो यह कि स्त्री इन ताकतों का सही समय और अवसर पर प्रयोग नहीं कर पाती या पुरुष वर्चस्व के समक्ष झुक जाती है। स्त्री उस पर पहनाए गए फैशनदार शब्दों के वस्त्र उतार फेंके और अपने मूल रूप में अपने अस्तित्व की पहचान के साथ खड़ी हो, पुरुष से अपने आर्थिक आधार का आधा हक छीन ले और शिक्षा में जितना शील और शालीनता का पाठ पढ़ती है उससे समाज में प्रचलित अश्लीलता और हिंसा को पराजित कर दे, घर से बाहर तक वह इस्पात की स्नायुओं के साथ खड़ी हो और पुरुष से डरने के बजाय अपने नैतिक बल से पुरुष को डरा सके, तभी स्त्री सशक्त भी होगी, स्वतंत्र भी और उसके स्त्रीत्व का स्वाभिमान भी जाग्रत होगा। स्त्री अपने स्त्री रूप में पुरुष से अधिक सशक्त है, नैतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वह सशक्तीकरण के नाम की दया पर जीने के बजाय स्वयं शक्ति बन कर खड़ी होगी, तो कभी अशक्त नहीं रहेगी।