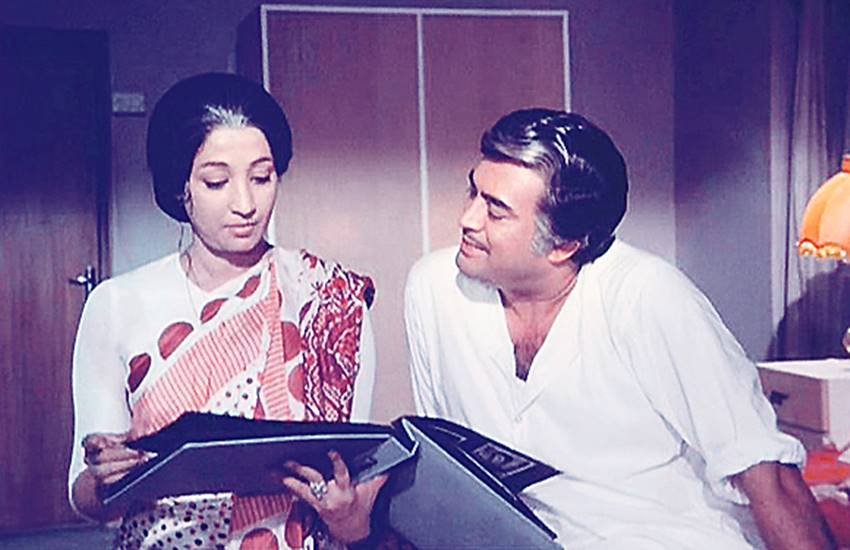हालांकि, साहित्य के चिंतक, लेखक और आलोचक सिनेमा को साहित्य का हिस्सा मानने से हमेशा हिचकते रहे हैं, यह जानते हुए भी कि सिनेमा का आरंभ ही साहित्य से होता है। साहित्य और सिनेमा कहीं न कहीं हमेशा ही एक दूसरे के विस्तार में सहयोग करते रहें हैं। कहना सर्वथा उचित ही होगा कि साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में बनने वाली पहली फीचर फिल्म भी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ‘हरिश्चंद्र’ से प्रेरित थी। प्रारंभ से ही हिंदी सिनेमा में लिखित और अलिखित साहित्य की भूमिका अहम रही है। आज भारत में फिल्म उद्योग ने सौ साल का सफर तय कर लिया है। भारत जैसे बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक परंपरा वाले देश में इसकी व्यापक पहुंच ने इसे लोगों के मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना दिया है और इसमें हिंदी का व्यापक योगदान है। 1931 में पहली बोलती फिल्म ‘आलम आरा’ से आज तक सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई गर्इं। इस तरह हिंदी भारत ही नहीं भारत के मुख्य सिनेमा की भी भाषा है। विश्व में हिंदी सिनेमा ही भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है।
अक्सर जब हम हिंदी सिनेमा में साहित्य के योगदान की बात करते हैं तो इसे लिखित साहित्य से जोड़ देते है। जबकि साहित्य चाहे लिखित हो या अलिखित वह हमेशा से समाज को प्रभावित करता रहा है। प्रारंभ में बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर पारसी थिएटर की विरासत भर था, जिसमें अतिनाटकीयता और गीत-संगीत का ज्यादा समावेश था। पहली बार हिंदी सिनेमा में स्थापित लेखक के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रवेश हुआ। वर्ष 1933 में हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी के निर्देशन में फिल्म ‘मिल मजदूर’ बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। 1934 में प्रेमचंद की ही कृतियों पर ‘नवजीवन’ और ‘सेवासदन’ बनीं लेकिन दोनों फिल्में फ्लॉप हो गर्इं। जो शुरुआत हुई थी, वह जारी रहे। भगवतीचरण वर्मा, पांडेय बेचन शर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री जैसे साहित्यकारों की रचनाओं पर भी फिल्में बनीं।
हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्यकारों का सुनहरा दौर सातवें दशक में नजर आता है। जिसमें उपन्यासकार कमलेश्वर का अहम योगदान है। उपेंद्रनाथ अश्क और अमृतलाल नागर के बाद कमलेश्वर ही ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने सिनेमा की भाषा और जरूरत को बेहतरीन ढंग से समझा। गुलजार ने कमलेश्वर की कृति पर ‘आंधी’ और ‘मौसम’ बनाई तो दोनों फिल्में मील का पत्थर साबित हुर्इं। सातवें दशक में जहां एक ओर हिंदी कथा-साहित्य में बदलाव आ रहा था वहीं हिंदी भाषी फिल्मकारों की संख्या भी बढ़ रही थी। फिल्मकार बासु चटर्जी बांग्ला भाषी थे लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने मन्नू भंडारी की कहानी ‘यही सच’ पर ‘रजनीगंधा’ बनाई, जो काफी लोकप्रिय साबित हुई। हिंदी फिल्मों की इस नई धारा को समांतर सिनेमा भी कहा गया। इसी दौर में हिंदी साहित्य को सबसे ज्यादा महत्त्व और निष्ठाभरी समझ फिल्मकार मणि कौल ने दी।
मणि कौल ने बाद में मोहन राकेश, विजयदान देथा, मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं पर फिल्में बनार्इं। कुमार शहानी ने निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनाई। इसके अलावा दामुल, परिणति,पतंग, कोख जैसी फिल्में भी साहित्यिक रचनाओं पर बनीं। साहित्य और सिनेमा के रिश्ते को जोड़े रखने में दूरदर्शन की बड़ी भूमिका रही है। इसमें तमस चंद्रकांता, राग दरबारी, कब तक पुकारूं मुझे चांद चाहिए, कक्काजी कहिन जैसे धारावाहिक हिट रहे। हिंदी फिल्मों का वर्तमान परिदृश्य काफी बदल चुका है। सिनेमा में हिंदी साहित्य पर आधारित अधिकांश फिल्मों का सफर बहुत आसान नहीं रहा। अधिकांश फिल्में असफल साबित हुर्इं। यही कारण है कि हिंदी में साहित्यिक कृतियों पर सबसे कम सफल फिल्में बन पाई हैं। इसकी बड़ी वजह कहानी के कथ्य को समझने में विफलता रही। दूसरा बड़ा कारण सिनेमा को उपन्यास की भांति पेश करना था। फिल्म, शब्दों का दृश्य विधा में ‘अनुवाद’ नहीं हो सकती। यह फिल्म की विधा को कमतर करके देखने के साथ ही साहित्य को भी कमतर देखने के समान होगा। फिल्मकार रचना को शब्दों के पार ले जाना चाहता है। जबकि साहित्य जगत फिल्म में भी साहित्य को जस का तस देखना चाहता है। एक हद तक यह लगभग असंभव अपेक्षा ही है। हम सभी जानते है कि भारतीय दर्शक वर्ग हिंदी सिनेमा को उसकी कल्पनाशीलता, रोमांटिसिज्म के कारण ज्यादा पसंद करता है।
सवाल है कि हिंदी सिनेमा की अखिल भारतीय पहुंच बनाने में हिंदी के साहित्यिक स्वरूप के अलावा इसके कौन-से स्वरूप का ज्यादा योगदान है। राष्ट्रभाषा, जनभाषा संपर्क भाषा या राजभाषा? सहज जवाब है जनभाषा। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने के पीछे पहली शर्त है निर्माता-निर्देशक का रचना के मर्म तक पहुंचने के साथ ही साहित्यकार के मानसिक बुनावट को भी समझना। बाजारवाद, तकनीकी विकास, उदारवाद का व्यापक और स्पष्ट प्रभाव हिंदी सिनेमा पर देखा जा सकता है। जो हिंदी कभी भारतीय सिनेमा की प्राण तत्त्व मानी जाती थी उसका स्थान अब खिचड़ी भाषा या हिंग्लिश ने ले लिया है। शुरू से ही भारतीय समाज में साहित्य की प्रखर भूमिका रही है। भाषा का समाज के इतर कोई अस्तित्व नहीं होता। भाषा से किसी व्यक्ति और समाज का रिश्ता, उसके अस्तित्व से गुंथा हुआ है। भाषा उन्नत वही है, जहां समाज उन्नति की राह पर है। हमने रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसी गाथाओं को मौखिक रूप से संरक्षित रखा। आज भी हमारे देश में हजारों सालों की लोकोक्तियां, मुहावरे जिंदा है, क्योंकि हमारा देश श्रुति परंपराओं का है। भारतीय सिनेमा ने भी प्रारंभ में इन्हीं परंपराओं, किस्सों-कहानियों पर फिल्में बनाने की परंपरा कायम रखी। इसलिए साहित्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका प्रारंभ से रही है। ऐसे में भी घबराए बिना हमें आगे देखने की जरूरत है।
हिंदी सिनेमा को शिखर पर ले जाने वाले साहित्य को पुष्पवित-पल्लवित करना जरूरी है। आज हिंदी फिल्में, हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का लोकदूत बनकर विश्वस्तर पर हिंदी की पताका फहरा रही है। ऐसे में जरूरत है इसकी पुनर्व्याख्या करने की। तभी हिंदी सिनेमा कुछ नकरात्मकता के बाद भी अपने मजबूत सकारात्मक पक्षों के बल पर अपनी खोई हुई विरासत को पा सकेगाऔर अपनी जड़ों को सिंचिंत कर पाएगा। इसके लिए कलमकारों को भी अपनी कलम को उस ओर मोड़ने की जरूरत है जहां भारतीय समाज उठता-जागता है। कलमकारों को फिर अपनी कलम उस ग्रामीण समाज की ओर मोड़ना होगा जहां आज भी बहुसंख्यक समाज रहता है। तभी हिंदी भाषा और साहित्य के संबंधों से भारतीय सिनेमा नया आकार ले पाएगा। ०