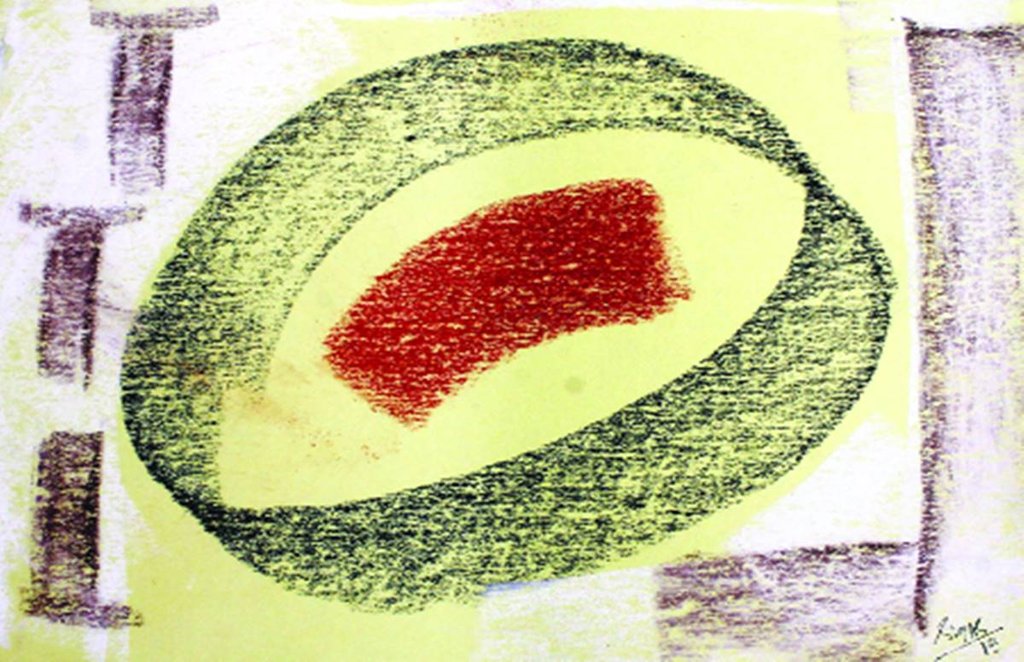आलोचक का जन्म तो तभी होता है जब अभिव्यक्ति मौलिक सर्जना की राह पकड़ आती है। साहित्यिक पुरखे कहते आए हैं कि एक सच्चे सर्जक के अगल-बगल, आगे-पीछे सैकड़ों झूठे और नकलची कवि-लेखक असली फसल के साथ-साथ खर-पतवार सरीखे पैदा हो लेते हैं, क्योंकि रचना की लहलहाती जमीन किसी प्रतिभा द्वारा जोत और बो दी गई है। माना कि नकल की कला में भी रसिकजनों की अभिरुचियों को फुसलाने और सहलाने की या अवकाश को कुछ काल तक भर देने की योग्यता होती है, लेकिन यह जल्दी ही ऊब पैदा करने लगती है। परिणाम यह होता है कि आलोचक की अपनी खेती लहलहाने के बदले सूखने लग जाती है। नकल में से वह असल पैदा करे भी तो कैसे?
यह भी सही है कि सर्जक की तरह आलोचक की भी अपनी प्रतिभा होती है। ऐसा न हो तो फिर शास्त्रज्ञ और आलोचक या फिर पंडित और आलोचक में कोई फर्क ही न रह जाए। पंडित या शास्त्रज्ञ चीजों को जानते हैं। वे जिसे परंपरा कहते हैं उसकी भी यत्किंचित जानकारी रखते हैं, किंतु परंपरा कैसे बनती और विकसित होती या बढ़ती है, इसका बोध जब तक नहीं होता वे पंडित ही बने रहते हैं। शास्त्र तो वह स्कूली पाठ है, जो हमें सज्ञान करता है, पर उसी को लेकर अगर हम आलोचना के जीवन में सीधे-सीधे चले जाएं तो रोजमर्रा के ताजा सवालों के जवाब ढूंढ़ने में कामयाब न होंगे। वह तो पुरखों का अर्जित ज्ञान है, जिसे उन्होंने अपने जीवन-अनुभव से अर्जित कर किताबों में रख छोड़ा है। पर जिसे रचना या सर्जना कहते हैं, वह इसी ज्ञान का न तो दुहराव है, न गवाही। वह तो हमारे अपने जीवन-संघर्षों की आवाज है। मनुष्य का उसके आसपास से बनाया गया एक और नया संबंध। इसलिए इस अदृश्य प्रक्रिया के सौंदर्य की तलाश और माध्यमों की भूमिका की पहचान ही आलोचना है। यह भले ही आम रसिकजनों के लिए गैरजरूरी हो, पर कवि या लेखक के लिए तो आह्लादकारी है।
इसलिए जो आलोचना को अनावश्यक उपस्थिति मानते हों, मानें, उनकी वे जानें। पर जिसने सचमुच कुछ ऐसा किया है, जो नायाब है, उसे तो यह उत्सुकता बनी ही रहती है कि समझदारों ने उसके इस अनोखे काम पर निगाह डाली या नहीं। उर्दू शायरी में जिस ‘दीदावर’ या संस्कृत साहित्य में जिस ‘समानधर्मा’ की बात की गई है, वह यही है। अंग्रेजी साहित्य में भी इस पर चर्चा की गई है। इलियट जैसे कवि-चिंतकों ने तो यहां तक कह दिया है कि आलोचक वही हो सकता है, जो सचमुच कवि हृदय हो। यानी कि समानधर्मा, बस सावधानी यह जरूर बरतनी पड़ेगी कि वह कवि या सर्जक के भाव-प्रवाह में बन न जाय या उसके विचारों या विचारधारा के साथ इतनी मैत्री निभाने न लगे कि न्यायालयों में दी जातीं अधिकांश झूठी गवाहियों जैसे कुकर्म पर उतर आए। या फिर पक्षकार वकीलों जैसा व्यवहार करने लगे। इस संदर्भ में उसकी तटस्थता और (निर्मम) काव्य-विवेक बेहद अनिवार्य है, क्योंकि उसकी अदालत तो सहृदयों की लोक-अदालत ही है। चूक करने पर न तो आचार्य आलोचक माफी का हकदार बनता है, न कोई परवर्ती आचार्य।
ईमानदार और सच्चा लेखक (यानी खांटी प्रतिभाधर) अपना काम पूरे होशो-हवास में करता है, न कि लेखक बनने मात्र या फिर दिखने मात्र के लिए। संस्कृति और परंपरा के जीवन में प्राय: जो रुकावटें पैदा हो जाती हैं और काव्य-रूढ़ियां पैदा हो उठती हैं, वे किसी भी रचनात्मकता के लिए खतरनाक बन जाती हैं। नए जीवन-अनुभवों और अभिनव अभिव्यक्तियों के लिए वे एक ऐसी संहारक रुकावट पैदा करती हैं कि आत्मविश्वास से क्षीण कई नई प्रतिभाएं भी चालू रीति-मार्ग की शरण में चली आती हैं। फलत: काव्य और कला के क्षेत्र में कोई नवाचार संभव हो पाना असंभव-सा हो जाता है। क्षेत्र चाहे काव्य (कविता) का हो या फिर गद्य-विधाओं का। आज कोई यह विचार करने को आगे नहीं आता कि ब्रजभाषा-काव्य के समक्ष खड़े होने का साहस जुटाती खड़ी बोली और उसका काव्य, या फिर देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों की आंधी के बीच प्रेमचंद या फिर द्विवेदी-युगीन कवियों के प्रवाह के बीच छायावादी कवियों का रचनात्मक साहस कितना और क्या था? इसके एक-दो उदाहरण देना यहां जरूरी है।
जरा निराला के ‘सरोज-स्मृति’ की इन पंक्तियों को याद करें- ‘तभी भी मैं इसी तरह समस्त/ कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त/ लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादकगण निरानंद/ वापस कर देते पढ़ कर सत्वर/ दे एक-पंक्ति-दो में उत्तर/ लौटी रचना लेकर उदास/ ताकता हुआ मैं दिशा काश/ बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर/ व्यतीत करता था गुनगुन कर/ संपादक के गुण; यथाभ्यास/ पास की नोचता हुआ घास।’
यही रचनात्मक साहस निराला से पहले उनके वरिष्ठ- निराला के संबोधनों में ‘श्रीमान बाबू साहब’- जयशंकर प्रसाद दिखा रहे थे, न केवल अपनी कविताओं में, बल्कि ‘कामायनी’ काव्य और नाटकों में। प्रेमचंद की कहानियों के साथ एक नए कहानी-स्कूल का प्रवर्तन करते चल रहे थे। पर यह काम सिर्फ वे प्रतिभाएं कर पाती हैं, जिन्हें परंपरा में सारस्वत कहा गया है। जो नकल या रीति या लोक-जीवी नहीं होतीं। भवभूति घनांनद, या कवि मुक्तिबोध इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं। इनके बीच लोकनायक कवि तुलसी की इन पंक्तियों की याद शायद अपराध न हो-
कवि न होऊं नहि बचन प्रबीनू/ सकल कला सब विद्याहीनू॥
आखर अरथ अलंकृत नाना/ छंद प्रबंध अनेक विधाना॥
भाव-भेद रस भेद अपारा/ कबित दोष गुन बिबिध पुकारा॥
कबित विवेक एक नहिं मोरें/ सत्य कहऊं लिखि कागद कोरे॥
प्रतिभावान कवि काव्य रचता है, शेष काव्याभ्यास का भारी कूड़ा-कबाड़ा इकट्ठा कर सहृदयों तक का काव्य-विवेक हर लेने का वातावरण रचते हैं। इस संदर्भ में अलंकारवादी ख्यात आचार्य भामह की याद बरबस हो आती है- एक सच्चे कवि के बीच अनेक कुकवि जन्म ले लेते हैं, जबकि कुकवित्व साक्षात मृत्यु और कवित्व एक तपस्या है। कोई चाहे तो इसे कवि-दिग्गजों से समझ सकता है।
आलोचक का जन्म इसी सच्चे कवित्व के गर्भ से होता है। प्रश्न यह कि यह सच्ची सर्जना पहचानी कैसे जाए? जवाब होगा, उस जीवनानुभव से जो केवल कवि का नहीं, समूचे लोक का है। इस जीवनानुभव को मौलिक ढंग से अभिव्यक्त करने की कला से भी। प्रसाद की ‘कामायनी’ में परंपरागत महाकाव्यों जैसा काव्य-विधान नहीं है। प्रश्न तो बीसवीं सदी के ही हैं, सो भी विज्ञान, धर्म, सत्ता और समाज के साथ सभ्यता के आचरण और गंतव्य के। दूसरे शब्दों में सकल मानवता के। बीसवीं सदी में कोई दूसरा तो यह नहीं ही कर सका। इसलिए कविता कोरा कलाभ्यास नहीं है। जमाने की पीड़ाओं का दस्तावेज तो है ही, उसके सपनों का इतिहास भी है। भारत की कविता की आदि पहचान यही वेदनानुभूति और करुणानुभूति है। वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, प्रेमचंद यही हैं। यह चाहे राष्ट्रीयता और आजादी के दरवाजे से आए, चाहे प्रेम और करुणा के।
आलोचक की पहचान यहीं से शुरू होती है कि कवि या लेखक की यह संवेदनशीलता किस और किस भाव-दृष्टि की उपज है। कला के लिए कला या फिर कविता के लिए कविता लिखना तो वह नहीं है! कहीं वह कविता के नाम पर कविता की प्रॉक्सी तो नहीं है! किसी नई और मौलिक सूझ की लकीर पीटना तो नहीं है! आलोचक की जरूरत यहीं बन पड़ती है कि वह सारे काव्याभ्यास से सच्चे कवित्व की आकर रक्षा करे। किंतु क्यों? उत्तर होगा, कला और संस्कृति की रक्षा के लिए। संवेदना और कवि-संस्था के संरक्षण और पहचान के लिए।
आलोचक किसी की आर्त-पुकार पर नहीं, अपने सहृदय के धर्म-निर्वाह के लिए आता है। कवि की ही तरह उसका यह सहृदय भी नैसर्गिक ही होता है। आलोचनाओं की किताब पढ़ कर नहीं। अन्यथा कोई कारण नहीं कि पांडित्य-प्रेरित, संवेदना-शून्य आलोचनाएं उपहासास्पद या फिर उपेक्षणीय मानी जातीं। स्कूली या अध्यापकीय आलोचनाओं की बात करना तो यों भी बेकार। वे तो शादी में काम आने वाले बरतनों की तरह हैं।
विजय बहादुर सिंह