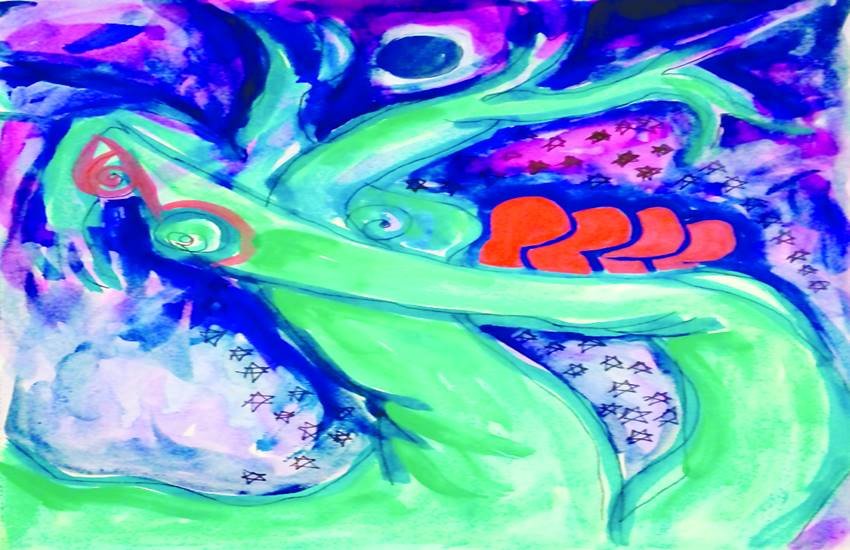उमेश प्रसाद सिंह
हमारा समय बहुत-सी चीजों से वंचित हो जाने का समय होता जा रहा है। हम रोज-रोज वंचित हो रहे हैं, मगर किंचित भी हमें आभास नहीं हो पा रहा है। शायद इस विकट समय में आदमी जो जिंदा बचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसे अपने ठगे जाने का एहसास नहीं है। इस एहसास का न होना, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन कर उसे बचाए हुए है। एक अविश्वसनीय अंतर्विरोध जीवन के कण-कण में, क्षण-क्षण में व्याप्त है, मगर हमारे अनुभव में नहीं है। जो नहीं है, उसके नहीं होने के सुख-दुख दोनों अपने हैं। शायद हम संचय की दुराशा से इतने आक्रांत हो चुके हैं कि हमें हर वंचना भी किसी संचय से भिन्न नहीं महसूस हो रही है। हम भर ही तो रहे हैं, भले अभाव से ही भर रहें हैं। खैर।
मुझे प्राय: बड़ा दुख होता है। होता रहता है। बहुत-सी चीजों के गायब हो जाने का मन में गहरा दुख है। मगर मुझे सबसे गहरा दुख अपने समय में खलनायक के गायब हो जाने का दुख है। हमारे समय के सारे के सारे नाटक ही बिना खलनायक के नाटक होकर रह गए हैं। मुझे लगता है, नाटक के प्रति रुझान में कमी के कारणों में सबसे बड़ा कारण यही है। वैसे और भी बहुत-से कारण हैं। बहुत-से कारण और भी हो सकते हैं, जिनका किसी को पता नहीं है।
हमारे समय का आदमी नाटक क्या देखे? क्यों देखे? हमारी तो जिंदगी ही नाटक होकर रह गई है। हमारे समय का हर आदमी नाटक कर रहा है। गांव-गांव में नाटक चल रहा है। घर-घर में नाटक हो रहा है। हर आदमी बिना किसी प्रशिक्षण के नाटक में पात्र है। हमारे समय में अभिनय सीखने की चीज नहीं रह गई है। हर कोई पेट में से ही अभिनय सीख कर पैदा हो रहा है। हर कहीं अभिनय का प्रेम है। अभिनय का क्रोध है। अभिनय की करुणा है। अभिनय की हंसी है। अभिनय के आंसू हैं। जिंदगी में कुछ नहीं है। वह पूरी की पूरी छूंछ है। छूंछी बटुली चूल्हे पर चढ़ी है। दाल एक दाना भी नहीं है। फिर भी हम दाल पका रहे हैं।
हमारे देखते-देखते हमारी आंखों के आगे हमारा बहुत कुछ गायब हो गया है। बहुत कुछ गुम हो गया है। हम कुछ नए के आने के इंतजार में गुम होती जा रही चीजों से बेखबर पड़े हैं।
हमारी आंखों के आगे हमारे चौपालों के ठहाके गुम हो गए। हमारे चउतरों से कौड़े की आंच गायब हो गई। हमारे घरों से हमारा पड़ोस न जाने कहां गुम हो गया। हमारे दिलों से हमारी पारस्परिकता न जाने कहां गायब हो गई। हमारे सावन से हमारे झूले, हमारी होली से हमारे रंग, हमारे त्योहारों से हमारी हुलास, हमारे कंठों से हमारे गान कहां चले गए, हमें कुछ पता नहीं। हम न जाने किसके इंतजार में हैं, जो कब से आने को कहते-कहते अभी तक नहीं आया। कभी नहीं आएगा। हम कभी न आने वाले के इंतजार में मुंह बाए खड़े हैं। हमारा जो था, जो हमारे पास था, जो हमारे हाथ में था, सब गायब हो गया। सब गुम हो गया।
अब? अब क्या! अब हमारे हाथ में खालीपन का झुनझुना है। बजाओ। खूब बजाओ। हम बजा भी रहे हैं। अब हम अपनी लाचारी को गा रहे हैं, बजा रहे हैं।
इन सबके गायब हो जाने का, गुम हो जाने का मुझे कम दुख नहीं है। मगर मुझे सबसे ज्यादा दुख अपने समय में खलनायकों के गुम हो जाने का है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैं दर्ज कराने को तत्पर हूं। मगर कहां? मालूम नहीं।
हमारे समूचे समय में कहीं भी, कोई भी खलनायक नहीं है। न आसपास, न दूर-दूर। न गांव में, न घर में, न देश में। न स्थानीय स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर पर। यहां तक कि हमें अपने में भी कहीं कोई खलनायक दिखाई नहीं देता। बड़ा अजीब है। नाटक हैं, लंबे-लंबे। दृश्य हैं, दृश्य पर दृश्य फैले हुए। संवाद हैं अटूट। सहलाते हुए। बहलाते हुए। सब कुछ है, मगर खलनायक कहीं नहीं है। ऐसा भला कैसे हो सकता है। क्या हमारे समय में सब कुछ ठीक है। शुभ है। शोभन है। सारे संकल्प, सारे अभियान कल्याणकारी हैं। लगता तो नहीं है। नहीं ऐसा कतई नहीं है। मगर खलनायक की अनुपस्थिति तो ऐसा ही कहती है। झूठ है… झूठ है, झूठ है मेरा मन चिल्ला-चिल्ला कर कहता है, यह झूठ है।
अंधेरा तो एक सूरज के उगने से ही छंट जाता है। हट जाता है। मिट जाता है। हमारे समय का नायक गला फाड़-फाड़ कर घोषणा कर रहा है, वह सूरज है। वही सूरज है। उसे उगने दो। आने दो। वह आता है। आ जाता है। आकाश में छा जाता है। मगर रोशनी नहीं आती। उजाला नहीं आता। ऊष्मा नहीं आती। ताप नहीं आता। ठिठुरन बनी रहती है। आंखें कंगाल की कंगाल बनी रहती हैं। अंधेरा तनिक भी पीछे नहीं सरकता। भूख, अकुलाहट, आशंका, असुरक्षा, असहायता, अकेलापन कुछ भी कम नहीं होता। सूरज होने का दावा एक का नहीं, सौ-सौ का है। न जाने कैसा सूरज? हमारे समय में सूरज ही सूरज हैं, मगर कहीं भी दिन नहीं है। उजाला नहीं है। आश्वस्ति नहीं है। स्फूर्ति नहीं है। उमंग नहीं है। उत्साह नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारे समय के सारे सूरज नकली हैं क्या? होंगे, तभी तो! कागज के सूरज होने न होने से क्या होता है। कुछ नहीं।
जब खलनायक होते थे, तो नायक के होने का मतलब होता था। खलनायक के आतंक के समक्ष नायक के होने की आश्वस्ति होती थी। नायक की निष्ठा का आलंब होता था। अवलंब होता था।
सुना जाता है, पहले के समय में दस्यु बीहड़ों में रहा करते थे। अब जंगल रहे नहीं। दुर्गम कहीं बचा नहीं। लोकतंत्र की आजादी में सारे दस्यु नागरिक होकर प्रतिष्ठित हैं। अब दस्यु जंगलों में नहीं, बस्तियों में हैं। गांव-गांव में हैं, नगर-नगर में हैं। अब वे दस्यु नहीं हैं। अंधेरे के वारिस नहीं हैं। अब वे सूरज होने के दावेदार हैं। उनसे प्रकाश का विस्फोट होता है।
कभी रावण लंका में रहता था। रावण की लंका सोने की थी। अलग थी दुनिया से। समुद्र से घिरी थी। आवागमन के संसाधन से विलग थी। अब तो रावण भी अयोध्या में ही रहने लगा है।
फिर…? फिर क्या? लंका में अयोध्या बनी न बनी। अयोध्या में लंका जरूर बन गई।
मैं परेशान हूं। हैरान हूं। हलकान हूं। हमारे समय में खलनायक कहां गायब हो गए? कहां गुम हो गए?
नहीं, नहीं, वे धरती से गायब नहीं हो गए हैं। उनके होने के पक्के सबूत हमारी आंखों के आगे साबुत हैं। इसमें सीबीआई इन्क्वाइरी की जरूरत भी नहीं है। वे हैं, हर कहीं हैं। हमारे अगल-बगल हैं। आसपास है। आमने-सामने हैं। मगर खलनायक की भूमिका में नहीं हैं।
हमारे समय के खलनायक नायक में छिप गए हैं। नायक में खलनायक का घुस जाना कितने अचंभे की बात है। कितने आश्चर्य की बात है। कितनी अविश्वसनीय बात है। इस अविश्वसनीय पर विश्वास कौन करेगा? कोई नहीं। व्यर्थ है। फालतू है। बकवास है।
हमारे समय में जो सच है, बकवास है। व्यर्थ है। फालतू है। सार्थक है केवल नाटक। बिना खलनायक का नाटक। जो हो रहा है, गली-गली। गांव-गांव। नगर-नगर। बिना खलनायक के नाटक में हम सब शामिल हैं। हम सब पात्र हैं। बेहद रोमांचक है नाटक, जिसमें सारे दर्शक नाटक के पात्र है। सारे पात्र जिंदाबाद हैं।